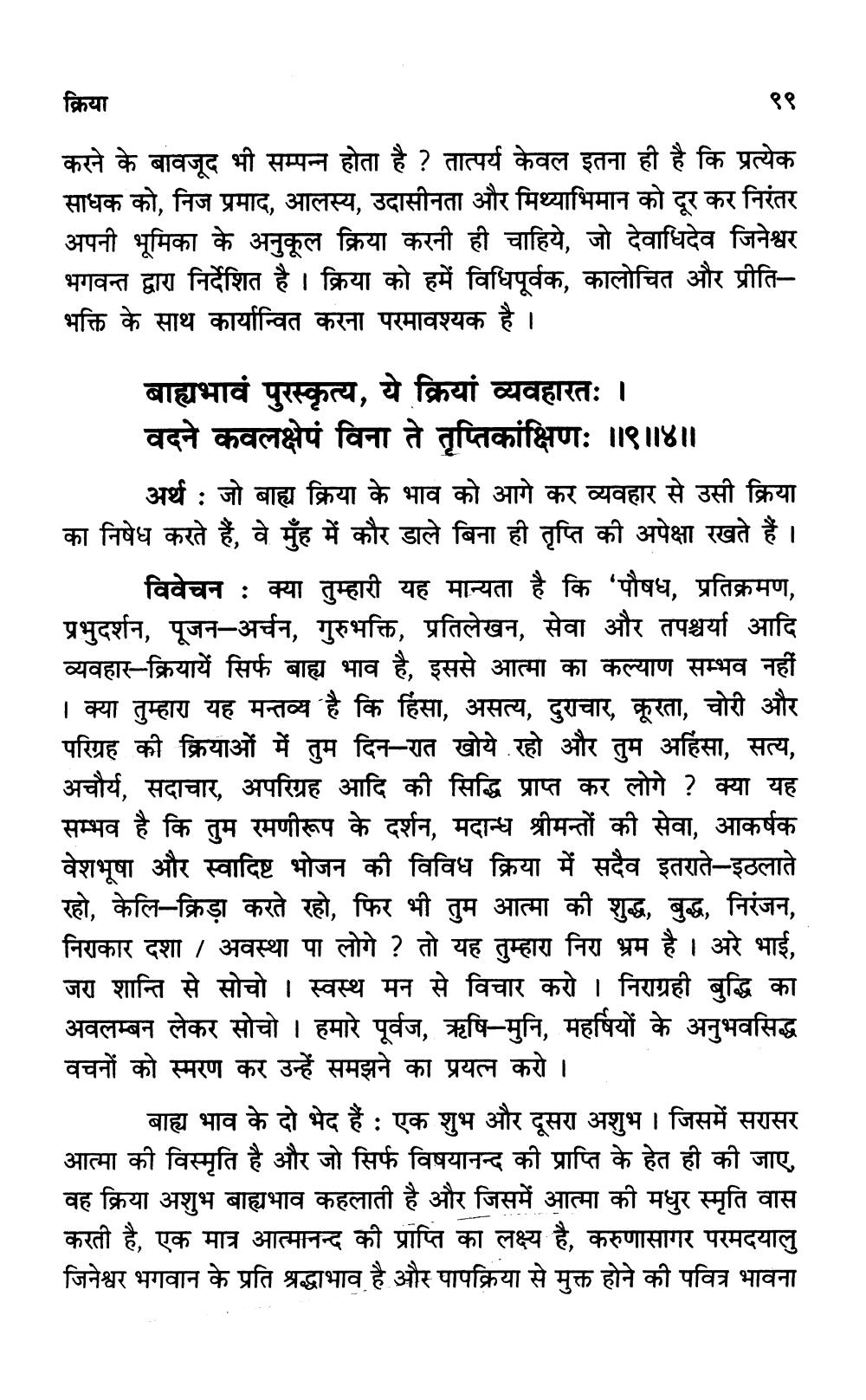________________
क्रिया
९९
करने के बावजूद भी सम्पन्न होता है ? तात्पर्य केवल इतना ही है कि प्रत्येक साधक को, निज प्रमाद, आलस्य, उदासीनता और मिथ्याभिमान को दूर कर निरंतर अपनी भूमिका के अनुकूल क्रिया करनी ही चाहिये, जो देवाधिदेव जिनेश्वर भगवन्त द्वारा निर्देशित है । क्रिया को हमें विधिपूर्वक, कालोचित और प्रीतिभक्ति के साथ कार्यान्वित करना परमावश्यक है ।
I
बाह्यभावं पुरस्कृत्य, ये क्रियां व्यवहारतः । वदने कवलक्षेपं विना ते तृप्तिकांक्षिणः ॥ ९ ॥४॥
अर्थ : जो बाह्य क्रिया के भाव को आगे कर व्यवहार से उसी क्रिया का निषेध करते हैं, वे मुँह में कौर डाले बिना ही तृप्ति की अपेक्षा रखते हैं ।
विवेचन : क्या तुम्हारी यह मान्यता है कि 'पौषध, प्रतिक्रमण, प्रभुदर्शन, पूजन-अर्चन, गुरुभक्ति, प्रतिलेखन, सेवा और तपश्चर्या आदि व्यवहार- क्रियायें सिर्फ बाह्य भाव है, इससे आत्मा का कल्याण सम्भव नहीं । क्या तुम्हारा यह मन्तव्य है कि हिंसा, असत्य, दुराचार, क्रूरता, चोरी और परिग्रह की क्रियाओं में तुम दिन-रात खोये रहो और तुम अहिंसा, सत्य, अचौर्य, सदाचार, अपरिग्रह आदि की सिद्धि प्राप्त कर लोगे ? क्या यह सम्भव है कि तुम रमणीरूप के दर्शन, मदान्ध श्रीमन्तों की सेवा, आकर्षक वेशभूषा और स्वादिष्ट भोजन की विविध क्रिया में सदैव इतराते - इठलाते रहो, केलि-क्रिड़ा करते रहो, फिर भी तुम आत्मा की शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निराकार दशा / अवस्था पा लोगे ? तो यह तुम्हारा निरा भ्रम है । अरे भाई, जरा शान्ति से सोचो । स्वस्थ मन से विचार करो । निराग्रही बुद्धि का अवलम्बन लेकर सोचो | हमारे पूर्वज, ऋषि-मुनि, महर्षियों के अनुभवसिद्ध वचनों को स्मरण कर उन्हें समझने का प्रयत्न करो ।
1
बाह्य भाव के दो भेद हैं : एक शुभ और दूसरा अशुभ। जिसमें सरासर आत्मा की विस्मृति है और जो सिर्फ विषयानन्द की प्राप्ति के हेत ही की जाए, वह क्रिया अशुभ बाह्यभाव कहलाती है और जिसमें आत्मा की मधुर स्मृति वास करती है, एक मात्र आत्मानन्द की प्राप्ति का लक्ष्य है, करुणासागर परमदयालु जिनेश्वर भगवान के प्रति श्रद्धाभाव है और पापक्रिया से मुक्त होने की पवित्र भावना