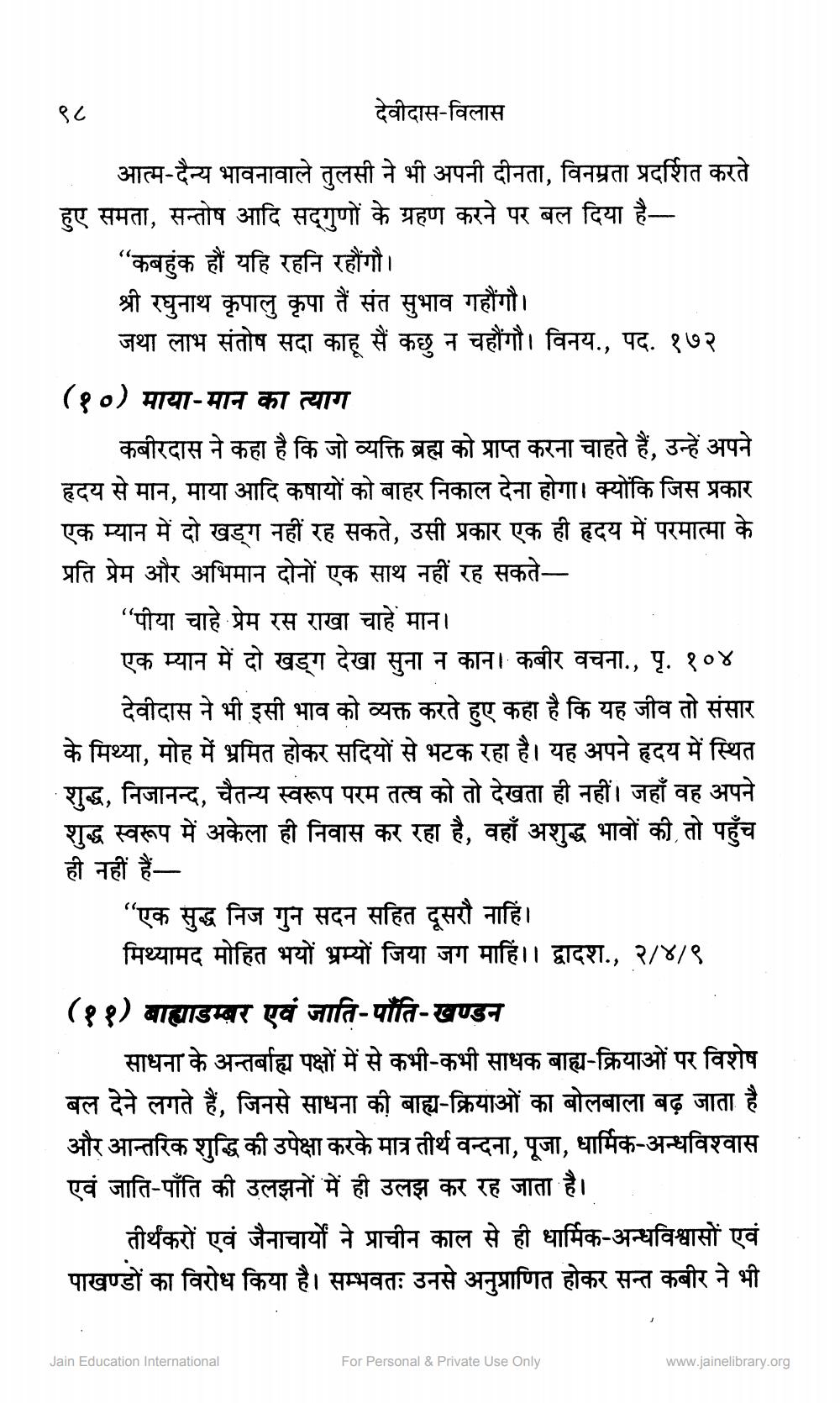________________
देवीदास-विलास
आत्म-दैन्य भावनावाले तुलसी ने भी अपनी दीनता, विनम्रता प्रदर्शित करते हुए समता, सन्तोष आदि सद्गुणों के ग्रहण करने पर बल दिया है
“कबहुंक हौं यहि रहनि रहौंगौ। श्री रघुनाथ कृपालु कृपा तैं संत सुभाव गहौंगौ।
जथा लाभ संतोष सदा काहू मैं कछु न चहौंगौ। विनय., पद. १७२ (१०) माया-मान का त्याग
कबीरदास ने कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने हृदय से मान, माया आदि कषायों को बाहर निकाल देना होगा। क्योंकि जिस प्रकार एक म्यान में दो खड्ग नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक ही हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम और अभिमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते
"पीया चाहे प्रेम रस राखा चाहें मान। एक म्यान में दो खड्ग देखा सुना न कान। कबीर वचना., पृ. १०४
देवीदास ने भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि यह जीव तो संसार के मिथ्या, मोह में भ्रमित होकर सदियों से भटक रहा है। यह अपने हृदय में स्थित शुद्ध, निजानन्द, चैतन्य स्वरूप परम तत्व को तो देखता ही नहीं। जहाँ वह अपने शुद्ध स्वरूप में अकेला ही निवास कर रहा है, वहाँ अशुद्ध भावों की तो पहुँच ही नहीं हैं
“एक सुद्ध निज गुन सदन सहित दूसरौ नाहिं।
मिथ्यामद मोहित भयों भ्रम्यों जिया जग माहिं।। द्वादश., २/४/९ (११) बाह्याडम्बर एवं जाति-पाँति-खण्डन
साधना के अन्तर्बाह्य पक्षों में से कभी-कभी साधक बाह्य-क्रियाओं पर विशेष बल देने लगते हैं, जिनसे साधना की बाह्य-क्रियाओं का बोलबाला बढ़ जाता है
और आन्तरिक शुद्धि की उपेक्षा करके मात्र तीर्थ वन्दना, पूजा, धार्मिक-अन्धविश्वास एवं जाति-पाँति की उलझनों में ही उलझ कर रह जाता है।
तीर्थंकरों एवं जैनाचार्यों ने प्राचीन काल से ही धार्मिक-अन्धविश्वासों एवं पाखण्डों का विरोध किया है। सम्भवतः उनसे अनुप्राणित होकर सन्त कबीर ने भी
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org