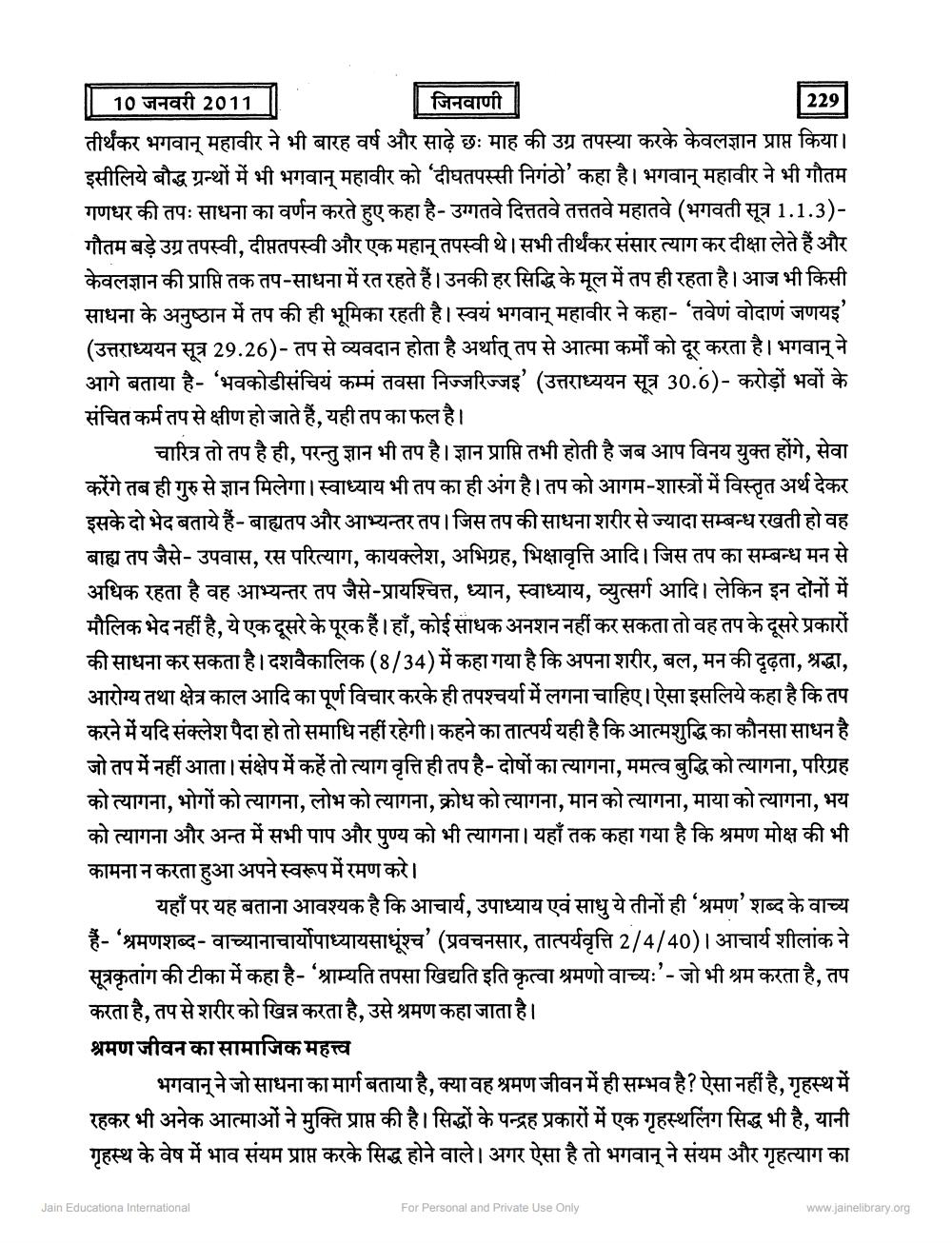________________
| 10 जनवरी 2011 ॥ | जिनवाणी
|229 तीर्थंकर भगवान् महावीर ने भी बारह वर्ष और साढ़े छः माह की उग्र तपस्या करके केवलज्ञान प्राप्त किया। इसीलिये बौद्ध ग्रन्थों में भी भगवान् महावीर को 'दीघतपस्सी निगंठो' कहा है। भगवान् महावीर ने भी गौतम गणधर की तपः साधना का वर्णन करते हुए कहा है- उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे (भगवती सूत्र 1.1.3)गौतम बड़े उग्र तपस्वी, दीप्ततपस्वी और एक महान् तपस्वी थे। सभी तीर्थंकर संसार त्याग कर दीक्षा लेते हैं और केवलज्ञान की प्राप्ति तक तप-साधना में रत रहते हैं। उनकी हर सिद्धि के मूल में तप ही रहता है। आज भी किसी साधना के अनुष्ठान में तप की ही भूमिका रहती है। स्वयं भगवान् महावीर ने कहा- 'तवेणं वोदाणं जणयइ' (उत्तराध्ययन सूत्र 29.26)- तप से व्यवदान होता है अर्थात् तप से आत्मा कर्मों को दूर करता है। भगवान् ने आगे बताया है- 'भवकोडीसंचियं कम्मं तवसा निज्जरिज्जई' (उत्तराध्ययन सूत्र 30.6)- करोड़ों भवों के संचित कर्म तप से क्षीण हो जाते हैं, यही तप का फल है।
___ चारित्र तो तप है ही, परन्तु ज्ञान भी तप है। ज्ञान प्राप्ति तभी होती है जब आप विनय युक्त होंगे, सेवा करेंगे तब ही गुरु से ज्ञान मिलेगा। स्वाध्याय भी तप का ही अंग है। तप को आगम-शास्त्रों में विस्तृत अर्थ देकर इसके दो भेद बताये हैं- बाह्यतप और आभ्यन्तर तप। जिस तप की साधना शरीर से ज्यादा सम्बन्ध रखती हो वह बाह्य तप जैसे- उपवास, रस परित्याग, कायक्लेश, अभिग्रह, भिक्षावृत्ति आदि। जिस तप का सम्बन्ध मन से अधिक रहता है वह आभ्यन्तर तप जैसे-प्रायश्चित्त, ध्यान, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग आदि। लेकिन इन दोनों में मौलिक भेद नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, कोई साधक अनशन नहीं कर सकता तो वह तप के दूसरे प्रकारों की साधना कर सकता है। दशवकालिक (8/34) में कहा गया है कि अपना शरीर, बल, मन की दृढ़ता, श्रद्धा, आरोग्य तथा क्षेत्र काल आदि का पूर्ण विचार करके ही तपश्चर्या में लगना चाहिए। ऐसा इसलिये कहा है कि तप करने में यदि संक्लेश पैदा हो तो समाधि नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य यही है कि आत्मशुद्धि का कौनसा साधन है जो तप में नहीं आता। संक्षेप में कहें तो त्याग वृत्ति ही तप है- दोषों का त्यागना, ममत्व बुद्धि को त्यागना, परिग्रह को त्यागना, भोगों को त्यागना, लोभ को त्यागना, क्रोध को त्यागना, मान को त्यागना, माया को त्यागना, भय को त्यागना और अन्त में सभी पाप और पुण्य को भी त्यागना। यहाँ तक कहा गया है कि श्रमण मोक्ष की भी कामना न करता हुआ अपने स्वरूप में रमण करे।
यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि आचार्य, उपाध्याय एवं साधु ये तीनों ही श्रमण' शब्द के वाच्य हैं- 'श्रमणशब्द- वाच्यानाचार्योपाध्यायसाधूंश्च' (प्रवचनसार, तात्पर्यवृत्ति 2/4/40)। आचार्य शीलांक ने सूत्रकृतांग की टीका में कहा है- 'श्राम्यति तपसा खिद्यति इति कृत्वा श्रमणो वाच्यः' - जो भी श्रम करता है, तप करता है, तप से शरीर को खिन्न करता है, उसे श्रमण कहा जाता है। श्रमण जीवन का सामाजिक महत्त्व
भगवान् ने जो साधना का मार्ग बताया है, क्या वह श्रमण जीवन में ही सम्भव है? ऐसा नहीं है, गृहस्थ में रहकर भी अनेक आत्माओं ने मुक्ति प्राप्त की है। सिद्धों के पन्द्रह प्रकारों में एक गृहस्थलिंग सिद्ध भी है, यानी गृहस्थ के वेष में भाव संयम प्राप्त करके सिद्ध होने वाले। अगर ऐसा है तो भगवान् ने संयम और गृहत्याग का
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org