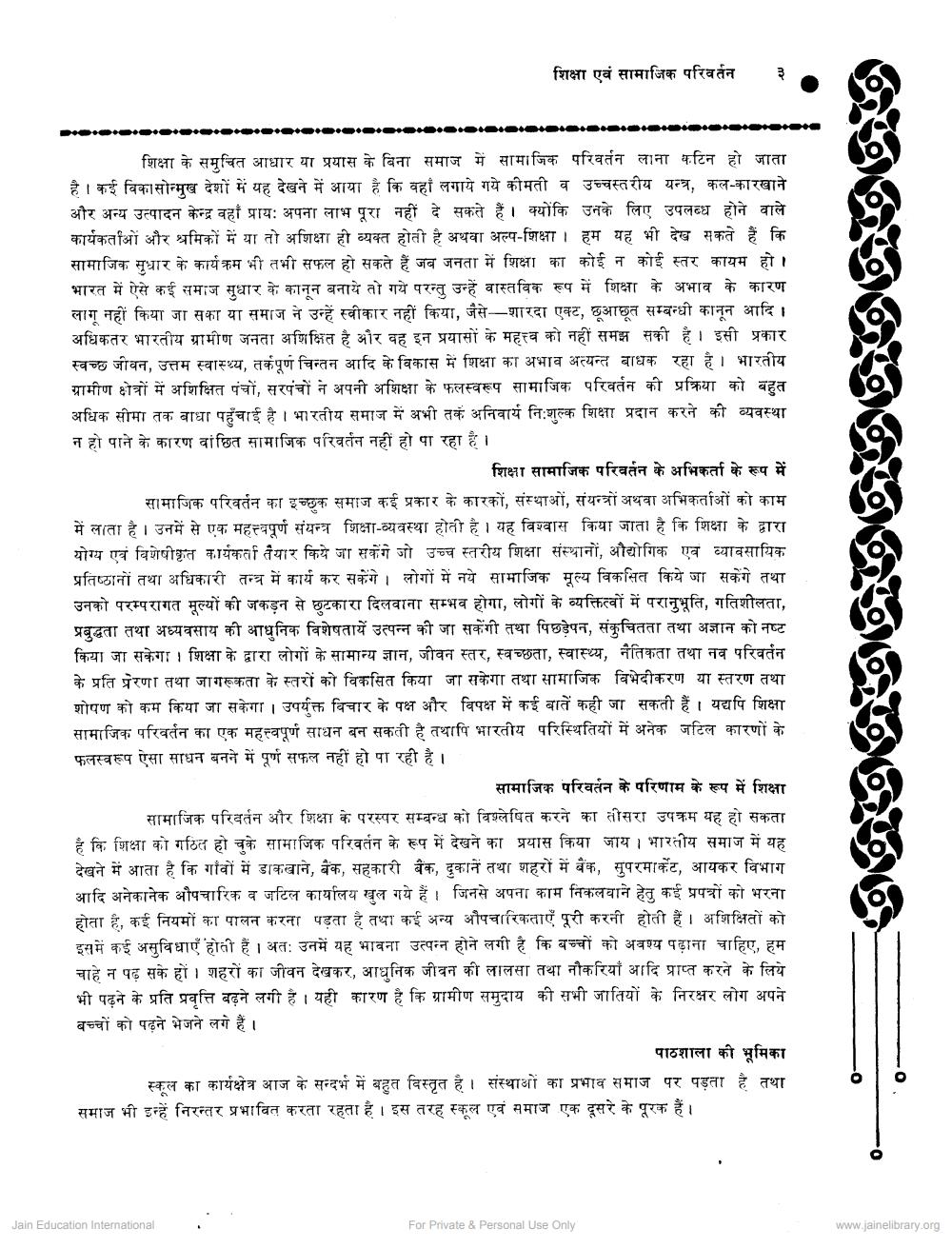Book Title: Shiksha evam Samajik parivartan Author(s): Bhavani Shankar Garg Publisher: Z_Kesarimalji_Surana_Abhinandan_Granth_012044.pdf View full book textPage 3
________________ शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन ३ ......................DIDDDDDDDDDDDDDO. शिक्षा के समुचित आधार या प्रयास के बिना समाज में सामाजिक परिवर्तन लाना कटिन हो जाता है। कई विकासोन्मुख देशों में यह देखने में आया है कि वहाँ लगाये गये कीमती व उच्चस्तरीय यन्त्र, कल-कारखाने और अन्य उत्पादन केन्द्र वहाँ प्राय: अपना लाभ पूरा नहीं दे सकते हैं। क्योंकि उनके लिए उपलब्ध होने वाले कार्यकर्ताओं और श्रमिकों में या तो अशिक्षा ही व्यक्त होती है अथवा अल्प-शिक्षा। हम यह भी देख सकते हैं कि सामाजिक सुधार के कार्यक्रम भी तभी सफल हो सकते हैं जब जनता में शिक्षा का कोई न कोई स्तर कायम हो। भारत में ऐसे कई समाज सुधार के कानून बनाये तो गये परन्तु उन्हें वास्तविक रूप में शिक्षा के अभाव के कारण लागू नहीं किया जा सका या समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, जैसे-शारदा एक्ट, छूआछूत सम्बन्धी कानून आदि । अधिकतर भारतीय ग्रामीण जनता अशिक्षित है और वह इन प्रयासों के महत्त्व को नहीं समझ सकी है। इसी प्रकार स्वच्छ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, तर्कपूर्ण चिन्तन आदि के विकास में शिक्षा का अभाव अत्यन्त बाधक रहा है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित पंचों, सरपंचों ने अपनी अशिक्षा के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को बहुत अधिक सीमा तक बाधा पहुँचाई है । भारतीय समाज में अभी तक अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था न हो पाने के कारण वांछित सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में सामाजिक परिवर्तन का इच्छुक समाज कई प्रकार के कारकों, संस्थाओं, संयन्त्रों अथवा अभिकर्ताओं को काम में लाता है। उनमें से एक महत्त्वपूर्ण संयन्त्र शिक्षा-व्यवस्था होती है। यह विश्वास किया जाता है कि शिक्षा के द्वारा योग्य एवं विशेषीकृत कार्यकर्ता तैयार किये जा सकेंगे जो उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों, औद्योगिक एव व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा अधिकारी तन्त्र में कार्य कर सकेंगे। लोगों में नये सामाजिक मूल्य विकसित किये जा सकेंगे तथा उनको परम्परागत मूल्यों की जकड़न से छुटकारा दिलवाना सम्भव होगा, लोगों के व्यक्तित्वों में परानुभूति, गतिशीलता, प्रबुद्धता तथा अध्यवसाय की आधुनिक विशेषतायें उत्पन्न की जा सकेंगी तथा पिछड़ेपन, संकुचितता तथा अज्ञान को नष्ट किया जा सकेगा। शिक्षा के द्वारा लोगों के सामान्य ज्ञान, जीवन स्तर, स्वच्छता, स्वास्थ्य, नैतिकता तथा नव परिवर्तन के प्रति प्रेरणा तथा जागरूकता के स्तरों को विकसित किया जा सकेगा तथा सामाजिक विभेदीकरण या स्तरण तथा शोषण को कम किया जा सकेगा। उपर्युक्त विचार के पक्ष और विपक्ष में कई बातें कही जा सकती हैं। यद्यपि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण साधन बन सकती है तथापि भारतीय परिस्थितियों में अनेक जटिल कारणों के फलस्वरूप ऐसा साधन बनने में पूर्ण सफल नहीं हो पा रही है। सामाजिक परिवर्तन के परिणाम के रूप में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के परस्पर सम्बन्ध को विश्लेषित करने का तीसरा उपक्रम यह हो सकता है कि शिक्षा को गठित हो चुके सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखने का प्रयास किया जाय । भारतीय समाज में यह देखने में आता है कि गाँवों में डाकखाने, बैंक, सहकारी बैक, दुकानें तथा शहरों में बैंक, सुपरमार्केट, आयकर विभाग आदि अनेकानेक औपचारिक व जटिल कार्यालय खुल गये हैं। जिनसे अपना काम निकलवाने हेतु कई प्रपत्रों को भरना होता है, कई नियमों का पालन करना पड़ता है तथा कई अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। अशिक्षितों को इसमें कई असुविधाएँ होती हैं । अत: उनमें यह भावना उत्पन्न होने लगी है कि बच्चों को अवश्य पढ़ाना चाहिए, हम चाहे न पढ़ सके हों। शहरों का जीवन देखकर, आधुनिक जीवन की लालसा तथा नौकरियाँ आदि प्राप्त करने के लिये भी पढ़ने के प्रति प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। यही कारण है कि ग्रामीण समुदाय की सभी जातियों के निरक्षर लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजने लगे हैं। पाठशाला की भूमिका स्कूल का कार्यक्षेत्र आज के सन्दर्भ में बहुत विस्तृत है। संस्थाओं का प्रभाव समाज पर पड़ता है तथा समाज भी इन्हें निरन्तर प्रभावित करता रहता है। इस तरह स्कूल एवं समाज एक दूसरे के पूरक हैं। Jain Education International ain Education International For Private & Personal Use Only For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5