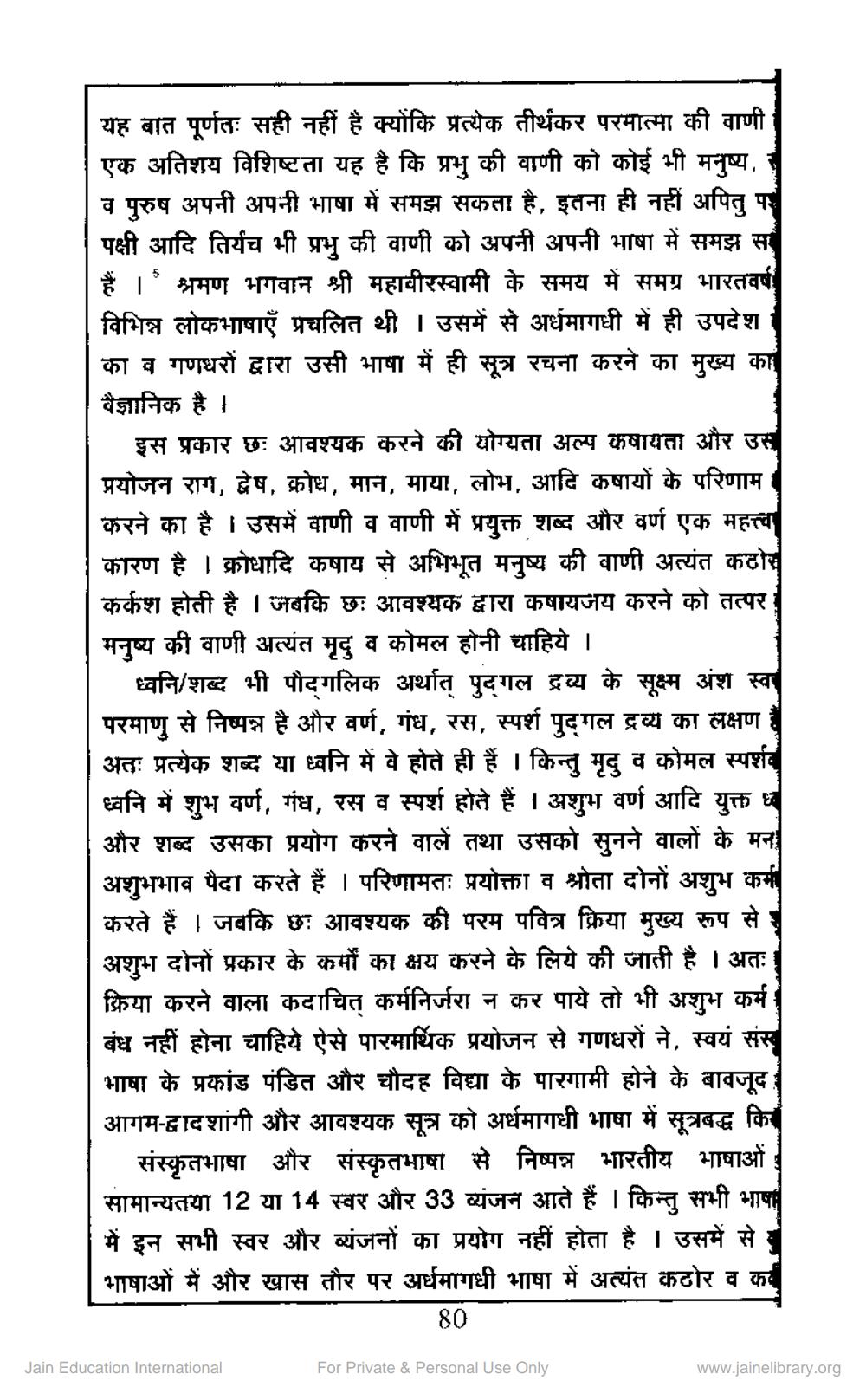Book Title: Shad Avashyak Ek Vaigyanik Vishleshan Author(s): Nandighoshvijay Publisher: Z_Jain_Dharm_Vigyan_ki_Kasoti_par_002549.pdf View full book textPage 2
________________ यह बात पूर्णत: सही नहीं है क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा की वाणी एक अतिशय विशिष्टता यह है कि प्रभु की वाणी को कोई भी मनुष्य, व पुरुष अपनी अपनी भाषा में समझ सकता है, इतना ही नहीं अपितु प पक्षी आदि तिर्यच भी प्रभु की वाणी को अपनी अपनी भाषा में समझ स हैं । श्रमण भगवान श्री महावीरस्वामी के समय में समग्र भारतवर्ष विभिन्न लोकभाषाएँ प्रचलित थी । उसमें से अर्धमागधी में ही उपदेश का व गणधरों द्वारा उसी भाषा में ही सूत्र रचना करने का मुख्य का वैज्ञानिक है । 5 इस प्रकार छः आवश्यक करने की योग्यता अल्प कषायता और उस प्रयोजन राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, आदि कषायों के परिणाम करने का है । उसमें वाणी व वाणी में प्रयुक्त शब्द और वर्ण एक महत्त्वा कारण है । क्रोधादि कषाय से अभिभूत मनुष्य की वाणी अत्यंत कठो कर्कश होती है । जबकि छः आवश्यक द्वारा कषायजय करने को तत्पर मनुष्य की वाणी अत्यंत मृदु व कोमल होनी चाहिये । ध्वनि / शब्द भी पौद्गलिक अर्थात् पुद्गल द्रव्य के सूक्ष्म अंश स्वर परमाणु से निष्पन्न है और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पुद्गल द्रव्य का लक्षण है। अतः प्रत्येक शब्द या ध्वनि में वे होते ही हैं । किन्तु मृदु व कोमल स्पर्शक ध्वनि में शुभ वर्ण, गंध, रस व स्पर्श होते हैं । अशुभ वर्ण आदि युक्त ध्व और शब्द उसका प्रयोग करने वालें तथा उसको सुनने वालों के मन अशुभभाव पैदा करते हैं । परिणामतः प्रयोक्ता व श्रोता दोनों अशुभ कर्म करते हैं । जबकि छः आवश्यक की परम पवित्र क्रिया मुख्य रूप से अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का क्षय करने के लिये की जाती है । अतः क्रिया करने वाला कदाचित् कर्मनिर्जरा न कर पाये तो भी अशुभ कर्म: बंध नहीं होना चाहिये ऐसे पारमार्थिक प्रयोजन से गणधरों ने स्वयं संस् भाषा के प्रकांड पंडित और चौदह विद्या के पारगामी होने के बावजूद आगम-द्वादशांगी और आवश्यक सूत्र को अर्धमागधी भाषा में सूत्रबद्ध किर संस्कृतभाषा और संस्कृतभाषा से निष्पन्न भारतीय भाषाओं सामान्यतया 12 या 14 स्वर और 33 व्यंजन आते हैं । किन्तु सभी भाषा में इन सभी स्वर और व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है । उसमें से € भाषाओं में और खास तौर पर अर्धमागधी भाषा में अत्यंत कठोर व क 80 For Private & Personal Use Only Jain Education International www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8