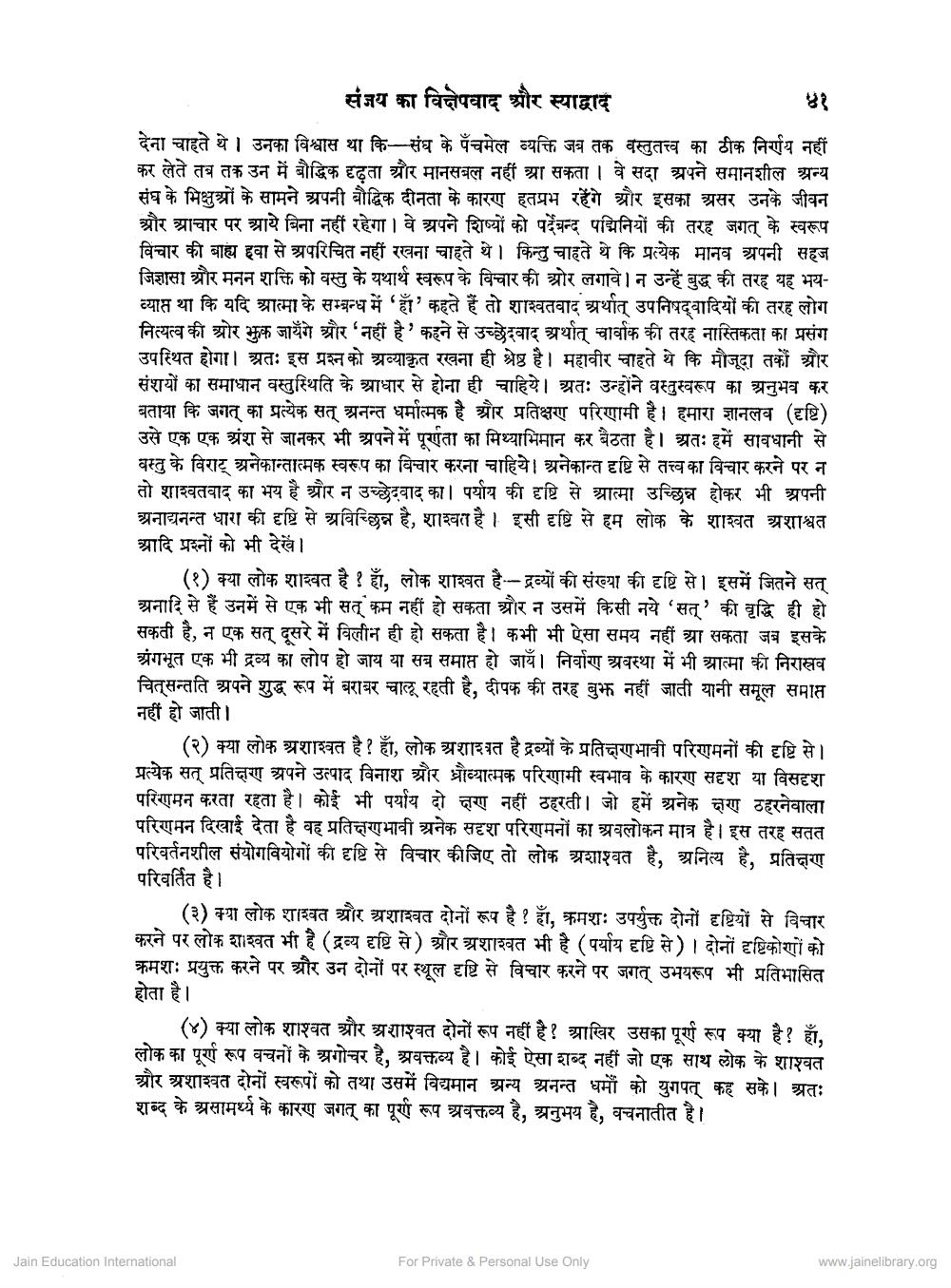Book Title: Sanjay ka Vikshepvada aur Syadwad Author(s): Mahendrakumar Jain Publisher: Z_Vijay_Vallabh_suri_Smarak_Granth_012060.pdf View full book textPage 3
________________ संजय का विक्षेपवाद और स्याद्वाद ४१ देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि संघ के पँचमेल व्यक्ति जब तक वस्तुतत्त्व का ठीक निर्णय नहीं कर लेते तब तक उन में बौद्धिक दृढ़ता और मानसबल नहीं पा सकता । वे सदा अपने समानशील अन्य संघ के भिक्षुत्रों के सामने अपनी बौद्धिक दीनता के कारण हतप्रभ रहेंगे और इसका असर उनके जीवन और प्राचार पर आये बिना नहीं रहेगा। वे अपने शिष्यों को पर्देचन्द पद्मिनियों की तरह जगत् के स्वरूप विचार की बाह्य हवा से अपरिचित नहीं रखना चाहते थे। किन्तु चाहते थे कि प्रत्येक मानव अपनी सहज जिज्ञासा और मनन शक्ति को वस्तु के यथार्थ स्वरूप के विचार की ओर लगावे। न उन्हें बुद्ध की तरह यह भयव्याप्त था कि यदि अात्मा के सम्बन्ध में 'हाँ' कहते हैं तो शाश्वतवाद अर्थात् उपनिषद्वादियों की तरह लोग नित्यत्व की ओर झुक जायेंगे और 'नहीं है' कहने से उच्छेदवाद अर्थात् चार्वाक की तरह नास्तिकता का प्रसंग उपस्थित होगा। अतः इस प्रश्न को अव्याकृत रखना ही श्रेष्ठ है। महावीर चाहते थे कि मौजूदा तों और संशयों का समाधान वस्तुस्थिति के आधार से होना ही चाहिये। अतः उन्होंने वस्तुस्वरूप का अनुभव कर बताया कि जगत् का प्रत्येक सत् अनन्त धर्मात्मक है और प्रतिक्षण परिणामी है। हमारा ज्ञानलव (दृष्टि) उसे एक एक अंश से जानकर भी अपने में पूर्णता का मिथ्याभिमान कर बैठता है। अतः हमें सावधानी से वस्तु के विराट् अनेकान्तात्मक स्वरूप का विचार करना चाहिये। अनेकान्त दृष्टि से तत्त्व का विचार करने पर न तो शाश्वतवाद का भय है और न उच्छेदवाद का। पर्याय की दृष्टि से अात्मा उच्छिन्न होकर भी अपनी अनाद्यनन्त धारा की दृष्टि से अविच्छिन्न है, शाश्वत है। इसी दृष्टि से हम लोक के शाश्वत अशाश्वत आदि प्रश्नों को भी देखें। (१) क्या लोक शाश्वत है ? हाँ, लोक शाश्वत है-द्रव्यों की संख्या की दृष्टि से। इसमें जितने सत् अनादि से हैं उनमें से एक भी सत् कम नहीं हो सकता और न उसमें किसी नये 'सत्' की वृद्धि ही हो सकती है, न एक सत् दूसरे में विलीन ही हो सकता है। कभी भी ऐसा समय नहीं पा सकता जब इसके अंगभूत एक भी द्रव्य का लोप हो जाय या सब समाप्त हो जायँ। निर्वाण अवस्था में भी आत्मा की निरास्रव चित्सन्तति अपने शुद्ध रूप में बराबर चालू रहती है, दीपक की तरह बुझ नहीं जाती यानी समूल समाप्त नहीं हो जाती। (२) क्या लोक अशाश्वत है? हाँ, लोक अशाश्वत है द्रव्यों के प्रतिक्षणभावी परिणमनों की दृष्टि से। प्रत्येक सत् प्रतिक्षण अपने उत्पाद विनाश और ध्रौव्यात्मक परिणामी स्वभाव के कारण सदृश या विसदृश परिणमन करता रहता है। कोई भी पर्याय दो क्षण नहीं ठहरती। जो हमें अनेक क्षण ठहरनेवाला परिणमन दिखाई देता है वह प्रतिक्षणभावी अनेक सदृश परिणमनों का अवलोकन मात्र है। इस तरह सतत परिवर्तनशील संयोगवियोगों की दृष्टि से विचार कीजिए तो लोक अशाश्वत है, अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तित है। (३) क्या लोक शाश्वत और अशाश्वत दोनों रूप है ? हाँ, क्रमशः उपर्युक्त दोनों दृष्टियों से विचार करने पर लोक शाश्वत भी है (द्रव्य दृष्टि से) और अशाश्वत भी है (पर्याय दृष्टि से)। दोनों दृष्टिकोणों को क्रमशः प्रयुक्त करने पर और उन दोनों पर स्थूल दृष्टि से विचार करने पर जगत् उभयरूप भी प्रतिभासित होता है। (४) क्या लोक शाश्वत और अशाश्वत दोनों रूप नहीं है ? आखिर उसका पूर्ण रूप क्या है ? हाँ, लोक का पूर्ण रूप वचनों के अगोचर है, अवक्तव्य है। कोई ऐसा शब्द नहीं जो एक साथ लोक के शाश्वत और अशाश्वत दोनों स्वरूपों को तथा उसमें विद्यमान अन्य अनन्त धर्मों को युगपत् कह सके। अतः शब्द के असामर्थ्य के कारण जगत् का पूर्ण रूप अवक्तव्य है, अनुभय है, वचनातीत है। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5