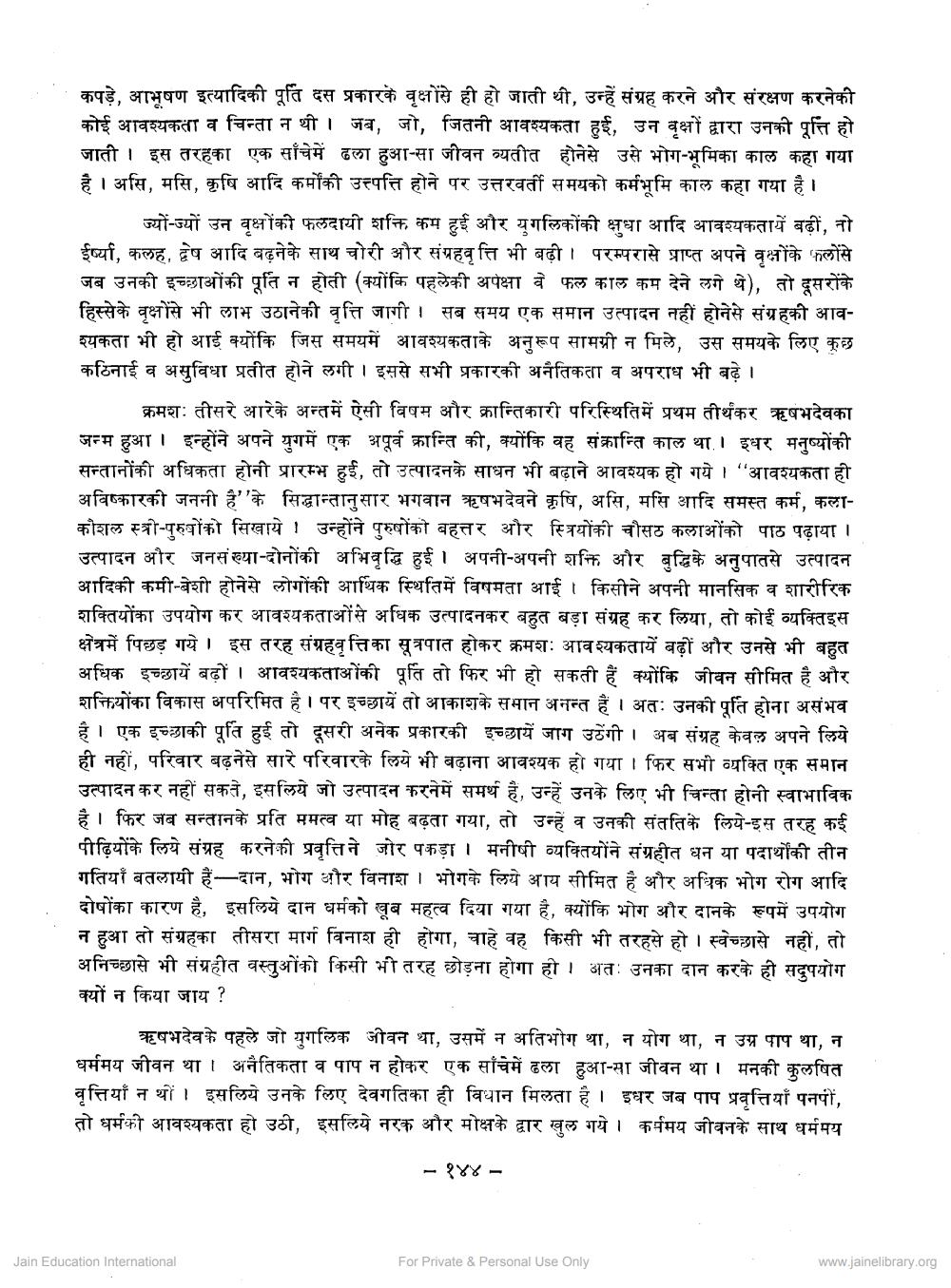Book Title: Sangraha vrutti se Asangraha vrutti ki aur Author(s): Agarchand Nahta Publisher: Z_Kailashchandra_Shastri_Abhinandan_Granth_012048.pdf View full book textPage 2
________________ कपड़े, आभषण इत्यादिकी पूर्ति दस प्रकारके वृक्षोंसे ही हो जाती थी, उन्हें संग्रह करने और संरक्षण करनेकी कोई आवश्यकता व चिन्ता न थी। जब, जो, जितनी आवश्यकता हुई, उन वृक्षों द्वारा उनकी पूति हो जाती। इस तरहका एक साँचे में ढला हुआ-सा जीवन व्यतीत होनेसे उसे भोग-भमिका काल कहा गया है । असि, मसि, कृषि आदि कर्मोंकी उत्पत्ति होने पर उत्तरवर्ती समयको कर्मभूमि काल कहा गया है। ज्यों-ज्यों उन वृक्षोंकी फलदायी शक्ति कम हुई और युगलिकोंकी क्षुधा आदि आवश्यकतायें बढ़ीं, नो ईर्ष्या, कलह, द्वष आदि बढ़ने के साथ चोरी और संग्रहवत्ति भी बढ़ी। परम्परासे प्राप्त अपने वक्षोंके फलोंसे जब उनकी इच्छाओंकी पूर्ति न होती (क्योंकि पहलेकी अपेक्षा वे फल काल कम देने लगे थे), तो दूसरोंके हिस्सेके वृक्षोंसे भी लाभ उठानेकी वृत्ति जागी। सब समय एक समान उत्पादन नहीं होनेसे संग्रहकी आवश्यकता भी हो आई क्योंकि जिस समयमें आवश्यकताके अनुरूप सामग्री न मिले, उस समयके लिए कुछ कठिनाई व असुविधा प्रतीत होने लगी। इससे सभी प्रकारकी अनैतिकता व अपराध भी बढ़े। क्रमशः तीसरे आरेके अन्तमें ऐसी विषम और क्रान्तिकारी परिस्थिति में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवका जन्म हुआ। इन्होंने अपने युगमें एक अपूर्व क्रान्ति की, क्योंकि वह संक्रान्ति काल था। इधर मनुष्योंकी सन्तानोंकी अधिकता होनी प्रारम्भ हुई, तो उत्पादनके साधन भी बढ़ाने आवश्यक हो गये । “आवश्यकता ही अविष्कारकी जननी है"के सिद्धान्तानुसार भगवान ऋषभदेवने कृषि, असि, मसि आदि समस्त कर्म, कलाकौशल स्त्री-पुरुषोंको सिखाये । उन्होंने पुरुषोंको बहत्तर और स्त्रियोंकी चौसठ कलाओंको पाठ पढ़ाया । उत्पादन और जनसंख्या-दोनोंकी अभिवृद्धि हुई। अपनी-अपनी शक्ति और बुद्धिके अनुपातसे उत्पादन आदिकी कमी-बेशी होनेसे लोगोंकी आर्थिक स्थितिमें विषमता आई। किसीने अपनी मानसिक व शारीरिक शक्तियोंका उपयोग कर आवश्यकताओंसे अधिक उत्पादनकर बहुत बड़ा संग्रह कर लिया, तो कोई व्यक्तिइस क्षेत्रमें पिछड गये। इस तरह संग्रहवत्तिका सूत्रपात होकर क्रमशः आवश्यकतायें बढों और उनसे भी बहत अधिक इच्छायें बढ़ों । आवश्यकताओंकी पूर्ति तो फिर भी हो सकती हैं क्योंकि जीवन सीमित है और शक्तियोंका विकास अपरिमित है। पर इच्छायें तो आकाशके समान अनन्त हैं । अतः उनकी पूर्ति होना असंभव है। एक इच्छाकी पूर्ति हुई तो दूसरी अनेक प्रकारकी इच्छायें जाग उठेगी। अब संग्रह केवल अपने लिये ही नहीं, परिवार बढ़नेसे सारे परिवारके लिये भी बढ़ाना आवश्यक हो गया। फिर सभी व्यक्ति एक समान उत्पादन कर नहीं सकते, इसलिये जो उत्पादन करनेमें समर्थ है, उन्हें उनके लिए भी चिन्ता होनी स्वाभाविक है। फिर जब सन्तानके प्रति ममत्व या मोह बढ़ता गया, तो उन्हें व उनकी संतति के लिये-इस तरह कई पीढ़ियोंके लिये संग्रह करने की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा। मनीषी व्यक्तियोंने संग्रहीत धन या पदार्थोकी तीन गतियाँ बतलायी हैं-दान, भोग और विनाश । भोगके लिये आय सीमित है और अधिक भोग रोग आदि दोषोंका कारण है, इसलिये दान धर्मको खूब महत्व दिया गया है, क्योंकि भोग और दानके रूपमें उपयोग न हआ तो संग्रहका तीसरा मार्ग विनाश ही होगा, चाहे वह किसी भी तरहसे हो । स्वेच्छासे नहीं, तो अनिच्छासे भी संग्रहीत वस्तुओंको किसी भी तरह छोड़ना होगा ही। अतः उनका दान करके ही सदुपयोग क्यों न किया जाय ? ऋषभदेवके पहले जो युगलिक जीवन था, उसमें न अतिभोग था, न योग था, न उन पाप था, न धर्ममय जीवन था। अनैतिकता व पाप न होकर एक साँचेमें ढला हआ-सा जीवन था । मनकी कुलषित वत्तियाँ न थों। इसलिये उनके लिए देवगतिका ही विधान मिलता है। इधर जब पाप प्रवत्तियाँ पनपों, तो धर्मकी आवश्यकता हो उठी, इसलिये नरक और मोक्षके द्वार खुल गये। कर्ममय जीवनके साथ धर्ममय -१४४ - Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4