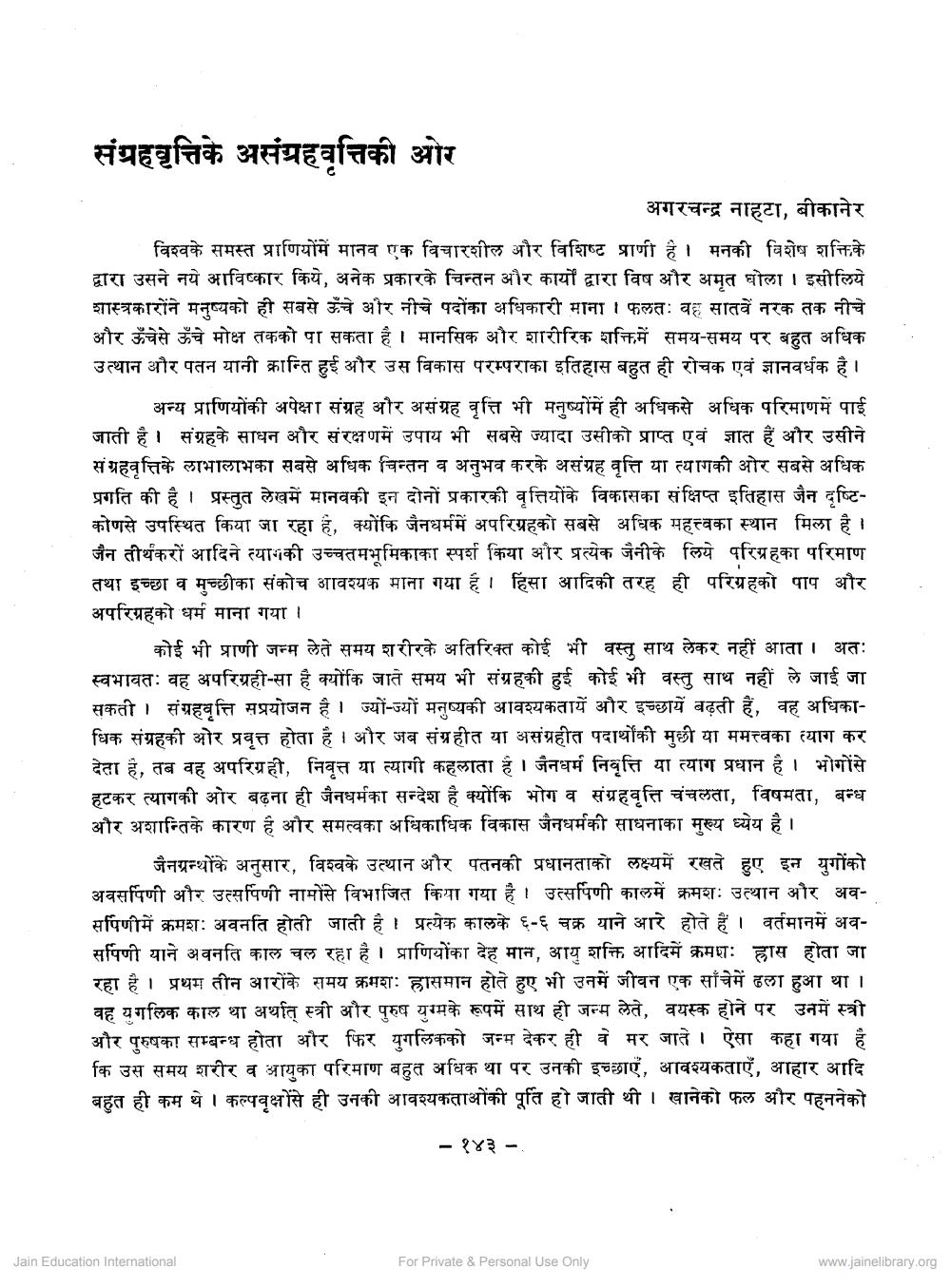Book Title: Sangraha vrutti se Asangraha vrutti ki aur Author(s): Agarchand Nahta Publisher: Z_Kailashchandra_Shastri_Abhinandan_Granth_012048.pdf View full book textPage 1
________________ संग्रहवृत्तिके असंग्रहवृत्तिकी ओर अगरचन्द्र नाहटा, बीकानेर विश्वके समस्त प्राणियोंमें मानव एक विचारशील और विशिष्ट प्राणी है। मनकी विशेष शक्तिके द्वारा उसने नये आविष्कार किये, अनेक प्रकारके चिन्तन और कार्यों द्वारा विष और अमत घोला । इसीलिये शास्त्रकारोंने मनुष्यको ही सबसे ऊँचे और नीचे पदोंका अधिकारी माना । फलतः वह सातवें नरक तक नीचे और ऊँचेसे ऊँचे मोक्ष तकको पा सकता है। मानसिक और शारीरिक शक्तिमें समय-समय पर बहुत अधिक उत्थान और पतन यानी क्रान्ति हुई और उस विकास परम्पराका इतिहास बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा संग्रह और असंग्रह वृत्ति भी मनुष्योंमें ही अधिकसे अधिक परिमाणमें पाई जाती है। संग्रहके साधन और संरक्षणमें उपाय भी सबसे ज्यादा उसीको प्राप्त एवं ज्ञात हैं और उसीने संग्रहवृत्तिके लाभालाभका सबसे अधिक चिन्तन व अनुभव करके असंग्रह वृत्ति या त्यागकी ओर सबसे अधिक प्रगति की है। प्रस्तुत लेखमें मानवकी इन दोनों प्रकारकी वृत्तियोंके विकासका संक्षिप्त इतिहास जैन दृष्टिकोणसे उपस्थित किया जा रहा है, क्योंकि जैनधर्ममें अपरिग्रहको सबसे अधिक महत्त्वका स्थान मिला है। जैन तीर्थंकरों आदिने त्यागकी उच्चतमभूमिकाका स्पर्श किया और प्रत्येक जैनीके लिये परिग्रहका परिमाण तथा इच्छा व मच्छीका संकोच आवश्यक माना गया है। हिंसा आदिकी तरह ही परिग्रहको पाप और अपरिग्रहको धर्म माना गया । कोई भी प्राणी जन्म लेते समय शरीरके अतिरिक्त कोई भी वस्तु साथ लेकर नहीं आता। अतः स्वभावतः वह अपरिग्रही-सा है क्योंकि जाते समय भी संग्रहकी हुई कोई भी वस्तु साथ नहीं ले जाई जा सकती। संग्रहवृत्ति सप्रयोजन है। ज्यों-ज्यों मनुष्यकी आवश्यकतायें और इच्छायें बढ़ती हैं, वह अधिकाधिक संग्रहकी ओर प्रवृत्त होता है। और जब संग्रहीत या असंग्रहीत पदार्थों की मुछी या ममत्त्वका त्याग कर देता है, तब वह अपरिग्रही, निवृत्त या त्यागी कहलाता है । जैनधर्म निवृत्ति या त्याग प्रधान है। भोगोंसे हटकर त्यागकी और बढ़ना ही जैनधर्मका सन्देश है क्योंकि भोग व संग्रहवृत्ति चंचलता, विषमता, बन्ध और अशान्तिके कारण है और समत्वका अधिकाधिक विकास जैनधर्मकी साधनाका मुख्य ध्येय है। जैनग्रन्थोंके अनुसार, विश्वके उत्थान और पतनकी प्रधानताको लक्ष्यमें रखते हुए इन युगोंको अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी नामोंसे विभाजित किया गया है। उत्सर्पिणी कालमें क्रमशः उत्थान और अवसर्पिणीमें क्रमशः अवनति होती जाती है। प्रत्येक कालके ६-६ चक्र याने आरे होते हैं। वर्तमानमें अवसर्पिणी याने अवनति काल चल रहा है। प्राणियोंका देह मान, आयु शक्ति आदिमें क्रमशः ह्रास होता जा रहा है। प्रथम तीन आरोके समय क्रमशः ह्रासमान होते हुए भी उनमें जीवन एक साँचेमें ढला हुआ था। वह य गलिक काल था अर्थात् स्त्री और पुरुष युग्मके रूपमें साथ ही जन्म लेते, वयस्क होने पर उनमें स्त्री और पुरुषका सम्बन्ध होता और फिर युगलिकको जन्म देकर ही वे मर जाते । ऐसा कहा गया है कि उस समय शरीर व आयुका परिमाण बहुत अधिक था पर उनकी इच्छाएँ, आवश्यकताएँ, आहार आदि बहत ही कम थे । कल्पवृक्षोंसे ही उनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति हो जाती थी। खानेको फल और पहननेको -१४३ - Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4