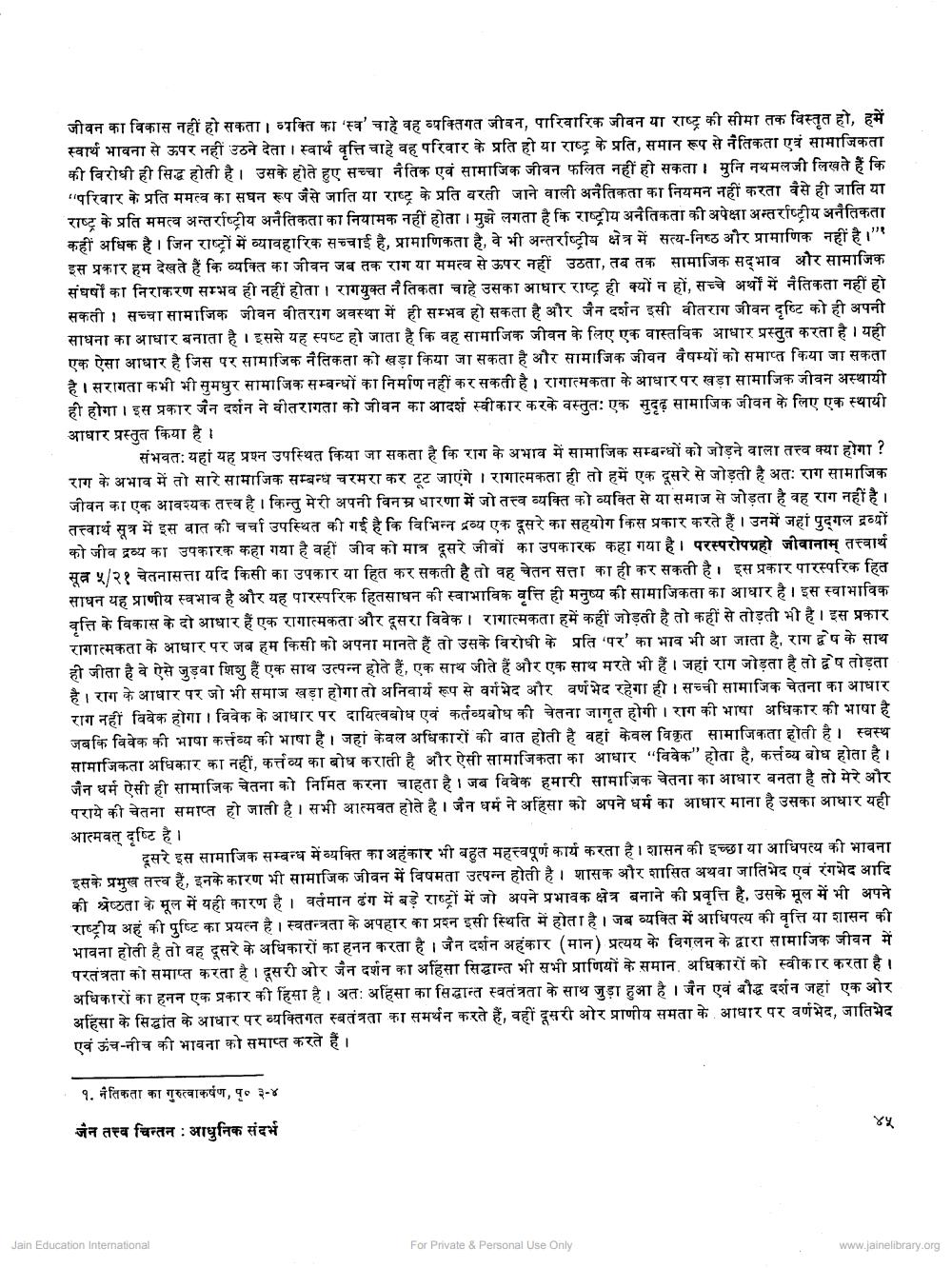Book Title: Samajik Samasyo me Samadhan me Jain Dharm ka Yogadan Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 6
________________ १११ जीवन का विकास नहीं हो सकता। व्यक्ति का 'स्व' चाहे वह व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन या राष्ट्र की सीमा तक विस्तृत हो, हमें स्वार्थ भावना से ऊपर नहीं उठने देता। स्वार्थ वृत्ति चाहे वह परिवार के प्रति हो या राष्ट्र के प्रति, समान रूप से नैतिकता एवं सामाजिकता की विरोधी ही सिद्ध होती है। उसके होते हुए सच्चा नैतिक एवं सामाजिक जीवन फलित नहीं हो सकता। मुनि नथमलजी लिखते हैं कि "परिवार के प्रति ममत्व का सघन रूप जैसे जाति या राष्ट्र के प्रति बरती जाने वाली अनैतिकता का नियमन नहीं करता वैसे ही जाति या राष्ट्र के प्रति ममत्व अन्तर्राष्ट्रीय अनैतिकता का नियामक नहीं होता। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अनैतिकता की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय अनैतिकता कहीं अधिक है। जिन राष्ट्रों में व्यावहारिक सच्चाई है, प्रामाणिकता है, वे भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सत्य-निष्ठ और प्रामाणिक नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का जीवन जब तक राग या ममत्व से ऊपर नहीं उठता, तब तक सामाजिक सद्भाव और सामाजिक संघर्षो का निराकरण सम्भव ही नहीं होता । रागयुक्त नैतिकता चाहे उसका आधार राष्ट्र ही क्यों न हों, सच्चे अर्थों में नैतिकता नहीं हो सकती । सच्चा सामाजिक जीवन वीतराग अवस्था में ही सम्भव हो सकता है और जैन दर्शन इसी वीतराग जीवन दृष्टि को ही अपनी साधना का आधार बनाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह सामाजिक जीवन के लिए एक वास्तविक आधार प्रस्तुत करता है । यही एक ऐसा आधार है जिस पर सामाजिक नैतिकता को खड़ा किया जा सकता है और सामाजिक जीवन वैषम्यों को समाप्त किया जा सकता है। सरागता कभी भी सुमधुर सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण नहीं कर सकती है। रागात्मकता के आधार पर खड़ा सामाजिक जीवन अस्थायी ही होगा। इस प्रकार जैन दर्शन ने वीतरागता को जीवन का आदर्श स्वीकार करके वस्तुतः एक सुदृढ़ सामाजिक जीवन के लिए एक आधार प्रस्तुत किया है । स्थायी संभवतः यहां यह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है कि राग के अभाव में सामाजिक सम्बन्धों को जोड़ने वाला तत्त्व क्या होगा ? राग के अभाव में तो सारे सामाजिक सम्बन्ध चरमरा कर टूट जाएंगे । रागात्मकता ही तो हमें एक दूसरे से जोड़ती है अतः राग सामाजिक जीवन का एक आवश्यक तत्त्व है। किन्तु मेरी अपनी विनम्र धारणा में जो तत्त्व व्यक्ति को व्यक्ति से या समाज से जोड़ता है वह राग नहीं है । तत्त्वार्थ सूत्र 'में इस बात की चर्चा उपस्थित की गई है कि विभिन्न द्रव्य एक दूसरे का सहयोग किस प्रकार करते हैं। उनमें जहां पुद्गल द्रव्यों को जीव द्रव्य का उपकारक कहा गया है वहीं जीव को मात्र दूसरे जीवों का उपकारक कहा गया है। परस्परोपग्रहो जीवानाम् तत्त्वार्थ सूत्र ५ / २१ चेतनासत्ता यदि किसी का उपकार या हित कर सकती है तो वह चेतन सत्ता का ही कर सकती है। इस प्रकार पारस्परिक हित साधन यह प्राणीय स्वभाव है और यह पारस्परिक हितसाधन की स्वाभाविक वृत्ति ही मनुष्य की सामाजिकता का आधार है । इस स्वाभाविक वृत्ति के विकास के दो आधार हैं एक रागात्मकता और दूसरा विवेक । रागात्मकता हमें कहीं जोड़ती है तो कहीं से तोड़ती भी है। इस प्रकार रागात्मकता के आधार पर जब हम किसी को अपना मानते हैं तो उसके विरोधी के प्रति 'पर' का भाव भी आ जाता है, राग द्वेष के साथ ही जीता है वे ऐसे जुड़वा शिशु हैं एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ जीते हैं और एक साथ मरते भी हैं। जहां राग जोड़ता है तो द्वेष तोड़ता है । राग के आधार पर जो भी समाज खड़ा होगा तो अनिवार्य रूप से वर्गभेद और वर्णभेद रहेगा ही। सच्ची सामाजिक चेतना का आधार राग नहीं विवेक होगा। विवेक के आधार पर दायित्वबोध एवं कर्तव्यबोध की चेतना जागृत होगी। राग की भाषा अधिकार की भाषा है जबकि विवेक की भाषा कर्त्तव्य की भाषा है। जहां केवल अधिकारों की बात होती है वहां केवल विकृत सामाजिकता होती है । स्वस्थ सामाजिकता अधिकार का नहीं, कर्तव्य का बोध कराती है और ऐसी सामाजिकता का आधार “विवेक" होता है, कर्तव्य बोध होता है। जैन धर्म ऐसी ही सामाजिक चेतना को निर्मित करना चाहता है। जब विवेक हमारी सामाजिक चेतना का आधार बनता है तो मेरे और पराये की चेतना समाप्त हो जाती है। सभी आत्मवत होते है। जैन धर्म ने अहिंसा को अपने धर्म का आधार माना है उसका आधार यही आत्मवत् दृष्टि है । दूसरे इस सामाजिक सम्बन्ध में व्यक्ति का अहंकार भी बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य करता है। शासन की इच्छा या आधिपत्य की भावना इसके प्रमुख तत्त्व हैं, इनके कारण भी सामाजिक जीवन में विषमता उत्पन्न होती है। शासक और शासित अथवा जातिभेद एवं रंगभेद आदि की श्रेष्ठता के मूल में यही कारण है। वर्तमान ढंग में बड़े राष्ट्रों में जो अपने प्रभावक क्षेत्र बनाने की प्रवृत्ति है, उसके मूल में भी अपने राष्ट्रीय अहं की पुष्टि का प्रयत्न है । स्वतन्त्रता के अपहार का प्रश्न इसी स्थिति में होता है। जब व्यक्ति में आधिपत्य की वृत्ति या शासन की भावना होती है तो वह दूसरे के अधिकारों का हनन करता है। जैन दर्शन अहंकार (मान) प्रत्यय के विगलन के द्वारा सामाजिक जीवन में परतंत्रता को समाप्त करता है। दूसरी ओर जैन दर्शन का अहिंसा सिद्धान्त भी सभी प्राणियों के समान अधिकारों को स्वीकार करता है । अधिकारों का हनन एक प्रकार की हिंसा है। अतः अहिंसा का सिद्धान्त स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ है। जैन एवं बौद्ध दर्शन जहां एक ओर अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्राणीय समता के आधार पर वर्णभेद, जातिभेद एवं ऊंच-नीच की भावना को समाप्त करते हैं । १. नैतिकता का गुरुत्वाकर्षण, पू० ३-४ जैन तत्व चिन्तन आधुनिक संदर्भ Jain Education International : For Private & Personal Use Only ४५ www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9