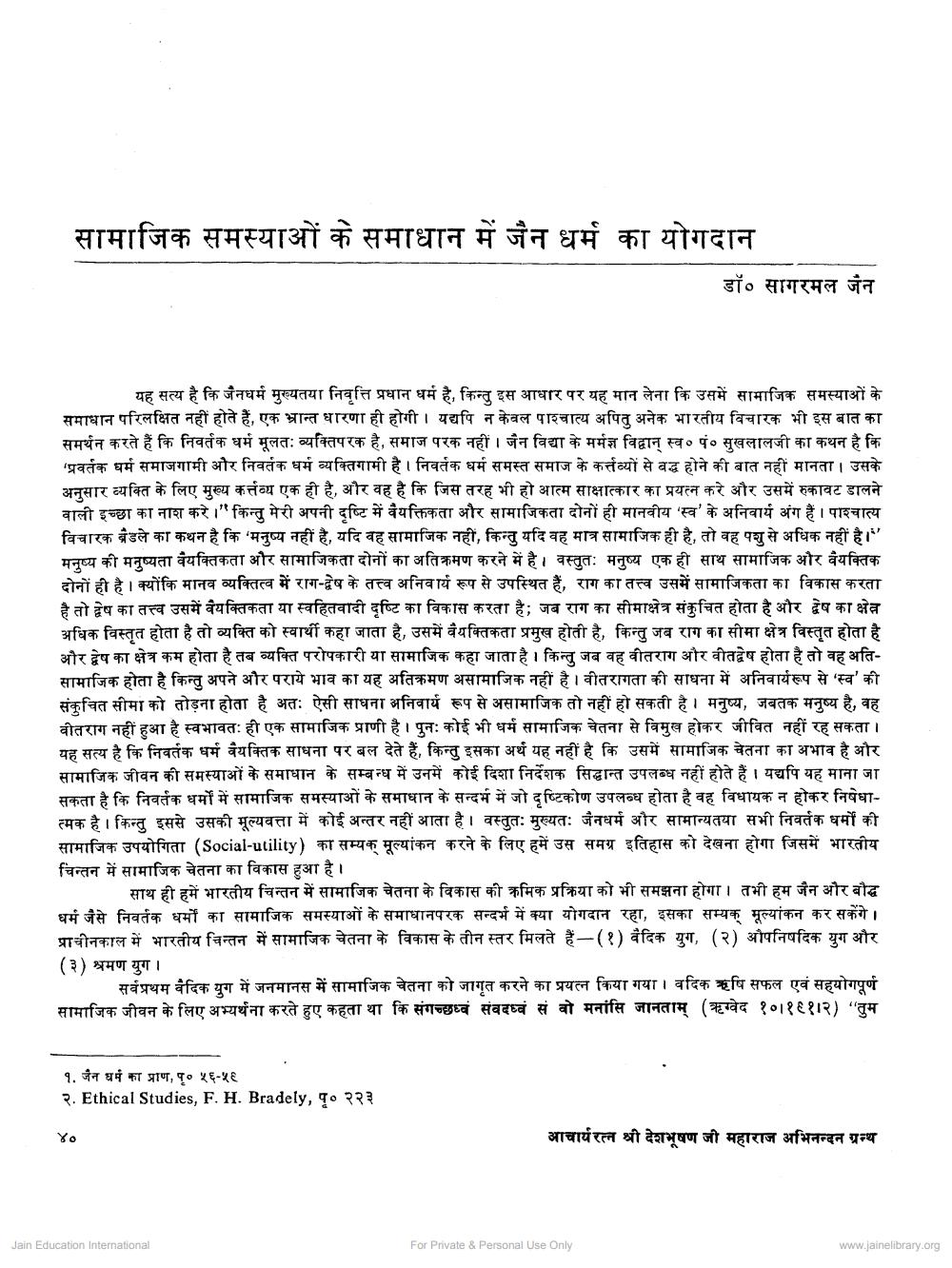Book Title: Samajik Samasyo me Samadhan me Jain Dharm ka Yogadan Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 1
________________ सामाजिक समस्याओं के समाधान में जैन धर्म का योगदान यह सत्य है कि जैनधर्म मुख्यतया निवृत्ति प्रधान धर्म है, किन्तु इस आधार पर यह मान लेना कि उसमें सामाजिक समस्याओं के समाधान परिलक्षित नहीं होते हैं, एक भ्रान्त धारणा ही होगी । यद्यपि न केवल पाश्चात्य अपितु अनेक भारतीय विचारक भी इस बात का समर्थन करते हैं कि निवर्तक धर्म मूलतः व्यक्तिपरक है, समाज परक नहीं । जैन विद्या के मर्मज्ञ विद्वान् स्व० पं० सुखलालजी का कथन है कि 'प्रवर्तक धर्म समाजगामी और निवर्तक धर्म व्यक्तिगामी है । निवर्तक धर्म समस्त समाज के कर्त्तव्यों से बद्ध होने की बात नहीं मानता। उसके अनुसार व्यक्ति के लिए मुख्य कर्त्तव्य एक ही है, और वह है कि जिस तरह भी हो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करे और उसमें रुकावट डालने वाली इच्छा का नाश करे ।" किन्तु मेरी अपनी दृष्टि में वैयक्तिकता और सामाजिकता दोनों ही मानवीय 'स्व' के अनिवार्य अंग हैं । पाश्चात्य विचारक ब्रेडले का कथन है कि 'मनुष्य नहीं है, यदि वह सामाजिक नहीं, किन्तु यदि वह मात्र सामाजिक ही है, तो वह पशु से अधिक नहीं है । " मनुष्य की मनुष्यता वैयक्तिकता और सामाजिकता दोनों का अतिक्रमण करने में है। वस्तुतः मनुष्य एक ही साथ सामाजिक और वैयक्तिक दोनों ही है । क्योंकि मानव व्यक्तित्व में राग-द्वेष के तत्त्व अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं, राग का तत्त्व उसमें सामाजिकता का विकास करता है तो द्वेष का तत्त्व उसमें वैयक्तिकता या स्वहितवादी दृष्टि का विकास करता है; जब राग का सीमाक्षेत्र संकुचित होता है और द्वेष का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है तो व्यक्ति को स्वार्थी कहा जाता है, उसमें वैयक्तिकता प्रमुख होती है, किन्तु जब राग का सीमा क्षेत्र विस्तृत होता है। और द्वेष का क्षेत्र कम होता है तब व्यक्ति परोपकारी या सामाजिक कहा जाता है। किन्तु जब वह वीतराग और बीतद्वेष होता है तो वह अतिसामाजिक होता है किन्तु अपने और पराये भाव का यह अतिक्रमण असामाजिक नहीं है। वीतरागता की साधना में अनिवार्यरूप से 'स्व' की संकुचित सीमा को तोड़ना होता है अतः ऐसी साधना अनिवार्य रूप से असामाजिक तो नहीं हो सकती है। मनुष्य, जबतक मनुष्य है, वह बीतराग नहीं हुआ है स्वभावतः ही एक सामाजिक प्राणी है पुनः कोई भी धर्म सामाजिक चेतना से विमुख होकर जीवित नहीं रह सकता। यह सत्य है कि निवर्तक धर्म वैयक्तिक साधना पर बल देते हैं, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें सामाजिक चेतना का अभाव है और सामाजिक जीवन की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में उनमें कोई दिशा निर्देशक सिद्धान्त उपलब्ध नहीं होते हैं । यद्यपि यह माना जा सकता है कि निवर्तक धर्मों में सामाजिक समस्याओं के समाधान के सन्दर्भ में जो दृष्टिकोण उपलब्ध होता है वह विधायक न होकर निषेधात्मक है । किन्तु इससे उसकी मूल्यवत्ता में कोई अन्तर नहीं आता है। वस्तुतः मुख्यतः जैनधर्म और सामान्यतया सभी निवर्तक धर्मो की सामाजिक उपयोगिता ( Social utility) का सम्यक् मूल्यांकन करने के लिए हमें उस समग्र इतिहास को देखना होगा जिसमें भारतीय चिन्तन में सामाजिक चेतना का विकास हुआ है । साथ ही हमें भारतीय चिन्तन में सामाजिक चेतना के विकास की क्रमिक प्रक्रिया को भी समझना होगा। तभी हम जैन और बौद्ध धर्म जैसे निवर्तक धर्मों का सामाजिक समस्याओं के समाधानपरक सन्दर्भ में क्या योगदान रहा, इसका सम्यक् मूल्यांकन कर सकेंगे । प्राचीनकाल में भारतीय चिन्तन में सामाजिक चेतना के विकास के तीन स्तर मिलते हैं - (१) वैदिक युग, (२) औपनिषदिक (३) श्रमण युग । सर्वप्रथम वैदिक युग में जनमानस में सामाजिक चेतना को जागृत करने का प्रयत्न किया गया। वदिक ऋषि सफल एवं सहयोगपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए अभ्यर्थना करते हुए कहता था कि संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् (ऋग्वेद १०।१९१०२) तुम युग और १. जैन धर्म का प्राण, पृ० ५६-५६ २. Ethical Studies, F. H. Bradely, पृ० २२३ ४० Jain Education International डॉ० सागरमल जैन आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9