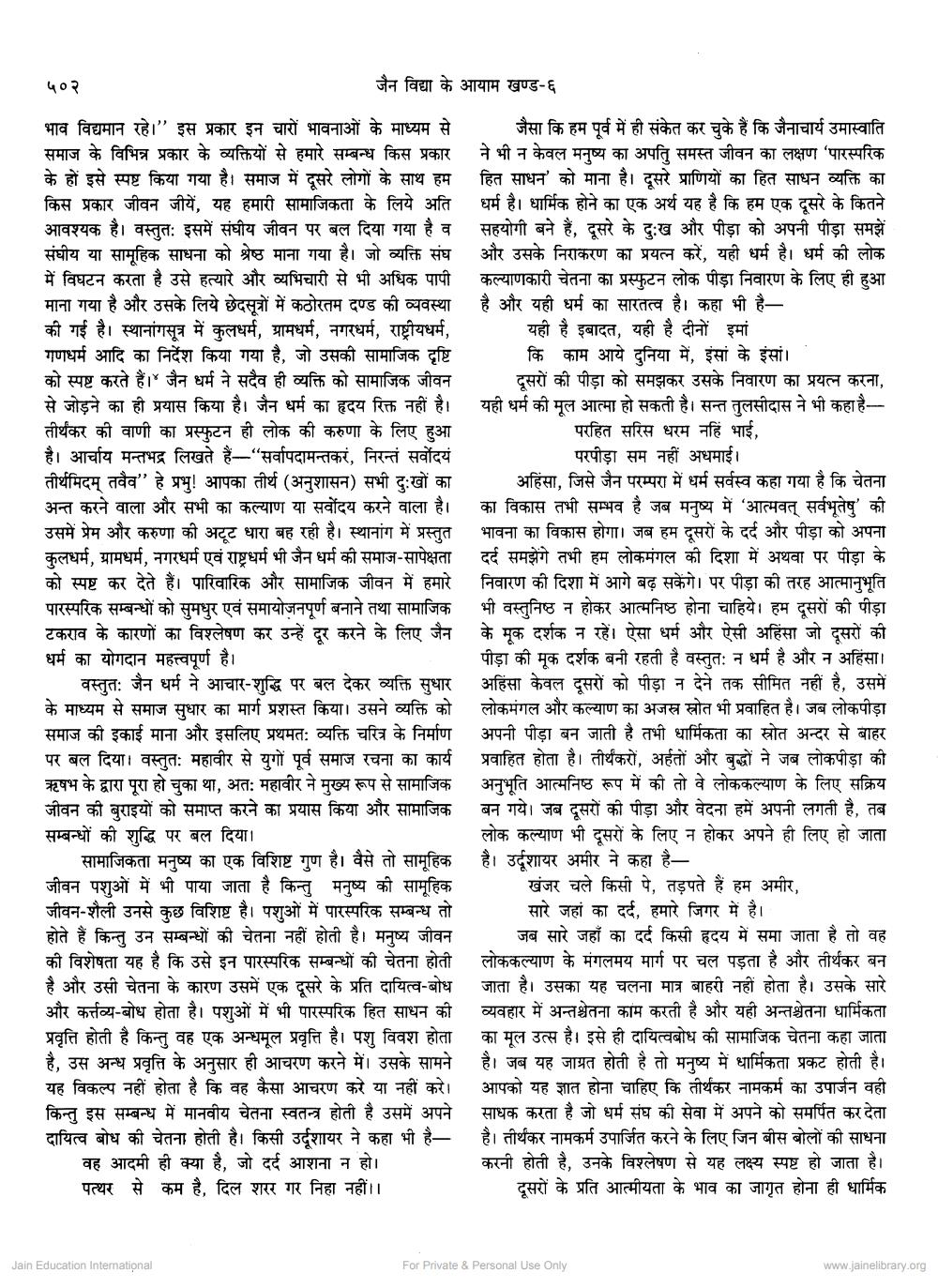Book Title: Sadhna aur Samaj Seva ka Saha Jain Dharm ke Pariprekshya me Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 2
________________ ५०२ जैन विद्या के आयाम खण्ड-६ भाव विद्यमान रहे।" इस प्रकार इन चारों भावनाओं के माध्यम से जैसा कि हम पूर्व में ही संकेत कर चुके हैं कि जैनाचार्य उमास्वाति समाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से हमारे सम्बन्ध किस प्रकार ने भी न केवल मनुष्य का अपतुि समस्त जीवन का लक्षण 'पारस्परिक के हों इसे स्पष्ट किया गया है। समाज में दूसरे लोगों के साथ हम हित साधन' को माना है। दूसरे प्राणियों का हित साधन व्यक्ति का किस प्रकार जीवन जीयें, यह हमारी सामाजिकता के लिये अति धर्म है। धार्मिक होने का एक अर्थ यह है कि हम एक दूसरे के कितने आवश्यक है। वस्तुत: इसमें संघीय जीवन पर बल दिया गया है व सहयोगी बने हैं, दूसरे के दु:ख और पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें संघीय या सामूहिक साधना को श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति संघ और उसके निराकरण का प्रयत्न करें, यही धर्म है। धर्म की लोक में विघटन करता है उसे हत्यारे और व्यभिचारी से भी अधिक पापी कल्याणकारी चेतना का प्रस्फुटन लोक पीड़ा निवारण के लिए ही हुआ माना गया है और उसके लिये छेदसूत्रों में कठोरतम दण्ड की व्यवस्था है और यही धर्म का सारतत्व है। कहा भी हैकी गई है। स्थानांगसूत्र में कुलधर्म, ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रीयधर्म, यही है इबादत, यही है दीनों इमां गणधर्म आदि का निर्देश किया गया है, जो उसकी सामाजिक दृष्टि कि काम आये दुनिया में, इंसां के इंसां। को स्पष्ट करते हैं। जैन धर्म ने सदैव ही व्यक्ति को सामाजिक जीवन दूसरों की पीड़ा को समझकर उसके निवारण का प्रयत्न करना, से जोड़ने का ही प्रयास किया है। जैन धर्म का हृदय रिक्त नहीं है। यही धर्म की मूल आत्मा हो सकती है। सन्त तुलसीदास ने भी कहा हैतीर्थंकर की वाणी का प्रस्फुटन ही लोक की करुणा के लिए हुआ परहित सरिस धरम नहिं भाई, है। आर्चाय मन्तभद्र लिखते हैं-"सर्वापदामन्तकरं, निरन्तं सर्वोदयं परपीड़ा सम नहीं अधमाई। तीर्थमिदम् तवैव' हे प्रभु! आपका तीर्थ (अनुशासन) सभी दुःखों का अहिंसा, जिसे जैन परम्परा में धर्म सर्वस्व कहा गया है कि चेतना अन्त करने वाला और सभी का कल्याण या सर्वोदय करने वाला है। का विकास तभी सम्भव है जब मनुष्य में 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की उसमें प्रेम और करुणा की अटूट धारा बह रही है। स्थानांग में प्रस्तुत भावना का विकास होगा। जब हम दूसरों के दर्द और पीड़ा को अपना कुलधर्म, ग्रामधर्म, नगरधर्म एवं राष्ट्रधर्म भी जैन धर्म की समाज-सापेक्षता दर्द समझेंगे तभी हम लोकमंगल की दिशा में अथवा पर पीड़ा के को स्पष्ट कर देते हैं। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में हमारे निवारण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। पर पीड़ा की तरह आत्मानुभूति पारस्परिक सम्बन्धों को सुमधुर एवं समायोजनपूर्ण बनाने तथा सामाजिक भी वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ होना चाहिये। हम दूसरों की पीड़ा टकराव के कारणों का विश्लेषण कर उन्हें दूर करने के लिए जैन के मूक दर्शक न रहें। ऐसा धर्म और ऐसी अहिंसा जो दूसरों की धर्म का योगदान महत्त्वपूर्ण है। पीड़ा की मूक दर्शक बनी रहती है वस्तुतः न धर्म है और न अहिंसा। वस्तुत: जैन धर्म ने आचार-शुद्धि पर बल देकर व्यक्ति सुधार अहिंसा केवल दूसरों को पीड़ा न देने तक सीमित नहीं है, उसमें के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। उसने व्यक्ति को लोकमंगल और कल्याण का अजस्र स्रोत भी प्रवाहित है। जब लोकपीड़ा समाज की इकाई माना और इसलिए प्रथमत: व्यक्ति चरित्र के निर्माण अपनी पीड़ा बन जाती है तभी धार्मिकता का स्रोत अन्दर से बाहर पर बल दिया। वस्तुत: महावीर से युगों पूर्व समाज रचना का कार्य प्रवाहित होता है। तीर्थंकरों, अर्हतों और बुद्धों ने जब लोकपीड़ा की ऋषभ के द्वारा पूरा हो चुका था, अत: महावीर ने मुख्य रूप से सामाजिक अनुभूति आत्मनिष्ठ रूप में की तो वे लोककल्याण के लिए सक्रिय जीवन की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया और सामाजिक बन गये। जब दूसरों की पीड़ा और वेदना हमें अपनी लगती है, तब सम्बन्धों की शुद्धि पर बल दिया। लोक कल्याण भी दूसरों के लिए न होकर अपने ही लिए हो जाता सामाजिकता मनुष्य का एक विशिष्ट गुण है। वैसे तो सामूहिक है। उर्दूशायर अमीर ने कहा हैजीवन पशुओं में भी पाया जाता है किन्तु मनुष्य की सामूहिक खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, जीवन-शैली उनसे कुछ विशिष्ट है। पशुओं में पारस्परिक सम्बन्ध तो सारे जहां का दर्द, हमारे जिगर में है। होते हैं किन्तु उन सम्बन्धों की चेतना नहीं होती है। मनुष्य जीवन जब सारे जहाँ का दर्द किसी हृदय में समा जाता है तो वह की विशेषता यह है कि उसे इन पारस्परिक सम्बन्धों की चेतना होती लोककल्याण के मंगलमय मार्ग पर चल पड़ता है और तीर्थंकर बन है और उसी चेतना के कारण उसमें एक दूसरे के प्रति दायित्व-बोध जाता है। उसका यह चलना मात्र बाहरी नहीं होता है। उसके सारे और कर्त्तव्य-बोध होता है। पशुओं में भी पारस्परिक हित साधन की व्यवहार में अन्तश्चेतना काम करती है और यही अन्तश्चेतना धार्मिकता प्रवृत्ति होती है किन्तु वह एक अन्धमूल प्रवृत्ति है। पशु विवश होता का मूल उत्स है। इसे ही दायित्वबोध की सामाजिक चेतना कहा जाता है, उस अन्ध प्रवृत्ति के अनुसार ही आचरण करने में। उसके सामने है। जब यह जाग्रत होती है तो मनुष्य में धार्मिकता प्रकट होती है। यह विकल्प नहीं होता है कि वह कैसा आचरण करे या नहीं करे। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि तीर्थकर नामकर्म का उपार्जन वही किन्तु इस सम्बन्ध में मानवीय चेतना स्वतन्त्र होती है उसमें अपने साधक करता है जो धर्म संघ की सेवा में अपने को समर्पित कर देता दायित्व बोध की चेतना होती है। किसी उर्दशायर ने कहा भी है- है। तीर्थकर नामकर्म उपार्जित करने के लिए जिन बीस बोलों की साधना वह आदमी ही क्या है, जो दर्द आशना न हो। करनी होती है, उनके विश्लेषण से यह लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। पत्थर से कम है, दिल शरर गर निहा नहीं।। दूसरों के प्रति आत्मीयता के भाव का जागृत होना ही धार्मिक Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4