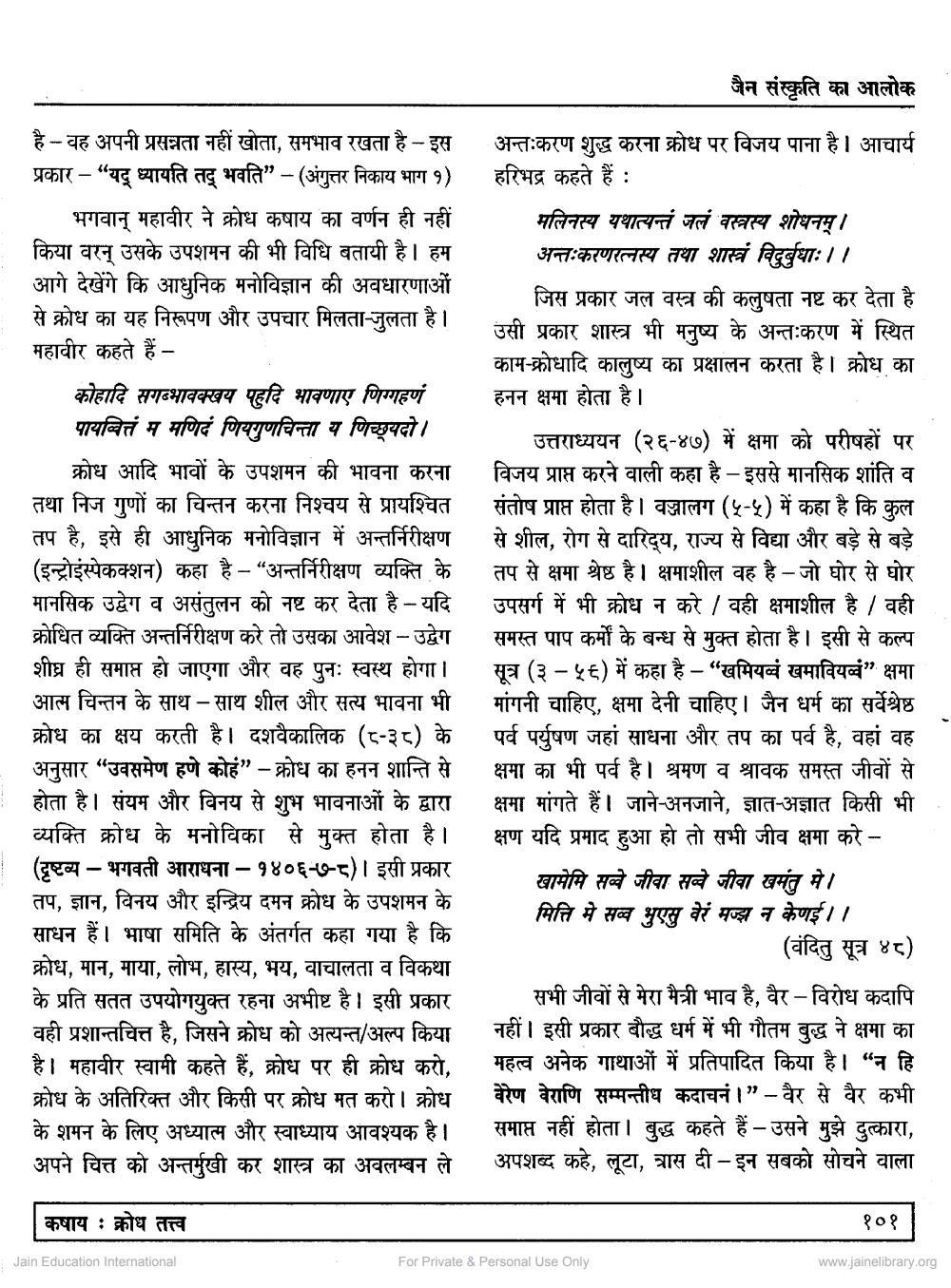Book Title: Kashay Krodh Tattva Author(s): Kalyanmal Lodha Publisher: Z_Sumanmuni_Padmamaharshi_Granth_012027.pdf View full book textPage 8
________________ जैन संस्कृति का आलोक है - वह अपनी प्रसन्नता नहीं खोता, समभाव रखता है - इस प्रकार – “यद् ध्यायति तद् भवति" – (अंगुत्तर निकाय भाग १) भगवान् महावीर ने क्रोध कषाय का वर्णन ही नहीं किया वरन् उसके उपशमन की भी विधि बतायी है। हम आगे देखेंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान की अवधारणाओं से क्रोध का यह निरूपण और उपचार मिलता-जुलता है। महावीर कहते हैं - कोहादि सगभावक्खय पहुदि भावणाए णिग्गहणं पायबित्तं म मणिदं णियगुणचिन्ता य णिच्छ्यदो। क्रोध आदि भावों के उपशमन की भावना करना तथा निज गुणों का चिन्तन करना निश्चय से प्रायश्चित तप है, इसे ही आधुनिक मनोविज्ञान में अन्तर्निरीक्षण (इन्ट्रोइंस्पेकक्शन) कहा है – “अन्तर्निरीक्षण व्यक्ति के मानसिक उद्वेग व असंतुलन को नष्ट कर देता है - यदि क्रोधित व्यक्ति अन्तर्निरीक्षण करे तो उसका आवेश - उद्वेग शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और वह पुनः स्वस्थ होगा। आम चिन्तन के साथ - साथ शील और सत्य भावना भी क्रोध का क्षय करती है। दशवैकालिक (८-३८) के अनुसार "उवसमेण हणे कोहं" - क्रोध का हनन शान्ति से होता है। संयम और विनय से शुभ भावनाओं के द्वारा व्यक्ति क्रोध के मनोविका से मुक्त होता है। (दृष्टव्य - भगवती आराधना - १४०६-७-८)। इसी प्रकार तप, ज्ञान, विनय और इन्द्रिय दमन क्रोध के उपशमन के साधन हैं। भाषा समिति के अंतर्गत कहा गया है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, वाचालता व विकथा के प्रति सतत उपयोगयुक्त रहना अभीष्ट है। इसी प्रकार वही प्रशान्तचित्त है, जिसने क्रोध को अत्यन्त/अल्प किया है। महावीर स्वामी कहते हैं, क्रोध पर ही क्रोध करो, क्रोध के अतिरिक्त और किसी पर क्रोध मत करो। क्रोध के शमन के लिए अध्यात्म और स्वाध्याय आवश्यक है। अपने चित्त को अन्तर्मुखी कर शास्त्र का अवलम्बन ले अन्तःकरण शुद्ध करना क्रोध पर विजय पाना है। आचार्य हरिभद्र कहते हैं : मलिनस्य यथात्यन्तं जलं वस्त्रस्य शोधनम् । अन्तःकरणरत्नस्य तथा शास्त्रं विदुर्बुधाः ।। जिस प्रकार जल वस्त्र की कलुषता नष्ट कर देता है उसी प्रकार शास्त्र भी मनुष्य के अन्तःकरण में स्थित काम-क्रोधादि कालुष्य का प्रक्षालन करता है। क्रोध का हनन क्षमा होता है। उत्तराध्ययन (२६-४७) में क्षमा को परीषहों पर विजय प्राप्त करने वाली कहा है - इससे मानसिक शांति व संतोष प्राप्त होता है। वज्जालग (५-५) में कहा है कि कुल से शील, रोग से दारिद्य, राज्य से विद्या और बड़े से बड़े तप से क्षमा श्रेष्ठ है। क्षमाशील वह है - जो घोर से घोर उपसर्ग में भी क्रोध न करे / वही क्षमाशील है / वही समस्त पाप कर्मों के बन्ध से मुक्त होता है। इसी से कल्प सूत्र (३-५६) में कहा है - "खमियब्वं खमावियबं" क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा देनी चाहिए। जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ पर्व पर्युषण जहां साधना और तप का पर्व है, वहां वह क्षमा का भी पर्व है। श्रमण व श्रावक समस्त जीवों से क्षमा मांगते हैं। जाने-अनजाने, ज्ञात-अज्ञात किसी भी क्षण यदि प्रमाद हुआ हो तो सभी जीव क्षमा करे - खामेमि सबे जीवा सब्वे जीवा खमंत मे। मित्ति मे सब्व भएसु वे मज्झ न केणई।।। (वंदितु सूत्र ४८) सभी जीवों से मेरा मैत्री भाव है, वैर - विरोध कदापि नहीं। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध ने क्षमा का महत्व अनेक गाथाओं में प्रतिपादित किया है। “न हि वरेण वेराणि सम्मन्तीध कदाचनं ।" - वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता। बुद्ध कहते हैं - उसने मुझे दुत्कारा, अपशब्द कहे, लूटा, त्रास दी - इन सबको सोचने वाला कषाय : क्रोध तत्त्व १०१ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17