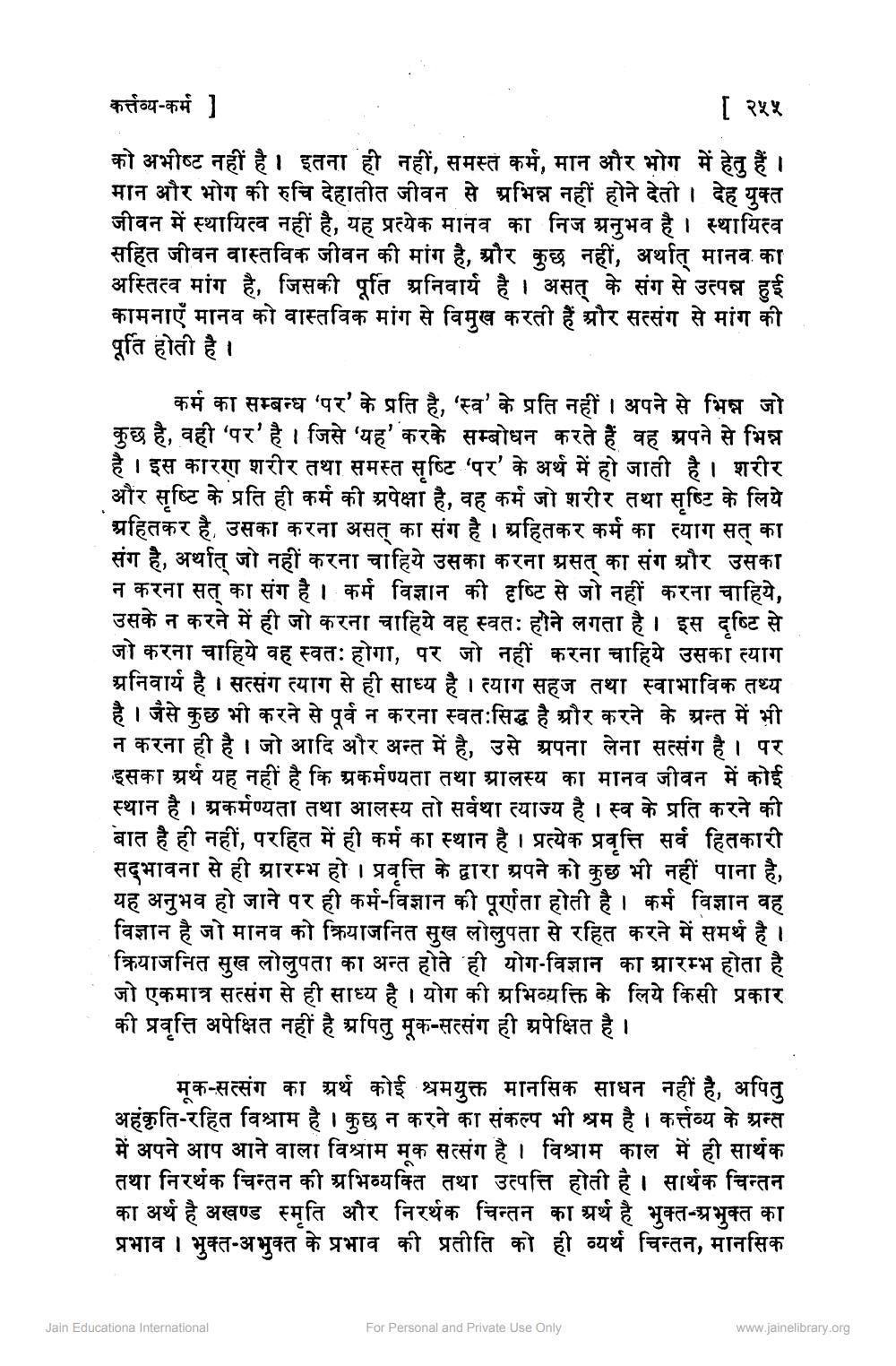Book Title: Karttavya Karm Author(s): Swami Sharnanand Publisher: Z_Jinvani_Karmsiddhant_Visheshank_003842.pdf View full book textPage 3
________________ कर्तव्य-कर्म ] [ २५५ को अभीष्ट नहीं है। इतना ही नहीं, समस्त कर्म, मान और भोग में हेतु हैं। मान और भोग की रुचि देहातीत जीवन से अभिन्न नहीं होने देती। देह युक्त जीवन में स्थायित्व नहीं है, यह प्रत्येक मानव का निज अनुभव है । स्थायित्व सहित जीवन वास्तविक जीवन की मांग है, और कुछ नहीं, अर्थात् मानव का अस्तित्व मांग है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य है । असत् के संग से उत्पन्न हुई कामनाएँ मानव को वास्तविक मांग से विमुख करती हैं और सत्संग से मांग की पूर्ति होती है। कर्म का सम्बन्ध 'पर' के प्रति है, 'स्व' के प्रति नहीं। अपने से भिन्न जो कुछ है, वही 'पर' है । जिसे 'यह' करके सम्बोधन करते हैं वह अपने से भिन्न है । इस कारण शरीर तथा समस्त सृष्टि 'पर' के अर्थ में हो जाती है। शरीर और सृष्टि के प्रति ही कर्म की अपेक्षा है, वह कर्म जो शरीर तथा सृष्टि के लिये अहितकर है, उसका करना असत् का संग है । अहितकर कर्म का त्याग सत् का संग है, अर्थात् जो नहीं करना चाहिये उसका करना असत् का संग और उसका न करना सत् का संग है। कर्म विज्ञान की दृष्टि से जो नहीं करना चाहिये, उसके न करने में ही जो करना चाहिये वह स्वतः होने लगता है। इस दष्टि से जो करना चाहिये वह स्वतः होगा, पर जो नहीं करना चाहिये उसका त्याग अनिवार्य है । सत्संग त्याग से ही साध्य है । त्याग सहज तथा स्वाभाविक तथ्य है । जैसे कुछ भी करने से पूर्व न करना स्वतःसिद्ध है और करने के अन्त में भी न करना ही है । जो आदि और अन्त में है, उसे अपना लेना सत्संग है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि अकर्मण्यता तथा आलस्य का मानव जीवन में कोई स्थान है । अकर्मण्यता तथा आलस्य तो सर्वथा त्याज्य है । स्व के प्रति करने की बात है ही नहीं, परहित में ही कर्म का स्थान है । प्रत्येक प्रवृत्ति सर्व हितकारी सद्भावना से ही प्रारम्भ हो । प्रवृत्ति के द्वारा अपने को कुछ भी नहीं पाना है, यह अनुभव हो जाने पर ही कर्म-विज्ञान की पूर्णता होती है। कर्म विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव को क्रियाजनित सुख लोलुपता से रहित करने में समर्थ है । क्रियाजनित सुख लोलुपता का अन्त होते ही योग-विज्ञान का प्रारम्भ होता है जो एकमात्र सत्संग से ही साध्य है । योग की अभिव्यक्ति के लिये किसी प्रकार की प्रवृत्ति अपेक्षित नहीं है अपितु मूक-सत्संग ही अपेक्षित है । मूक-सत्संग का अर्थ कोई श्रमयुक्त मानसिक साधन नहीं है, अपितु अहंकृति-रहित विश्राम है । कुछ न करने का संकल्प भी श्रम है । कर्त्तव्य के अन्त में अपने आप आने वाला विश्राम मक सत्संग है । विश्राम काल में ही सार्थक तथा निरर्थक चिन्तन की अभिव्यक्ति तथा उत्पत्ति होती है। सार्थक चिन्तन का अर्थ है अखण्ड स्मृति और निरर्थक चिन्तन का अर्थ है भुक्त-अभुक्त का प्रभाव । भुक्त-अभुक्त के प्रभाव की प्रतीति को ही व्यर्थ चिन्तन, मानसिक Jain Educationa International For Personal and Private Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5