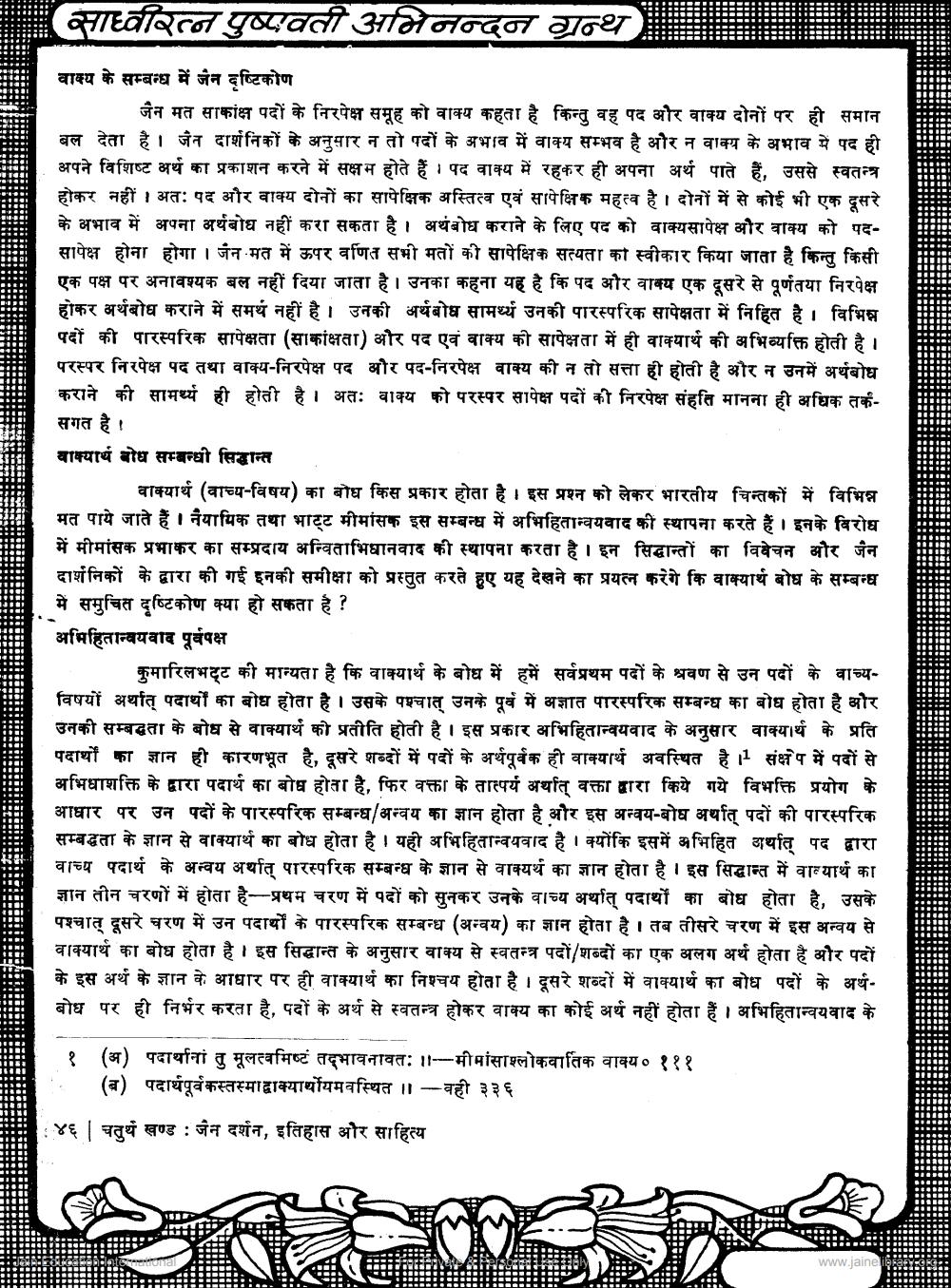Book Title: Jain Vakya Darshan Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Sadhviratna_Pushpvati_Abhinandan_Granth_012024.pdf View full book textPage 7
________________ साध्वीरत्न पुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ वाक्य के सम्बन्ध में जैन दृष्टिकोण जैन मत साकांक्ष पदों के निरपेक्ष समूह को वाक्य कहता है किन्तु वह पद और वाक्य दोनों पर ही समान बल देता है। जैन दार्शनिकों के अनुसार न तो पदों के अभाव में वाक्य सम्भव है और न वाक्य के अभाव में पद ही अपने विशिष्ट अर्थ का प्रकाशन करने में सक्षम होते हैं। पद वाक्य में रहकर ही अपना अर्थ पाते हैं, उससे स्वतन्त्र होकर नहीं । अतः पद और वाक्य दोनों का सापेक्षिक अस्तित्व एवं सापेक्षिक महत्व है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अभाव में अपना अर्थबोध नहीं करा सकता है । अर्थबोध कराने के लिए पद को वाक्यसापेक्ष और वाक्य को पदसापेक्ष होना होगा । जैन मत में ऊपर वर्णित सभी मतों की सापेक्षिक सत्यता को स्वीकार किया जाता है किन्तु किसी एक पक्ष पर अनावश्यक बल नहीं दिया जाता है। उनका कहना यह है कि पद और वाक्य एक दूसरे से पूर्णतया निरपेक्ष होकर अर्थबोध कराने में समर्थ नहीं है । उनकी अर्थबोध सामर्थ्यं उनकी पारस्परिक सापेक्षता में निहित है । विभिन्न पदों की पारस्परिक सापेक्षता ( साकांक्षता) और पद एवं वाक्य की सापेक्षता में ही वाक्यार्थ की अभिव्यक्ति होती है। परस्पर निरपेक्ष पद तथा वाक्य-निरपेक्ष पद और पद-निरपेक्ष वाक्य की न तो सत्ता ही होती है और न उनमें अर्थबोध कराने की सामर्थ्य ही होती है । अतः वाक्य को परस्पर सापेक्ष पदों की निरपेक्ष संहति मानना ही अधिक तर्कसगत है । वाक्यार्थ बोध सम्बन्धी सिद्धान्त वाक्यार्थ ( वाच्य विषय) का बोध किस प्रकार होता है। इस प्रश्न को लेकर भारतीय चिन्तकों में विभिन्न मत पाये जाते हैं। नैयायिक तथा भाट्ट मीमांसक इस सम्बन्ध में अभिहितान्वयवाद की स्थापना करते हैं। इनके विरोध में मीमांसक प्रभाकर का सम्प्रदाय अन्विताभिधानवाद की स्थापना करता है । इन सिद्धान्तों का विवेचन और जैन दार्शनिकों के द्वारा की गई इनकी समीक्षा को प्रस्तुत करते हुए यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि वाक्यार्थ बोध के सम्बन्ध में समुचित दृष्टिकोण क्या हो सकता है ? अभिहितान्वयवाद पूर्वपक्ष कुमारिलभट्ट की मान्यता है कि वाक्यार्थ के बोध में हमें सर्वप्रथम पदों के श्रवण से उन पदों के वाक्यविषयों अर्थात् पदार्थों का बोध होता है । उसके पश्चात् उनके पूर्व में अज्ञात पारस्परिक सम्बन्ध का बोध होता है और उनकी सम्बद्धता के बोध से वाक्यार्थ को प्रतीति होती है। इस प्रकार अभिहितान्वयवाद के अनुसार वाक्यार्थ के प्रति पदार्थों का ज्ञान ही कारणभूत है, दूसरे शब्दों में पदों के अर्थपूर्वक ही वाक्यार्थ अवस्थित है। संक्षेप में पदों से अभिधाशक्ति के द्वारा पदार्थ का बोध होता है, फिर वक्ता के तात्पर्य अर्थात् वक्ता द्वारा किये गये विभक्ति प्रयोग के आधार पर उन पदों के पारस्परिक सम्बन्ध / अन्वय का ज्ञान होता है और इस अन्वय-बोध अर्थात् पदों की पारस्परिक सम्बद्धता के ज्ञान से वाक्यार्थ का बोध होता है। यही अभिहितान्यववाद है क्योंकि इसमें अभिहित अर्थात् पद द्वारा वाच्य पदार्थ के अन्वय अर्थात् पारस्परिक सम्बन्ध के ज्ञान से वाक्यर्थ का ज्ञान होता है । इस सिद्धान्त में वाव्यार्थ का ज्ञान तीन चरणों में होता है--प्रथम चरण में पदों को सुनकर उनके वाच्य अर्थात् पदार्थों का बोध होता है, उसके पश्चात् दूसरे चरण में उन पदार्थों के पारस्परिक सम्बन्ध (अन्वय) का ज्ञान होता है । तब तीसरे चरण में इस अन्वय से वाक्यार्थ का बोध होता है। इस सिद्धान्त के अनुसार वाक्य से स्वतन्त्र पदों / शब्दों का एक अलग अर्थ होता है और पदों के इस अर्थ के ज्ञान के आधार पर ही वाक्यार्थ का निश्चय होता है । दूसरे शब्दों में वाक्यार्थ का बोध पदों के अर्थबोध पर ही निर्भर करता है, पदों के अर्थ से स्वतन्त्र होकर वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता हैं । अभिहितान्वयवाद के १ (अ) पदार्थानां तु मूलत्वमिष्टं तद्भावनावतः ॥ -- (ब) पदार्थ पूर्व कस्तस्माद्वाक्यार्थोयमनस्थित ।। - यही ३३६ ४६ | चतुर्थ खण्ड जैन दर्शन इतिहास और साहित्य 1: 1 Pellings Cational मीमांसाश्लोकवार्तिक वाक्य ० १११ Five & Ha www.jaine toranePage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12