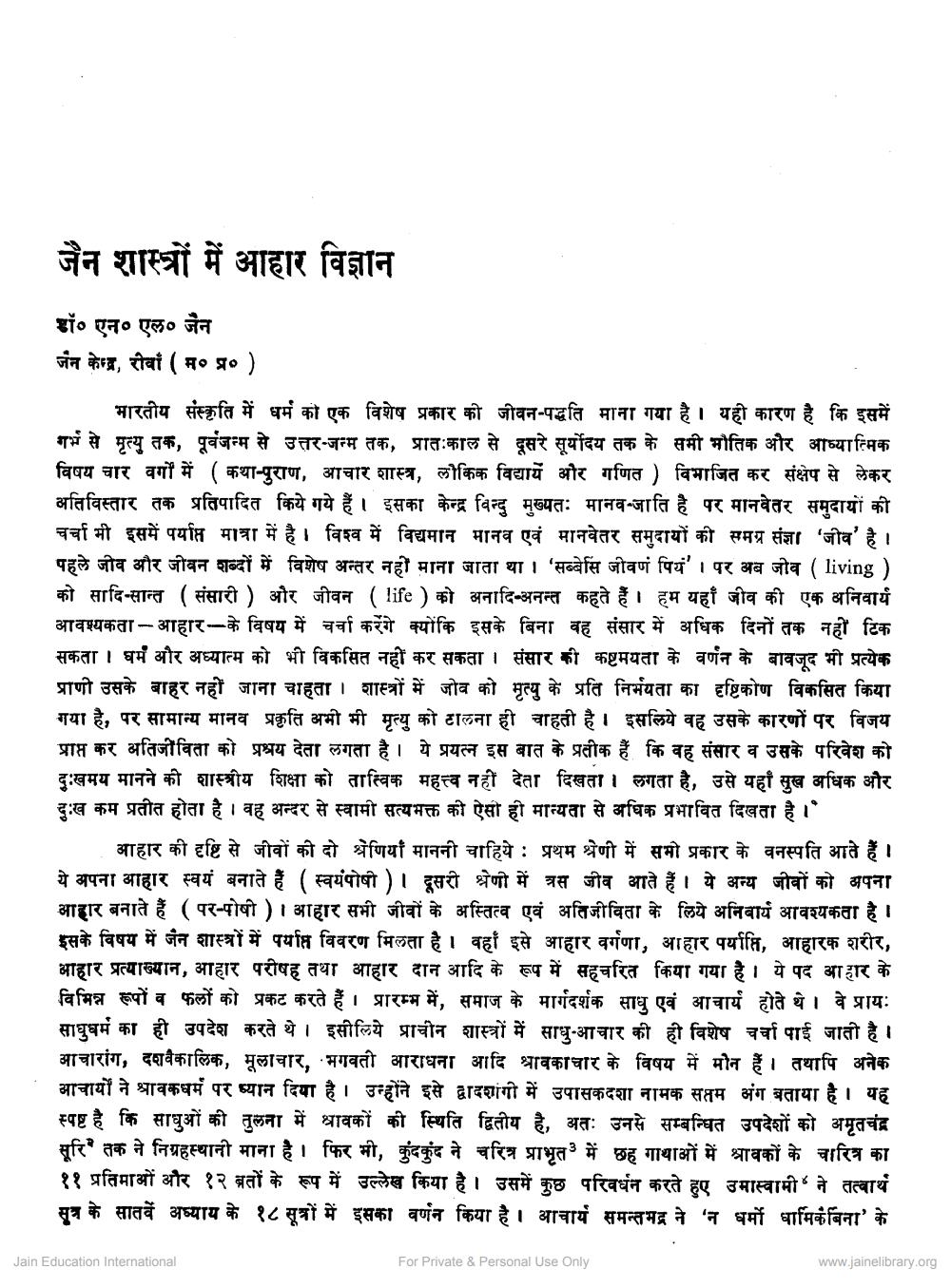Book Title: Jain Shastro me Ahar Vigyan Author(s): N L Jain Publisher: Z_Jaganmohanlal_Pandit_Sadhuwad_Granth_012026.pdf View full book textPage 1
________________ जैन शास्त्रों में आहार विज्ञान डॉ० एन० एल० जैन जंन केन्द्र, रीवां ( म०प्र०) ___ भारतीय संस्कृति में धर्म को एक विशेष प्रकार की जीवन-पद्धति माना गया है। यही कारण है कि इसमें गर्भ से मृत्यु तक, पूर्वजन्म से उत्तर-जन्म तक, प्रातःकाल से दूसरे सूर्योदय तक के समी भौतिक और आध्यात्मिक विषय चार वर्गों में ( कथा-पुराण, आचार शास्त्र, लौकिक विद्यायें और गणित ) विभाजित कर संक्षेप से लेकर अतिविस्तार तक प्रतिपादित किये गये हैं। इसका केन्द्र विन्दु मुख्यतः मानव-जाति है पर मानवेतर समुदायों की चर्चा भी इसमें पर्याप्त मात्रा में है। विश्व में विद्यमान मानव एवं मानवेतर समुदायों की समग्र संज्ञा 'जीव' है। पहले जीव और जीवन शब्दों में विशेष अन्तर नहीं माना जाता था । 'सब्बेसि जीवणं पियं' । पर अब जोव ( living ) को सादि-सान्त ( संसारी) और जीवन ( life ) को अनादि-अनन्त कहते हैं। हम यहाँ जीव की एक अनिवार्य आवश्यकता-आहार-के विषय में चर्चा करेंगे क्योंकि इसके बिना वह संसार में अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। धर्म और अध्यात्म को भी विकसित नहीं कर सकता। संसार की कष्टमयता के वर्णन के बावजूद भी प्रत्येक प्राणी उसके बाहर नहीं जाना चाहता। शास्त्रों में जोव को मृत्यु के प्रति निर्भयता का दृष्टिकोण विकसित किया गया है, पर सामान्य मानव प्रकृति अभी भी मृत्यु को टालना ही चाहती है। इसलिये वह उसके कारणों पर विजय प्राप्त कर अतिजीविता को प्रश्रय देता लगता है। ये प्रयत्न इस बात के प्रतीक हैं कि वह संसार व उसके परिवेश को दुःखमय मानने की शास्त्रीय शिक्षा को तात्विक महत्त्व नहीं देता दिखता। लगता है, उसे यहाँ सुख अधिक और दुःख कम प्रतीत होता है । वह अन्दर से स्वामी सत्यभक्त को ऐसी ही मान्यता से अधिक प्रभावित दिखता है।' आहार की दृष्टि से जीवों को दो श्रेणियां माननी चाहिये : प्रथम श्रेणी में सभी प्रकार के वनस्पति आते हैं। ये अपना आहार स्वयं बनाते हैं ( स्वयंपोषी)। दूसरी श्रेणी में त्रस जीव आते हैं । ये अन्य जीवों को अपना आहार बनाते हैं (पर-पोषी)। आहार सभी जीवों के अस्तित्व एवं अतिजीविता के लिये अनिवार्य आवश्यकता है । इसके विषय में जैन शास्त्रों में पर्याप्त विवरण मिलता है। वहाँ इसे आहार वर्गणा, आहार पर्याप्ति, आहारक शरीर, आहार प्रत्याख्यान, आहार परीषह तथा आहार दान आदि के रूप में सहचरित किया गया है। ये पद आहार के विभिन्न रूपों व फलों को प्रकट करते हैं। प्रारम्भ में, समाज के मार्गदर्शक साधू एवं आचार्य होते थे। वे प्रायः साधुधर्म का ही उपदेश करते थे। इसीलिये प्राचीन शास्त्रों में साधु-आचार की ही विशेष चर्चा पाई जाती है। आचारांग, दशवैकालिक, मूलाचार, भगवती आराधना आदि श्रावकाचार के विषय में मौन हैं। तथापि अनेक आचार्यों ने श्रावकधर्म पर ध्यान दिया है। उन्होंने इसे द्वादशांगी में उपासकदशा नामक सप्तम अंग बताया है। यह स्पष्ट है कि साधुओं की तुलना में श्रावकों की स्थिति द्वितीय है, अतः उनसे सम्बन्धित उपदेशों को अमृतचंद्र सूरि' तक ने निग्रहस्थानी माना है। फिर भी, कुंदकुंद ने चरित्र प्राभृत में छह गाथाओं में श्रावकों के चारित्र का ११ प्रतिमाओं और १२ ब्रतों के रूप में उल्लेख किया है। उसमें कुछ परिवर्धन करते हुए उमास्वामी ने तत्वार्थ सुत्र के सातवें अध्याय के १८ सूत्रों में इसका वर्णन किया है । आचार्य समन्तभद्र ने 'न धर्मो धार्मिकबिना' के Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12