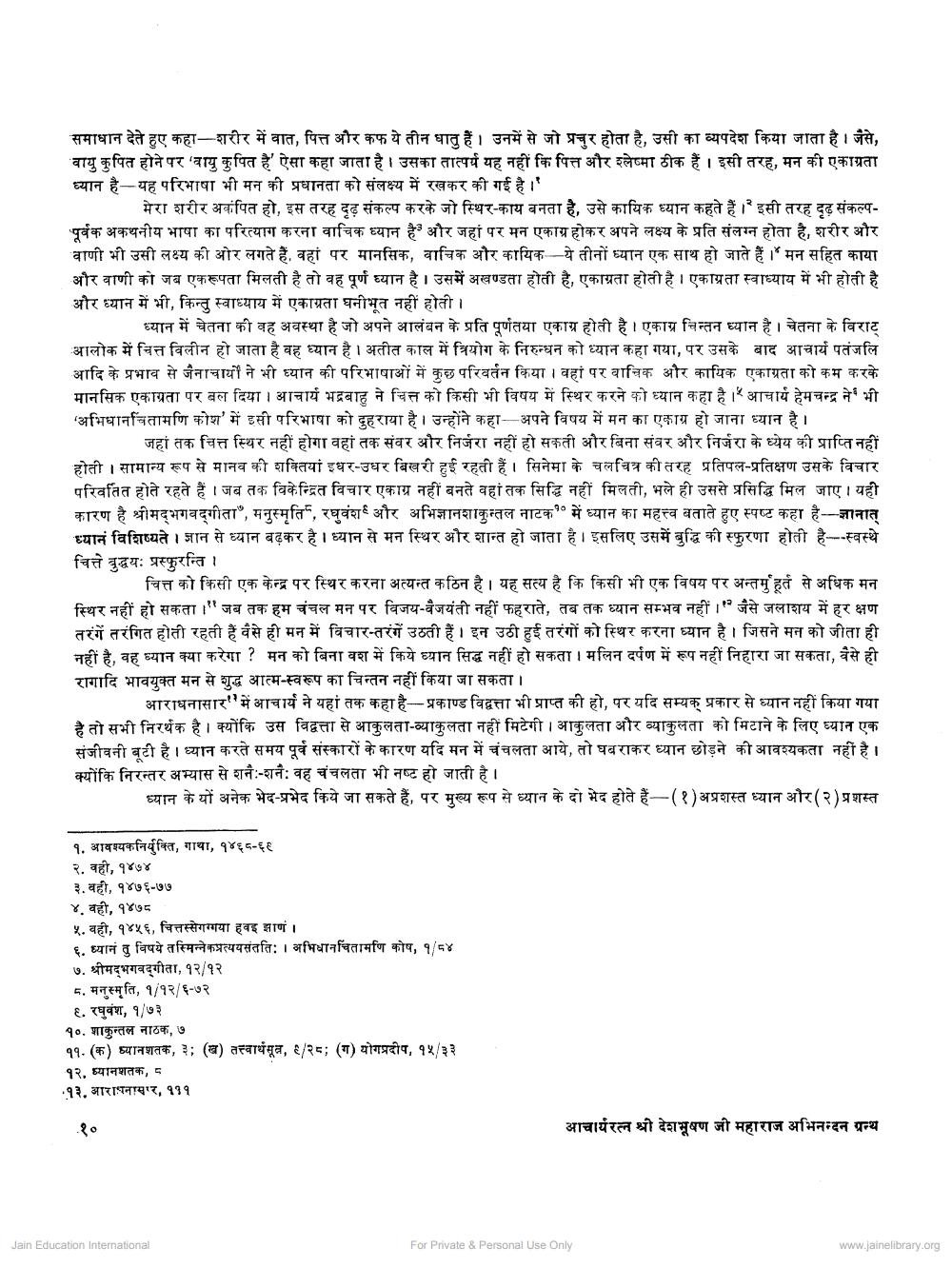Book Title: Jain Sadhna me Dhyan swarup aur Darshan Author(s): Devendramuni Shastri Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 2
________________ समाधान देते हुए कहा-शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीन धातु हैं। उनमें से जो प्रचुर होता है, उसी का व्यपदेश किया जाता है। जैसे, वायु कुपित होने पर 'वायु कुपित है ऐसा कहा जाता है। उसका तात्पर्य यह नहीं कि पित्त और श्लेष्मा ठीक हैं । इसी तरह, मन की एकाग्रता ध्यान है-यह परिभाषा भी मन की प्रधानता को संलक्ष्य में रखकर की गई है।' मेरा शरीर अकंपित हो, इस तरह दृढ़ संकल्प करके जो स्थिर-काय बनता है, उसे कायिक ध्यान कहते हैं। इसी तरह दृढ़ संकल्पपूर्वक अकथनीय भाषा का परित्याग करना वाचिक ध्यान है और जहां पर मन एकाग्र होकर अपने लक्ष्य के प्रति संलग्न होता है, शरीर और वाणी भी उसी लक्ष्य की ओर लगते हैं, वहां पर मानसिक, वाचिक और कायिक—ये तीनों ध्यान एक साथ हो जाते हैं। मन सहित काया और वाणी को जब एकरूपता मिलती है तो वह पूर्ण ध्यान है। उसमें अखण्डता होती है, एकाग्रता होती है । एकाग्रता स्वाध्याय में भी होती है और ध्यान में भी, किन्तु स्वाध्याय में एकाग्रता घनीभूत नहीं होती। ध्यान में चेतना की वह अवस्था है जो अपने आलंबन के प्रति पूर्णतया एकाग्र होती है। एकाग्र चिन्तन ध्यान है। चेतना के विराट आलोक में चित्त विलीन हो जाता है वह ध्यान है। अतीत काल में त्रियोग के निरुन्धन को ध्यान कहा गया, पर उसके बाद आचार्य पतंजलि आदि के प्रभाव से जैनाचार्यों ने भी ध्यान की परिभाषाओं में कुछ परिवर्तन किया। वहां पर वाचिक और कायिक एकाग्रता को कम करके मानसिक एकाग्रता पर बल दिया। आचार्य भद्रबाहु ने चित्त को किसी भी विषय में स्थिर करने को ध्यान कहा है। आचार्य हेमचन्द्र ने भी 'अभिधानचितामणि कोश' में इसी परिभाषा को दुहराया है। उन्होंने कहा-अपने विषय में मन का एकाग्र हो जाना ध्यान है। जहां तक चित्त स्थिर नहीं होगा वहां तक संवर और निर्जरा नहीं हो सकती और बिना संवर और निर्जरा के ध्येय की प्राप्ति नहीं होती। सामान्य रूप से मानव की शक्तियां इधर-उधर बिखरी हुई रहती हैं। सिनेमा के चलचित्र की तरह प्रतिपल-प्रतिक्षण उसके विचार परिवर्तित होते रहते हैं । जब तक विकेन्द्रित विचार एकाग्र नहीं बनते वहां तक सिद्धि नहीं मिलती, भले ही उससे प्रसिद्धि मिल जाए। यही कारण है श्रीमद्भगवद्गीता", मनुस्मृति , रघुवंश और अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक में ध्यान का महत्त्व बताते हुए स्पष्ट कहा है-ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते । ज्ञान से ध्यान बढ़कर है । ध्यान से मन स्थिर और शान्त हो जाता है। इसलिए उसमें बुद्धि की स्फुरणा होती है--स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति । चित्त को किसी एक केन्द्र पर स्थिर करना अत्यन्त कठिन है। यह सत्य है कि किसी भी एक विषय पर अन्तर्मुहूर्त से अधिक मन स्थिर नहीं हो सकता।" जब तक हम चंचल मन पर विजय-वैजयंती नहीं फहराते, तब तक ध्यान सम्भव नहीं।" जैसे जलाशय में हर क्षण तरंगें तरंगित होती रहती हैं वैसे ही मन में विचार-तरंगें उठती हैं। इन उठी हुई तरंगों को स्थिर करना ध्यान है। जिसने मन को जीता ही नहीं है, वह ध्यान क्या करेगा ? मन को बिना वश में किये ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता । मलिन दर्पण में रूप नहीं निहारा जा सकता, वैसे ही रागादि भावयुक्त मन से शुद्ध आत्म-स्वरूप का चिन्तन नहीं किया जा सकता। आराधनासार" में आचार्य ने यहां तक कहा है-प्रकाण्ड विद्वत्ता भी प्राप्त की हो, पर यदि सम्यक् प्रकार से ध्यान नहीं किया गया है तो सभी निरर्थक है। क्योंकि उस विद्वत्ता से आकुलता-व्याकुलता नहीं मिटेगी। आकुलता और व्याकुलता को मिटाने के लिए ध्यान एक संजीवनी बूटी है । ध्यान करते समय पूर्व संस्कारों के कारण यदि मन में चंचलता आये, तो घबराकर ध्यान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि निरन्तर अभ्यास से शनैः-शनै: वह चंचलता भी नष्ट हो जाती है। ध्यान के यों अनेक भेद-प्रभेद किये जा सकते हैं, पर मुख्य रूप से ध्यान के दो भेद होते हैं-(१) अप्रशस्त ध्यान और (२)प्रशस्त १. आवश्यकनियुक्ति, गाथा, १४६८-६६ २. वही, १४७४ ३. वही, १४७६-७७ ४. वही, १४७८ ५. वही, १४५६, चित्तस्सेगग्गया हवइ झाणं । ६. ध्यानं तु विषये तस्मिन्नेकप्रत्ययसततिः । अभिधानचिंतामणि कोष, १/८४ ७. श्रीमद्भगवद्गीता, १२/१२ ८. मनुस्मृति, १/१२/६-७२ ६. रघुवंश, १/७३ १०. शाकुन्तल नाठक,७ ११. (क) ध्यानशतक, ३; (ख) तत्त्वार्थसूत्र, ६/२८; (ग) योगप्रदीप, १५/३३ १२. ध्यानशतक,८ १३. आराधनासर, १११ -१० आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7