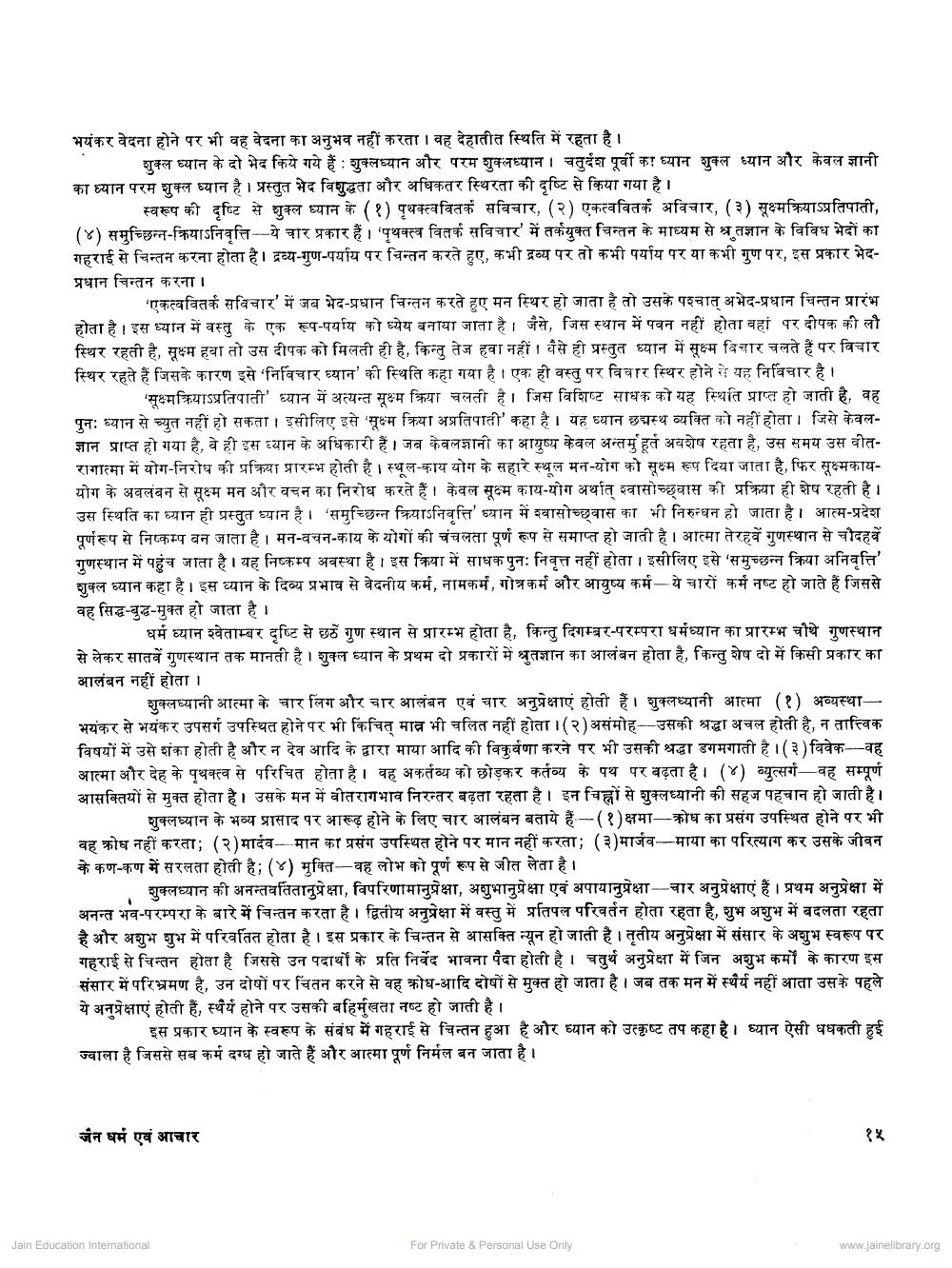Book Title: Jain Sadhna me Dhyan swarup aur Darshan Author(s): Devendramuni Shastri Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 7
________________ भयंकर वेदना होने पर भी वह वेदना का अनुभव नहीं करता / वह देहातीत स्थिति में रहता है। शुक्ल ध्यान के दो भेद किये गये हैं : शुक्लध्यान और परम शुक्लध्यान / चतुर्दश पूर्वी का ध्यान शुक्ल ध्यान और केवल ज्ञानी का ध्यान परम शुक्ल ध्यान है। प्रस्तुत भेद विशुद्धता और अधिकतर स्थिरता की दृष्टि से किया गया है। स्वरूप की दृष्टि से शुक्ल ध्यान के (1) पृथक्त्ववितर्क सविचार, (2) एकत्ववितर्क अविचार, (3) सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपाती, (4) समुच्छिन्न-क्रियाऽनिवृत्ति-ये चार प्रकार हैं। 'पृथक्त्व वितर्क सविचार' में तर्कयुक्त चिन्तन के माध्यम से श्र तज्ञान के विविध भेदों का गहराई से चिन्तन करना होता है। द्रव्य-गुण-पर्याय पर चिन्तन करते हुए, कभी द्रव्य पर तो कभी पर्याय पर या कभी गुण पर, इस प्रकार भेदप्रधान चिन्तन करना। 'एकत्ववितर्क सविचार' में जब भेद-प्रधान चिन्तन करते हुए मन स्थिर हो जाता है तो उसके पश्चात् अभेद-प्रधान चिन्तन प्रारंभ होता है। इस ध्यान में वस्तु के एक रूप-पर्याय को ध्येय बनाया जाता है। जैसे, जिस स्थान में पवन नहीं होता वहां पर दीपक की लौ स्थिर रहती है, सूक्ष्म हवा तो उस दीपक को मिलती ही है, किन्तु तेज हवा नहीं। वैसे ही प्रस्तुत ध्यान में सूक्ष्म विचार चलते हैं पर विचार स्थिर रहते हैं जिसके कारण इसे 'निर्विचार ध्यान' की स्थिति कहा गया है। एक ही वस्तु पर विचार स्थिर होने से यह निर्विचार है। 'सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपाती' ध्यान में अत्यन्त सूक्ष्म क्रिया चलती है। जिस विशिष्ट साधक को यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, वह पुनः ध्यान से च्युत नहीं हो सकता। इसीलिए इसे 'सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती' कहा है। यह ध्यान छद्मस्थ व्यक्ति को नहीं होता। जिसे केवलज्ञान प्राप्त हो गया है, वे ही इस ध्यान के अधिकारी हैं। जब केवलज्ञानी का आयुष्य केवल अन्तर्मुहूर्त अवशेष रहता है, उस समय उस बीतरागात्मा में योग-निरोध की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। स्थूल-काय योग के सहारे स्थूल मन-योग को सूक्ष्म रूप दिया जाता है, फिर सूक्ष्मकाययोग के अवलंबन से सूक्ष्म मन और बचन का निरोध करते हैं। केवल सूक्ष्म काय-योग अर्थात् श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया ही शेष रहती है। उस स्थिति का ध्यान ही प्रस्तुत ध्यान है। 'समुच्छिन्न क्रियाऽनिवृत्ति' ध्यान में श्वासोच्छ्वास का भी निरुन्धन हो जाता है। आत्म-प्रदेश पूर्णरूप से निष्कम्प बन जाता है। मन-वचन-काय के योगों की चंचलता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। आत्मा तेरहवें गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान में पहुंच जाता है। यह निष्कम्प अवस्था है। इस क्रिया में साधक पुनः निवृत्त नहीं होता। इसीलिए इसे 'समुच्छन्न क्रिया अनिवृत्ति' शुक्ल ध्यान कहा है। इस ध्यान के दिव्य प्रभाव से वेदनीय कर्म, नामकर्म, गोत्रकर्म और आयुष्य कर्म-ये चारों कर्म नष्ट हो जाते हैं जिससे वह सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाता है। धर्म ध्यान श्वेताम्बर दृष्टि से छठे गुण स्थान से प्रारम्भ होता है, किन्तु दिगम्बर-परम्परा धर्मध्यान का प्रारम्भ चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक मानती है / शुक्ल ध्यान के प्रथम दो प्रकारों में श्रुतज्ञान का आलंबन होता है, किन्तु शेष दो में किसी प्रकार का आलंबन नहीं होता। शुक्लध्यानी आत्मा के चार लिंग और चार आलंबन एवं चार अनुप्रेक्षाएं होती हैं। शुक्लध्यानी आत्मा (1) अव्यस्थाभयंकर से भयंकर उपसर्ग उपस्थित होने पर भी किंचित् मान भी चलित नहीं होता / (2) असंमोह-उसकी श्रद्धा अचल होती है, न तात्त्विक विषयों में उसे शंका होती है और न देव आदि के द्वारा माया आदि की विकुर्वणा करने पर भी उसकी श्रद्धा डगमगाती है / (3) विवेक-वह आत्मा और देह के पृथक्त्व से परिचित होता है। वह अकर्तव्य को छोड़कर कर्तव्य के पथ पर बढ़ता है। (4) व्युत्सर्ग—वह सम्पूर्ण आसक्तियों से मुक्त होता है। उसके मन में वीतरागभाव निरन्तर बढ़ता रहता है। इन चिह्नों से शुक्लध्यानी की सहज पहचान हो जाती है। शुक्लध्यान के भव्य प्रासाद पर आरूढ़ होने के लिए चार आलंबन बताये हैं-(१)क्षमा-क्रोध का प्रसंग उपस्थित होने पर भी वह क्रोध नहीं करता; (2) मार्दव-मान का प्रसंग उपस्थित होने पर मान नहीं करता; (३)मार्जव-माया का परित्याग कर उसके जीवन के कण-कण में सरलता होती है; (4) मुक्ति–वह लोभ को पूर्ण रूप से जीत लेता है। . शुक्लध्यान की अनन्तवर्तितानुप्रेक्षा, विपरिणामानुप्रेक्षा, अशुभानुप्रेक्षा एवं अपायानुप्रेक्षा-चार अनुप्रेक्षाएं हैं / प्रथम अनुप्रेक्षा में अनन्त भव-परम्परा के बारे में चिन्तन करता है। द्वितीय अनुप्रेक्षा में वस्तु में प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है, शुभ अशुभ में बदलता रहता है और अशुभ शुभ में परिवर्तित होता है / इस प्रकार के चिन्तन से आसक्ति न्यून हो जाती है / तृतीय अनुप्रेक्षा में संसार के अशुभ स्वरूप पर गहराई से चिन्तन होता है जिससे उन पदार्थों के प्रति निर्वेद भावना पैदा होती है। चतुर्थ अनुप्रेक्षा में जिन अशुभ कर्मों के कारण इस संसार में परिभ्रमण है, उन दोषों पर चिंतन करने से वह क्रोध-आदि दोषों से मुक्त हो जाता है / जब तक मन में स्थैर्य नहीं आता उसके पहले ये अनुप्रेक्षाएं होती हैं, स्थैर्य होने पर उसकी बहिर्मुखता नष्ट हो जाती है / ___इस प्रकार ध्यान के स्वरूप के संबंध में गहराई से चिन्तन हुआ है और ध्यान को उत्कृष्ट तप कहा है। ध्यान ऐसी धधकती हुई ज्वाला है जिससे सब कर्म दग्ध हो जाते हैं और आत्मा पूर्ण निर्मल बन जाता है। जैन धर्म एवं आचार Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7