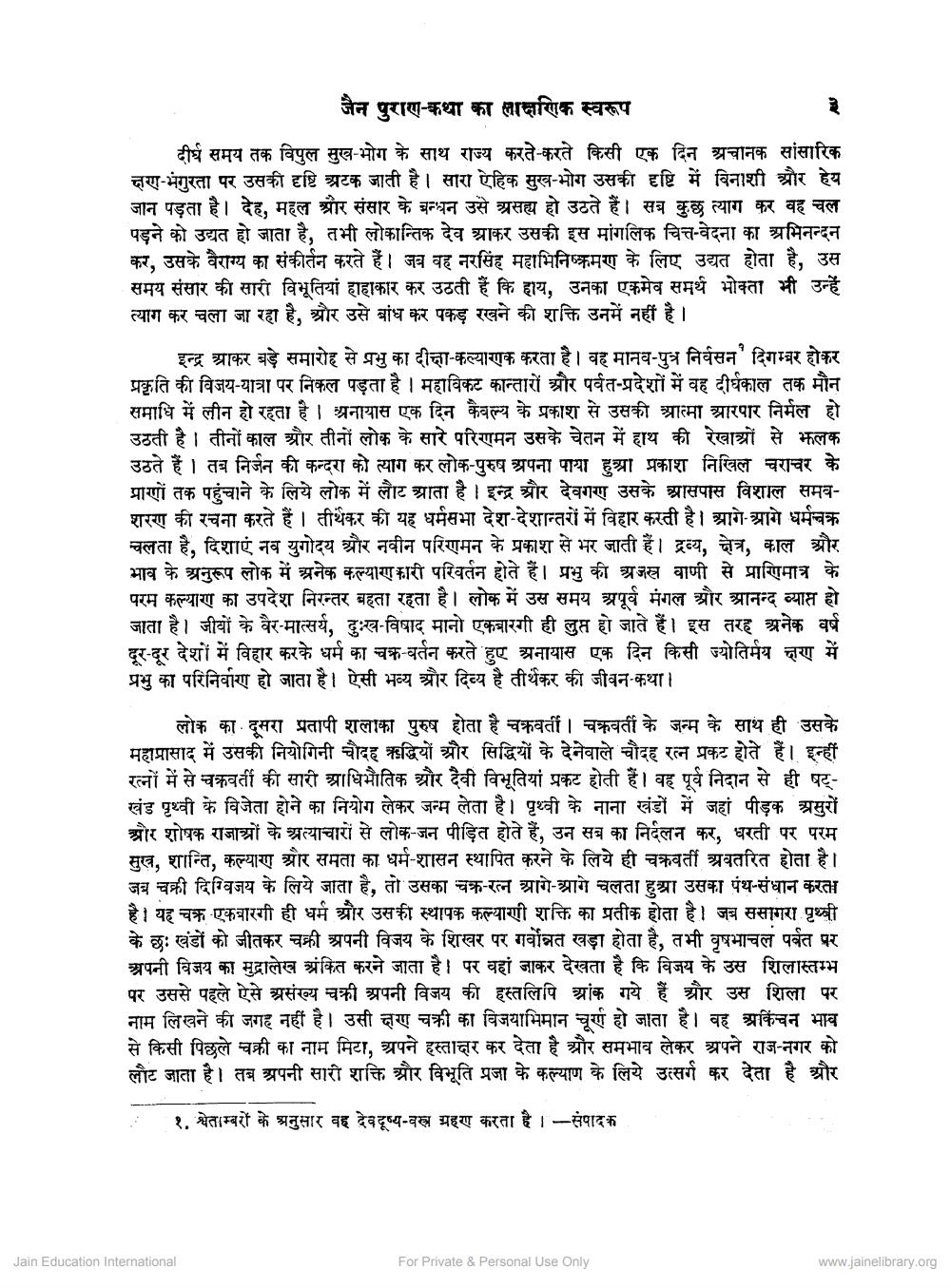Book Title: Jain Puran katha ka Lakshanik Swarup Author(s): Virendrakumar Jain Publisher: Z_Vijay_Vallabh_suri_Smarak_Granth_012060.pdf View full book textPage 3
________________ जैन पुराण-कथा का लाक्षणिक स्वरूप दीर्घ समय तक विपुल सुख-भोग के साथ राज्य करते-करते किसी एक दिन अचानक सांसारिक क्षण-भंगुरता पर उसकी दृष्टि अटक जाती है। सारा ऐहिक सुख-भोग उसकी दृष्टि में विनाशी और हेय जान पड़ता है। देह, महल और संसार के बन्धन उसे असह्य हो उठते हैं। सब कुछ त्याग कर वह चल पड़ने को उद्यत हो जाता है, तभी लोकान्तिक देव अाकर उसकी इस मांगलिक चित्त-वेदना का अभिनन्दन कर, उसके वैराग्य का संकीर्तन करते हैं। जब वह नरसिंह महाभिनिष्क्रमण के लिए उद्यत होता है, उस समय संसार की सारी विभूतियां हाहाकार कर उठती हैं कि हाय, उनका एकमेव समर्थ भोक्ता भी उन्हें त्याग कर चला जा रहा है, और उसे बांध कर पकड़ रखने की शक्ति उनमें नहीं है। इन्द्र श्राकर बड़े समारोह से प्रभु का दीक्षा-कल्याणक करता है। वह मानव-पुत्र निर्वसन' दिगम्बर होकर प्रकृति की विजय-यात्रा पर निकल पड़ता है। महाविकट कान्तारों और पर्वत-प्रदेशों में वह दीर्घकाल तक मौन समाधि में लीन हो रहता है। अनायास एक दिन कैवल्य के प्रकाश से उसकी श्रात्मा पारपार निर्मल हो उठती है। तीनों काल और तीनों लोक के सारे परिणमन उसके चेतन में हाथ की रेखाओं से झलक उठते हैं | तब निर्जन की कन्दरा को त्याग कर लोक-पुरुष अपना पाया हा प्रकाश निखिल चराचर के प्राणों तक पहुंचाने के लिये लोक में लौट पाता है। इन्द्र और देवगण उसके आसपास विशाल समवशरण की रचना करते हैं। तीर्थकर की यह धर्मसभा देश-देशान्तरों में विहार करती है। आगे-आगे धर्मचक्र चलता है, दिशाएं नव युगोदय और नवीन परिणमन के प्रकाश से भर जाती हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुरूप लोक में अनेक कल्याणकारी परिवर्तन होते हैं। प्रभु की अजस्र वाणी से प्राणिमात्र के परम कल्याण का उपदेश निरन्तर बहता रहता है। लोक में उस समय अपूर्व मंगल और आनन्द व्याप्त हो जाता है। जीवों के वैर-मात्सर्य, दुःख-विषाद मानो एकबारगी ही लुप्त हो जाते हैं। इस तरह अनेक वर्ष दूर-दूर देशों में विहार करके धर्म का चक्र-वर्तन करते हुए अनायास एक दिन किसी ज्योतिर्मय क्षण में प्रभु का परिनिर्वाण हो जाता है। ऐसी भव्य और दिव्य है तीर्थकर की जीवन-कथा। लोक का दूसरा प्रतापी शलाका पुरुष होता है चक्रवर्ती । चक्रवर्ती के जन्म के साथ ही उसके महाप्रासाद में उसकी नियोगिनी चौदह ऋद्धियों और सिद्धियों के देनेवाले चौदह रत्न प्रकट होते हैं। इन्हीं रत्नों में से चक्रवर्ती की सारी आधिभौतिक और दैवी विभूतियां प्रकट होती हैं। वह पूर्व निदान से ही षट्खंड पृथ्वी के विजेता होने का नियोग लेकर जन्म लेता है। पृथ्वी के नाना खंडों में जहां पीड़क असुरों और शोषक राजाओं के अत्याचारों से लोक-जन पीड़ित होते हैं, उन सब का निर्दलन कर, धरती पर परम सुख, शान्ति, कल्याण और समता का धर्म-शासन स्थापित करने के लिये ही चक्रवर्ती अवतरित होता है। जब चक्री दिग्विजय के लिये जाता है, तो उसका चक्र-रत्न आगे-आगे चलता हुआ उसका पंथ-संधान करता है। यह चक्र एकबारगी ही धर्म और उसकी स्थापक कल्याणी शक्ति का प्रतीक होता है। जब ससागरा पृथ्वी के छः खंडों को जीतकर चक्री अपनी विजय के शिखर पर गर्वोन्नत खड़ा होता है, तभी वृषभाचल पर्वत पर अपनी विजय का मुद्रालेख अंकित करने जाता है। पर वहां जाकर देखता है कि विजय के उस शिलास्तम्भ पर उससे पहले ऐसे असंख्य चक्री अपनी विजय की हस्तलिपि अांक गये हैं और उस शिला पर नाम लिखने की जगह नहीं है। उसी क्षण चक्री का विजयाभिमान चूर्ण हो जाता है। वह अकिंचन भाव से किसी पिछले चक्री का नाम मिटा, अपने हस्ताक्षर कर देता है और समभाव लेकर अपने राज-नगर को लौट जाता है। तब अपनी सारी शक्ति और विभूति प्रजा के कल्याण के लिये उत्सर्ग कर देता है और १. श्वेताम्बरों के अनुसार वह देवदूष्य-वस्त्र ग्रहण करता है । -संपादक Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5