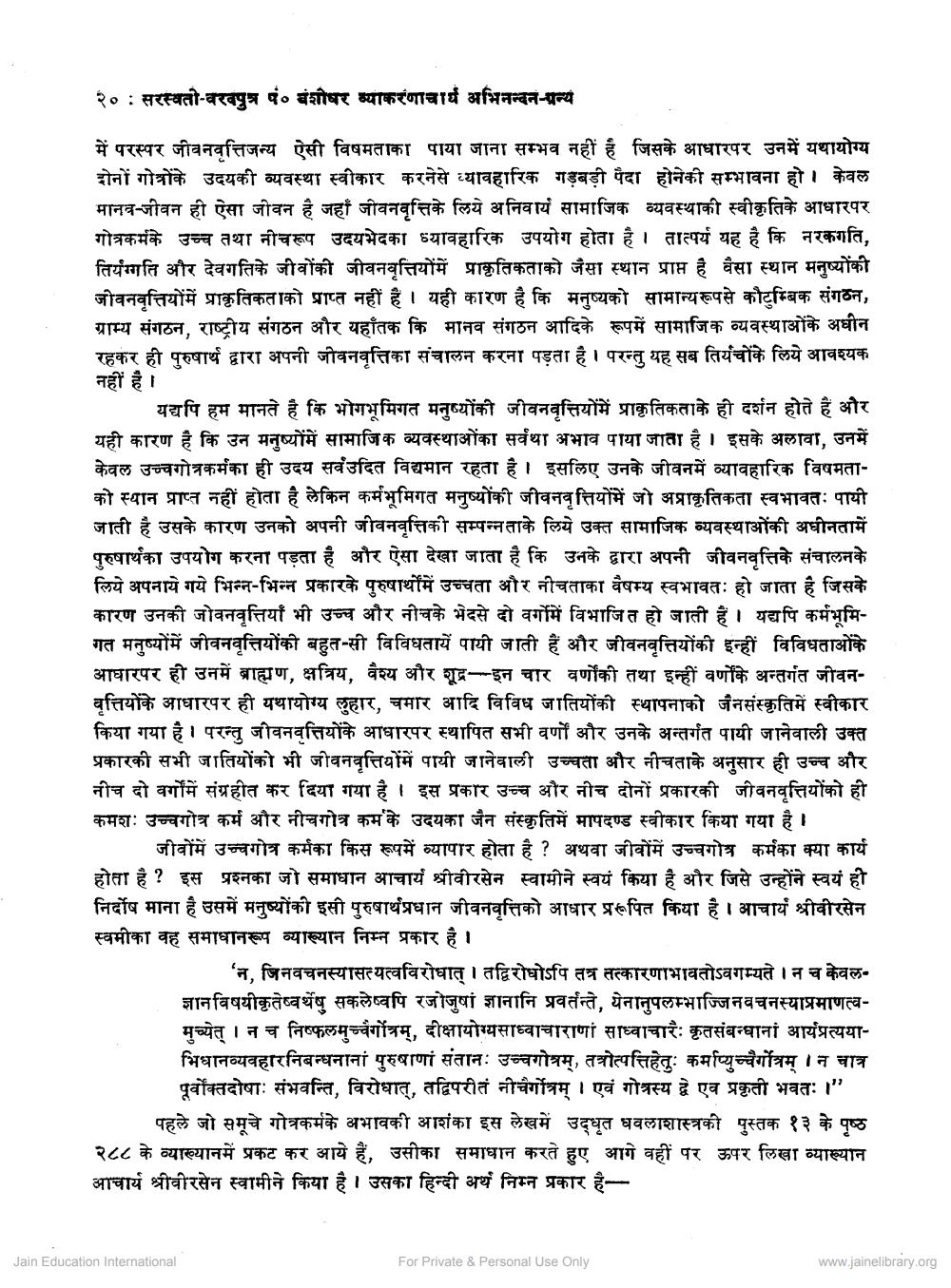Book Title: Jain Drushti se Manushyo me Uccha Niccha Vyavasthaka Adhar Author(s): Bansidhar Pandit Publisher: Z_Bansidhar_Pandit_Abhinandan_Granth_012047.pdf View full book textPage 6
________________ २० : सरस्वती - वरवपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन ग्रन्य में परस्पर जीवनवृत्तिजन्य ऐसी विषमताका पाया जाना सम्भव नहीं है जिसके आधारपर उनमें यथायोग्य दोनों गोत्रोंके उदयकी व्यवस्था स्वीकार करनेसे व्यावहारिक गड़बड़ी पैदा होनेकी सम्भावना हो । केवल मानव-जीवन ही ऐसा जीवन है जहाँ जीवनवृत्तिके लिये अनिवार्य सामाजिक व्यवस्थाकी स्वीकृति के आधारपर गोत्रकर्मके उच्च तथा नीचरूप उदयभेदका व्यावहारिक उपयोग होता है । तात्पर्य यह है कि नरकगति, तिर्यग्गति और देवगतिके जीवोंकी जीवनवृत्तियोंमें प्राकृतिकताको जैसा स्थान प्राप्त है वैसा स्थान मनुष्योंकी जीवनवृत्तियों में प्राकृतिकताको प्राप्त नहीं हैं । यही कारण है कि मनुष्यको सामान्यरूपसे कौटुम्बिक संगठन, ग्राम्य संगठन, राष्ट्रीय संगठन और यहाँतक कि मानव संगठन आदिके रूपमें सामाजिक व्यवस्थाओंके अधीन रहकर ही पुरुषार्थ द्वारा अपनी जीवनवृत्तिका संचालन करना पड़ता है । परन्तु यह सब तिर्यंचोंके लिये आवश्यक नहीं है । यद्यपि हम मानते है कि भोगभूमिगत मनुष्योंकी जीवनवृत्तियोंमें प्राकृतिकता के ही दर्शन होते हैं और यही कारण है कि उन मनुष्योंमें सामाजिक व्यवस्थाओंका सर्वथा अभाव पाया जाता है । इसके अलावा, उनमें केवल उच्चगोत्रकर्मका ही उदय सर्व उदित विद्यमान रहता है । इसलिए उनके जीवन में व्यावहारिक विषमताको स्थान प्राप्त नहीं होता है लेकिन कर्मभूमिगत मनुष्योंकी जीवनवृत्तियोंमें जो अप्राकृतिकता स्वभावतः पायी जाती है उसके कारण उनको अपनी जीवनवृत्तिकी सम्पन्नताके लिये उक्त सामाजिक व्यवस्थाओंकी अधीनता में पुरुषार्थका उपयोग करना पड़ता है और ऐसा देखा जाता है कि उनके द्वारा अपनी जीवनवृत्तिके संचालन के लिये अपनाये गये भिन्न-भिन्न प्रकारके पुरुषार्थों में उच्चता और नीचताका वैषम्य स्वभावतः हो जाता है जिसके कारण उनकी जोवनवृत्तियाँ भी उच्च और नीचके भेदसे दो वर्गोमें विभाजित हो जाती हैं । यद्यपि कर्मभूमिगत मनुष्यों में जीवनवृत्तियोंकी बहुत-सी विविधतायें पायी जाती हैं और जीवनवृत्तियोंकी इन्हीं विविधताओंके आधारपर ही उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र- इन चार वर्णोंकी तथा इन्हीं वर्णोंके अन्तर्गत जीवनवृत्तियों के आधारपर ही यथायोग्य लुहार, चमार आदि विविध जातियोंकी स्थापनाको जैनसंस्कृतिमें स्वीकार किया गया है । परन्तु जीवनवृत्तियोंके आधारपर स्थापित सभी वर्णों और उनके अन्तर्गत पायी जानेवाली उक्त प्रकारकी सभी जातियोंको भी जीवनवृत्तियों में पायी जानेवाली उच्चता और नीचताके अनुसार ही उच्च और नीच दो वर्गों में संग्रहीत कर दिया गया है । इस प्रकार उच्च और नीच दोनों प्रकारकी जीवनवृत्तियोंको ही कमशः उच्चगोत्र कर्म और नीचगोत्र कर्म के उदयका जैन संस्कृतिमें मापदण्ड स्वीकार किया गया है । जीवोंमें उच्चगोत्र कर्मका किस रूपमें व्यापार होता है ? अथवा जीवोंमें उच्चगोत्र कर्मका क्या कार्य होता है ? इस प्रश्नका जो समाधान आचार्य श्रीवीरसेन स्वामीने स्वयं किया है और जिसे उन्होंने स्वयं ही निर्दोष माना है उसमें मनुष्योंकी इसी पुरुषार्थप्रधान जीवनवृत्तिको आधार प्ररूपित किया है। आचार्य श्रीवीरसेन स्वमीका वह समाधानरूप व्याख्यान निम्न प्रकार है । 'न, जिनवचनस्यासत्यत्वविरोधात् । तद्विरोधोऽपि तत्र तत्कारणाभावतोऽवगम्यते । न च केवलज्ञान विषयीकृतेष्वर्थेषु सकलेष्वपि रजोजुषां ज्ञानानि प्रवर्तन्ते येनानुपलम्भाज्जिनवचनस्याप्रमाणत्वमुच्येत् । न च निष्फलमुच्चैर्गोत्रम्, दीक्षायोग्यसाध्वाचाराणां साध्वाचारैः कृतसंबन्धानां आर्यप्रत्ययाभिधानव्यवहारनिबन्धनानां पुरुषाणां संतानः उच्चगोत्रम्, तत्रोत्पत्तिहेतुः कर्माप्युच्चैर्गोत्रम् । न चात्र पूर्वोक्तदोषाः संभवन्ति, विरोधात्, तद्विपरीतं नीचैर्गोत्रम् । एवं गोत्रस्य द्वे एव प्रकृती भवतः । " पहले जो समूचे गोत्रकर्मके अभावकी आशंका इस लेखमें उद्धृत धवलाशास्त्रको पुस्तक १३ के पृष्ठ २८८ के व्याख्यानमें प्रकट कर आये हैं, उसीका समाधान करते हुए आगे वहीं पर ऊपर लिखा व्याख्यान आचार्य श्री वीरसेन स्वामीने किया है। उसका हिन्दी अर्थ निम्न प्रकार है Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11