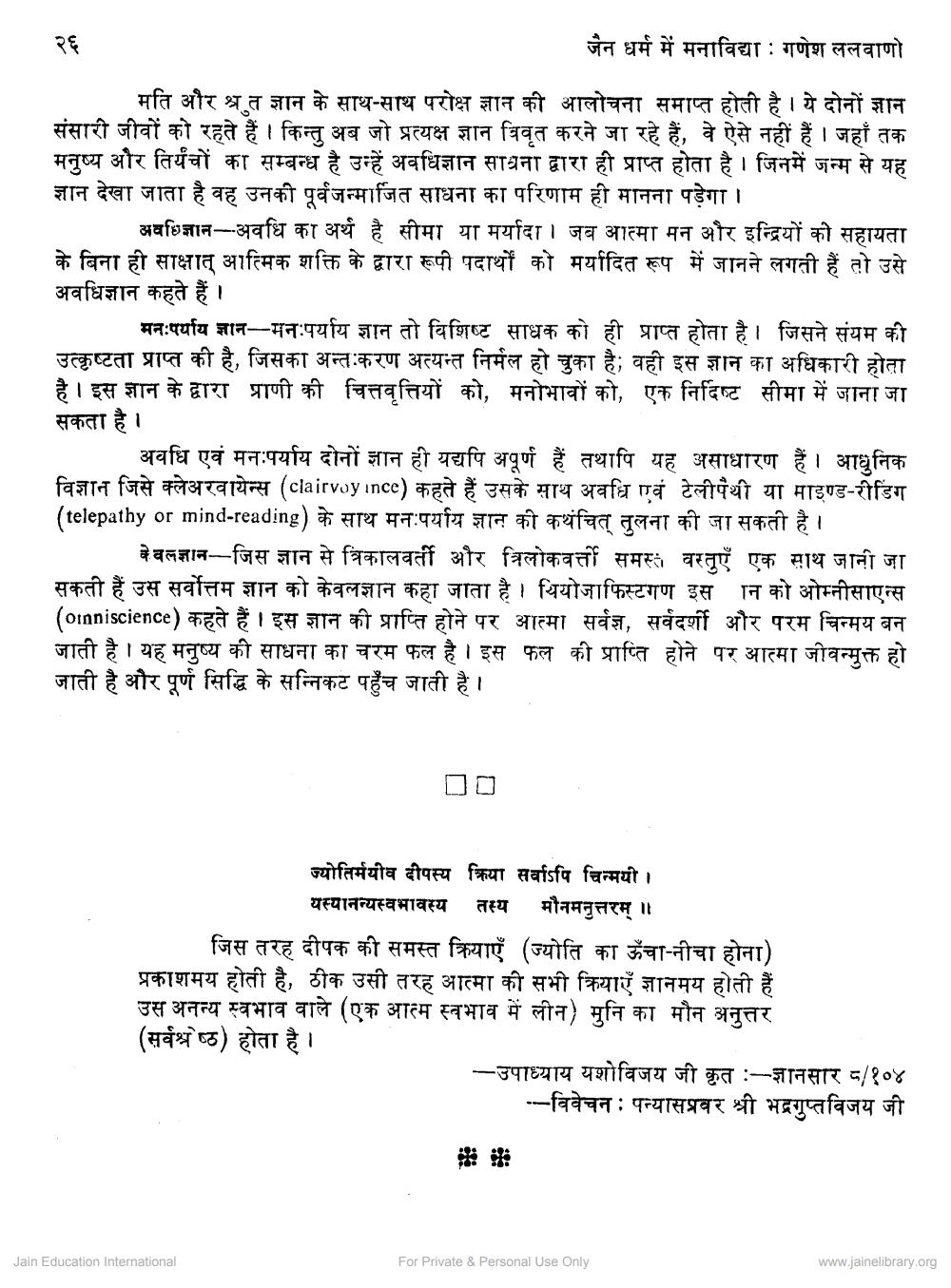Book Title: Jain Dharm me Manovidya Author(s): Ganesh Lalwani Publisher: Z_Sajjanshreeji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012028.pdf View full book textPage 7
________________ जैन धर्म में मनाविद्या : गणेश ललवाणो मति और श्र त ज्ञान के साथ-साथ परोक्ष ज्ञान की आलोचना समाप्त होती है / ये दोनों ज्ञान संसारी जीवों को रहते हैं / किन्तु अब जो प्रत्यक्ष ज्ञान विवृत करने जा रहे हैं, वे ऐसे नहीं हैं / जहाँ तक मनुष्य और तिर्यंचों का सम्बन्ध है उन्हें अवधिज्ञान साधना द्वारा ही प्राप्त होता है / जिनमें जन्म से यह ज्ञान देखा जाता है वह उनकी पूर्वजन्मार्जित साधना का परिणाम ही मानना पड़ेगा। अवधिज्ञान-अवधि का अर्थ है सीमा या मर्यादा। जब आत्मा मन और इन्द्रियों को सहायता के बिना ही साक्षात् आत्मिक शक्ति के द्वारा रूपी पदार्थों को मर्यादित रूप में जानने लगती हैं तो उसे अवधिज्ञान कहते हैं। मनःपर्याय ज्ञान-मनःपर्याय ज्ञान तो विशिष्ट साधक को ही प्राप्त होता है। जिसने संयम की उत्कृष्टता प्राप्त की है, जिसका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो चुका है। वही इस ज्ञान का अधिकारी होता है। इस ज्ञान के द्वारा प्राणी की चित्तवृत्तियों को, मनोभावों को, एक निर्दिष्ट सीमा में जाना जा सकता है। अवधि एवं मनःपर्याय दोनों ज्ञान ही यद्यपि अपूर्ण हैं तथापि यह असाधारण हैं। आधुनिक विज्ञान जिसे क्लेअरवायेन्स (clairvoy ince) कहते हैं उसके साथ अवधि एवं टेलीपैथी या माइण्ड-रीडिंग (telepathy or mind-reading) के साथ मनःपर्याय ज्ञान की कथंचित् तुलना की जा सकती है / केवलज्ञान-जिस ज्ञान से त्रिकालवर्ती और त्रिलोकवर्ती समस्त वस्तुएँ एक साथ जानी जा सकती हैं उस सर्वोत्तम ज्ञान को केवलज्ञान कहा जाता है। थियोजाफिस्टगण इस नि को ओम्नीसाएन्स (ornniscience) कहते हैं / इस ज्ञान की प्राप्ति होने पर आत्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और परम चिन्मय बन जाती है / यह मनुष्य की साधना का चरम फल है / इस फल की प्राप्ति होने पर आत्मा जीवन्मुक्त हो जाती है और पूर्ण सिद्धि के सन्निकट पहुँच जाती है। 10 ज्योतिर्मयीव दीपस्य क्रिया सर्वाऽपि चिन्मयी। यस्यानन्यस्वभावस्य तस्य मौनमनुत्तरम् // जिस तरह दीपक की समस्त क्रियाएँ (ज्योति का ऊँचा-नीचा होना) प्रकाशमय होती है, ठीक उसी तरह आत्मा की सभी क्रियाएँ ज्ञानमय होती हैं उस अनन्य स्वभाव वाले (एक आत्म स्वभाव में लीन) मुनि का मौन अनुत्तर (सर्वश्रेष्ठ) होता है। -उपाध्याय यशोविजय जी कृत :-ज्ञानसार 8/104 --विवेचन : पन्यासप्रवर श्री भद्रगुप्तविजय जी Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7