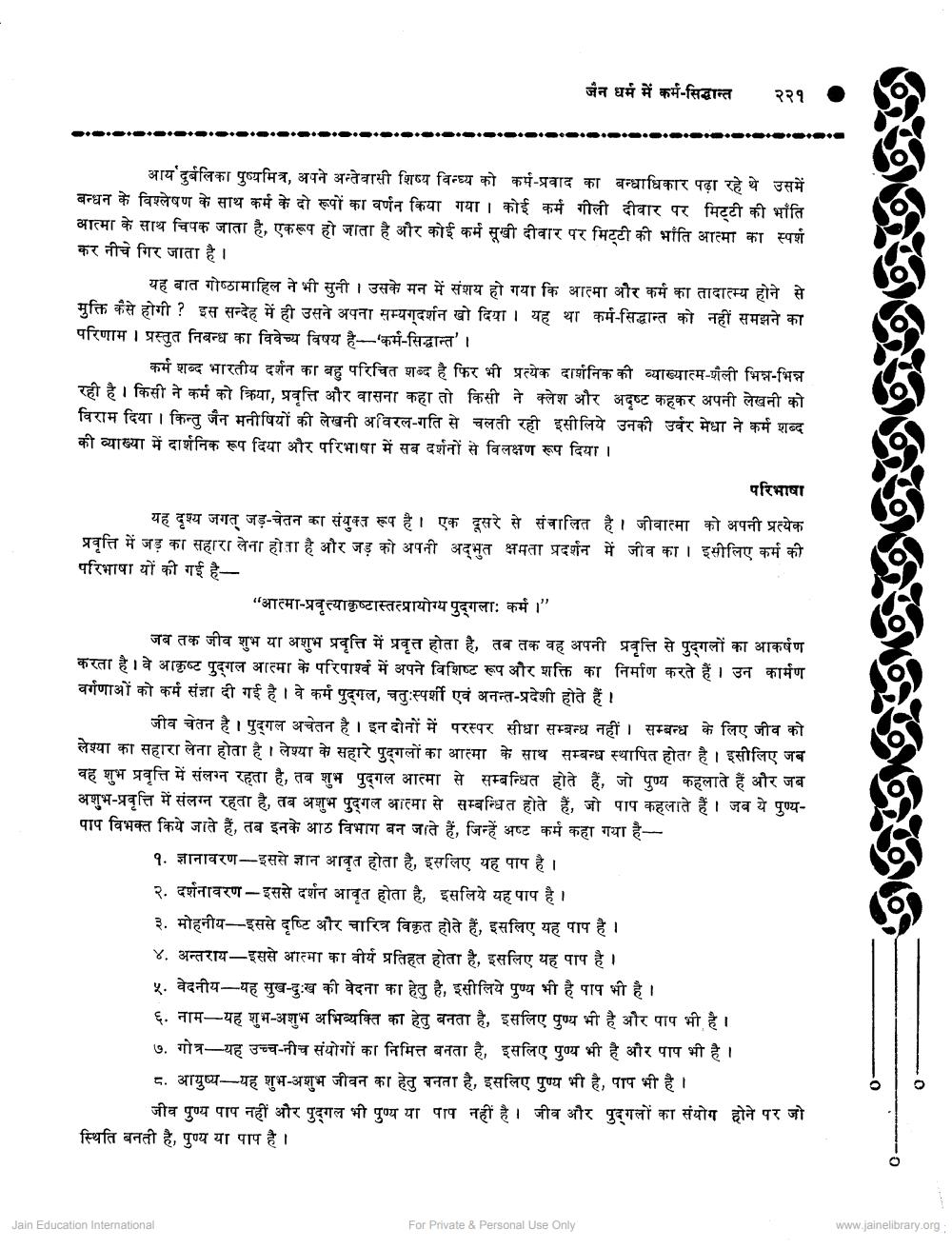Book Title: Jain Dharm me Karma Siddhant Author(s): Jatankumarishreeji Publisher: Z_Kesarimalji_Surana_Abhinandan_Granth_012044.pdf View full book textPage 2
________________ जैन धर्म में कर्म-सिद्धान्त २२१ आय दुर्बलिका पुष्यमित्र, अपने अन्तेवासी शिष्य विन्ध्य को कर्म-प्रवाद का बन्धाधिकार पढ़ा रहे थे उसमें बन्धन के विश्लेषण के साथ कर्म के दो रूपों का वर्णन किया गया। कोई कर्म गीली दीवार पर मिट्टी की भाँति आत्मा के साथ चिपक जाता है, एकरूप हो जाता है और कोई कर्म सूखी दीवार पर मिट्टी की भांति आत्मा का स्पर्श कर नीचे गिर जाता है। यह बात गोष्ठामाहिल ने भी सुनी । उसके मन में संशय हो गया कि आत्मा और कर्म का तादात्म्य होने से मुक्ति कैसे होगी? इस सन्देह में ही उसने अपना सम्यग्दर्शन खो दिया । यह था कर्म-सिद्धान्त को नहीं समझने का परिणाम । प्रस्तुत निबन्ध का विवेच्य विषय है-'कर्म-सिद्धान्त' । कर्म शब्द भारतीय दर्शन का बहु परिचित शब्द है फिर भी प्रत्येक दार्शनिक की व्याख्यात्म-शैली भिन्न-भिन्न रही है। किसी ने कर्म को क्रिया, प्रवृत्ति और वासना कहा तो किसी ने क्लेश और अदृष्ट कहकर अपनी लेखनी को विराम दिया। किन्तु जैन मनीषियों की लेखनी अविरल-गति से चलती रही इसीलिये उनकी उर्वर मेधा ने कर्म शब्द की व्याख्या में दार्शनिक रूप दिया और परिभाषा में सब दर्शनों से विलक्षण रूप दिया । परिभाषा यह दृश्य जगत् जड़-चेतन का संयुक्त रूप है। एक दूसरे से संचालित है। जीवात्मा को अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति में जड़ का सहारा लेना होता है और जड़ को अपनी अद्भुत क्षमता प्रदर्शन में जीव का । इसीलिए कर्म की परिभाषा यों की गई है "आत्मा-प्रवृत्त्याकृष्टास्तत्प्रायोग्य पुद्गलाः कर्म ।” जब तक जीव शुभ या अशुभ प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता है, तब तक वह अपनी प्रवृत्ति से पुद्गलों का आकर्षण करता है। वे आकृष्ट पुद्गल आत्मा के परिपार्श्व में अपने विशिष्ट रूप और शक्ति का निर्माण करते हैं। उन कार्मण वर्गणाओं को कर्म संज्ञा दी गई है। वे कर्म पुद्गल, चतुःस्पर्शी एवं अनन्त-प्रदेशी होते हैं। जीव चेतन है। पुद्गल अचेतन है। इन दोनों में परस्पर सीधा सम्बन्ध नहीं। सम्बन्ध के लिए जीव को लेश्या का सहारा लेना होता है । लेश्या के सहारे पुद्गलों का आत्मा के साथ सम्बन्ध स्थापित होता है। इसीलिए जब वह शुभ प्रवृत्ति में संलग्न रहता है, तब शुभ पुद्गल आत्मा से सम्बन्धित होते हैं, जो पुण्य कहलाते हैं और जब अशुभ-प्रवृत्ति में संलग्न रहता है, तब अशुभ पुद्गल आत्मा से सम्बन्धित होते हैं, जो पाप कहलाते हैं। जब ये पुण्यपाप विभक्त किये जाते हैं, तब इनके आठ विभाग बन जाते हैं, जिन्हें अष्ट कर्म कहा गया है १. ज्ञानावरण-इससे ज्ञान आवृत होता है, इसलिए यह पाप है। २. दर्शनावरण-इससे दर्शन आवृत होता है, इसलिये यह पाप है। ३. मोहनीय-इससे दृष्टि और चारित्र विकृत होते हैं, इसलिए यह पाप है। ४. अन्तराय-इससे आत्मा का वीर्य प्रतिहत होता है, इसलिए यह पाप है। ५. वेदनीय-यह सुख-दुःख की वेदना का हेतु है, इसीलिये पुण्य भी है पाप भी है। ६. नाम-यह शुभ-अशुभ अभिव्यक्ति का हेतु बनता है, इसलिए पुण्य भी है और पाप भी है। ७. गोत्र-यह उच्च-नीच संयोगों का निमित्त बनता है, इसलिए पुण्य भी है और पाप भी है। ८. आयुष्य-यह शुभ-अशुभ जीवन का हेतु बनता है, इसलिए पुण्य भी है, पाप भी है। जीव पुण्य पाप नहीं और पुद्गल भी पुण्य या पाप नहीं है। जीव और पुद्गलों का संयोग होने पर जो स्थिति बनती है, पुण्य या पाप है। - 0 Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org.Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7