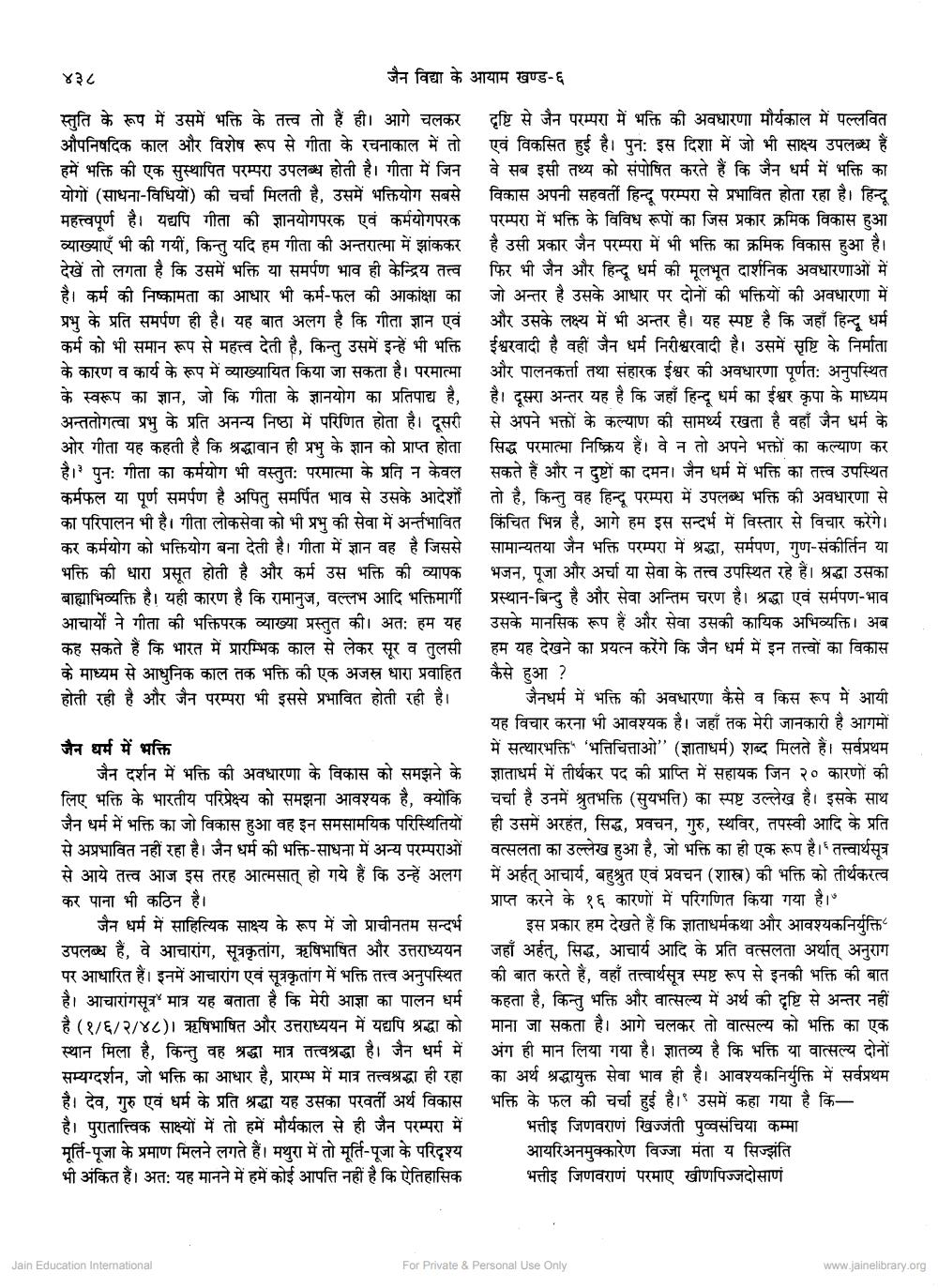Book Title: Jain Dharm me Bhakti ki Avadharna Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 3
________________ ४३८ स्तुति के रूप में उसमें भक्ति के तत्त्व तो हैं ही। आगे चलकर औपनिषदिक काल और विशेष रूप से गीता के रचनाकाल में तो हमें भक्ति की एक सुस्थापित परम्परा उपलब्ध होती है। गीता में जिन योगों (साधना-विधियों) की चर्चा मिलती है, उसमें भक्तियोग सबसे महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि गीता की ज्ञानयोगपरक एवं कर्मयोगपरक व्याख्याएँ भी की गयीं, किन्तु यदि हम गीता की अन्तरात्मा में झांककर देखें तो लगता है कि उसमें भक्ति या समर्पण भाव ही केन्द्रिय तत्त्व है। कर्म की निष्कामता का आधार भी कर्म फल की आकांक्षा का प्रभु के प्रति समर्पण ही है। यह बात अलग है कि गीता ज्ञान एवं कर्म को भी समान रूप से महत्व देती है, किन्तु उसमें इन्हें भी भक्ति के कारण व कार्य के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, जो कि गीता के ज्ञानयोग का प्रतिपाद्य है, अन्ततोगत्वा प्रभु के प्रति अनन्य निष्ठा में परिणित होता है। दूसरी ओर गीता यह कहती है कि श्रद्धावान ही प्रभु के ज्ञान को प्राप्त होता है । पुनः गीता का कर्मयोग भी वस्तुतः परमात्मा के प्रति न केवल कर्मफल या पूर्ण समर्पण है अपितु समर्पित भाव से उसके आदेशों का परिपालन भी है। गीता लोकसेवा को भी प्रभु की सेवा में अतभावित कर कर्मयोग को भक्तियोग बना देती है। गीता में ज्ञान वह है जिससे भक्ति की धारा प्रसूत होती है और कर्म उस भक्ति की व्यापक बाह्याभिव्यक्ति है। यही कारण है कि रामानुज, वल्लभ आदि भक्तिमार्गी आचार्यों ने गीता की भक्तिपरक व्याख्या प्रस्तुत की। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत में प्रारम्भिक काल से लेकर सूर व तुलसी के माध्यम से आधुनिक काल तक भक्ति की एक अजस्र धारा प्रवाहित होती रही है और जैन परम्परा भी इससे प्रभावित होती रही है। जैन विद्या के आयाम खण्ड ६ जैन धर्म में भक्ति जैन दर्शन में भक्ति की अवधारणा के विकास को समझने के लिए भक्ति के भारतीय परिप्रेक्ष्य को समझना आवश्यक है, क्योंकि जैन धर्म में भक्ति का जो विकास हुआ वह इन समसामयिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं रहा है। जैन धर्म की भक्ति-साधना में अन्य परम्पराओं से आये तत्त्व आज इस तरह आत्मसात हो गये हैं कि उन्हें अलग कर पाना भी कठिन है। जैन धर्म में साहित्यिक साक्ष्य के रूप में जो प्राचीनतम सन्दर्भ उपलब्ध हैं, वे आचारांग सूत्रकृतांग, ऋषिभाषित और उत्तराध्ययन पर आधारित हैं। इनमें आचारांग एवं सूत्रकृतांग में भक्ति तत्त्व अनुपस्थित है। आचारांगसूत्र' मात्र यह बताता है कि मेरी आज्ञा का पालन धर्म है (१/६/२/४८) । ऋषिभाषित और उत्तराध्ययन में यद्यपि श्रद्धा को स्थान मिला है, किन्तु वह श्रद्धा मात्र तत्त्वश्रद्धा है। जैन धर्म में सम्यग्दर्शन, जो भक्ति का आधार है, प्रारम्भ में मात्र तत्त्वश्रद्धा ही रहा है देव, गुरु एवं धर्म के प्रति श्रद्धा यह उसका परवर्ती अर्थ विकास है । पुरातात्त्विक साक्ष्यों में तो हमें मौर्यकाल से ही जैन परम्परा में मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलने लगते हैं। मथुरा में तो मूर्ति पूजा के परिदृश्य भी अंकित है। अतः यह मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है कि ऐतिहासिक Jain Education International दृष्टि से जैन परम्परा में भक्ति की अवधारणा मौर्यकाल में पल्लवित एवं विकसित हुई है। पुन: इस दिशा में जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं। वे सब इसी तथ्य को संपोषित करते हैं कि जैन धर्म में भक्ति का विकास अपनी सहवर्ती हिन्दू परम्परा से प्रभावित होता रहा है। हिन्दू परम्परा में भक्ति के विविध रूपों का जिस प्रकार क्रमिक विकास हुआ है उसी प्रकार जैन परम्परा में भी भक्ति का क्रमिक विकास हुआ है। फिर भी जैन और हिन्दू धर्म की मूलभूत दार्शनिक अवधारणाओं में जो अन्तर है उसके आधार पर दोनों की भक्तियों की अवधारणा में और उसके लक्ष्य में भी अन्तर है। यह स्पष्ट है कि जहाँ हिन्दू धर्म ईश्वरवादी है वहीं जैन धर्म निरीश्वरवादी है। उसमें सृष्टि के निर्माता और पालनकर्त्ता तथा संहारक ईश्वर की अवधारणा पूर्णतः अनुपस्थित है। दूसरा अन्तर यह है कि जहाँ हिन्दू धर्म का ईश्वर कृपा के माध्यम से अपने भक्तों के कल्याण की सामर्थ्य रखता है यहाँ जैन धर्म के सिद्ध परमात्मा निष्क्रिय हैं। वे न तो अपने भक्तों का कल्याण कर सकते हैं और न दुष्टों का दमन जैन धर्म में भक्ति का तत्त्व उपस्थित तो है, किन्तु वह हिन्दू परम्परा में उपलब्ध भक्ति की अवधारणा से किंचित भिन्न है, आगे हम इस सन्दर्भ में विस्तार से विचार करेंगे। सामान्यतया जैन भक्ति परम्परा में श्रद्धा, सर्मपण, गुण-संकीर्तिन या भजन, पूजा और अर्चा या सेवा के तत्त्व उपस्थित रहे हैं। श्रद्धा उसका प्रस्थानबिन्दु है और सेवा अन्तिम चरण है। श्रद्धा एवं सर्मपण भाव उसके मानसिक रूप हैं और सेवा उसकी कायिक अभिव्यक्ति । अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि जैन धर्म में इन तत्त्वों का विकास कैसे हुआ ? जैनधर्म में भक्ति की अवधारणा कैसे व किस रूप में आयी यह विचार करना भी आवश्यक है जहाँ तक मेरी जानकारी है आगमों में सत्यारभक्ति' 'भतिचित्ताओ" (ज्ञाताधर्म) शब्द मिलते हैं। सर्वप्रथम ज्ञाताधर्म में तीर्थकर पद की प्राप्ति में सहायक जिन २० कारणों की चर्चा है उनमें श्रुतभक्ति (सुयभत्ति) का स्पष्ट उल्लेख है। इसके साथ ही उसमें अरहंत, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थविर, तपस्वी आदि के प्रति वत्सलता का उल्लेख हुआ है, जो भक्ति का ही एक रूप है । तत्त्वार्थ सूत्र में अर्हत् आचार्य, बहुश्रुत एवं प्रवचन (शास्त्र) की भक्ति को तीर्थंकरत्व प्राप्त करने के १६ कारणों में परिगणित किया गया है।" इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञाताधर्मकथा और आवश्यकनिर्युक्ति जहाँ अर्हतु, सिद्ध, आचार्य आदि के प्रति वत्सलता अर्थात् अनुराग की बात करते हैं, वहाँ तत्त्वार्थसूत्र स्पष्ट रूप से इनकी भक्ति की बात कहता है, किन्तु भक्ति और वात्सल्य में अर्थ की दृष्टि से अन्तर नहीं माना जा सकता है। आगे चलकर तो वात्सल्य को भक्ति का एक अंग ही मान लिया गया है। ज्ञातव्य है कि भक्ति या वात्सल्य दोनों का अर्थ श्रद्धायुक्त सेवा भाव ही है। आवश्यकनियुक्ति में सर्वप्रथम भक्ति के फल की चर्चा हुई है।" उसमें कहा गया है किभत्तीइ जिणवराणं खिज्जंती पुव्वसंचिया कम्मा आयरिअनमुक्कारेण विज्जा मंता य सिज्झति भत्तीइ जिणवराणं परमाएखीणपिज्जदोसाणं For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org.Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10