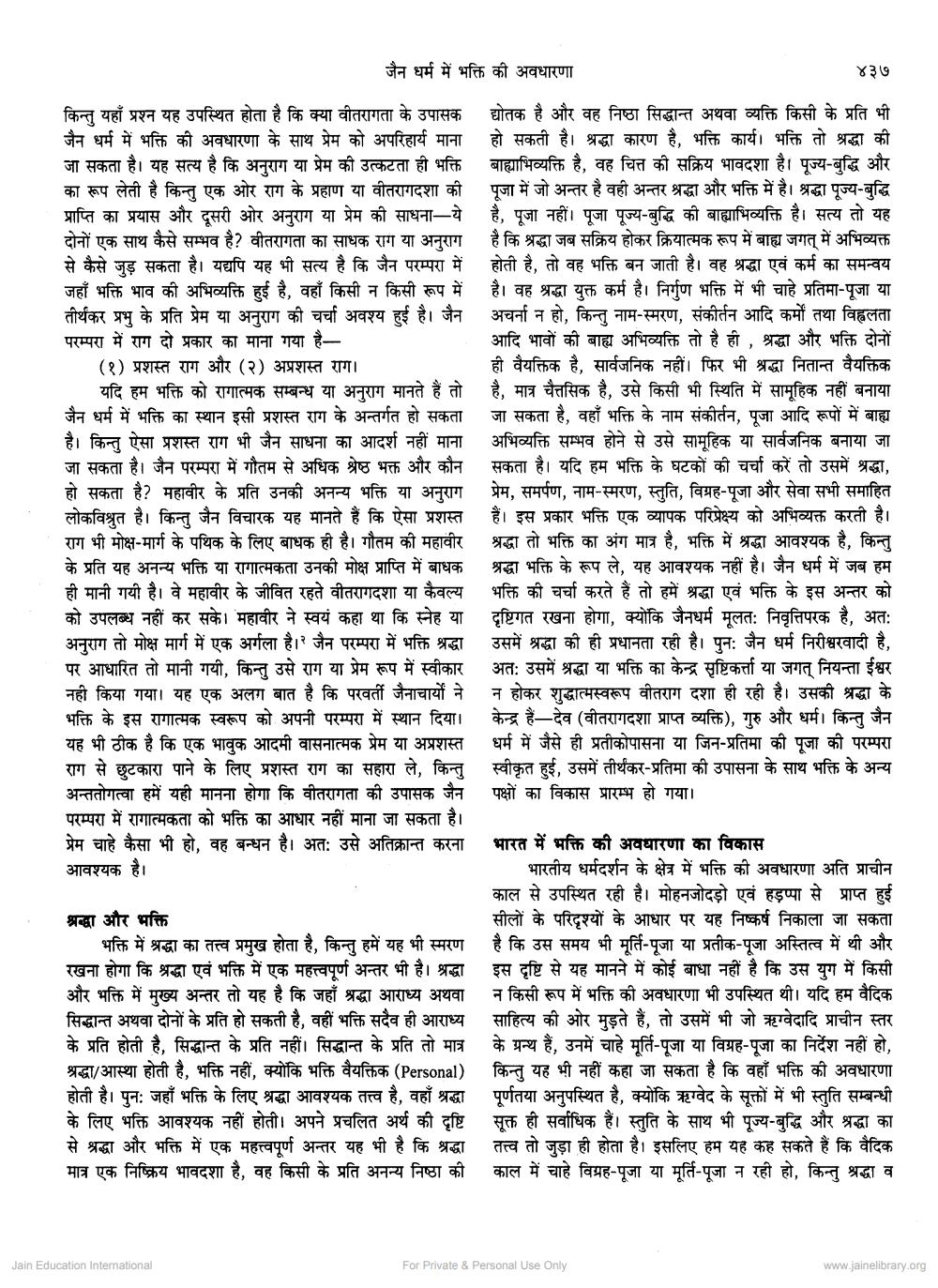Book Title: Jain Dharm me Bhakti ki Avadharna Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 2
________________ जैन धर्म में भक्ति की अवधारणा ४३७ किन्तु यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या वीतरागता के उपासक द्योतक है और वह निष्ठा सिद्धान्त अथवा व्यक्ति किसी के प्रति भी जैन धर्म में भक्ति की अवधारणा के साथ प्रेम को अपरिहार्य माना हो सकती है। श्रद्धा कारण है, भक्ति कार्य। भक्ति तो श्रद्धा की जा सकता है। यह सत्य है कि अनुराग या प्रेम की उत्कटता ही भक्ति बाह्याभिव्यक्ति है, वह चित्त की सक्रिय भावदशा है। पूज्य-बुद्धि और का रूप लेती है किन्तु एक ओर राग के प्रहाण या वीतरागदशा की पूजा में जो अन्तर है वही अन्तर श्रद्धा और भक्ति में है। श्रद्धा पूज्य-बुद्धि प्राप्ति का प्रयास और दूसरी ओर अनुराग या प्रेम की साधना—ये है, पूजा नहीं। पूजा पूज्य-बुद्धि की बाह्याभिव्यक्ति है। सत्य तो यह दोनों एक साथ कैसे सम्भव है? वीतरागता का साधक राग या अनुराग है कि श्रद्धा जब सक्रिय होकर क्रियात्मक रूप में बाह्य जगत् में अभिव्यक्त से कैसे जुड़ सकता है। यद्यपि यह भी सत्य है कि जैन परम्परा में होती है, तो वह भक्ति बन जाती है। वह श्रद्धा एवं कर्म का समन्वय जहाँ भक्ति भाव की अभिव्यक्ति हुई है, वहाँ किसी न किसी रूप में है। वह श्रद्धा युक्त कर्म है। निर्गुण भक्ति में भी चाहे प्रतिमा-पूजा या तीर्थकर प्रभु के प्रति प्रेम या अनुराग की चर्चा अवश्य हुई है। जैन अचर्ना न हो, किन्तु नाम-स्मरण, संकीर्तन आदि कर्मों तथा विह्वलता परम्परा में राग दो प्रकार का माना गया है आदि भावों की बाह्य अभिव्यक्ति तो है ही , श्रद्धा और भक्ति दोनों (१) प्रशस्त राग और (२) अप्रशस्त राग। ही वैयक्तिक है, सार्वजनिक नहीं। फिर भी श्रद्धा नितान्त वैयक्तिक यदि हम भक्ति को रागात्मक सम्बन्ध या अनुराग मानते हैं तो है, मात्र चैत्तसिक है, उसे किसी भी स्थिति में सामूहिक नहीं बनाया जैन धर्म में भक्ति का स्थान इसी प्रशस्त राग के अन्तर्गत हो सकता जा सकता है, वहाँ भक्ति के नाम संकीर्तन, पूजा आदि रूपों में बाह्य है। किन्तु ऐसा प्रशस्त राग भी जैन साधना का आदर्श नहीं माना अभिव्यक्ति सम्भव होने से उसे सामूहिक या सार्वजनिक बनाया जा जा सकता है। जैन परम्परा में गौतम से अधिक श्रेष्ठ भक्त और कौन सकता है। यदि हम भक्ति के घटकों की चर्चा करें तो उसमें श्रद्धा, हो सकता है? महावीर के प्रति उनकी अनन्य भक्ति या अनुराग प्रेम, समर्पण, नाम-स्मरण, स्तुति, विग्रह-पूजा और सेवा सभी समाहित लोकविश्रुत है। किन्तु जैन विचारक यह मानते हैं कि ऐसा प्रशस्त हैं। इस प्रकार भक्ति एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को अभिव्यक्त करती है। राग भी मोक्ष-मार्ग के पथिक के लिए बाधक ही है। गौतम की महावीर श्रद्धा तो भक्ति का अंग मात्र है, भक्ति में श्रद्धा आवश्यक है, किन्तु के प्रति यह अनन्य भक्ति या रागात्मकता उनकी मोक्ष प्राप्ति में बाधक श्रद्धा भक्ति के रूप ले, यह आवश्यक नहीं है। जैन धर्म में जब हम ही मानी गयी है। वे महावीर के जीवित रहते वीतरागदशा या कैवल्य भक्ति की चर्चा करते हैं तो हमें श्रद्धा एवं भक्ति के इस अन्तर को को उपलब्ध नहीं कर सके। महावीर ने स्वयं कहा था कि स्नेह या दृष्टिगत रखना होगा, क्योंकि जैनधर्म मूलत: निवृत्तिपरक है, अत: अनुराग तो मोक्ष मार्ग में एक अर्गला है। जैन परम्परा में भक्ति श्रद्धा उसमें श्रद्धा की ही प्रधानता रही है। पुन: जैन धर्म निरीश्वरवादी है, पर आधारित तो मानी गयी, किन्तु उसे राग या प्रेम रूप में स्वीकार अत: उसमें श्रद्धा या भक्ति का केन्द्र सृष्टिकर्ता या जगत् नियन्ता ईश्वर नही किया गया। यह एक अलग बात है कि परवर्ती जैनाचार्यों ने न होकर शुद्धात्मस्वरूप वीतराग दशा ही रही है। उसकी श्रद्धा के भक्ति के इस रागात्मक स्वरूप को अपनी परम्परा में स्थान दिया। केन्द्र हैं—देव (वीतरागदशा प्राप्त व्यक्ति), गुरु और धर्म। किन्तु जैन यह भी ठीक है कि एक भावुक आदमी वासनात्मक प्रेम या अप्रशस्त धर्म में जैसे ही प्रतीकोपासना या जिन-प्रतिमा की पूजा की परम्परा राग से छुटकारा पाने के लिए प्रशस्त राग का सहारा ले, किन्तु स्वीकृत हुई, उसमें तीर्थकर-प्रतिमा की उपासना के साथ भक्ति के अन्य अन्ततोगत्वा हमें यही मानना होगा कि वीतरागता की उपासक जैन पक्षों का विकास प्रारम्भ हो गया। परम्परा में रागात्मकता को भक्ति का आधार नहीं माना जा सकता है। प्रेम चाहे कैसा भी हो, वह बन्धन है। अत: उसे अतिक्रान्त करना भारत में भक्ति की अवधारणा का विकास आवश्यक है। भारतीय धर्मदर्शन के क्षेत्र में भक्ति की अवधारणा अति प्राचीन काल से उपस्थित रही है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त हुई श्रद्धा और भक्ति सीलों के परिदृश्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता भक्ति में श्रद्धा का तत्त्व प्रमुख होता है, किन्तु हमें यह भी स्मरण है कि उस समय भी मूर्ति-पूजा या प्रतीक-पूजा अस्तित्व में थी और रखना होगा कि श्रद्धा एवं भक्ति में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर भी है। श्रद्धा इस दृष्टि से यह मानने में कोई बाधा नहीं है कि उस युग में किसी और भक्ति में मुख्य अन्तर तो यह है कि जहाँ श्रद्धा आराध्य अथवा न किसी रूप में भक्ति की अवधारणा भी उपस्थित थी। यदि हम वैदिक सिद्धान्त अथवा दोनों के प्रति हो सकती है, वहीं भक्ति सदैव ही आराध्य साहित्य की ओर मुड़ते हैं, तो उसमें भी जो ऋग्वेदादि प्राचीन स्तर के प्रति होती है, सिद्धान्त के प्रति नहीं। सिद्धान्त के प्रति तो मात्र के ग्रन्थ हैं, उनमें चाहे मूर्ति-पूजा या विग्रह-पूजा का निर्देश नहीं हो, श्रद्धा/आस्था होती है, भक्ति नहीं, क्योंकि भक्ति वैयक्तिक (Personal) किन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ भक्ति की अवधारणा होती है। पुन: जहाँ भक्ति के लिए श्रद्धा आवश्यक तत्त्व है, वहाँ श्रद्धा पूर्णतया अनुपस्थित है, क्योंकि ऋग्वेद के सूक्तों में भी स्तुति सम्बन्धी के लिए भक्ति आवश्यक नहीं होती। अपने प्रचलित अर्थ की दृष्टि सूक्त ही सर्वाधिक हैं। स्तुति के साथ भी पूज्य-बुद्धि और श्रद्धा का से श्रद्धा और भक्ति में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह भी है कि श्रद्धा तत्त्व तो जुड़ा ही होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वैदिक मात्र एक निष्क्रिय भावदशा है, वह किसी के प्रति अनन्य निष्ठा की काल में चाहे विग्रह-पूजा या मूर्ति-पूजा न रही हो, किन्तु श्रद्धा व Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10