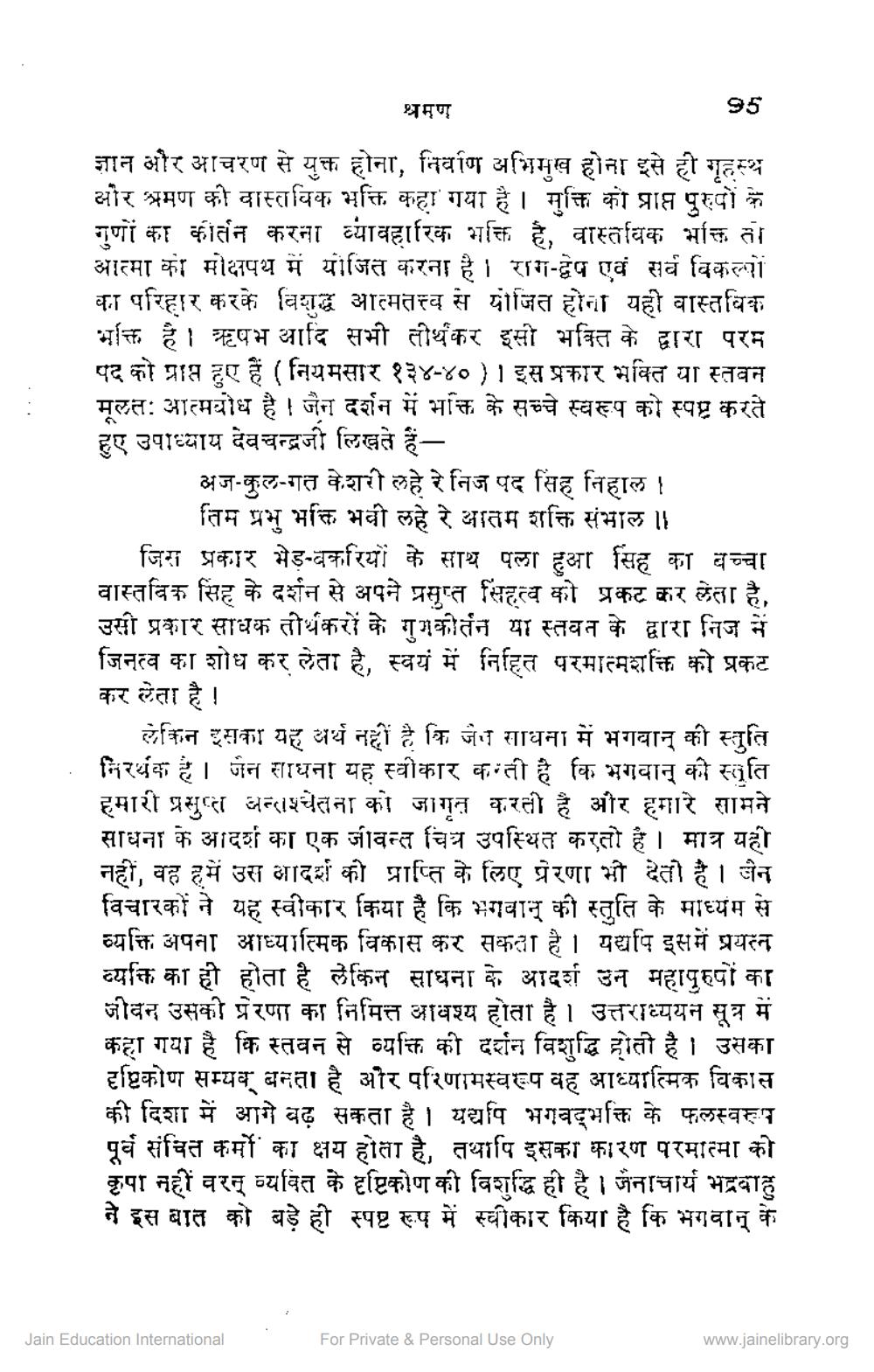Book Title: Jain Dharm me Bhakti ka Sthan Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Sagar_Jain_Vidya_Bharti_Part_2_001685.pdf View full book textPage 3
________________ श्रमण 95 ज्ञान और आचरण से युक्त होना, निर्वाण अभिमुख होना इसे ही गृहस्थ और श्रमण की वास्तविक भक्ति कहा गया है। मुक्ति को प्राप्त पुरुषों के गणों का कीर्तन करना व्यावहारिक भक्ति है, वास्तविक भक्ति तो आत्मा को मोक्षपथ में योजित करना है। राग-द्वेष एवं सर्व विकल्पों का परिहार करके विशुद्ध आत्मतत्त्व से योजित होना यही वास्तविक भक्ति है। अपभ आदि सभी तीर्थंकर इसी भक्ति के द्वारा परम पद को प्राप्त हुए हैं (नियमसार १३४-४०)। इस प्रकार भक्ति या स्तवन मलत: आत्मबोध है । जैन दर्शन में भक्ति के सच्चे स्वरूप को स्पष्ट करते हए उपाध्याय देवचन्द्रजी लिखते हैं अज-कुल-गत केशरी लहे रे निज पद सिंह निहाल ! तिम प्रभु भक्ति भवी लहे रे आतम शक्ति संभाल । जिस प्रकार भेड-बकरियों के साथ पला हा सिंह का बच्चा वास्तविक सिंह के दर्शन से अपने प्रसुप्त सिंहत्व को प्रकट कर लेता है, उसी प्रकार साधक तीर्थकरों के गगकीर्तन या स्तवन के द्वारा निज में जिनत्व का शोध कर लेता है, स्वयं में निहित परमात्मशक्ति को प्रकट कर लेता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जैन साधना में भगवान् की स्तुति निरर्थक है। जन साधना यह स्वीकार करती है कि भगवान् की स्तुति हमारी प्रसुप्त अन्तश्चेतना को जागृत करती है और हमारे सामने साधना के आदर्श का एक जीवन्त चित्र उपस्थित करतो है। मात्र यही नहीं, वह हमें उस आदर्शको प्राप्ति के लिए प्रेरणा भी देती है। जैन विचारकों ने यह स्वीकार किया है कि भगवान् की स्तुति के माध्यम से व्यक्ति अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। यद्यपि इसमें प्रयत्न व्यक्ति का ही होता है लेकिन साधना के आदर्श उन महापुरुषों का जीवन उसकी प्रेरणा का निमित्त आवश्य होता है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि स्तवन से व्यक्ति की दर्शन विद्धि होती है। उसका दृष्टिकोण सम्यक् बनता है और परिणामस्वरूप वह आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यद्यपि भगवद्भक्ति के फलस्वरूप पूर्व संचित कर्मो का क्षय होता है, तथापि इसका कारण परमात्मा को कृपा नहीं वरन् व्यक्ति के दृष्टिकोण की विशुद्धि ही है। जनाचार्य भद्रबाहु ने इस बात को बड़े ही स्पष्ट रूप में स्वीकार किया है कि भगवान् के Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4