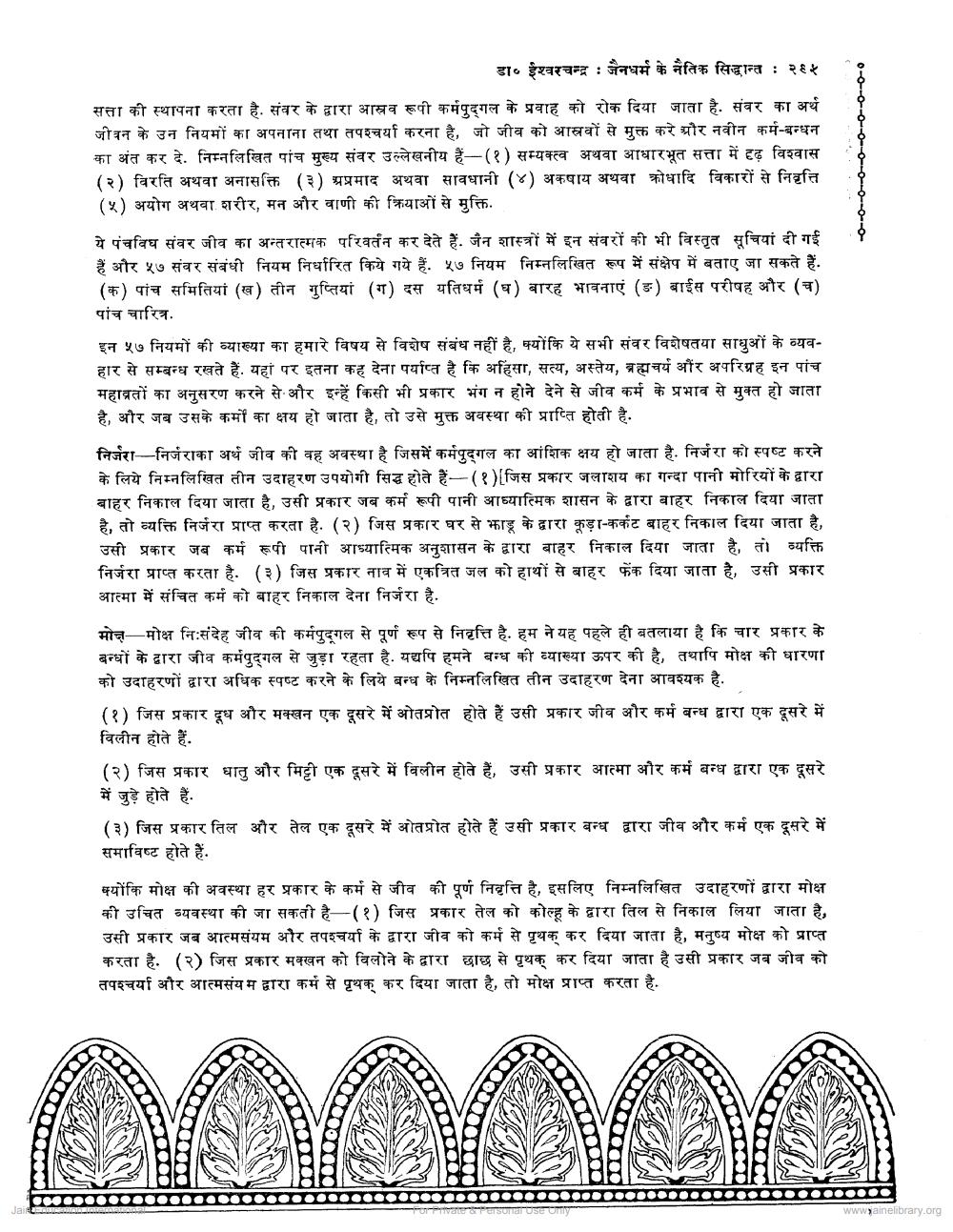Book Title: Jain Dharm ke Naitik Siddhant Author(s): Ishwarchand Sharma Publisher: Z_Hajarimalmuni_Smruti_Granth_012040.pdf View full book textPage 7
________________ Jait डा० ईश्वरचन्द्र : जैनधर्म के नैतिक सिद्धान्त २१५ सत्ता की स्थापना करता है. संवर के द्वारा आस्रव रूपी कर्मपुद्गल के प्रवाह को रोक दिया जाता है. संबर का अर्थ जीवन के उन नियमों का अपनाना तथा तपश्चर्या करना है, जो जीव को आस्रवों से मुक्त करे और नवीन कर्म-बन्धन का अंत कर दे . निम्नलिखित पांच मुख्य संवर उल्लेखनीय हैं- ( १ ) सम्यक्त्व अथवा आधारभूत सत्ता में दृढ़ विश्वास (२) विरति अथवा अनासक्ति (३) श्रप्रमाद अथवा सावधानी (४) अकषाय अथवा क्रोधादि विकारों से निवृत्ति (५) अयोग अथवा शरीर, मन और वाणी की क्रियाओं से मुक्ति. ये पंचविध संवर जीव का अन्तरात्मक परिवर्तन कर देते हैं. जैन शास्त्रों में इन संवरों की भी विस्तृत सूचियां दी गई हैं और ५७ संवर संबंधी नियम निर्धारित किये गये हैं. ५७ नियम निम्नलिखित रूप में संक्षेप में बताए जा सकते हैं. (क) पांच समितियां (ख) तीन गुप्तियां (ग) दस यतिधर्म (घ) बारह भावनाएं (ङ) बाईस परीषह और (च) पांच चारित्र. इन ५७ नियमों की व्याख्या का हमारे विषय से विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि ये सभी संवर विशेषतया साधुओं के व्यव हार से सम्बन्ध रखते हैं. यहां पर इतना कह देना पर्याप्त है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच महाव्रतों का अनुसरण करने से और इन्हें किसी भी प्रकार भंग न होने देने से जीव कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, और जब उसके कर्मों का क्षय हो जाता है, तो उसे मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है. निर्जरा - निर्जराका अर्थ जीव की वह अवस्था है जिसमें कर्मपुद्गल का आंशिक क्षय हो जाता है. निर्जरा को स्पष्ट करने के लिये निम्नलिखित तीन उदाहरण उपयोगी सिद्ध होते हैं- ( १ ) [ जिस प्रकार जलाशय का गन्दा पानी मोरियों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार जब कर्म रूपी पानी आध्यात्मिक शासन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो व्यक्ति निर्जरा प्राप्त करता है. (२) जिस प्रकार घर से झाड़ू के द्वारा कूड़ा-कर्कट बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार जब कर्म रूपी पानी आध्यात्मिक अनुशासन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो व्यक्ति निर्जरा प्राप्त करता है. (३) जिस प्रकार नाव में एकत्रित जल को हाथों से बाहर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा में संचित कर्म को बाहर निकाल देना निर्जरा है. मोक्ष - मोक्ष निःसंदेह जीव की कर्मपुद्गल से पूर्ण रूप से निवृत्ति है. हम ने यह पहले ही बतलाया है कि चार प्रकार के बन्धों के द्वारा जीव कर्मपुद्गल से जुड़ा रहता है. यद्यपि हमने बन्ध की व्याख्या ऊपर की है, तथापि मोक्ष की धारणा को उदाहरणों द्वारा अधिक स्पष्ट करने के लिये बन्ध के निम्नलिखित तीन उदाहरण देना आवश्यक है. (१) जिस प्रकार दूध और मक्खन एक दूसरे में ओतप्रोत होते हैं उसी प्रकार जीव और कर्म बन्ध द्वारा एक दूसरे में विलीन होते हैं. (२) जिस प्रकार धातु और मिट्टी एक दूसरे में विलीन होते हैं, उसी प्रकार आत्मा और कर्म बन्ध द्वारा एक दूसरे में जुड़े होते हैं. (३) जिस प्रकार तिल और तेल एक दूसरे में ओतप्रोत होते हैं उसी प्रकार बन्ध द्वारा जीव और कर्म एक दूसरे में समाविष्ट होते हैं. क्योंकि मोक्ष की अवस्था हर प्रकार के कर्म से जीव की पूर्ण निवृत्ति है, इसलिए निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा मोक्ष की उचित व्यवस्था की जा सकती है— ( १ ) जिस प्रकार तेल को कोल्हू के द्वारा तिल से निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार जब आत्मसंयम और तपश्चर्या के द्वारा जीव को कर्म से पृथक् कर दिया जाता है, मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है. (२) जिस प्रकार मक्खन को विलोने के द्वारा छाछ से पृथक् कर दिया जाता है उसी प्रकार जब जीव को तपश्चर्या और आत्मसंयम द्वारा कर्म से पृथक् कर दिया जाता है, तो मोक्ष प्राप्त करता है. טרך mal Use Only www.ainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14