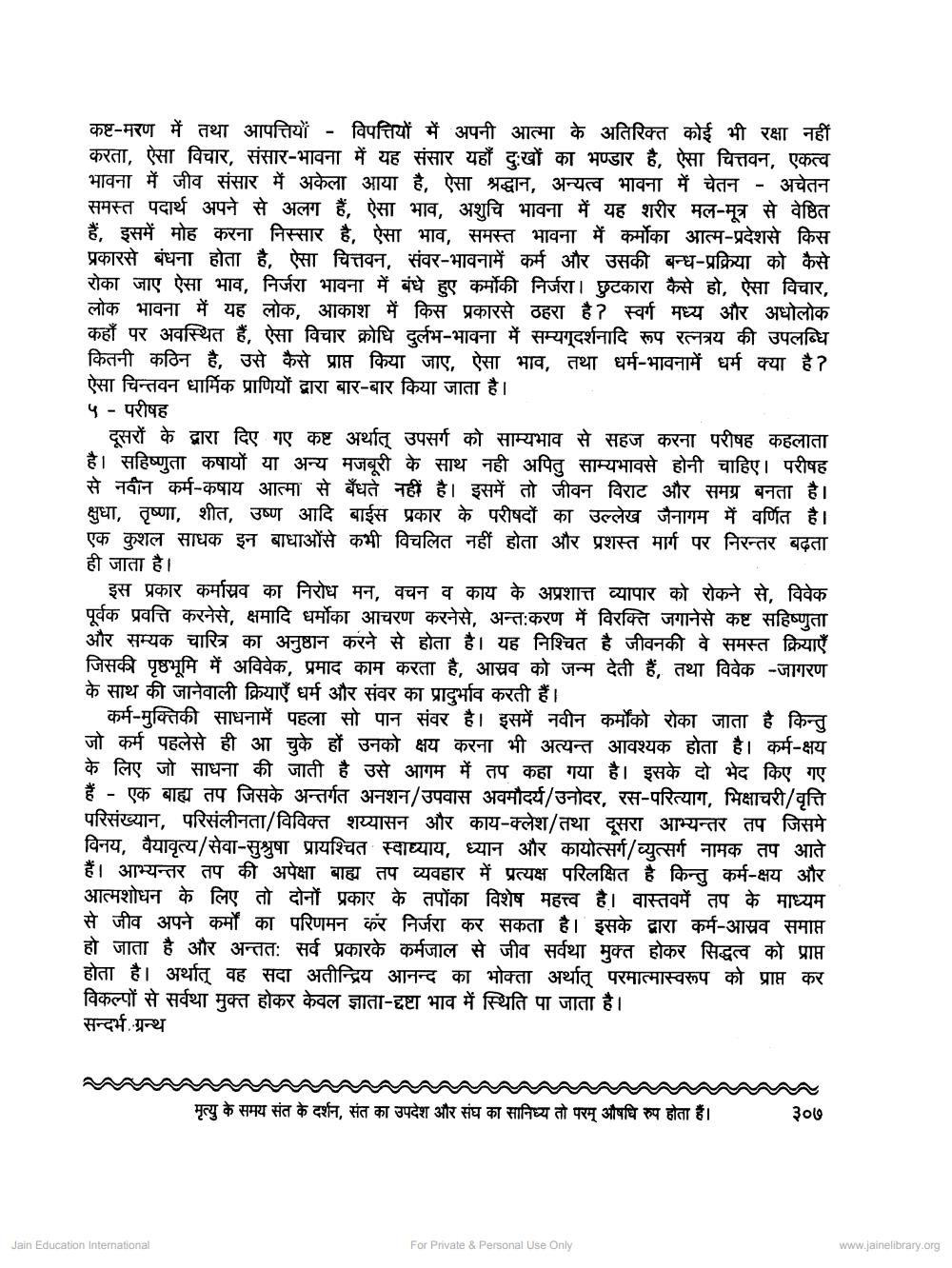Book Title: Jain Darshan me Karm Mimansa Author(s): Rajiv Prachandiya Publisher: Z_Lekhendrashekharvijayji_Abhinandan_Granth_012037.pdf View full book textPage 7
________________ अ कष्ट - मरण में तथा आपत्तियों विपत्तियों में अपनी आत्मा के अतिरिक्त कोई भी रक्षा नहीं करता, ऐसा विचार, संसार-भावना में यह संसार यहाँ दुःखों का भण्डार है, ऐसा चित्तवन, एकत्व भावना में जीव संसार में अकेला आया है, ऐसा श्रद्धान, अन्यत्व भावना में चेतन समस्त पदार्थ अपने से अलग हैं, ऐसा भाव, अशुचि भावना में यह शरीर मल-मूत्र से वेष्ठित हैं, इसमें मोह करना निस्सार है, ऐसा भाव, समस्त भावना में कर्मोका आत्म-प्रदेशसे किस प्रकारसे बंधना होता है, ऐसा चित्तवन संवर भावनामें कर्म और उसकी बन्ध- प्रक्रिया को कैसे रोका जाए ऐसा भाव, निर्जरा भावना में बंधे हुए कर्मोकी निर्जरा। छुटकारा कैसे हो, ऐसा विचार, लोक भावना में यह लोक, आकाश में किस प्रकारसे ठहरा है ? स्वर्ग मध्य और अधोलोक कहाँ पर अवस्थित हैं, ऐसा विचार क्रोधि दुर्लभ भावना में सम्यग्दर्शनादि रूप रत्नत्रय की उपलब्धि कितनी कठिन है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसा भाव तथा धर्म-भावनामें धर्म क्या है ? ऐसा चिन्तवन धार्मिक प्राणियों द्वारा बार-बार किया जाता है। ५ - परीषह - दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट अर्थात् उपसर्ग को साम्यभाव से सहज करना परीषह कहलाता है। सहिष्णुता कषायों या अन्य मजबूरी के साथ नही अपितु साम्यभावसे होनी चाहिए। परीषह से नवीन कर्म कषाय आत्मा से बँधते नहीं है। इसमें तो जीवन विराट और समग्र बनता है। क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण आदि बाईस प्रकार के परीषदों का उल्लेख जैनागम में वर्णित है। एक कुशल साधक इन बाधाओंसे कभी विचलित नहीं होता ही जाता है। और प्रशस्त मार्ग पर निरन्तर बढ़ता - इस प्रकार कर्मास्रव का निरोध मन, वचन व काय के अप्रशात व्यापार को रोकने से, विवेक पूर्वक प्रवत्ति करनेसे, क्षमादि धर्मोका आचरण करनेसे, अन्तःकरण में विरक्ति जगानेसे कष्ट सहिष्णुता और सम्यक चारित्र का अनुष्ठान करने से होता है। यह निश्चित है जीवनकी वे समस्त क्रियाएँ जिसकी पृष्ठभूमि में अविवेक, प्रमाद काम करता है, आस्रव को जन्म देती हैं, तथा विवेक -जागरण के साथ की जानेवाली क्रियाएँ धर्म और संवर का प्रादुर्भाव करती हैं। कर्म - मुक्तिकी साधनामें पहला सो पान संवर है। इसमें नवीन कर्मोंको रोका जाता है किन्तु जो कर्म पहलेसे ही आ चुके हों उनको क्षय करना भी अत्यन्त आवश्यक होता है। कर्म-क्षय के लिए जो साधना की जाती है उसे आगम में तप कहा गया है। इसके दो भेद किए गए हैं एक बाह्य तप जिसके अन्तर्गत अनशन / उपवास अवमौदर्य / उनोदर, रस-परित्याग, भिक्षाचरी / वृत्ति परिसंख्यान, परिसंलीनता / विविक्त शय्यासन और काय - क्लेश / तथा दूसरा आभ्यन्तर तप जिसमे विनय, वैयावृत्य / सेवा-सुश्रुषा प्रायश्चित स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग / व्युत्सर्ग नामक तप आते हैं। आभ्यन्तर तप की अपेक्षा बाह्य तप व्यवहार में प्रत्यक्ष परिलक्षित है किन्तु कर्म-क्षय और आत्मशोधन के लिए तो दोनों प्रकार के तपोंका विशेष महत्त्व है। वास्तवमें तप के माध्यम से जीव अपने कर्मों का परिणमन कर निर्जरा कर सकता है। इसके द्वारा कर्म आस्रव समाप्त हो जाता है और अन्ततः सर्व प्रकारके कर्मजाल से जीव सर्वथा मुक्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त होता है। अर्थात् वह सदा अतीन्द्रिय आनन्द का भोक्ता अर्थात् परमात्मास्वरूप को प्राप्त कर विकल्पों से सर्वथा मुक्त होकर केवल ज्ञाता द्दष्टा भाव में स्थिति पा जाता है। सन्दर्भ ग्रन्थ Jain Education International - मृत्यु के समय संत के दर्शन, संत का उपदेश और संघ का सानिध्य तो परम् औषधि रुप होता हैं। For Private Personal Use Only ३०७ www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8