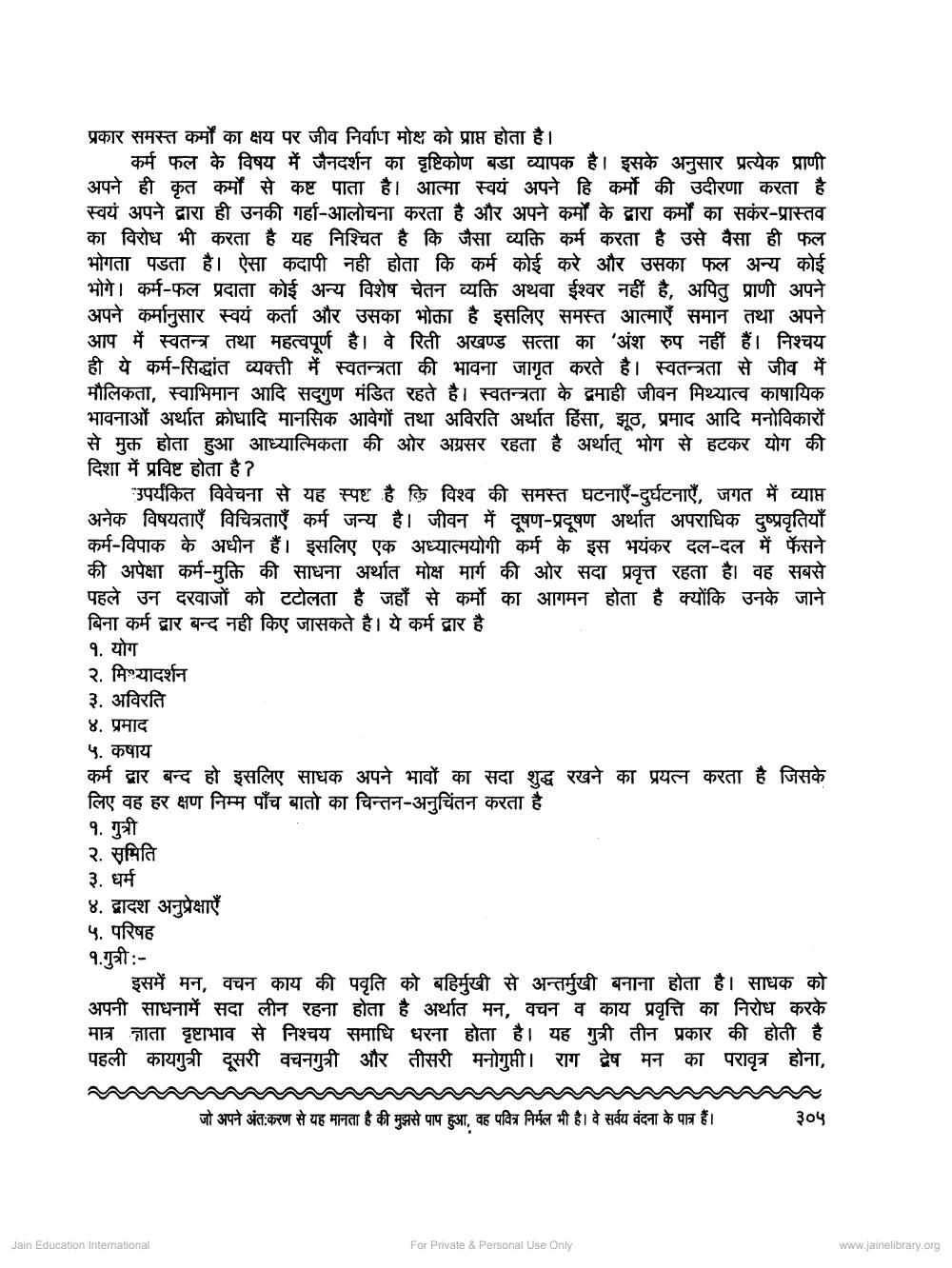Book Title: Jain Darshan me Karm Mimansa Author(s): Rajiv Prachandiya Publisher: Z_Lekhendrashekharvijayji_Abhinandan_Granth_012037.pdf View full book textPage 5
________________ प्रकार समस्त कर्मों का क्षय पर जीव निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। कर्म फल के विषय में जैनदर्शन का दृष्टिकोण बडा व्यापक है। इसके अनुसार प्रत्येक प्राणी अपने ही कृत कर्मों से कष्ट पाता है। आत्मा स्वयं अपने हि कर्मों की उदीरणा करता है स्वयं अपने द्वारा ही उनकी गर्हा आलोचना करता है और अपने कर्मों के द्वारा कर्मों का सकंर - प्रास्तव का विरोध भी करता है यह निश्चित है कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगता पडता है। ऐसा कदापी नही होता कि कर्म कोई करे और उसका फल अन्य कोई भोगे । कर्म-फल प्रदाता कोई अन्य विशेष चेतन व्यक्ति अथवा ईश्वर नहीं है, अपितु प्राणी अपने अपने कर्मानुसार स्वयं कर्ता और उसका भोक्ता है इसलिए समस्त आत्माएँ समान तथा अपने आप में स्वतन्त्र तथा महत्वपूर्ण है। वे रिती अखण्ड सत्ता का 'अंश रूप नहीं हैं। निश्चय ही ये कर्म-सिद्धांत व्यक्ती में स्वतन्त्रता की भावना जागृत करते है । स्वतन्त्रता से जीव में मौलिकता, स्वाभिमान आदि सद्गुण मंडित रहते है । स्वतन्त्रता के द्वमाही जीवन मिथ्यात्व काषायिक भावनाओं अर्थात क्रोधादि मानसिक आवेगों तथा अविरति अर्थात हिंसा, झूठ, प्रमाद आदि मनोविकारों से मुक्त होता हुआ आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर रहता है अर्थात् भोग से हटकर योग की दिशा में प्रविष्ट होता है ? उपर्यंकित विवेचना से यह स्पष्ट है कि विश्व की समस्त घटनाएँ - दुर्घटनाएँ, जगत में व्याप्त अनेक विषयताएँ विचित्रताएँ कर्म जन्य है। जीवन में दूषण- प्रदूषण अर्थात अपराधिक दुष्प्रवृतियाँ कर्म - विपाक के अधीन हैं। इसलिए एक अध्यात्मयोगी कर्म के इस भयंकर दल-दल में फॅसने की अपेक्षा कर्म-मुक्ति की साधना अर्थात मोक्ष मार्ग की ओर सदा प्रवृत्त रहता है। वह सबसे पहले उन दरवाजों को टटोलता है जहाँ से कर्मों का आगमन होता है क्योंकि उनके जाने बिना कर्म द्वार बन्द नही किए जासकते है। ये कर्म द्वार है १. योग २. मिथ्यादर्शन ३. अविरति ४. प्रमाद ५. कषाय कर्म द्वार बन्द हो इसलिए साधक अपने भावों का सदा शुद्ध रखने का प्रयत्न करता है जिसके लिए वह हर क्षण निम्म पाँच बातो का चिन्तन - अनुचिंतन करता है १. गुत्री २. समिति ३. धर्म ४. द्वादश अनुप्रेक्षाएँ ५. परिषह १. गुत्री : - इसमें मन, वचन काय की पवृति को बहिर्मुखी से अन्तर्मुखी बनाना होता है। साधक को अपनी साधनामें सदा लीन रहना होता है अर्थात मन, वचन व काय प्रवृत्ति का निरोध करके मात्र ज्ञाता दृष्टाभाव से निश्चय समाधि धरना होता है। यह गुत्री तीन प्रकार की होती है पहली कायगुत्री दूसरी वचनगुत्री और तीसरी मनोगुप्ती । राग द्वेष मन का परावृत्र होना, जो अपने अंत:करण से यह मानता है की मुझसे पाप हुआ, वह पवित्र निर्मल भी है। वे सर्वय वंदना के पात्र हैं। Jain Education International For Private Personal Use Only ३०५ www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8