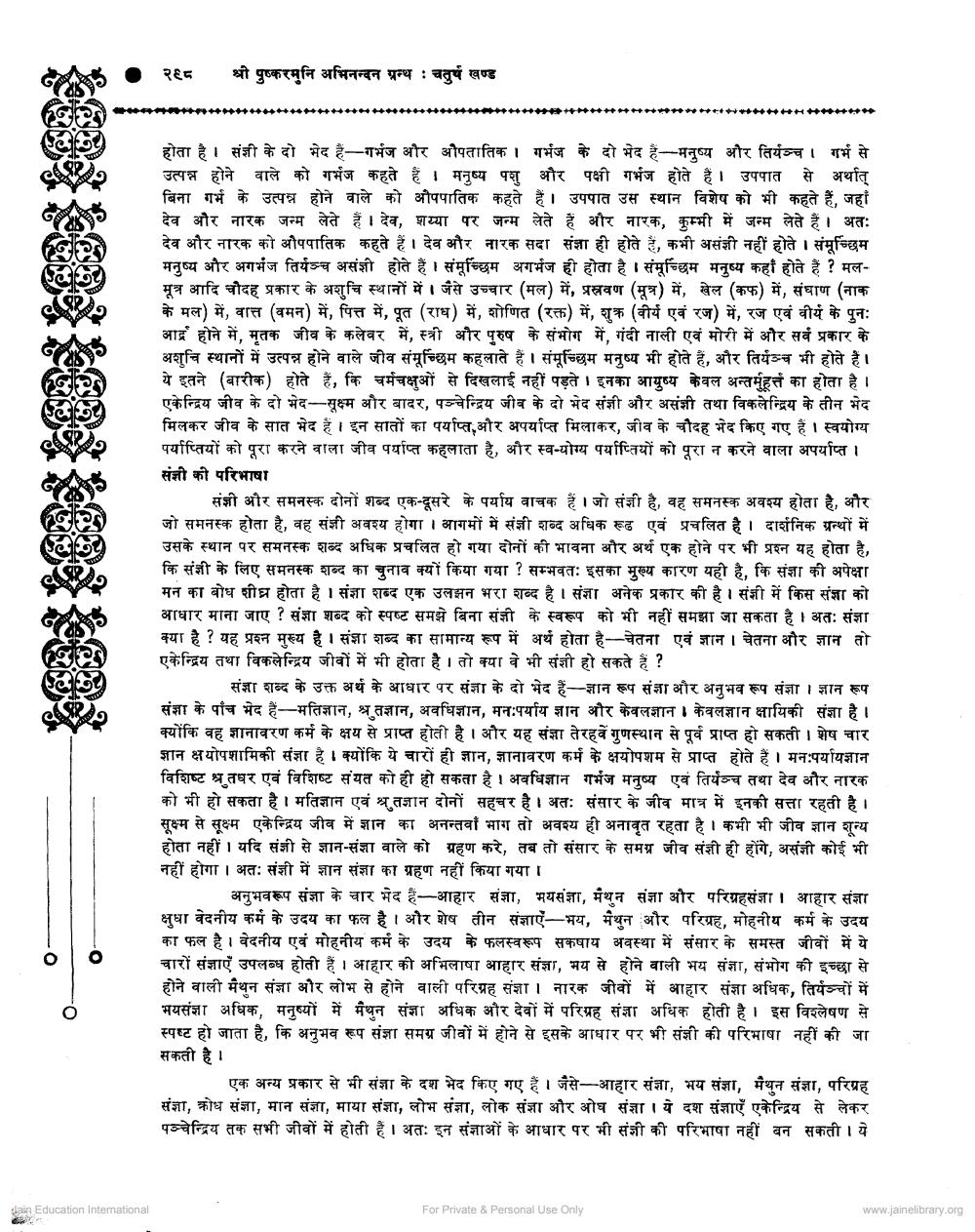Book Title: Jain Darshan me Jivtattva Ek Vivechan Author(s): Vijay Muni Publisher: Z_Pushkarmuni_Abhinandan_Granth_012012.pdf View full book textPage 9
________________ GA . २६८ श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : चतुर्थ खण्ड होता है। संज्ञी के दो भेद हैं-गर्भज और औपतातिक । गर्भज के दो भेद है-मनुष्य और तिर्यञ्च । गर्भ से उत्पन्न होने वाले को गर्भज कहते हैं । मनुष्य पशु और पक्षी गर्भज होते हैं। उपपात से अर्थात् बिना गर्भ के उत्पन्न होने वाले को औपपातिक कहते हैं। उपपात उस स्थान विशेष को भी कहते हैं, जहाँ देव और नारक जन्म लेते हैं । देव, शय्या पर जन्म लेते हैं और नारक, कुम्भी में जन्म लेते हैं। अतः देव और नारक को औपपातिक कहते हैं। देव और नारक सदा संज्ञा ही होते हैं, कभी असंज्ञी नहीं होते । संमूच्छिम मनुष्य और अगर्भज तिर्यञ्च असंज्ञी होते हैं । संमूच्छिम अगर्भज ही होता है । संमूच्छिम मनुष्य कहाँ होते हैं ? मलमूत्र आदि चौदह प्रकार के अशुचि स्थानों में । जैसे उच्चार (मल) में, प्रस्रवण (मूत्र) में, खेल (कफ) में, संघाण (नाक के मल) में, वात्त (वमन) में, पित्त में, पूत (राध) में, शोणित (रक्त) में, शुक्र (वीर्य एवं रज) में, रज एवं वीर्य के पुनः आर्द्र होने में, मृतक जीव के कलेवर में, स्त्री और पुरुष के संभोग में, गंदी नाली एवं मोरी में और सर्व प्रकार के अशुचि स्थानों में उत्पन्न होने वाले जीव संमूच्छिम कहलाते हैं । संमूच्छिम मनुष्य भी होते हैं, और तिर्यञ्च भी होते हैं। ये इतने (बारीक) होते हैं, कि चर्मचक्षुओं से दिखलाई नहीं पड़ते । इनका आयुष्य केवल अन्तर्मुहर्त का होता है । एकेन्द्रिय जीव के दो भेद-सूक्ष्म और बादर, पञ्चेन्द्रिय जीव के दो भेद संज्ञी और असंज्ञी तथा विकलेन्द्रिय के तीन भेद मिलकर जीव के सात भेद हैं । इन सातों का पर्याप्त,और अपर्याप्त मिलाकर, जीव के चौदह भेद किए गए हैं। स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूरा करने वाला जीव पर्याप्त कहलाता है, और स्व-योग्य पर्याप्तियों को पूरा न करने वाला अपर्याप्त । संज्ञी को परिभाषा संज्ञी और समनस्क दोनों शब्द एक-दूसरे के पर्याय वाचक हैं । जो संज्ञी है, वह समनस्क अवश्य होता है, और जो समनस्क होता है, वह संज्ञी अवश्य होगा । आगमों में संज्ञी शब्द अधिक रूढ एवं प्रचलित है। दार्शनिक ग्रन्थों में उसके स्थान पर समनस्क शब्द अधिक प्रचलित हो गया दोनों की भावना और अर्थ एक होने पर भी प्रश्न यह होता है, कि संजी के लिए समनस्क शब्द का चुनाव क्यों किया गया ? सम्भवतः इसका मुख्य कारण यही है, कि संज्ञा की अपेक्षा मन का बोध शीघ्र होता है । संज्ञा शब्द एक उलझन भरा शब्द है । संज्ञा अनेक प्रकार की है। संज्ञी में किस संज्ञा को आधार माना जाए ? संज्ञा शब्द को स्पष्ट समझे बिना संज्ञी के स्वरूप को भी नहीं समझा जा सकता है। अतः संज्ञा क्या है ? यह प्रश्न मुख्य है । संज्ञा शब्द का सामान्य रूप में अर्थ होता है-चेतना एवं ज्ञान । चेतना और ज्ञान तो एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय जीवों में भी होता है । तो क्या वे भी संजी हो सकते हैं ? संज्ञा शब्द के उक्त अर्थ के आधार पर संज्ञा के दो भेद हैं-ज्ञान रूप संज्ञा और अनुभव रूप संज्ञा । ज्ञान रूप संज्ञा के पांच भेद हैं-मतिज्ञान, श्रु तज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और केवलज्ञान । केवलज्ञान क्षायिकी संज्ञा है । क्योंकि वह ज्ञानावरण कर्म के क्षय से प्राप्त होती है । और यह संज्ञा तेरहवें गुणस्थान से पूर्व प्राप्त हो सकती। शेष चार ज्ञान क्षयोपशामिकी संज्ञा है। क्योंकि ये चारों ही ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होते हैं। मनःपर्यायज्ञान विशिष्ट श्रुतधर एवं विशिष्ट संयत को ही हो सकता है । अवधिज्ञान गर्भज मनुष्य एवं तिर्यञ्च तथा देव और नारक को भी हो सकता है। मतिज्ञान एवं श्रु तज्ञान दोनों सहचर है। अतः संसार के जीव मात्र में इनकी सत्ता रहती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव में ज्ञान का अनन्तवाँ भाग तो अवश्य ही अनावृत रहता है। कभी भी जीव ज्ञान शुन्य होता नहीं। यदि संज्ञी से ज्ञान-संज्ञा वाले को ग्रहण करे, तब तो संसार के समग्र जीव संज्ञी ही होंगे, असंज्ञी कोई भी नहीं होगा। अतः संज्ञी में ज्ञान संज्ञा का ग्रहण नहीं किया गया । अनुभवरूप संज्ञा के चार भेद हैं-आहार संज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रहसंज्ञा । आहार संज्ञा क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय का फल है । और शेष तीन संज्ञाएँ-भय, मैथुन और परिग्रह, मोहनीय कर्म के उदय का फल है । वेदनीय एवं मोहनीय कर्म के उदय के फलस्वरूप सकषाय अवस्था में संसार के समस्त जीवों में ये चारों संज्ञाएँ उपलब्ध होती हैं । आहार की अभिलाषा आहार संज्ञा, भय से होने वाली भय संज्ञा, संभोग की इच्छा से होने वाली मैथुन संज्ञा और लोभ से होने वाली परिग्रह संज्ञा । नारक जीवों में आहार संज्ञा अधिक, तिर्यञ्चों में भयसंज्ञा अधिक, मनुष्यों में मैथुन संज्ञा अधिक और देवों में परिग्रह संज्ञा अधिक होती है। इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है, कि अनुभव रूप संज्ञा समग्र जीवों में होने से इसके आधार पर भी संज्ञी की परिभाषा नहीं की जा सकती है। एक अन्य प्रकार से भी संज्ञा के दश भेद किए गए हैं । जैसे-आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, लोक संज्ञा और ओघ संज्ञा । ये दश संज्ञाएँ एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक सभी जीवों में होती हैं । अतः इन संज्ञाओं के आधार पर भी संज्ञी की परिभाषा नहीं बन सकती। ये an Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13