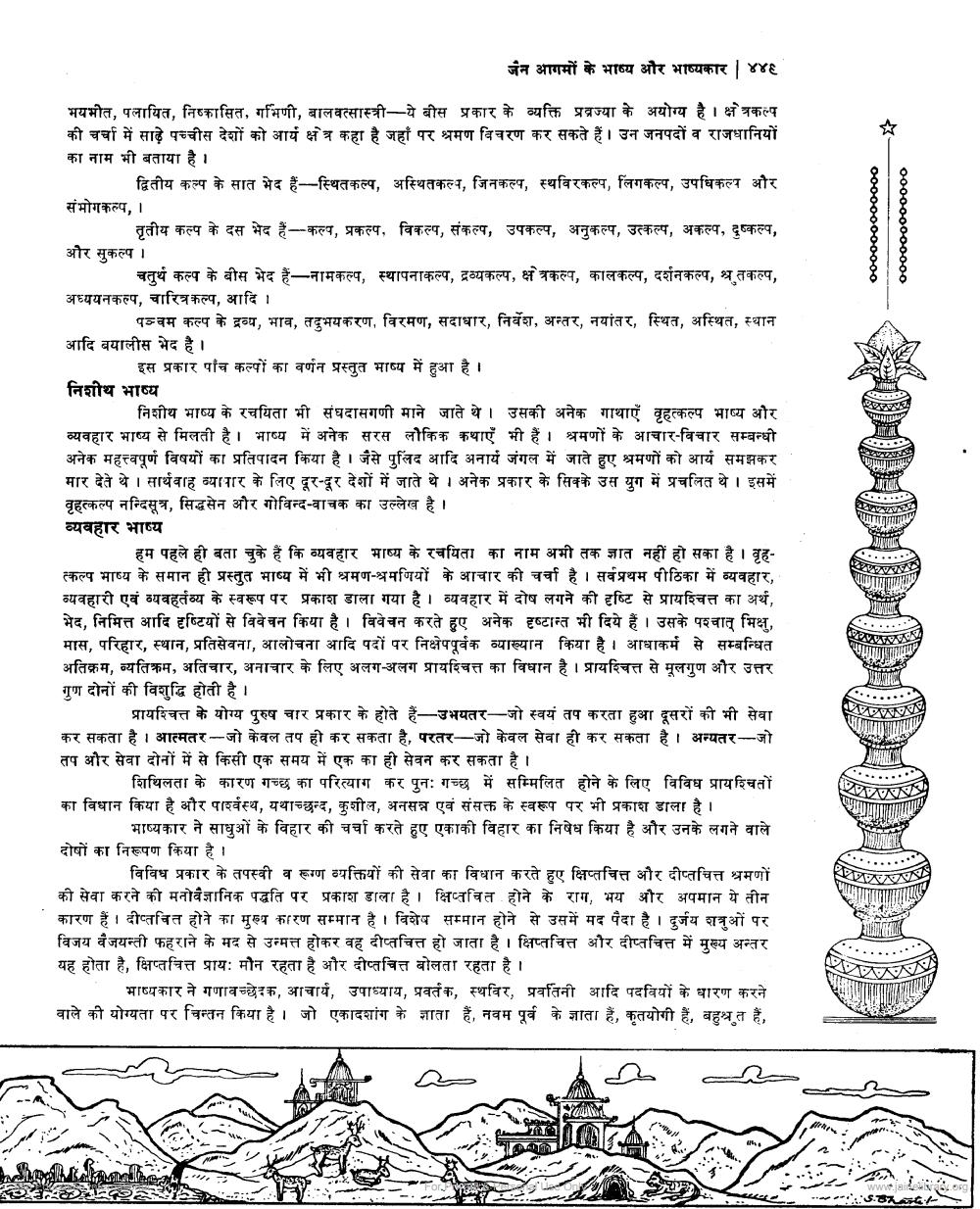Book Title: Jain Agamo ke Bhashya aur Bhashyakar Author(s): Pushkar Muni Publisher: Z_Ambalalji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012038.pdf View full book textPage 7
________________ जैन आगमों के भाष्य और भाष्यकार | ४४६ ०००००००००००० ०००००००००००० HINNEL श्र '.... PAAAAmy HITTER भयभीत, पलायित, निष्कासित, गर्भिणी, बालवत्सास्त्री-ये बीस प्रकार के व्यक्ति प्रव्रज्या के अयोग्य है । क्षेत्रकल्प की चर्चा में साढ़े पच्चीस देशों को आर्य क्षेत्र कहा है जहाँ पर श्रमण विचरण कर सकते हैं। उन जनपदों व राजधानियों का नाम भी बताया है। द्वितीय कल्प के सात भेद हैं-स्थितकल्प, अस्थितकल्प, जिनकल्प, स्थविरकल्प, लिंगकल्प, उपधिकल्प और संभोगकल्प,। तृतीय कल्प के दस भेद हैं--कल्प, प्रकल्प, विकल्प, संकल्प, उपकल्प, अनुकल्प, उत्कल्प, अकल्प, दुष्कल्प, और सुकल्प । चतुर्थ कल्प के बीस भेद हैं-नामकल्प, स्थापनाकल्प, द्रव्यकल्प, क्षेत्रकल्प, कालकल्प, दर्शनकल्प, श्र तकल्प, अध्ययनकल्प, चारित्रकल्प, आदि । पञ्चम कल्प के द्रव्य, भाव, तदुभयकरण, विरमण, सदाधार, निवेश, अन्तर, नयांतर, स्थित, अस्थित, स्थान आदि बयालीस भेद है। इस प्रकार पाँच कल्पों का वर्णन प्रस्तुत भाष्य में हुआ है। निशीथ भाष्य निशीथ भाष्य के रचयिता भी संघदासगणी माने जाते थे। उसकी अनेक गाथाएँ वृहत्कल्प भाष्य और व्यवहार भाष्य से मिलती है। भाष्य में अनेक सरस लौकिक कथाएँ भी हैं। श्रमणों के आचार-विचार सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन किया है । जैसे पुलिंद आदि अनार्य जंगल में जाते हुए श्रमणों को आर्य समझकर मार देते थे । सार्थवाह व्यापार के लिए दूर-दूर देशों में जाते थे । अनेक प्रकार के सिक्के उस युग में प्रचलित थे । इसमें वृहत्कल्प नन्दिसूत्र, सिद्धसेन और गोविन्द-वाचक का उल्लेख है। व्यवहार भाष्य हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यवहार भाष्य के रचयिता का नाम अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। वृहकल्प भाष्य के समान ही प्रस्तुत भाष्य में भी श्रमण-श्रमणियों के आचार की चर्चा है । सर्वप्रथम पीठिका में व्यवहार, व्यवहारी एवं व्यवहर्तव्य के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। व्यवहार में दोष लगने की दृष्टि से प्रायश्चित्त का अर्थ, भेद, निमित्त आदि दृष्टियों से विवेचन किया है। विवेचन करते हुए अनेक दृष्टान्त भी दिये हैं। उसके पश्चात् भिक्षु, मास, परिहार, स्थान, प्रतिसेवना, आलोचना आदि पदों पर निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया है। आधाकर्म से सम्बन्धित अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार के लिए अलग-अलग प्रायश्चित्त का विधान है । प्रायश्चित्त से मूलगुण और उत्तर गुण दोनों की विशुद्धि होती है। प्रायश्चित्त के योग्य पुरुष चार प्रकार के होते हैं-उभयतर-जो स्वयं तप करता हुआ दूसरों की भी सेवा कर सकता है । आत्मतर-जो केवल तप ही कर सकता है, परतर-जो केवल सेवा ही कर सकता है। अन्यतर-जो तप और सेवा दोनों में से किसी एक समय में एक का ही सेवन कर सकता है। शिथिलता के कारण गच्छ का परित्याग कर पुनः गच्छ में सम्मिलित होने के लिए विविध प्रायश्चितों का विधान किया है और पार्श्वस्थ, यथाच्छन्द, कुशील, अनसन एवं संसक्त के स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है। भाष्यकार ने साधुओं के विहार की चर्चा करते हुए एकाकी विहार का निषेध किया है और उनके लगने वाले दोषों का निरूपण किया है। विविध प्रकार के तपस्वी व रूग्ण व्यक्तियों की सेवा का विधान करते हुए क्षिप्तचित्त और दीप्तचित्त श्रमणों की सेवा करने की मनोवैज्ञानिक पद्धति पर प्रकाश डाला है। क्षिप्तचित्त होने के राग, भय और अपमान ये तीन कारण हैं । दीप्तचित होने का मुख्य कारण सम्मान है । विशेष सम्मान होने से उसमें मद पैदा है । दुर्जय शत्रुओं पर विजय वैजयन्ती फहराने के मद से उन्मत्त होकर वह दीप्तचित्त हो जाता है । क्षिप्तचित्त और दीप्तचित्त में मुख्य अन्तर यह होता है, क्षिप्तचित्त प्रायः मौन रहता है और दीप्तचित्त बोलता रहता है। भाष्यकार ने गणावच्छेदक, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, प्रवर्तिनी आदि पदवियों के धारण करने वाले की योग्यता पर चिन्तन किया है। जो एकादशांग के ज्ञाता हैं, नवम पूर्व के ज्ञाता हैं, कृतयोगी हैं, बहुश्रुत हैं, S AAMSARTAIN "/ ... M h . ... .. Lama -:- -: wwejaitain.org :SazontPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9