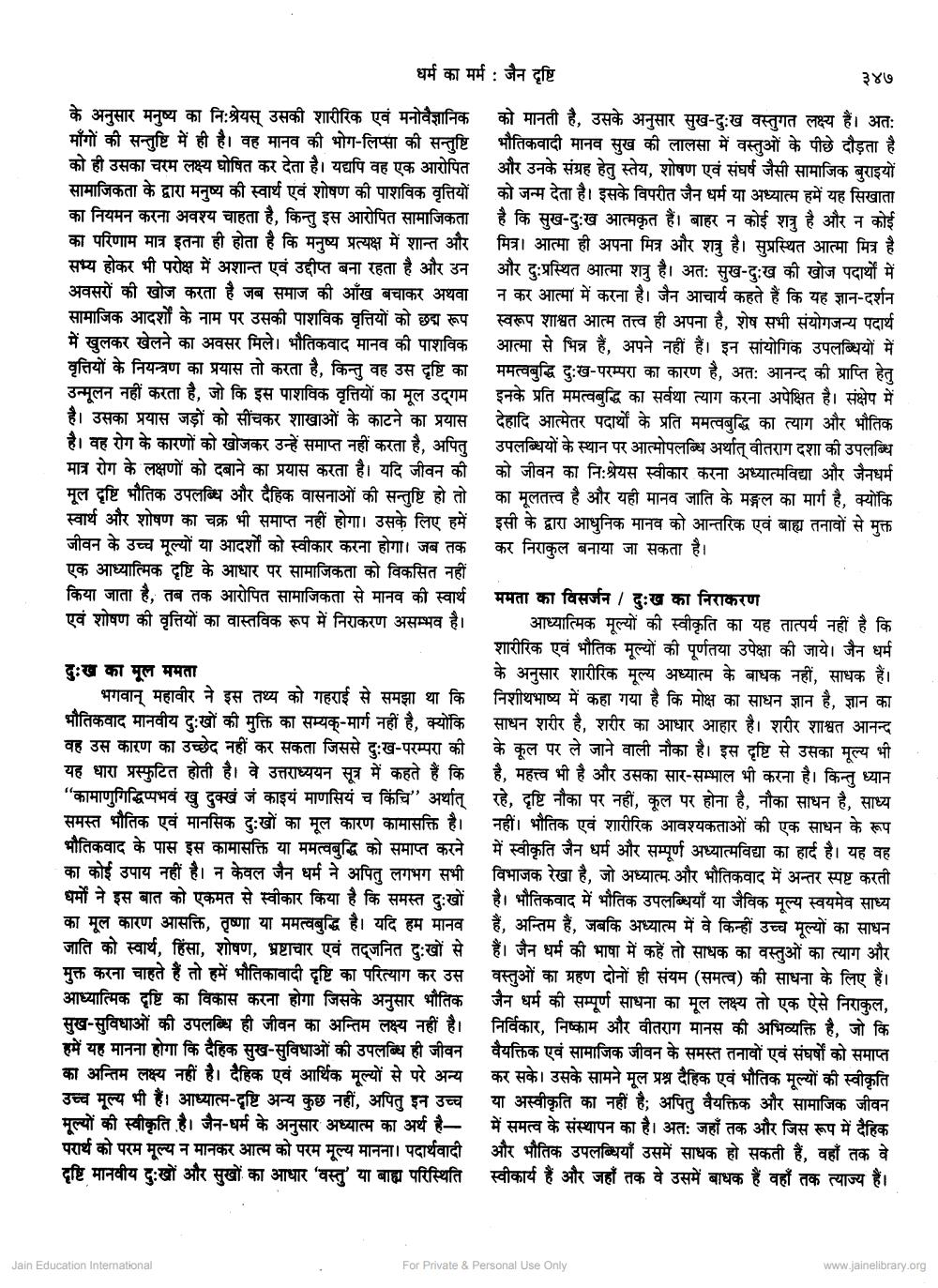Book Title: Dharm ka Marm Jain Drushti Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 3
________________ धर्म का मर्म : जैन दृष्टि ३४७ के अनुसार मनुष्य का निःश्रेयस् उसकी शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक को मानती है, उसके अनुसार सुख-दुःख वस्तुगत लक्ष्य हैं। अत: माँगों की सन्तुष्टि में ही है। वह मानव की भोग-लिप्सा की सन्तुष्टि भौतिकवादी मानव सुख की लालसा में वस्तुओं के पीछे दौड़ता है को ही उसका चरम लक्ष्य घोषित कर देता है। यद्यपि वह एक आरोपित और उनके संग्रह हेतु स्तेय, शोषण एवं संघर्ष जैसी सामाजिक बुराइयों सामाजिकता के द्वारा मनुष्य की स्वार्थ एवं शोषण की पाशविक वृत्तियों को जन्म देता है। इसके विपरीत जैन धर्म या अध्यात्म हमें यह सिखाता का नियमन करना अवश्य चाहता है, किन्तु इस आरोपित सामाजिकता है कि सुख-दुःख आत्मकृत हैं। बाहर न कोई शत्रु है और न कोई का परिणाम मात्र इतना ही होता है कि मनुष्य प्रत्यक्ष में शान्त और मित्र। आत्मा ही अपना मित्र और शत्रु है। सुप्रस्थित आत्मा मित्र है सभ्य होकर भी परोक्ष में अशान्त एवं उद्दीप्त बना रहता है और उन और दुःप्रस्थित आत्मा शत्रु है। अत: सुख-दुःख की खोज पदार्थों में अवसरों की खोज करता है जब समाज की आँख बचाकर अथवा न कर आत्मा में करना है। जैन आचार्य कहते हैं कि यह ज्ञान-दर्शन सामाजिक आदर्शों के नाम पर उसकी पाशविक वृत्तियों को छद्म रूप स्वरूप शाश्वत आत्म तत्त्व ही अपना है, शेष सभी संयोगजन्य पदार्थ में खुलकर खेलने का अवसर मिले। भौतिकवाद मानव की पाशविक आत्मा से भिन्न हैं, अपने नहीं हैं। इन सांयोगिक उपलब्धियों में वृत्तियों के नियन्त्रण का प्रयास तो करता है, किन्तु वह उस दृष्टि का ममत्वबुद्धि दुःख-परम्परा का कारण है, अत: आनन्द की प्राप्ति हेतु उन्मूलन नहीं करता है, जो कि इस पाशविक वृत्तियों का मूल उद्गम इनके प्रति ममत्वबुद्धि का सर्वथा त्याग करना अपेक्षित है। संक्षेप में है। उसका प्रयास जड़ों को सींचकर शाखाओं के काटने का प्रयास देहादि आत्मेतर पदार्थों के प्रति ममत्वबुद्धि का त्याग और भौतिक है। वह रोग के कारणों को खोजकर उन्हें समाप्त नहीं करता है, अपितु उपलब्धियों के स्थान पर आत्मोपलब्धि अर्थात् वीतराग दशा की उपलब्धि मात्र रोग के लक्षणों को दबाने का प्रयास करता है। यदि जीवन की को जीवन का निःश्रेयस स्वीकार करना अध्यात्मविद्या और जैनधर्म मूल दृष्टि भौतिक उपलब्धि और दैहिक वासनाओं की सन्तुष्टि हो तो का मूलतत्त्व है और यही मानव जाति के मङ्गल का मार्ग है, क्योंकि स्वार्थ और शोषण का चक्र भी समाप्त नहीं होगा। उसके लिए हमें इसी के द्वारा आधुनिक मानव को आन्तरिक एवं बाह्य तनावों से मुक्त जीवन के उच्च मूल्यों या आदर्शों को स्वीकार करना होगा। जब तक कर निराकुल बनाया जा सकता है। एक आध्यात्मिक दृष्टि के आधार पर सामाजिकता को विकसित नहीं किया जाता है, तब तक आरोपित सामाजिकता से मानव की स्वार्थ ममता का विसर्जन / दुःख का निराकरण एवं शोषण की वृत्तियों का वास्तविक रूप में निराकरण असम्भव है। आध्यात्मिक मूल्यों की स्वीकृति का यह तात्पर्य नहीं है कि शारीरिक एवं भौतिक मूल्यों की पूर्णतया उपेक्षा की जाये। जैन धर्म दुःख का मूल ममता के अनुसार शारीरिक मूल्य अध्यात्म के बाधक नहीं, साधक हैं। भगवान् महावीर ने इस तथ्य को गहराई से समझा था कि निशीथभाष्य में कहा गया है कि मोक्ष का साधन ज्ञान है, ज्ञान का भौतिकवाद मानवीय दुःखों की मुक्ति का सम्यक्-मार्ग नहीं है, क्योंकि साधन शरीर है, शरीर का आधार आहार है। शरीर शाश्वत आनन्द वह उस कारण का उच्छेद नहीं कर सकता जिससे दुःख-परम्परा की के कूल पर ले जाने वाली नौका है। इस दृष्टि से उसका मूल्य भी यह धारा प्रस्फुटित होती है। वे उत्तराध्ययन सूत्र में कहते हैं कि है, महत्त्व भी है और उसका सार-सम्भाल भी करना है। किन्तु ध्यान "कामाणुगिद्धिप्पभवं खु दुक्खं जं काइयं माणसियं च किंचि” अर्थात् रहे, दृष्टि नौका पर नहीं, कूल पर होना है, नौका साधन है, साध्य समस्त भौतिक एवं मानसिक दुःखों का मूल कारण कामासक्ति है। नहीं। भौतिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं की एक साधन के रूप भौतिकवाद के पास इस कामासक्ति या ममत्वबुद्धि को समाप्त करने में स्वीकृति जैन धर्म और सम्पूर्ण अध्यात्मविद्या का हार्द है। यह वह का कोई उपाय नहीं है। न केवल जैन धर्म ने अपितु लगभग सभी विभाजक रेखा है, जो अध्यात्म. और भौतिकवाद में अन्तर स्पष्ट करती धर्मों ने इस बात को एकमत से स्वीकार किया है कि समस्त दुःखों है। भौतिकवाद में भौतिक उपलब्धियाँ या जैविक मूल्य स्वयमेव साध्य का मूल कारण आसक्ति, तृष्णा या ममत्वबुद्धि है। यदि हम मानव हैं, अन्तिम हैं, जबकि अध्यात्म में वे किन्हीं उच्च मूल्यों का साधन जाति को स्वार्थ, हिंसा, शोषण, भ्रष्टाचार एवं तद्जनित दुःखों से हैं। जैन धर्म की भाषा में कहें तो साधक का वस्तुओं का त्याग और मुक्त करना चाहते हैं तो हमें भौतिकावादी दृष्टि का परित्याग कर उस वस्तुओं का ग्रहण दोनों ही संयम (समत्व) की साधना के लिए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि का विकास करना होगा जिसके अनुसार भौतिक जैन धर्म की सम्पूर्ण साधना का मूल लक्ष्य तो एक ऐसे निराकुल, सुख-सुविधाओं की उपलब्धि ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य नहीं है। निर्विकार, निष्काम और वीतराग मानस की अभिव्यक्ति है, जो कि हमें यह मानना होगा कि दैहिक सुख-सुविधाओं की उपलब्धि ही जीवन वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन के समस्त तनावों एवं संघर्षों को समाप्त का अन्तिम लक्ष्य नहीं है। दैहिक एवं आर्थिक मूल्यों से परे अन्य कर सके। उसके सामने मूल प्रश्न दैहिक एवं भौतिक मूल्यों की स्वीकृति उच्च मूल्य भी हैं। आध्यात्म-दृष्टि अन्य कुछ नहीं, अपितु इन उच्च या अस्वीकृति का नहीं है; अपितु वैयक्तिक और सामाजिक जीवन मूल्यों की स्वीकृति है। जैन-धर्म के अनुसार अध्यात्म का अर्थ है- में समत्व के संस्थापन का है। अत: जहाँ तक और जिस रूप में दैहिक परार्थ को परम मूल्य न मानकर आत्म को परम मूल्य मानना। पदार्थवादी और भौतिक उपलब्धियाँ उसमें साधक हो सकती हैं, वहाँ तक वे दृष्टि मानवीय दु:खों और सुखों का आधार 'वस्तु' या बाह्य परिस्थिति स्वीकार्य हैं और जहाँ तक वे उसमें बाधक हैं वहाँ तक त्याज्य हैं। Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19