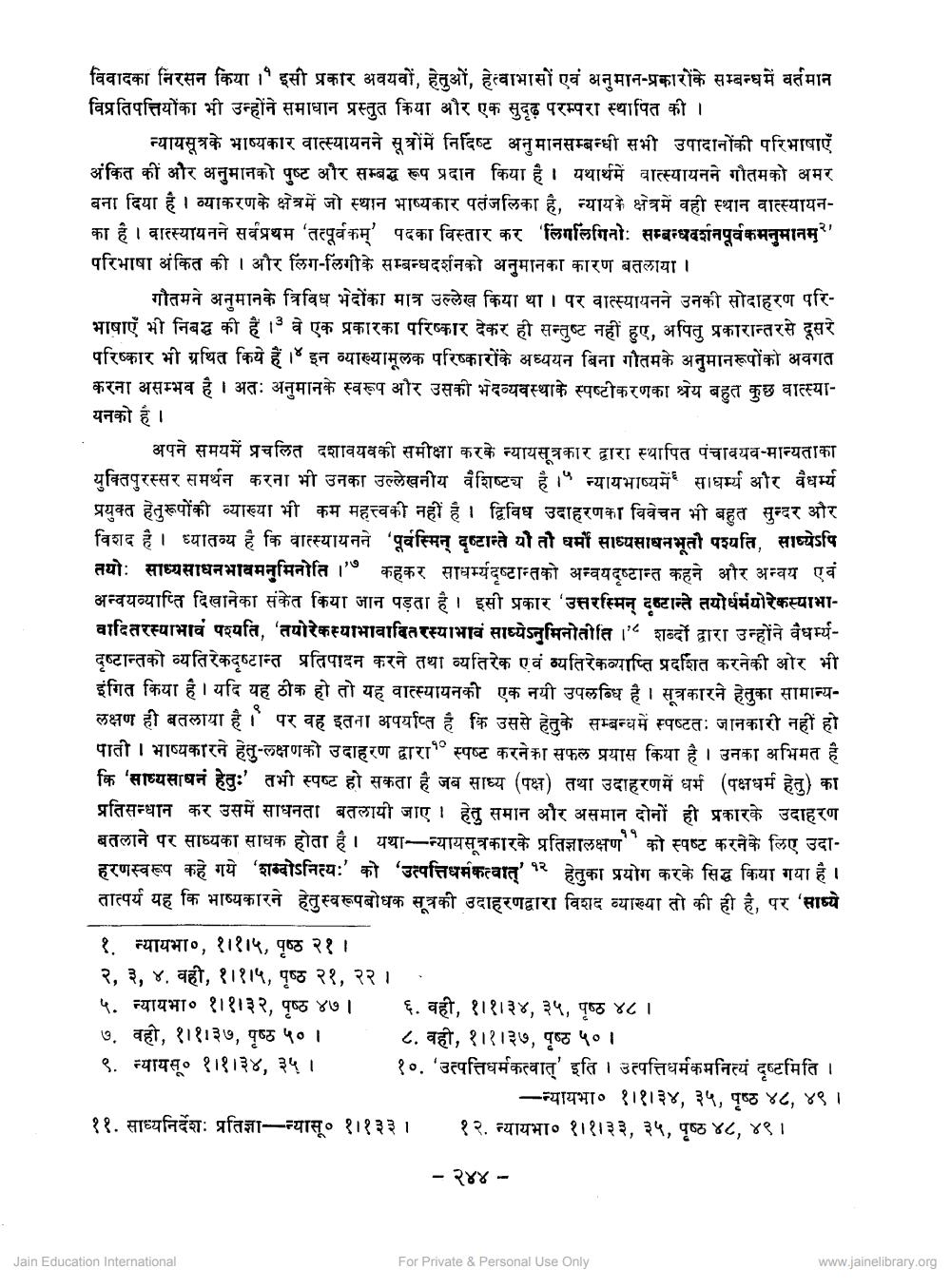Book Title: Bharatiya Vangamay me Anuman Vichar Author(s): Darbarilal Kothiya Publisher: Z_Darbarilal_Kothiya_Abhinandan_Granth_012020.pdf View full book textPage 6
________________ विवादका निरसन किया। इसी प्रकार अवयवों, हेतुओं, हेत्वाभासों एवं अनुमान-प्रकारोंके सम्बन्ध में वर्तमान विप्रतिपत्तियोंका भी उन्होंने समाधान प्रस्तुत किया और एक सुदृढ़ परम्परा स्थापित की । न्यायसूत्रके भाष्यकार वात्स्यायनने सूत्रोंमें निर्दिष्ट अनुमानसम्बन्धी सभी उपादानोंकी परिभाषाएँ अंकित की और अनुमानको पुष्ट और सम्बद्ध रूप प्रदान किया है। यथार्थमें वात्स्यायनने गौतमको अमर बना दिया है । व्याकरणके क्षेत्र में जो स्थान भाष्यकार पतंजलिका है, न्यायके क्षेत्रमें वही स्थान वात्स्यायनका है । वात्स्यायनने सर्वप्रथम 'तत्पूर्वकम्' पदका विस्तार कर लिगलिगिनोः सम्बन्धदर्शनपूर्वकमनुमानम् परिभाषा अंकित की। और लिंग-लिंगीके सम्बन्धदर्शनको अनुमानका कारण बतलाया। गौतमने अनुमानके त्रिविध भेदोंका मात्र उल्लेख किया था। पर वात्स्यायनने उनकी सोदाहरण परिभाषाएँ भी निबद्ध की हैं। वे एक प्रकारका परिष्कार देकर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, अपितु प्रकारान्तरसे दूसरे परिष्कार भी ग्रथित किये हैं। इन व्याख्यामूलक परिष्कारोंके अध्ययन बिना गौतमके अनुमानरूपोंको अवगत करना असम्भव है । अतः अनुमानके स्वरूप और उसकी भेदव्यवस्थाके स्पष्टीकरणका श्रेय बहुत कुछ वात्स्यायनको है। अपने समयमें प्रचलित दशावयवकी समीक्षा करके न्यायसूत्रकार द्वारा स्थापित पंचाक्यव-मान्यताका युक्तिपुरस्सर समर्थन करना भी उनका उल्लेखनीय वैशिष्ट्य है।५ न्यायभाष्यमें साधर्म्य और वैधर्म्य प्रयुक्त हेतुरूपोंकी व्याख्या भी कम महत्त्वकी नहीं है । द्विविध उदाहरणका विवेचन भी बहुत सुन्दर और विशद है । ध्यातव्य है कि वात्स्यायनने 'पूर्वस्मिन् दृष्टान्ते यो तो धर्मों साध्यसाधनभूतौ पश्यति, साध्येऽपि तयोः साध्यसाधनभावमनुमिनोति ।' कहकर साधर्म्यदृष्टान्तको अन्वयदृष्टान्त कहने और अन्वय एवं अन्वयव्याप्ति दिखानेका संकेत किया जान पड़ता है। इसी प्रकार 'उत्तरस्मिन् दृष्टान्ते तयोर्धर्मयोरेकस्याभावादितरस्याभावं पश्यति, 'तयोरेकस्याभावावितरस्याभावं साध्येऽनुमिनोतीति ।८ शब्दों द्वारा उन्होंने वैधर्म्यदष्टान्तको व्यतिरेकदृष्टान्त प्रतिपादन करने तथा व्यतिरेक एवं व्यतिरेकव्याप्ति प्रदर्शित करनेकी ओर भी इंगित किया है। यदि यह ठीक हो तो यह वात्स्यायनको एक नयी उपलब्धि है । सूत्रकारने हेतुका सामान्यलक्षण ही बतलाया है। पर वह इतना अपर्याप्त है कि उससे हेतुके सम्बन्धमें स्पष्टतः जानकारी नहीं हो पाती । भाष्यकारने हेतु-लक्षणको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है । उनका अभिमत है कि 'साध्यसाधनं हेतुः' तभी स्पष्ट हो सकता है जब साध्य (पक्ष) तथा उदाहरण में धर्म (पक्षधर्म हेतु) का प्रतिसन्धान कर उसमें साधनता बतलायी जाए। हेतु समान और असमान दोनों ही प्रकारके उदाहरण बतलाने पर साध्यका साधक होता है। यथा-न्यायसूत्रकारके प्रतिज्ञालक्षण' को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणस्वरूप कहे गये 'शब्दोऽनित्यः' को 'उत्पत्तिधर्मकत्वात' १२ हेतका प्रयोग करके सिद्ध किया गया है । तात्पर्य यह कि भाष्यकारने हेतुस्वरूपबोधक सूत्रकी उदाहरणद्वारा विशद व्याख्या तो की ही है, पर 'साध्ये १. न्यायभा०, ११११५, पृष्ठ २१ । २, ३, ४. वही, १।१।५, पृष्ठ २१, २२ । । ५. न्यायभा० १।११३२, पृष्ठ ४७ । ६. वही, १।१।३४, ३५, पृष्ठ ४८ । ७. वही, ११११३७, पृष्ठ ५०। ८. वही,१११।३७, पृष्ठ ५०। ९. न्यायसू० १।१।३४, ३५ । १०. 'उत्पत्तिधर्मकत्वात्' इति । उत्पत्तिधर्मकमनित्यं दृष्टमिति । -न्यायभा० १।१।३४, ३५, पृष्ठ ४८, ४९ । ११. साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा-न्यासू० १।१३३ । १२. न्यायभा० १।१।३३, ३५, पृष्ठ ४८, ४९ । - २४४ - Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org |Page Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42