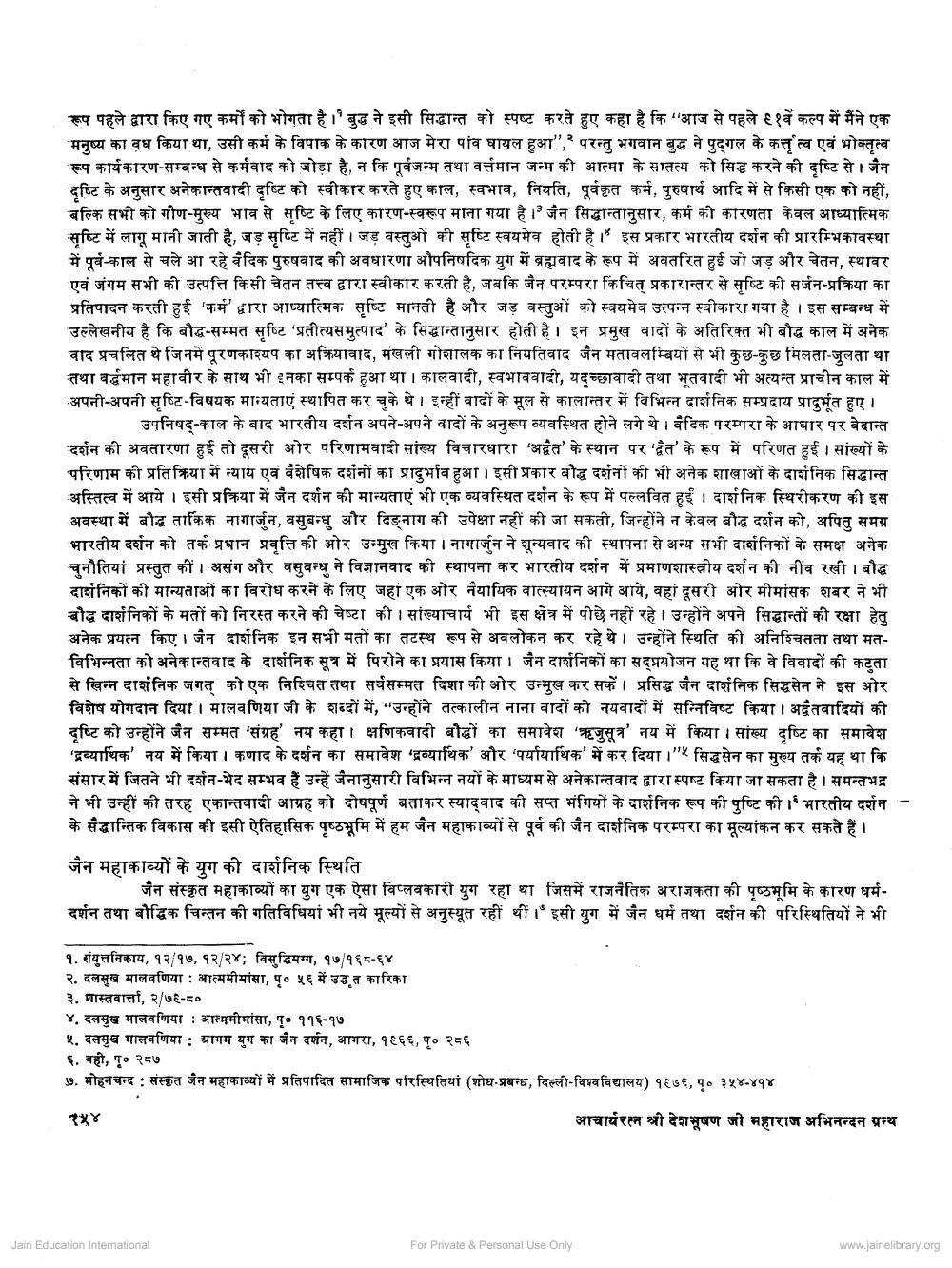Book Title: Bharatiya Darshan ke Sandarbh me jain Mahakavyo dwara Vivechit Author(s): Mohanchand Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 4
________________ रूप पहले द्वारा किए गए कर्मों को भोगता है।' बुद्ध ने इसी सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए कहा है कि "आज से पहले ६१वें कल्प में मैंने एक मनुष्य का वध किया था, उसी कर्म के विपाक के कारण आज मेरा पांव घायल हुआ", परन्तु भगवान बुद्ध ने पुद्गल के कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व रूप कार्यकारण-सम्बन्ध से कर्मवाद को जोड़ा है, न कि पूर्वजन्म तथा वर्तमान जन्म की आत्मा के सातत्य को सिद्ध करने की दृष्टि से। जैन दृष्टि के अनुसार अनेकान्तवादी दृष्टि को स्वीकार करते हुए काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत कर्म, पुरुषार्थ आदि में से किसी एक को नहीं, बल्कि सभी को गौण-मुख्य भाव से सृष्टि के लिए कारण-स्वरूप माना गया है। जैन सिद्धान्तानुसार, कर्म की कारणता केवल आध्यात्मिक सृष्टि में लागू मानी जाती है, जड़ सृष्टि में नहीं। जड़ बस्तुओं की सृष्टि स्वयमेव होती है। इस प्रकार भारतीय दर्शन की प्रारम्भिकावस्था में पूर्व-काल से चले आ रहे वैदिक पुरुषवाद की अवधारणा औपनिषदिक युग में ब्रह्मवाद के रूप में अवतरित हुई जो जड़ और चेतन, स्थावर एवं जंगम सभी की उत्पत्ति किसी चेतन तत्त्व द्वारा स्वीकार करती है, जबकि जैन परम्परा किंचित प्रकारान्तर से सृष्टि की सर्जन-प्रक्रिया का प्रतिपादन करती हुई 'कर्म' द्वारा आध्यात्मिक सृष्टि मानती है और जड़ वस्तुओं को स्वयमेव उत्पन्न स्वीकारा गया है । इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि बौद्ध-सम्मत सृष्टि 'प्रतीत्यसमुत्पाद' के सिद्धान्तानुसार होती है। इन प्रमुख वादों के अतिरिक्त भी बौद्ध काल में अनेक वाद प्रचलित थे जिनमें पूरणकाश्यप का अक्रियावाद, मंखली गोशालक का नियतिवाद जैन मतावलम्बियों से भी कुछ-कुछ मिलता-जुलता था तथा वर्द्धमान महावीर के साथ भी इनका सम्पर्क हुआ था । कालवादी, स्वभाववादी, यदृच्छावादी तथा भूतवादी भी अत्यन्त प्राचीन काल में अपनी-अपनी सृष्टि-विषयक मान्यताएं स्थापित कर चुके थे। इन्हीं वादों के मूल से कालान्तर में विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदाय प्रादुर्भत हुए। उपनिषद्-काल के बाद भारतीय दर्शन अपने-अपने वादों के अनुरूप व्यवस्थित होने लगे थे। वैदिक परम्परा के आधार पर वेदान्त दर्शन की अवतारणा हुई तो दूसरी ओर परिणामवादी सांख्य विचारधारा 'अद्वैत' के स्थान पर 'द्वैत' के रूप में परिणत हुई। सांख्यों के परिणाम की प्रतिक्रिया में न्याय एवं वैशेषिक दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार बौद्ध दर्शनों की भी अनेक शाखाओं के दार्शनिक सिद्धान्त अस्तित्व में आये । इसी प्रक्रिया में जैन दर्शन की मान्यताएं भी एक व्यवस्थित दर्शन के रूप में पल्लवित हुई । दार्शनिक स्थिरीकरण की इस अवस्था में बौद्ध तार्किक नागार्जुन, वसुबन्धु और दिङ्नाग की उपेक्षा नहीं की जा सकती, जिन्होंने न केवल बौद्ध दर्शन को, अपितु समग्र भारतीय दर्शन को तर्क-प्रधान प्रवृत्ति की ओर उन्मुख किया । नागार्जुन ने शून्यवाद की स्थापना से अन्य सभी दार्शनिकों के समक्ष अनेक चुनौतियां प्रस्तुत की। असंग और वसुबन्धु ने विज्ञानवाद की स्थापना कर भारतीय दर्शन में प्रमाणशास्त्रीय दर्शन की नींव रखी । बौद्ध दार्शनिकों की मान्यताओं का विरोध करने के लिए जहां एक ओर नैयायिक वात्स्यायन आगे आये, वहां दूसरी ओर मीमांसक शबर ने भी बौद्ध दार्शनिकों के मतों को निरस्त करने की चेष्टा की। सांख्याचार्य भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहे । उन्होंने अपने सिद्धान्तों की रक्षा हेतु अनेक प्रयत्न किए। जैन दार्शनिक इन सभी मतों का तटस्थ रूप से अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने स्थिति की अनिश्चितता तथा मतविभिन्नता को अनेकान्तवाद के दार्शनिक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। जैन दार्शनिकों का सद्प्रयोजन यह था कि वे विवादों की कटुता से खिन्न दार्शनिक जगत् को एक निश्चित तथा सर्वसम्मत दिशा की ओर उन्मुख कर सकें। प्रसिद्ध जैन दार्शनिक सिद्धसेन ने इस ओर विशेष योगदान दिया। मालवणिया जी के शब्दों में, "उन्होंने तत्कालीन नाना वादों को नयवादों में सन्निविष्ट किया। अद्वैतवादियों की दृष्टि को उन्होंने जैन सम्मत 'संग्रह' नय कहा। क्षणिकवादी बौद्धों का समावेश 'ऋजुसूत्र' नय में किया। सांख्य दृष्टि का समावेश 'द्रव्याथिक' नय में किया। कणाद के दर्शन का समावेश 'द्रव्यार्थिक' और 'पर्यायार्थिक' में कर दिया।"५ सिद्धसेन का मुख्य तर्क यह था कि संसार में जितने भी दर्शन-भेद सम्भव हैं उन्हें जैनानुसारी विभिन्न नयों के माध्यम से अनेकान्तवाद द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। समन्तभद्र ने भी उन्हीं की तरह एकान्तवादी आग्रह को दोषपूर्ण बताकर स्याद्वाद की सप्त भंगियों के दार्शनिक रूप की पुष्टि की। भारतीय दर्शन - के सैद्धान्तिक विकास की इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम जैन महाकाव्यों से पूर्व की जैन दार्शनिक परम्परा का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैन महाकाव्यों के युग की दार्शनिक स्थिति जैन संस्कृत महाकाव्यों का युग एक ऐसा विप्लवकारी युग रहा था जिसमें राजनैतिक अराजकता की पृष्ठभूमि के कारण धर्मदर्शन तथा बौद्धिक चिन्तन की गतिविधियां भी नये मूल्यों से अनुस्यूत रहीं थीं। इसी युग में जैन धर्म तथा दर्शन की परिस्थितियों ने भी १. संयुत्तनिकाय, १२/१७, १२/२४; विसुद्धिमग्ग, १७/१६८-६४ २. दलसुख मालवणिया : आत्ममीमांसा, पृ० ५६ में उद्ध त कारिका ३. शास्त्रवार्ता, २/७६-८० ४. दलसुख मालवणिया : आत्ममीमांसा, पृ० ११६-१७ ५. दलसुख मालवणिया : पागम युग का जैन दर्शन, आगरा, १९६६, पृ० २८६ ६. वही, पृ०२८७ ७. मोहनचन्द : संस्कृत जैन महाकाव्यों में प्रतिपादित सामाजिक परिस्थितियां (शोध-प्रबन्ध, दिल्ली विश्वविद्यालय) १९७६, पृ० ३५४-४१४ आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10