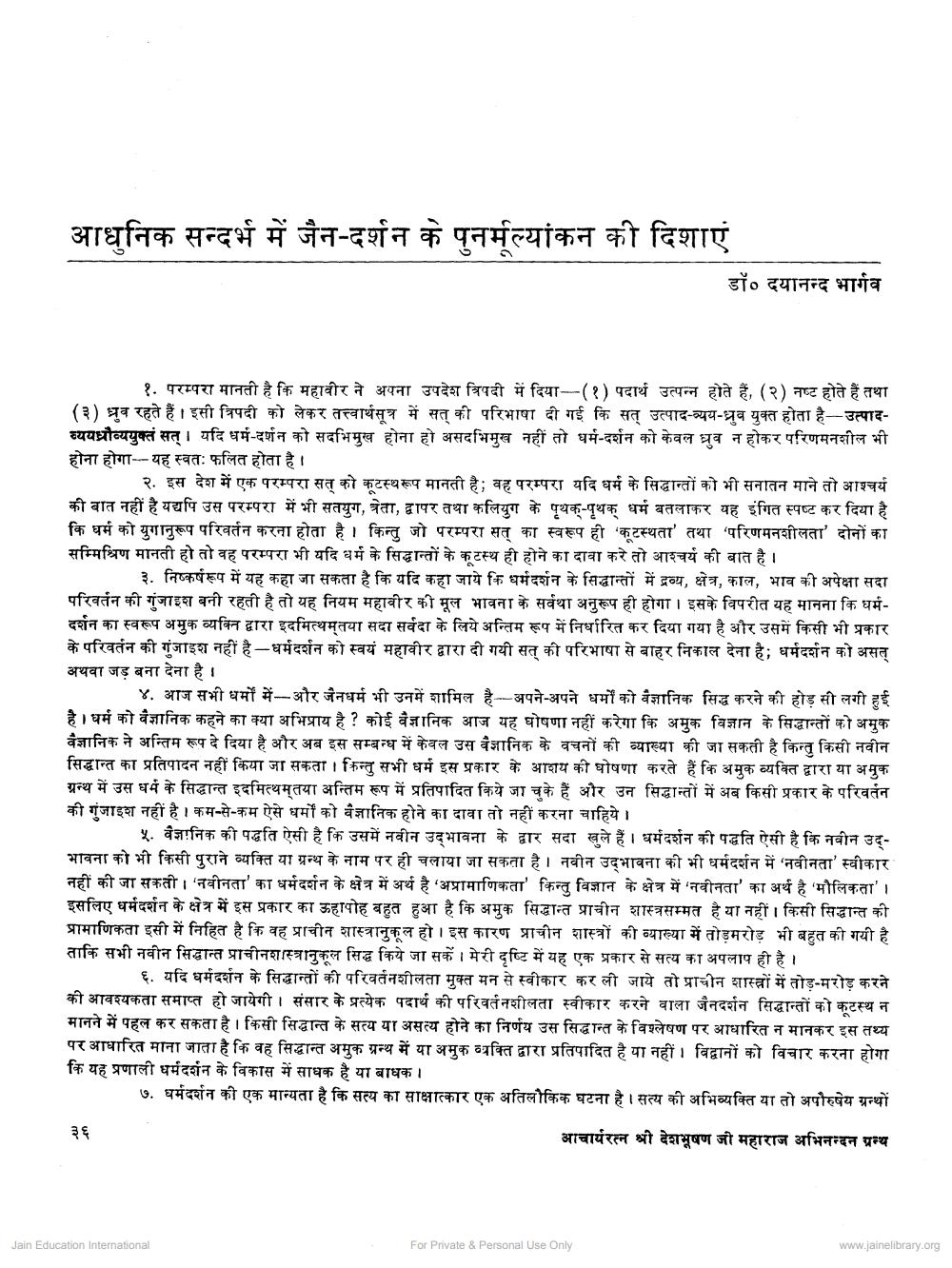Book Title: Adhunik Sandarbh me Jain Darshan ke Punarmulyankan ki Dishaye Author(s): Dayanand Bhargav Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 1
________________ आधनिक सन्दर्भ में जैन-दर्शन के पुनर्मल्यांकन की दिशाएं डॉ० दयानन्द भार्गव १. परम्परा मानती है कि महावीर ने अपना उपदेश त्रिपदी में दिया-(१) पदार्थ उत्पन्न होते हैं, (२) नष्ट होते हैं तथा (३) ध्रुव रहते हैं। इसी त्रिपदी को लेकर तत्त्वार्थसूत्र में सत् की परिभाषा दी गई कि सत् उत्पाद-व्यय-ध्रुव युक्त होता है-उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् । यदि धर्म-दर्शन को सदभिमुख होना हो असदभिमुख नहीं तो धर्म-दर्शन को केवल ध्रुव न होकर परिणमनशील भी होना होगा-यह स्वतः फलित होता है। २. इस देश में एक परम्परा सत् को कूटस्थ रूप मानती है; वह परम्परा यदि धर्म के सिद्धान्तों को भी सनातन माने तो आश्चर्य की बात नहीं है यद्यपि उस परम्परा में भी सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग के पृथक्-पृथक् धर्म बतलाकर यह इंगित स्पष्ट कर दिया है कि धर्म को युगानुरूप परिवर्तन करना होता है। किन्तु जो परम्परा सत् का स्वरूप ही 'कूटस्थता' तथा 'परिणमनशीलता' दोनों का सम्मिश्रिण मानती हो तो वह परम्परा भी यदि धर्म के सिद्धान्तों के कूटस्थ ही होने का दावा करे तो आश्चर्य की बात है। ३. निष्कर्षरूप में यह कहा जा सकता है कि यदि कहा जाये कि धर्मदर्शन के सिद्धान्तों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा सदा परिवर्तन की गुंजाइश बनी रहती है तो यह नियम महावीर की मूल भावना के सर्वथा अनुरूप ही होगा। इसके विपरीत यह मानना कि धर्मदर्शन का स्वरूप अमुक व्यक्ति द्वारा इदमित्थम्तया सदा सर्वदा के लिये अन्तिम रूप में निर्धारित कर दिया गया है और उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है -धर्मदर्शन को स्वयं महावीर द्वारा दी गयी सत् की परिभाषा से बाहर निकाल देना है; धर्मदर्शन को असत् अथवा जड़ बना देना है। ४. आज सभी धर्मों में-और जैनधर्म भी उनमें शामिल है-अपने-अपने धर्मों को वैज्ञानिक सिद्ध करने की होड़ सी लगी हुई है। धर्म को वैज्ञानिक कहने का क्या अभिप्राय है? कोई वैज्ञानिक आज यह घोषणा नहीं करेगा कि अमुक विज्ञान के सिद्धान्तों को अमुक वैज्ञानिक ने अन्तिम रूप दे दिया है और अब इस सम्बन्ध में केवल उस वैज्ञानिक के वचनों की व्याख्या की जा सकती है किन्तु किसी नवीन सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता । किन्तु सभी धर्म इस प्रकार के आशय की घोषणा करते हैं कि अमुक व्यक्ति द्वारा या अमुक ग्रन्थ में उस धर्म के सिद्धान्त इदमित्थम्तया अन्तिम रूप में प्रतिपादित किये जा चुके हैं और उन सिद्धान्तों में अब किसी प्रकार के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। कम-से-कम ऐसे धर्मों को वैज्ञानिक होने का दावा तो नहीं करना चाहिये। ५. वैज्ञानिक की पद्धति ऐसी है कि उसमें नवीन उद्भावना के द्वार सदा खुले हैं । धर्मदर्शन की पद्धति ऐसी है कि नवीन उद्भावना को भी किसी पुराने व्यक्ति या ग्रन्थ के नाम पर ही चलाया जा सकता है। नवीन उद्भावना की भी धर्मदर्शन में 'नवीनता' स्वीकार नहीं की जा सकती। 'नवीनता' का धर्मदर्शन के क्षेत्र में अर्थ है 'अप्रामाणिकता' किन्तु विज्ञान के क्षेत्र में 'नवीनता' का अर्थ है 'मौलिकता'। इसलिए धर्मदर्शन के क्षेत्र में इस प्रकार का ऊहापोह बहुत हुआ है कि अमुक सिद्धान्त प्राचीन शास्त्रसम्मत है या नहीं। किसी सिद्धान्त की प्रामाणिकता इसी में निहित है कि वह प्राचीन शास्त्रानुकूल हो । इस कारण प्राचीन शास्त्रों की व्याख्या में तोड़मरोड़ भी बहुत की गयी है ताकि सभी नवीन सिद्धान्त प्राचीनशास्त्रानुकूल सिद्ध किये जा सकें। मेरी दृष्टि में यह एक प्रकार से सत्य का अपलाप ही है। ६. यदि धर्मदर्शन के सिद्धान्तों की परिवर्तनशीलता मुक्त मन से स्वीकार कर ली जाये तो प्राचीन शास्त्रों में तोड़-मरोड़ करने की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी। संसार के प्रत्येक पदार्थ की परिवर्तनशीलता स्वीकार करने वाला जैनदर्शन सिद्धान्तों को कूटस्थ न मानने में पहल कर सकता है। किसी सिद्धान्त के सत्य या असत्य होने का निर्णय उस सिद्धान्त के विश्लेषण पर आधारित न मानकर इस तथ्य पर आधारित माना जाता है कि वह सिद्धान्त अमुक ग्रन्थ में या अमुक व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित है या नहीं। विद्वानों को विचार करना होगा कि यह प्रणाली धर्मदर्शन के विकास में साधक है या बाधक । ७. धर्मदर्शन की एक मान्यता है कि सत्य का साक्षात्कार एक अतिलौकिक घटना है। सत्य की अभिव्यक्ति या तो अपौरुषेय ग्रन्थों आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4