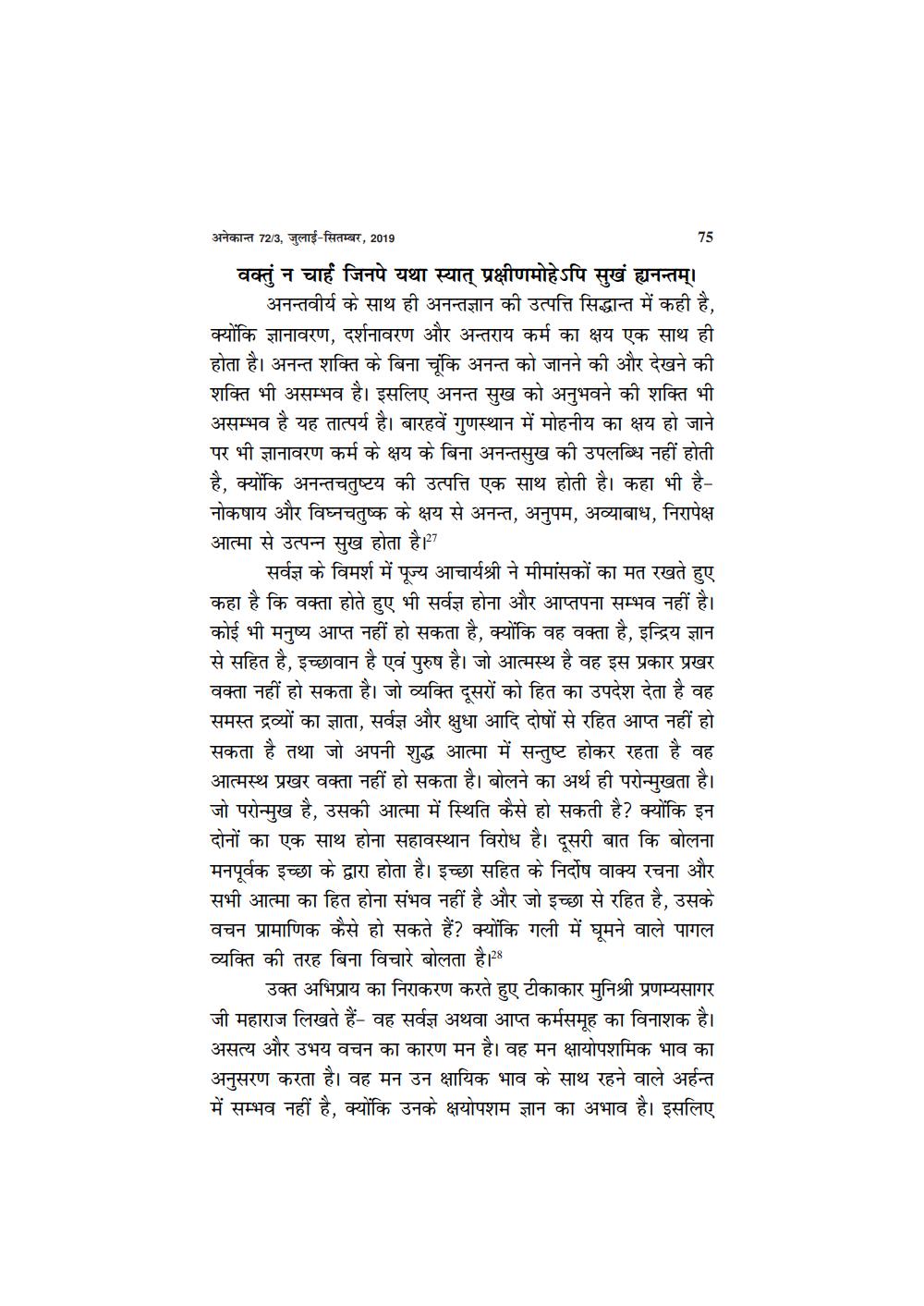________________
अनेकान्त 72/3, जुलाई-सितम्बर, 2019 वक्तुं न चाहं जिनपे यथा स्यात् प्रक्षीणमोहेऽपि सुखं ह्यनन्तम्।
अनन्तवीर्य के साथ ही अनन्तज्ञान की उत्पत्ति सिद्धान्त में कही है, क्योंकि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म का क्षय एक साथ ही होता है। अनन्त शक्ति के बिना चूंकि अनन्त को जानने की और देखने की शक्ति भी असम्भव है। इसलिए अनन्त सुख को अनुभवने की शक्ति भी असम्भव है यह तात्पर्य है। बारहवें गुणस्थान में मोहनीय का क्षय हो जाने पर भी ज्ञानावरण कर्म के क्षय के बिना अनन्तसुख की उपलब्धि नहीं होती है, क्योंकि अनन्तचतुष्टय की उत्पत्ति एक साथ होती है। कहा भी हैनोकषाय और विघ्नचतुष्क के क्षय से अनन्त, अनुपम, अव्याबाध, निरापेक्ष आत्मा से उत्पन्न सुख होता है।
सर्वज्ञ के विमर्श में पूज्य आचार्यश्री ने मीमांसकों का मत रखते हुए कहा है कि वक्ता होते हुए भी सर्वज्ञ होना और आप्तपना सम्भव नहीं है। कोई भी मनुष्य आप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वह वक्ता है, इन्द्रिय ज्ञान से सहित है, इच्छावान है एवं पुरुष है। जो आत्मस्थ है वह इस प्रकार प्रखर वक्ता नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति दूसरों को हित का उपदेश देता है वह समस्त द्रव्यों का ज्ञाता, सर्वज्ञ और क्षुधा आदि दोषों से रहित आप्त नहीं हो सकता है तथा जो अपनी शुद्ध आत्मा में सन्तुष्ट होकर रहता है वह आत्मस्थ प्रखर वक्ता नहीं हो सकता है। बोलने का अर्थ ही परोन्मुखता है। जो परोन्मुख है, उसकी आत्मा में स्थिति कैसे हो सकती है? क्योंकि इन दोनों का एक साथ होना सहावस्थान विरोध है। दूसरी बात कि बोलना मनपूर्वक इच्छा के द्वारा होता है। इच्छा सहित के निर्दोष वाक्य रचना और सभी आत्मा का हित होना संभव नहीं है और जो इच्छा से रहित है, उसके वचन प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि गली में घूमने वाले पागल व्यक्ति की तरह बिना विचारे बोलता है।
उक्त अभिप्राय का निराकरण करते हुए टीकाकार मुनिश्री प्रणम्यसागर जी महाराज लिखते हैं- वह सर्वज्ञ अथवा आप्त कर्मसमूह का विनाशक है। असत्य और उभय वचन का कारण मन है। वह मन क्षायोपशमिक भाव का अनुसरण करता है। वह मन उन क्षायिक भाव के साथ रहने वाले अर्हन्त में सम्भव नहीं है, क्योंकि उनके क्षयोपशम ज्ञान का अभाव है। इसलिए