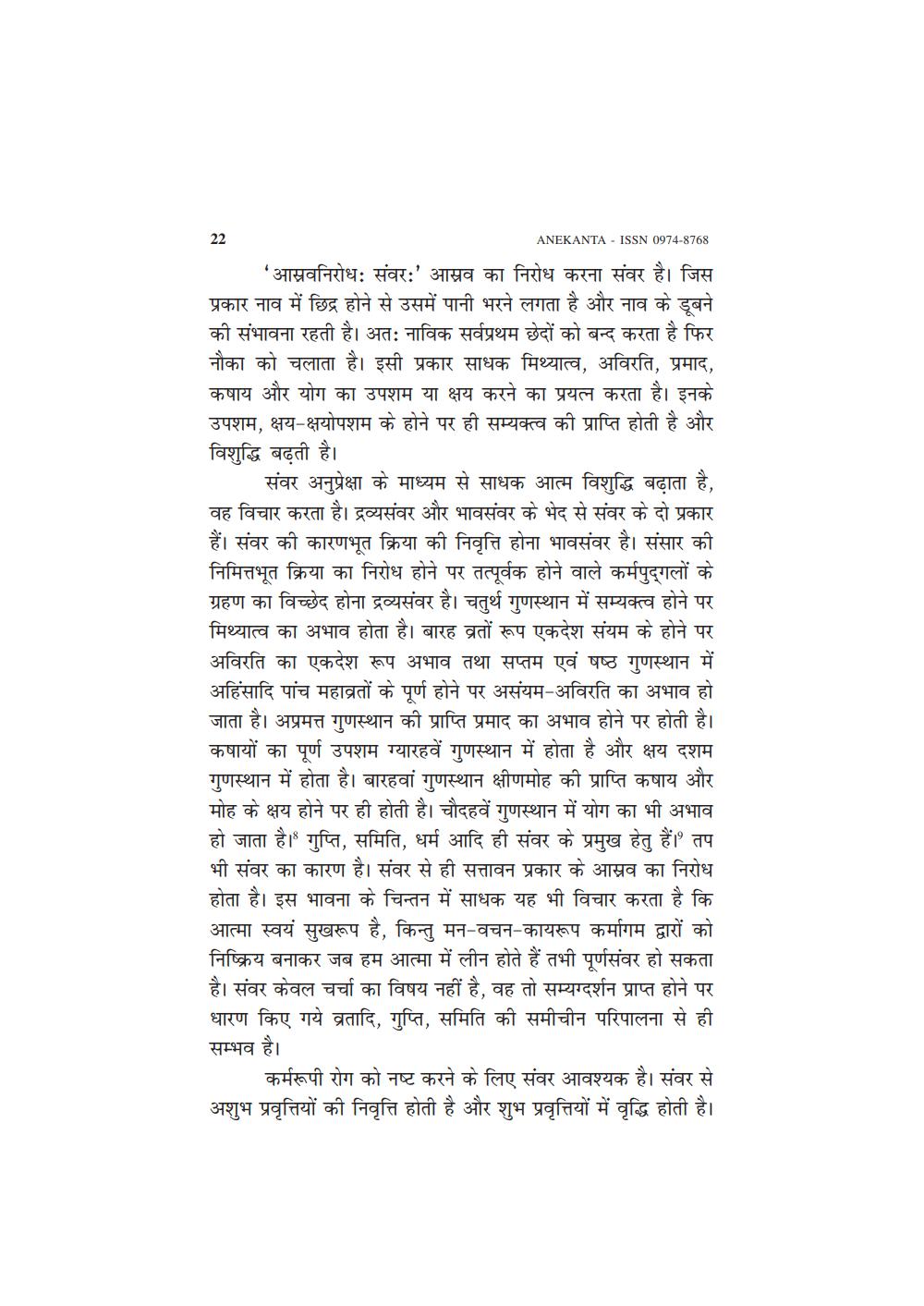________________
ANEKANTA - ISSN 0974-8768
'आस्रवनिरोधः संवरः' आस्रव का निरोध करना संवर है। जिस प्रकार नाव में छिद्र होने से उसमें पानी भरने लगता है और नाव के डूबने की संभावना रहती है। अतः नाविक सर्वप्रथम छेदों को बन्द करता है फिर नौका को चलाता है। इसी प्रकार साधक मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग का उपशम या क्षय करने का प्रयत्न करता है। इनके उपशम, क्षय-क्षयोपशम के होने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और विशुद्धि बढ़ती है।
संवर अनुप्रेक्षा के माध्यम से साधक आत्म विशुद्धि बढ़ाता है, वह विचार करता है। द्रव्यसंवर और भावसंवर के भेद से संवर के दो प्रकार हैं। संवर की कारणभूत क्रिया की निवृत्ति होना भावसंवर है। संसार की निमित्तभूत क्रिया का निरोध होने पर तत्पूर्वक होने वाले कर्मपुद्गलों के ग्रहण का विच्छेद होना द्रव्यसंवर है। चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त्व होने पर मिथ्यात्व का अभाव होता है। बारह व्रतों रूप एकदेश संयम के होने पर अविरति का एकदेश रूप अभाव तथा सप्तम एवं षष्ठ गुणस्थान में अहिंसादि पांच महाव्रतों के पूर्ण होने पर असंयम-अविरति का अभाव हो जाता है। अप्रमत्त गुणस्थान की प्राप्ति प्रमाद का अभाव होने पर होती है। कषायों का पूर्ण उपशम ग्यारहवें गुणस्थान में होता है और क्षय दशम गुणस्थान में होता है। बारहवां गुणस्थान क्षीणमोह की प्राप्ति कषाय और मोह के क्षय होने पर ही होती है। चौदहवें गणस्थान में योग का भी अभाव हो जाता है। गुप्ति, समिति, धर्म आदि ही संवर के प्रमुख हेतु हैं। तप भी संवर का कारण है। संवर से ही सत्तावन प्रकार के आस्रव का निरोध होता है। इस भावना के चिन्तन में साधक यह भी विचार करता है कि
आत्मा स्वयं सुखरूप है, किन्तु मन-वचन-कायरूप कर्मागम द्वारों को निष्क्रिय बनाकर जब हम आत्मा में लीन होते हैं तभी पूर्णसंवर हो सकता है। संवर केवल चर्चा का विषय नहीं है, वह तो सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर धारण किए गये व्रतादि, गुप्ति, समिति की समीचीन परिपालना से ही सम्भव है।
कर्मरूपी रोग को नष्ट करने के लिए संवर आवश्यक है। संवर से अशुभ प्रवृत्तियों की निवृत्ति होती है और शुभ प्रवृत्तियों में वृद्धि होती है।