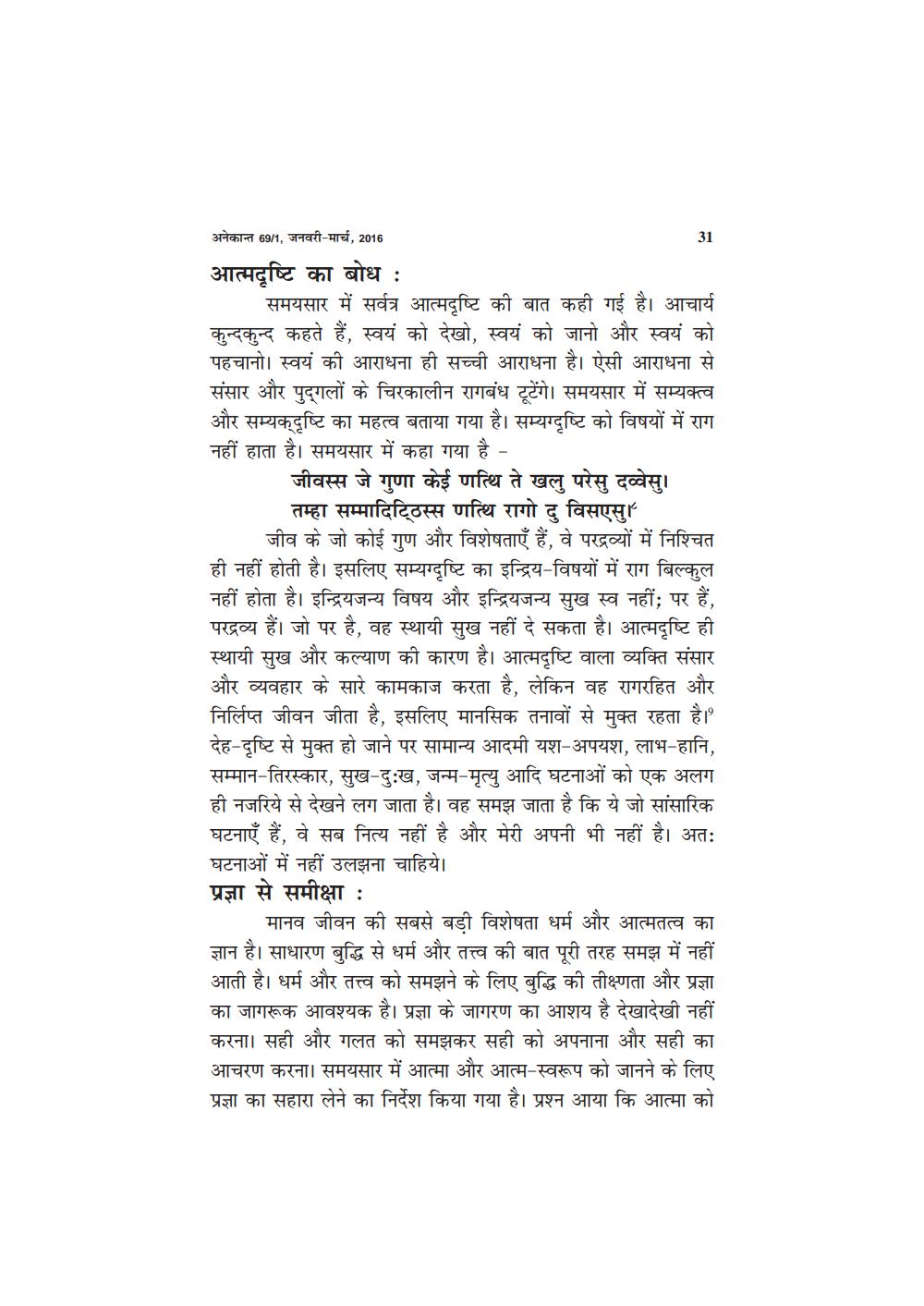________________
अनेकान्त 69/1, जनवरी-मार्च, 2016 आत्मदृष्टि का बोध :
समयसार में सर्वत्र आत्मदृष्टि की बात कही गई है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं, स्वयं को देखो, स्वयं को जानो और स्वयं को पहचानो। स्वयं की आराधना ही सच्ची आराधना है। ऐसी आराधना से संसार और पुद्गलों के चिरकालीन रागबंध टूटेंगे। समयसार में सम्यक्त्व और सम्यक्दृष्टि का महत्व बताया गया है। सम्यग्दृष्टि को विषयों में राग नहीं हाता है। समयसार में कहा गया है -
जीवस्स जे गुणा केई णत्थि ते खलु परेसु दव्वेसु। __तम्हा सम्मादिट्ठिस्स णत्थि रागो दु विसएसु।
जीव के जो कोई गुण और विशेषताएँ हैं, वे परद्रव्यों में निश्चित ही नहीं होती है। इसलिए सम्यग्दष्टि का इन्द्रिय-विषयों में राग बिल्कल नहीं होता है। इन्द्रियजन्य विषय और इन्द्रियजन्य सुख स्व नहीं; पर हैं, परद्रव्य हैं। जो पर है, वह स्थायी सुख नहीं दे सकता है। आत्मदृष्टि ही स्थायी सुख और कल्याण की कारण है। आत्मदृष्टि वाला व्यक्ति संसार
और व्यवहार के सारे कामकाज करता है, लेकिन वह रागरहित और निर्लिप्त जीवन जीता है, इसलिए मानसिक तनावों से मुक्त रहता है।' देह-दृष्टि से मुक्त हो जाने पर सामान्य आदमी यश-अपयश, लाभ-हानि, सम्मान-तिरस्कार, सुख-दु:ख, जन्म-मृत्यु आदि घटनाओं को एक अलग ही नजरिये से देखने लग जाता है। वह समझ जाता है कि ये जो सांसारिक घटनाएँ हैं, वे सब नित्य नहीं है और मेरी अपनी भी नहीं है। अतः घटनाओं में नहीं उलझना चाहिये। प्रज्ञा से समीक्षा :
मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता धर्म और आत्मतत्व का ज्ञान है। साधारण बुद्धि से धर्म और तत्त्व की बात पूरी तरह समझ में नहीं आती है। धर्म और तत्त्व को समझने के लिए बुद्धि की तीक्ष्णता और प्रज्ञा का जागरूक आवश्यक है। प्रज्ञा के जागरण का आशय है देखादेखी नहीं करना। सही और गलत को समझकर सही को अपनाना और सही का आचरण करना। समयसार में आत्मा और आत्म-स्वरूप को जानने के लिए प्रज्ञा का सहारा लेने का निर्देश किया गया है। प्रश्न आया कि आत्मा को