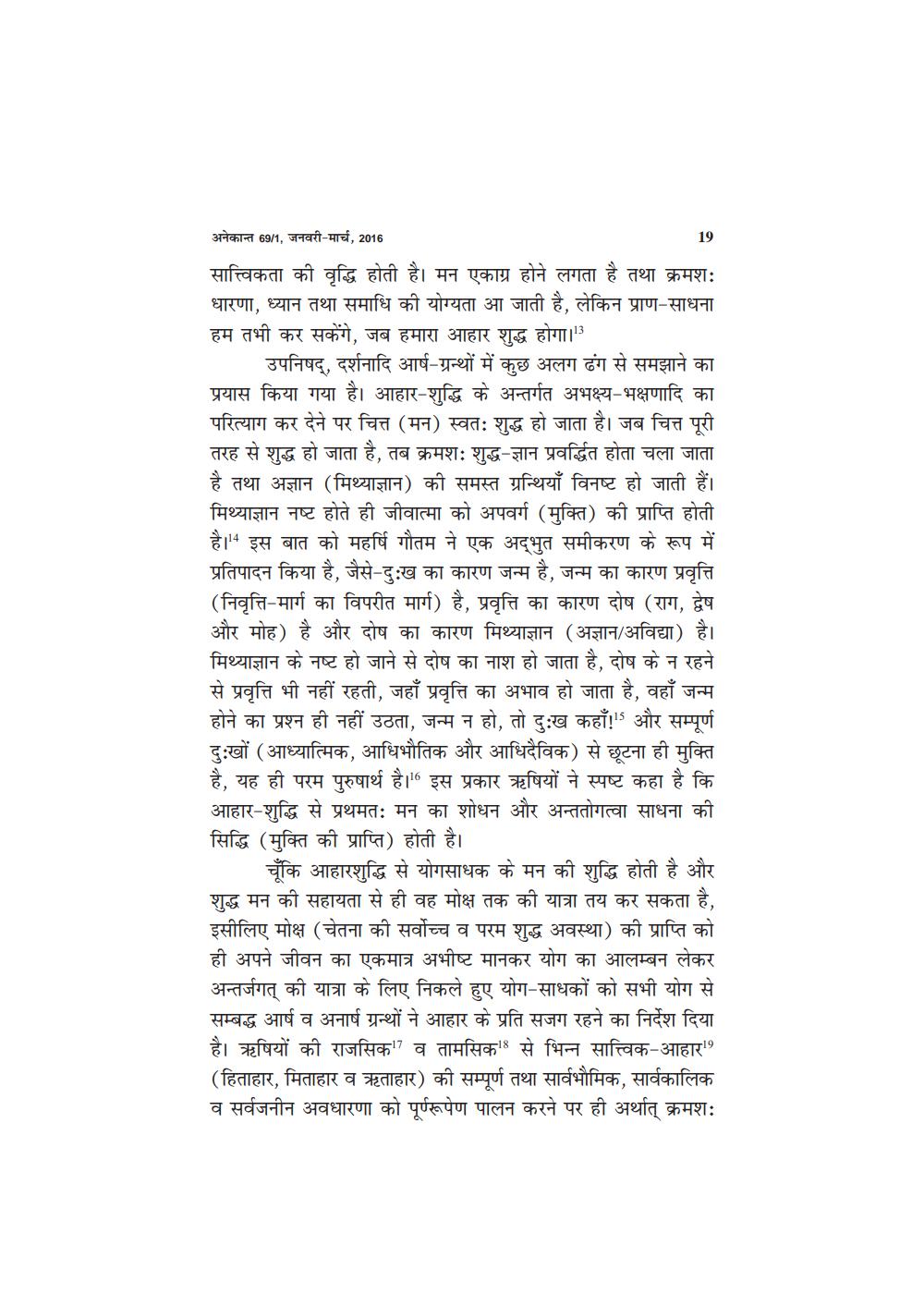________________
अनेकान्त 69/1, जनवरी-मार्च, 2016
19
सात्त्विकता की वृद्धि होती है। मन एकाग्र होने लगता है तथा क्रमशः धारणा, ध्यान तथा समाधि की योग्यता आ जाती है, लेकिन प्राण-साधना हम तभी कर सकेंगे, जब हमारा आहार शुद्ध होगा।
उपनिषद्, दर्शनादि आर्ष-ग्रन्थों में कुछ अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। आहार-शुद्धि के अन्तर्गत अभक्ष्य-भक्षणादि का परित्याग कर देने पर चित्त (मन) स्वतः शुद्ध हो जाता है। जब चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब क्रमशः शुद्ध-ज्ञान प्रवर्द्धित होता चला जाता है तथा अज्ञान (मिथ्याज्ञान) की समस्त ग्रन्थियाँ विनष्ट हो जाती हैं। मिथ्याज्ञान नष्ट होते ही जीवात्मा को अपवर्ग (मुक्ति) की प्राप्ति होती है। इस बात को महर्षि गौतम ने एक अद्भुत समीकरण के रूप में प्रतिपादन किया है, जैसे-दु:ख का कारण जन्म है, जन्म का कारण प्रवृत्ति (निवृत्ति-मार्ग का विपरीत मार्ग) है, प्रवृत्ति का कारण दोष (राग, द्वेष
और मोह) है और दोष का कारण मिथ्याज्ञान (अज्ञान/अविद्या) है। मिथ्याज्ञान के नष्ट हो जाने से दोष का नाश हो जाता है, दोष के न रहने से प्रवृत्ति भी नहीं रहती, जहाँ प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है, वहाँ जन्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता, जन्म न हो, तो दुःख कहाँ! और सम्पूर्ण दु:खों (आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक) से छूटना ही मुक्ति है, यह ही परम पुरुषार्थ है।" इस प्रकार ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि आहार-शुद्धि से प्रथमतः मन का शोधन और अन्ततोगत्वा साधना की सिद्धि (मुक्ति की प्राप्ति) होती है।
चूँकि आहारशुद्धि से योगसाधक के मन की शुद्धि होती है और शुद्ध मन की सहायता से ही वह मोक्ष तक की यात्रा तय कर सकता है, इसीलिए मोक्ष (चेतना की सर्वोच्च व परम शुद्ध अवस्था) की प्राप्ति को ही अपने जीवन का एकमात्र अभीष्ट मानकर योग का आलम्बन लेकर अन्तर्जगत् की यात्रा के लिए निकले हुए योग-साधकों को सभी योग से सम्बद्ध आर्ष व अनार्ष ग्रन्थों ने आहार के प्रति सजग रहने का निर्देश दिया है। ऋषियों की राजसिक'7 व तामसिक' से भिन्न सात्त्विक-आहार (हिताहार, मिताहार व ऋताहार) की सम्पूर्ण तथा सार्वभौमिक, सार्वकालिक व सर्वजनीन अवधारणा को पूर्णरूपेण पालन करने पर ही अर्थात् क्रमशः