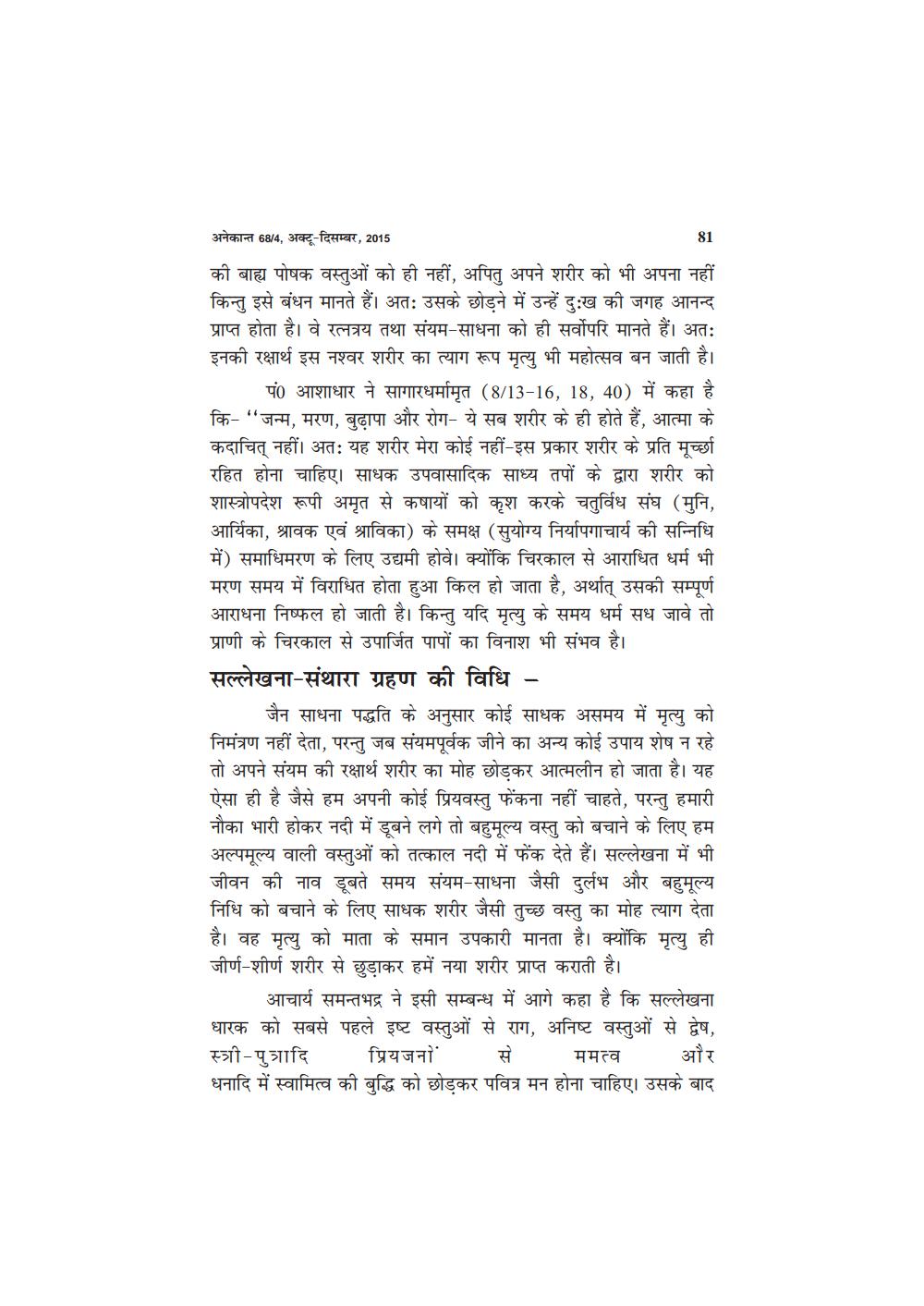________________
81
अनेकान्त 68/4, अक्टू-दिसम्बर, 2015 की बाह्य पोषक वस्तुओं को ही नहीं, अपितु अपने शरीर को भी अपना नहीं किन्तु इसे बंधन मानते हैं। अत: उसके छोड़ने में उन्हें दुःख की जगह आनन्द प्राप्त होता है। वे रत्नत्रय तथा संयम-साधना को ही सर्वोपरि मानते हैं। अतः इनकी रक्षार्थ इस नश्वर शरीर का त्याग रूप मृत्यु भी महोत्सव बन जाती है।
पं0 आशाधार ने सागारधर्मामृत (8/13-16, 18, 40) में कहा है कि- "जन्म, मरण, बुढ़ापा और रोग- ये सब शरीर के ही होते हैं, आत्मा के कदाचित् नहीं। अतः यह शरीर मेरा कोई नहीं-इस प्रकार शरीर के प्रति मूर्छा रहित होना चाहिए। साधक उपवासादिक साध्य तपों के द्वारा शरीर को शास्त्रोपदेश रूपी अमृत से कषायों को कृश करके चतुर्विध संघ (मुनि, आर्यिका, श्रावक एवं श्राविका) के समक्ष (सुयोग्य निर्यापगाचार्य की सन्निधि में) समाधिमरण के लिए उद्यमी होवे। क्योंकि चिरकाल से आराधित धर्म भी मरण समय में विराधित होता हुआ किल हो जाता है, अर्थात् उसकी सम्पूर्ण आराधना निष्फल हो जाती है। किन्तु यदि मृत्यु के समय धर्म सध जावे तो प्राणी के चिरकाल से उपार्जित पापों का विनाश भी संभव है। सल्लेखना-संथारा ग्रहण की विधि -
जैन साधना पद्धति के अनुसार कोई साधक असमय में मृत्यु को निमंत्रण नहीं देता, परन्तु जब संयमपूर्वक जीने का अन्य कोई उपाय शेष न रहे तो अपने संयम की रक्षार्थ शरीर का मोह छोड़कर आत्मलीन हो जाता है। यह ऐसा ही है जैसे हम अपनी कोई प्रियवस्तु फेंकना नहीं चाहते, परन्तु हमारी नौका भारी होकर नदी में डूबने लगे तो बहुमूल्य वस्तु को बचाने के लिए हम अल्पमूल्य वाली वस्तुओं को तत्काल नदी में फेंक देते हैं। सल्लेखना में भी जीवन की नाव डूबते समय संयम-साधना जैसी दुर्लभ और बहुमूल्य निधि को बचाने के लिए साधक शरीर जैसी तुच्छ वस्तु का मोह त्याग देता है। वह मृत्यु को माता के समान उपकारी मानता है। क्योंकि मृत्यु ही जीर्ण-शीर्ण शरीर से छुडाकर हमें नया शरीर प्राप्त कराती है।
आचार्य समन्तभद्र ने इसी सम्बन्ध में आगे कहा है कि सल्लेखना धारक को सबसे पहले इष्ट वस्तुओं से राग, अनिष्ट वस्तुओं से द्वेष, स्त्री-पुत्रादि प्रियजनों से ममत्व और धनादि में स्वामित्व की बुद्धि को छोड़कर पवित्र मन होना चाहिए। उसके बाद