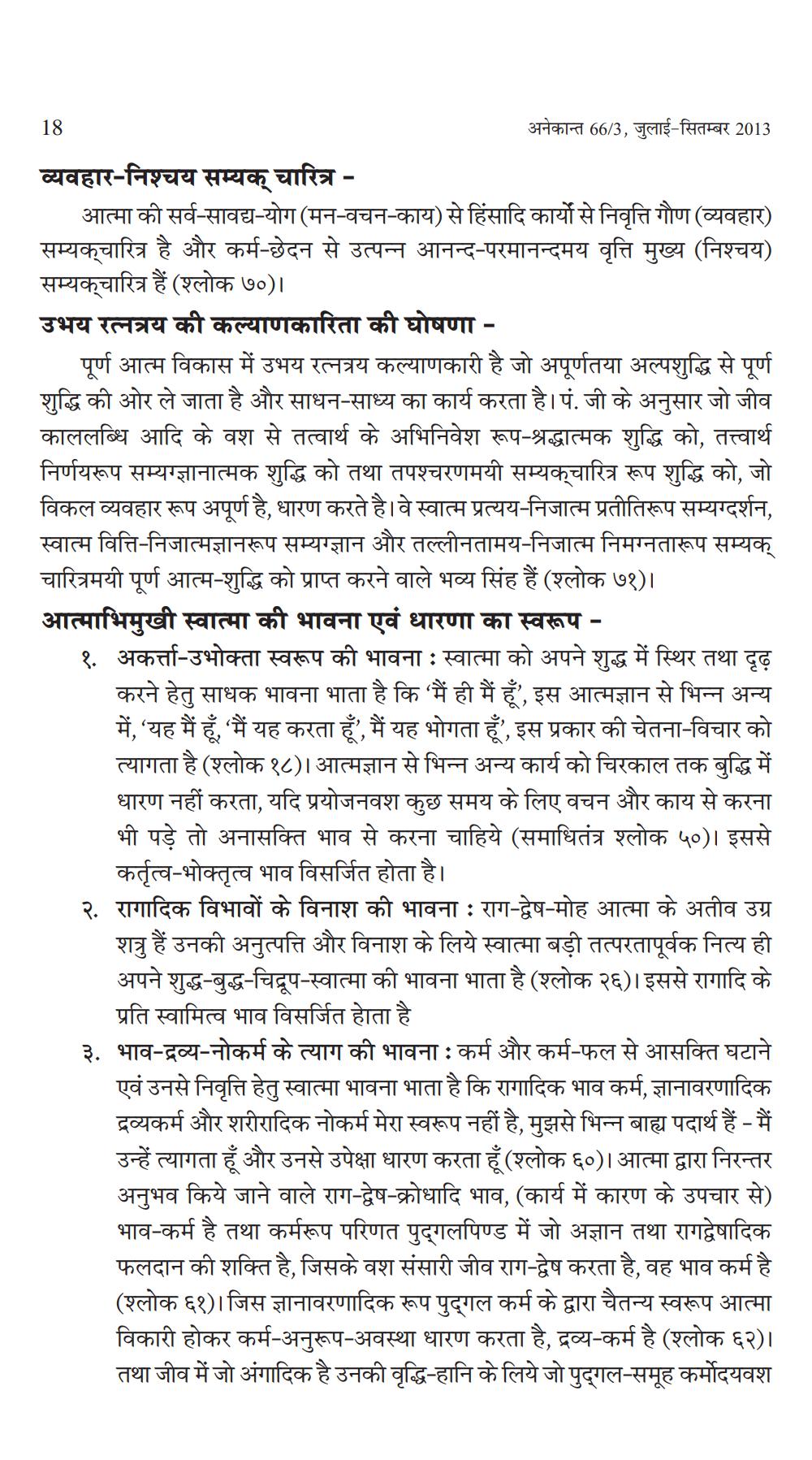________________
18
अनेकान्त 66/3, जुलाई-सितम्बर 2013
व्यवहार-निश्चय सम्यक् चारित्र -
आत्मा की सर्व-सावद्य-योग (मन-वचन-काय) से हिंसादि कार्यों से निवृत्ति गौण (व्यवहार) सम्यक्चारित्र है और कर्म-छेदन से उत्पन्न आनन्द-परमानन्दमय वृत्ति मुख्य (निश्चय) सम्यक्चारित्र हैं (श्लोक ७०)। उभय रत्नत्रय की कल्याणकारिता की घोषणा - __ पूर्ण आत्म विकास में उभय रत्नत्रय कल्याणकारी है जो अपूर्णतया अल्पशुद्धि से पूर्ण शुद्धि की ओर ले जाता है और साधन-साध्य का कार्य करता है। पं. जी के अनुसार जो जीव काललब्धि आदि के वश से तत्वार्थ के अभिनिवेश रूप-श्रद्धात्मक शुद्धि को, तत्त्वार्थ निर्णयरूप सम्यग्ज्ञानात्मक शुद्धि को तथा तपश्चरणमयी सम्यक्चारित्र रूप शुद्धि को, जो विकल व्यवहार रूप अपूर्ण है, धारण करते है। वे स्वात्म प्रत्यय-निजात्म प्रतीतिरूप सम्यग्दर्शन, स्वात्म वित्ति-निजात्मज्ञानरूप सम्यग्ज्ञान और तल्लीनतामय-निजात्म निमग्नतारूप सम्यक् चारित्रमयी पूर्ण आत्म-शुद्धि को प्राप्त करने वाले भव्य सिंह हैं (श्लोक ७१)। आत्माभिमुखी स्वात्मा की भावना एवं धारणा का स्वरूप - १. अकर्ता-उभोक्ता स्वरूप की भावना : स्वात्मा को अपने शुद्ध में स्थिर तथा दृढ़
करने हेतु साधक भावना भाता है कि 'मैं ही मैं हूँ', इस आत्मज्ञान से भिन्न अन्य में, 'यह मैं हूँ, मैं यह करता हूँ', मैं यह भोगता हूँ', इस प्रकार की चेतना-विचार को त्यागता है (श्लोक १८)। आत्मज्ञान से भिन्न अन्य कार्य को चिरकाल तक बुद्धि में धारण नहीं करता, यदि प्रयोजनवश कुछ समय के लिए वचन और काय से करना भी पड़े तो अनासक्ति भाव से करना चाहिये (समाधितंत्र श्लोक ५०)। इससे
कर्तृत्व-भोक्तृत्व भाव विसर्जित होता है। २. रागादिक विभावों के विनाश की भावना : राग-द्वेष-मोह आत्मा के अतीव उग्र
शत्रु हैं उनकी अनुत्पत्ति और विनाश के लिये स्वात्मा बड़ी तत्परतापूर्वक नित्य ही अपने शुद्ध-बुद्ध-चिद्रूप-स्वात्मा की भावना भाता है (श्लोक २६)। इससे रागादि के
प्रति स्वामित्व भाव विसर्जित होता है । ३. भाव-द्रव्य-नोकर्म के त्याग की भावना : कर्म और कर्म-फल से आसक्ति घटाने
एवं उनसे निवृत्ति हेतु स्वात्मा भावना भाता है कि रागादिक भाव कर्म, ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्म और शरीरादिक नोकर्म मेरा स्वरूप नहीं है, मुझसे भिन्न बाह्य पदार्थ हैं - मैं उन्हें त्यागता हूँ और उनसे उपेक्षा धारण करता हूँ (श्लोक ६०)। आत्मा द्वारा निरन्तर अनुभव किये जाने वाले राग-द्वेष-क्रोधादि भाव, (कार्य में कारण के उपचार से) भाव-कर्म है तथा कर्मरूप परिणत पुद्गलपिण्ड में जो अज्ञान तथा रागद्वेषादिक फलदान की शक्ति है, जिसके वश संसारी जीव राग-द्वेष करता है, वह भाव कर्म है (श्लोक ६१)। जिस ज्ञानावरणादिक रूप पुद्गल कर्म के द्वारा चैतन्य स्वरूप आत्मा विकारी होकर कर्म-अनुरूप-अवस्था धारण करता है, द्रव्य-कर्म है (श्लोक ६२)। तथा जीव में जो अंगादिक है उनकी वृद्धि-हानि के लिये जो पुद्गल-समूह कर्मोदयवश