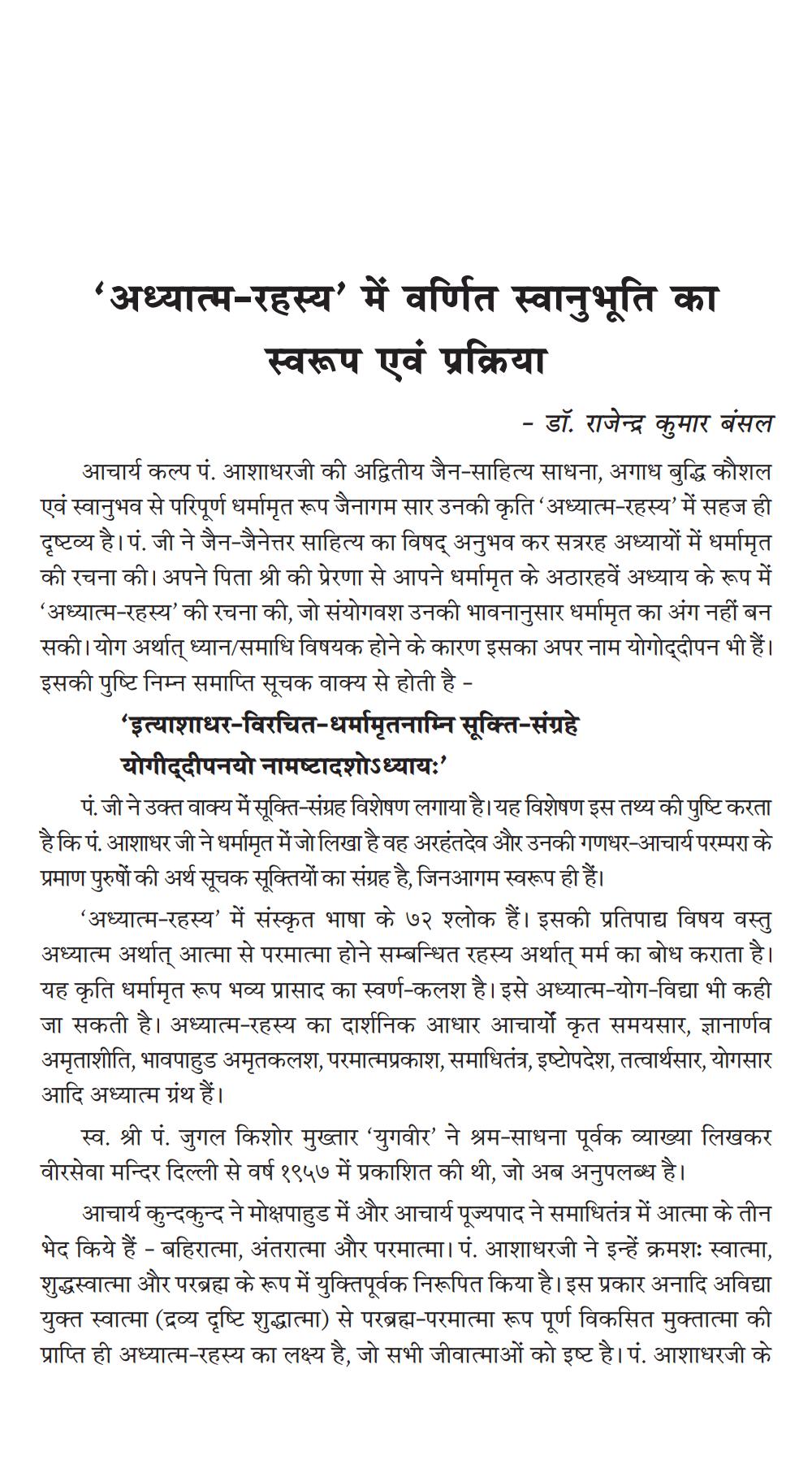________________
'अध्यात्म-रहस्य' में वर्णित स्वानुभूति का स्वरूप एवं प्रक्रिया
___- डॉ. राजेन्द्र कुमार बंसल आचार्य कल्प पं. आशाधरजी की अद्वितीय जैन-साहित्य साधना, अगाध बुद्धि कौशल एवं स्वानुभव से परिपूर्ण धर्मामृत रूप जैनागम सार उनकी कृति 'अध्यात्म-रहस्य' में सहज ही दृष्टव्य है। पं. जी ने जैन-जैनेत्तर साहित्य का विषद् अनुभव कर सत्ररह अध्यायों में धर्मामृत की रचना की। अपने पिता श्री की प्रेरणा से आपने धर्मामृत के अठारहवें अध्याय के रूप में 'अध्यात्म-रहस्य' की रचना की, जो संयोगवश उनकी भावनानुसार धर्मामृत का अंग नहीं बन सकी। योग अर्थात् ध्यान/समाधि विषयक होने के कारण इसका अपर नाम योगोद्दीपन भी हैं। इसकी पुष्टि निम्न समाप्ति सूचक वाक्य से होती है -
'इत्याशाधर-विरचित-धर्मामृतनाम्नि सूक्ति-संग्रहे
योगीद्दीपनयो नामष्टादशोऽध्यायः' पं.जी ने उक्त वाक्य में सूक्ति-संग्रह विशेषण लगाया है। यह विशेषण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि पं. आशाधर जी ने धर्मामृत में जो लिखा है वह अरहंतदेव और उनकी गणधर-आचार्य परम्परा के प्रमाण पुरुषों की अर्थ सूचक सूक्तियों का संग्रह है, जिनआगम स्वरूप ही हैं। ___ 'अध्यात्म-रहस्य' में संस्कृत भाषा के ७२ श्लोक हैं। इसकी प्रतिपाद्य विषय वस्तु अध्यात्म अर्थात् आत्मा से परमात्मा होने सम्बन्धित रहस्य अर्थात् मर्म का बोध कराता है। यह कृति धर्मामृत रूप भव्य प्रासाद का स्वर्ण-कलश है। इसे अध्यात्म-योग-विद्या भी कही जा सकती है। अध्यात्म-रहस्य का दार्शनिक आधार आचार्यों कृत समयसार, ज्ञानार्णव अमृताशीति, भावपाहुड अमृतकलश, परमात्मप्रकाश, समाधितंत्र, इष्टोपदेश, तत्वार्थसार, योगसार आदि अध्यात्म ग्रंथ हैं।
स्व. श्री पं. जुगल किशोर मुख्तार 'युगवीर' ने श्रम-साधना पूर्वक व्याख्या लिखकर वीरसेवा मन्दिर दिल्ली से वर्ष १९५७ में प्रकाशित की थी, जो अब अनुपलब्ध है। __ आचार्य कुन्दकुन्द ने मोक्षपाहुड में और आचार्य पूज्यपाद ने समाधितंत्र में आत्मा के तीन भेद किये हैं - बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। पं. आशाधरजी ने इन्हें क्रमशः स्वात्मा, शुद्धस्वात्मा और परब्रह्म के रूप में युक्तिपूर्वक निरूपित किया है। इस प्रकार अनादि अविद्या युक्त स्वात्मा (द्रव्य दृष्टि शुद्धात्मा) से परब्रह्म-परमात्मा रूप पूर्ण विकसित मुक्तात्मा की प्राप्ति ही अध्यात्म-रहस्य का लक्ष्य है, जो सभी जीवात्माओं को इष्ट है। पं. आशाधरजी के