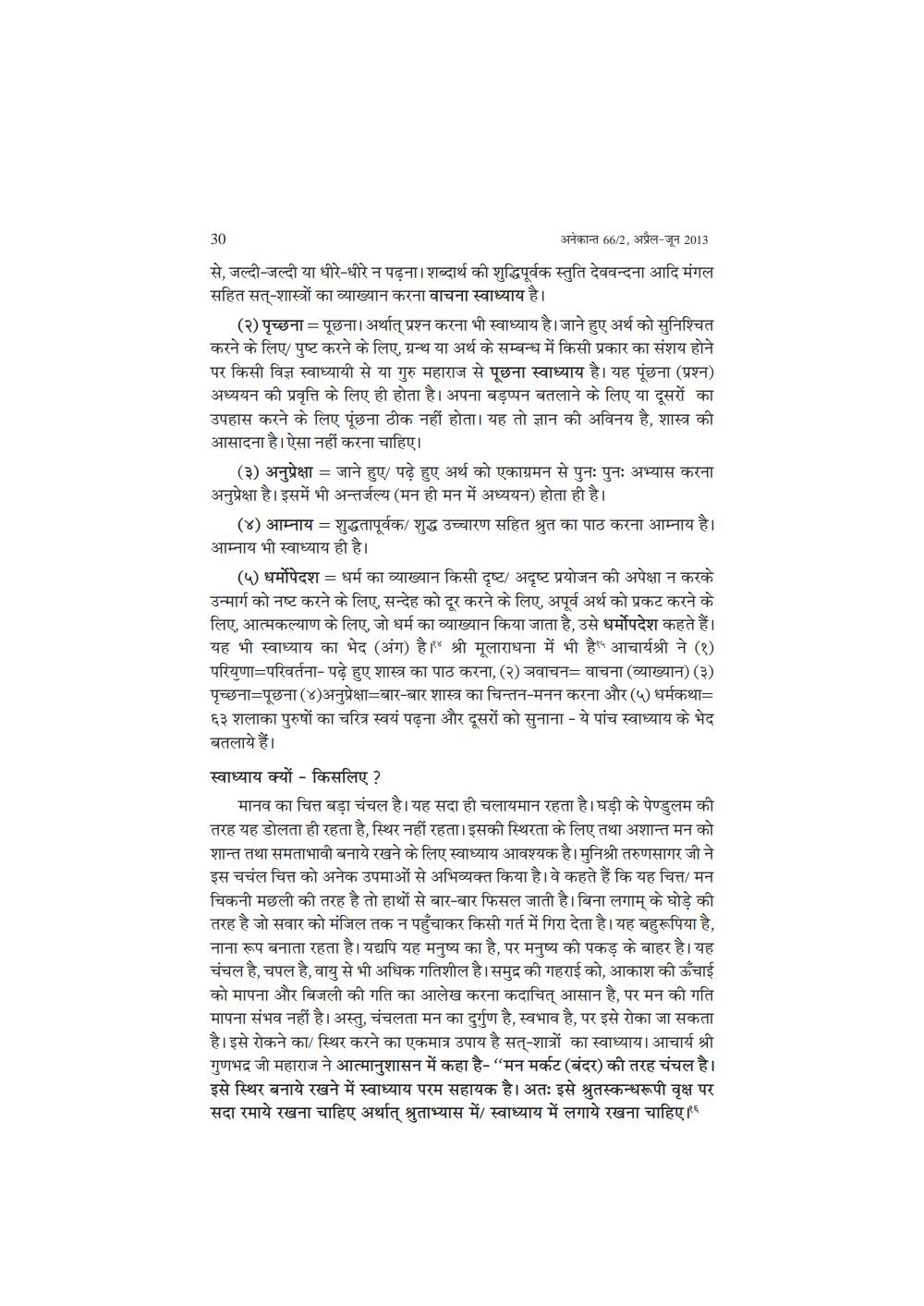________________
30
अनेकान्त 66/2, अप्रैल-जून 2013 से, जल्दी-जल्दी या धीरे-धीरे न पढ़ना। शब्दार्थ की शुद्धिपूर्वक स्तुति देववन्दना आदि मंगल सहित सत्-शास्त्रों का व्याख्यान करना वाचना स्वाध्याय है।
(२) पृच्छना = पूछना। अर्थात् प्रश्न करना भी स्वाध्याय है। जाने हुए अर्थ को सुनिश्चित करने के लिए/पुष्ट करने के लिए, ग्रन्थ या अर्थ के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संशय होने पर किसी विज्ञ स्वाध्यायी से या गुरु महाराज से पूछना स्वाध्याय है। यह पूंछना (प्रश्न) अध्ययन की प्रवृत्ति के लिए ही होता है। अपना बड़प्पन बतलाने के लिए या दूसरों का उपहास करने के लिए पूंछना ठीक नहीं होता। यह तो ज्ञान की अविनय है, शास्त्र की आसादना है। ऐसा नहीं करना चाहिए।
(३) अनुप्रेक्षा = जाने हुए/ पढ़े हुए अर्थ को एकाग्रमन से पुनः पुनः अभ्यास करना अनुप्रेक्षा है। इसमें भी अन्तर्जल्य (मन ही मन में अध्ययन) होता ही है।
(४) आम्नाय = शुद्धतापूर्वक/ शुद्ध उच्चारण सहित श्रुत का पाठ करना आम्नाय है। आम्नाय भी स्वाध्याय ही है।
(५) धर्मोपेदश = धर्म का व्याख्यान किसी दृष्ट/ अदृष्ट प्रयोजन की अपेक्षा न करके उन्मार्ग को नष्ट करने के लिए, सन्देह को दूर करने के लिए, अपूर्व अर्थ को प्रकट करने के लिए, आत्मकल्याण के लिए, जो धर्म का व्याख्यान किया जाता है, उसे धर्मोपदेश कहते हैं। यह भी स्वाध्याय का भेद (अंग) है। श्री मूलाराधना में भी है१५ आचार्यश्री ने (१) परियणा परिवर्तना- पढ़े हुए शास्त्र का पाठ करना, (२) ञवाचन= वाचना (व्याख्यान) (३) पृच्छना पूछना (४)अनुप्रेक्षा बार-बार शास्त्र का चिन्तन-मनन करना और (५) धर्मकथा ६३ शलाका पुरुषों का चरित्र स्वयं पढ़ना और दूसरों को सुनाना - ये पांच स्वाध्याय के भेद बतलाये हैं। स्वाध्याय क्यों - किसलिए?
मानव का चित्त बड़ा चंचल है। यह सदा ही चलायमान रहता है। घड़ी के पेण्डुलम की तरह यह डोलता ही रहता है, स्थिर नहीं रहता। इसकी स्थिरता के लिए तथा अशान्त मन को शान्त तथा समताभावी बनाये रखने के लिए स्वाध्याय आवश्यक है। मुनिश्री तरुणसागर जी ने इस चचंल चित्त को अनेक उपमाओं से अभिव्यक्त किया है। वे कहते हैं कि यह चित्त/मन चिकनी मछली की तरह है तो हाथों से बार-बार फिसल जाती है। बिना लगाम् के घोड़े की तरह है जो सवार को मंजिल तक न पहुँचाकर किसी गर्त में गिरा देता है। यह बहुरूपिया है, नाना रूप बनाता रहता है। यद्यपि यह मनुष्य का है, पर मनुष्य की पकड़ के बाहर है। यह चंचल है, चपल है, वायु से भी अधिक गतिशील है। समुद्र की गहराई को, आकाश की ऊँचाई को मापना और बिजली की गति का आलेख करना कदाचित् आसान है, पर मन की गति मापना संभव नहीं है। अस्तु, चंचलता मन का दुर्गुण है, स्वभाव है, पर इसे रोका जा सकता है। इसे रोकने का/ स्थिर करने का एकमात्र उपाय है सत्-शात्रों का स्वाध्याय। आचार्य श्री गुणभद्र जी महाराज ने आत्मानुशासन में कहा है- “मन मर्कट (बंदर) की तरह चंचल है। इसे स्थिर बनाये रखने में स्वाध्याय परम सहायक है। अतः इसे श्रुतस्कन्धरूपी वृक्ष पर सदा रमाये रखना चाहिए अर्थात् श्रुताभ्यास में/ स्वाध्याय में लगाये रखना चाहिए।