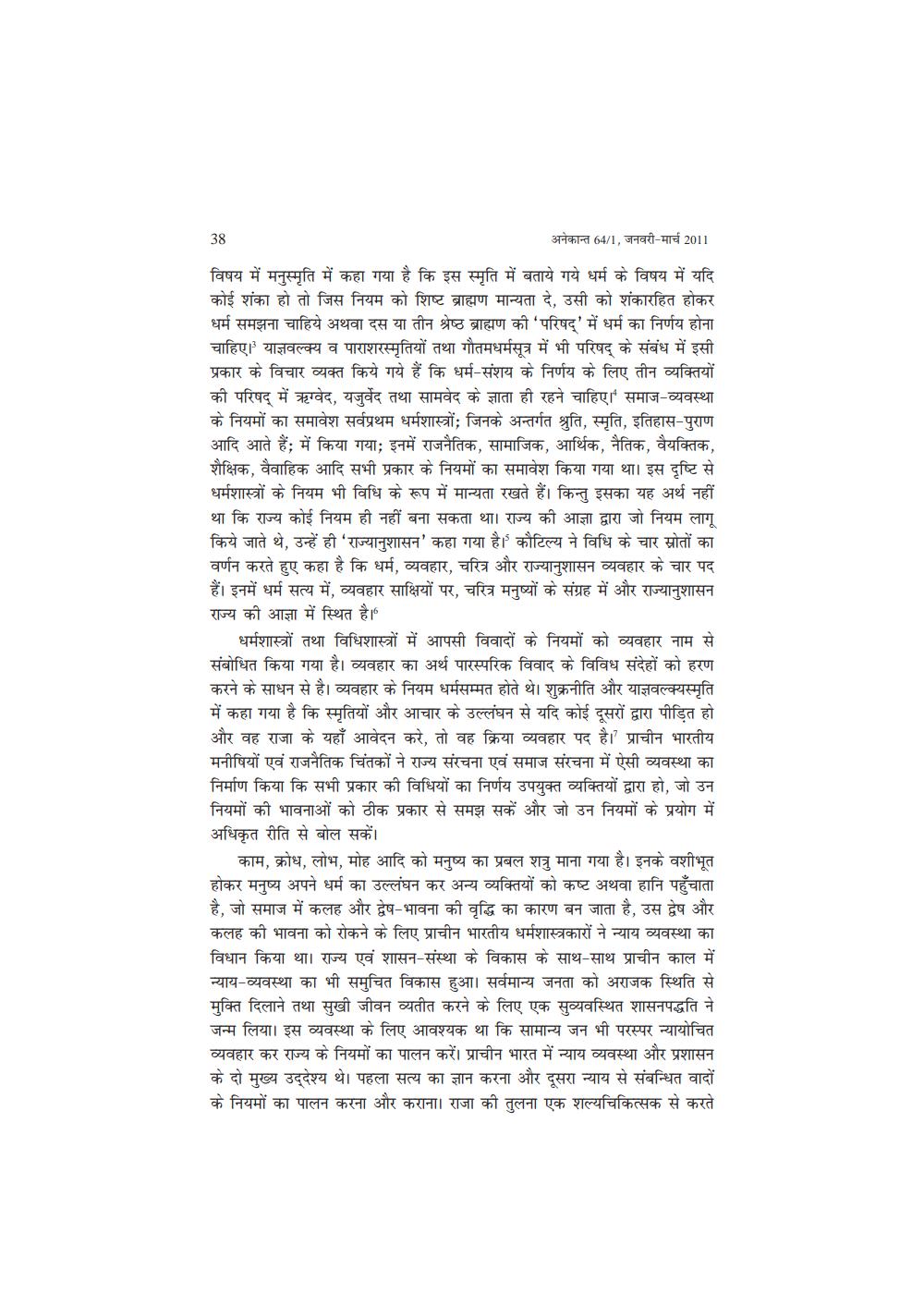________________
38
अनेकान्त 64/1, जनवरी-मार्च 2011
विषय में मनुस्मृति में कहा गया है कि इस स्मृति में बताये गये धर्म के विषय में यदि कोई शंका हो तो जिस नियम को शिष्ट ब्राह्मण मान्यता दे, उसी को शंकारहित होकर धर्म समझना चाहिये अथवा दस या तीन श्रेष्ठ ब्राह्मण की 'परिषद्' में धर्म का निर्णय होना चाहिए। याज्ञवल्क्य व पाराशरस्मृतियों तथा गौतमधर्मसूत्र में भी परिषद् के संबंध में इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं कि धर्म-संशय के निर्णय के लिए तीन व्यक्तियों की परिषद् में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के ज्ञाता ही रहने चाहिए।' समाज-व्यवस्था के नियमों का समावेश सर्वप्रथम धर्मशास्त्रों; जिनके अन्तर्गत श्रुति, स्मृति, इतिहास-पुराण आदि आते हैं; में किया गया; इनमें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, वैयक्तिक, शैक्षिक, वैवाहिक आदि सभी प्रकार के नियमों का समावेश किया गया था। इस दृष्टि से धर्मशास्त्रों के नियम भी विधि के रूप में मान्यता रखते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं था कि राज्य कोई नियम ही नहीं बना सकता था। राज्य की आज्ञा द्वारा जो नियम लागू किये जाते थे, उन्हें ही राज्यानुशासन' कहा गया है। कौटिल्य ने विधि के चार स्रोतों का वर्णन करते हुए कहा है कि धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्यानुशासन व्यवहार के चार पद हैं। इनमें धर्म सत्य में, व्यवहार साक्षियों पर, चरित्र मनुष्यों के संग्रह में और राज्यानुशासन राज्य की आज्ञा में स्थित है।
धर्मशास्त्रों तथा विधिशास्त्रों में आपसी विवादों के नियमों को व्यवहार नाम से संबोधित किया गया है। व्यवहार का अर्थ पारस्परिक विवाद के विविध संदेहों को हरण करने के साधन से है। व्यवहार के नियम धर्मसम्मत होते थे। शुक्रनीति और याज्ञवल्क्यस्मृति में कहा गया है कि स्मृतियों और आचार के उल्लंघन से यदि कोई दूसरों द्वारा पीड़ित हो
और वह राजा के यहाँ आवेदन करे, तो वह क्रिया व्यवहार पद है। प्राचीन भारतीय मनीषियों एवं राजनैतिक चिंतकों ने राज्य संरचना एवं समाज संरचना में ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया कि सभी प्रकार की विधियों का निर्णय उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा हो, जो उन नियमों की भावनाओं को ठीक प्रकार से समझ सकें और जो उन नियमों के प्रयोग में अधिकृत रीति से बोल सकें।
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को मनुष्य का प्रबल शत्रु माना गया है। इनके वशीभूत होकर मनुष्य अपने धर्म का उल्लंघन कर अन्य व्यक्तियों को कष्ट अथवा हानि पहुँचाता है, जो समाज में कलह और द्वेष-भावना की वृद्धि का कारण बन जाता है, उस द्वेष और कलह की भावना को रोकने के लिए प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने न्याय व्यवस्था का विधान किया था। राज्य एवं शासन-संस्था के विकास के साथ-साथ प्राचीन काल में न्याय-व्यवस्था का भी समुचित विकास हुआ। सर्वमान्य जनता को अराजक स्थिति से मुक्ति दिलाने तथा सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए एक सुव्यवस्थित शासनपद्धति ने जन्म लिया। इस व्यवस्था के लिए आवश्यक था कि सामान्य जन भी परस्पर न्यायोचित व्यवहार कर राज्य के नियमों का पालन करें। प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था और प्रशासन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला सत्य का ज्ञान करना और दूसरा न्याय से संबन्धित वादों के नियमों का पालन करना और कराना। राजा की तुलना एक शल्यचिकित्सक से करते