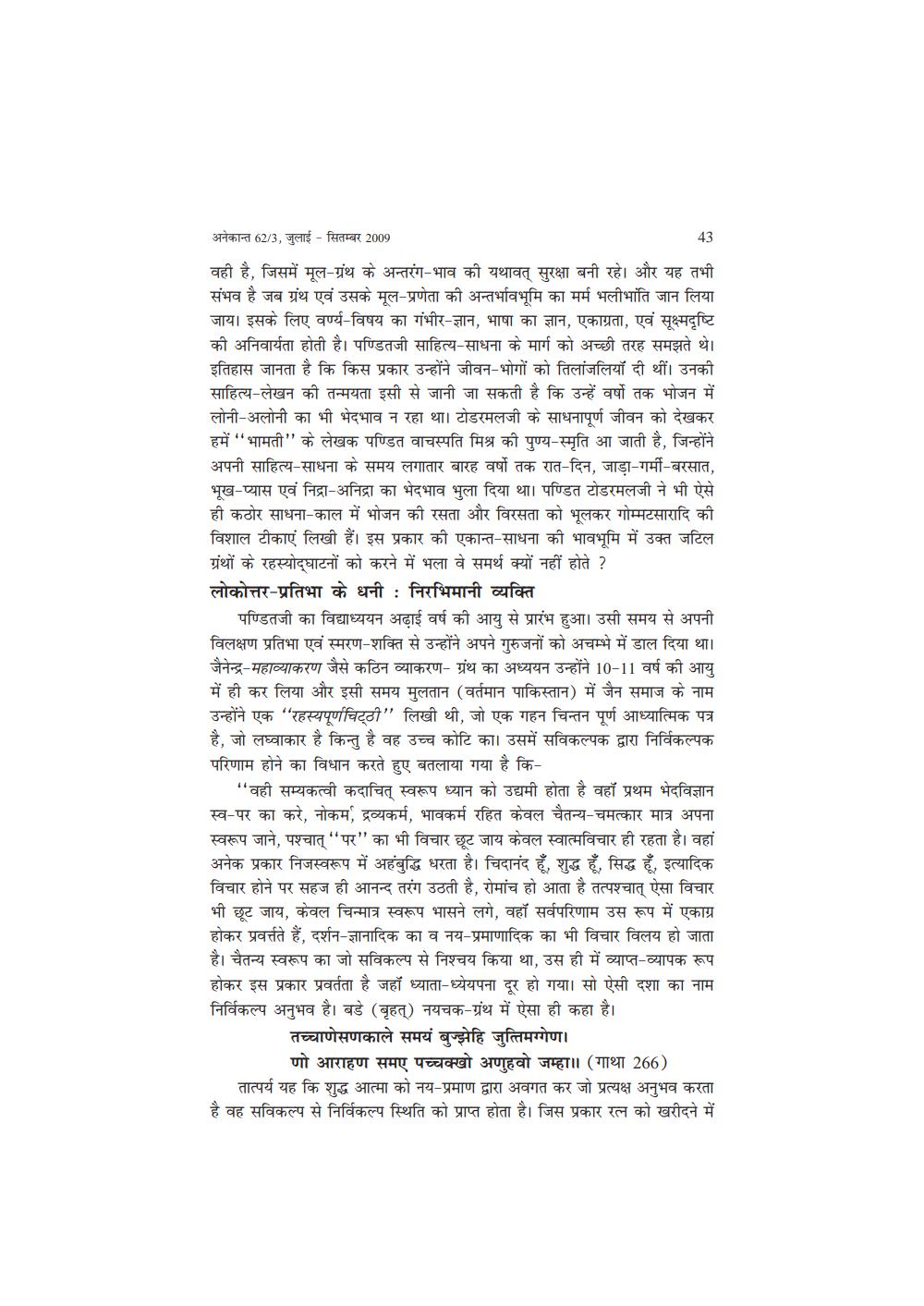________________
अनेकान्त 62/3, जुलाई - सितम्बर 2009
43
=
वही है, जिसमें मूल ग्रंथ के अन्तरंग भाव की यथावत् सुरक्षा बनी रहे और यह तभी संभव है जब ग्रंथ एवं उसके मूल प्रणेता की अन्तर्भावभूमि का मर्म भलीभांति जान लिया जाय। इसके लिए वर्ण्य विषय का गंभीर - ज्ञान, भाषा का ज्ञान, एकाग्रता, एवं सूक्ष्मदृष्टि की अनिवार्यता होती है। पण्डितजी साहित्य साधना के मार्ग को अच्छी तरह समझते थे। इतिहास जानता है कि किस प्रकार उन्होंने जीवन भोगों को तिलांजलियाँ दी थीं। उनकी साहित्य लेखन की तन्मयता इसी से जानी जा सकती है कि उन्हें वर्षों तक भोजन में लोनी अलोनी का भी भेदभाव न रहा था। टोडरमलजी के साधनापूर्ण जीवन को देखकर हमें “भामती' के लेखक पण्डित वाचस्पति मिश्र की पुण्य स्मृति आ जाती है, जिन्होंने अपनी साहित्य-साधना के समय लगातार बारह वर्षो तक रात-दिन, जाड़ा-गर्मी बरसात, भूख-प्यास एवं निद्रा अनिद्रा का भेदभाव भुला दिया था। पण्डित टोडरमलजी ने भी ऐसे ही कठोर साधना-काल में भोजन की रसता और विरसता को भूलकर गोम्मटसारादि की विशाल टीकाएं लिखी हैं। इस प्रकार की एकान्त - साधना की भावभूमि में उक्त जटिल ग्रंथों के रहस्योद्घाटनों को करने में भला वे समर्थ क्यों नहीं होते ?
लोकोत्तर- प्रतिभा के धनी : निरभिमानी व्यक्ति
पण्डितजी का विद्याध्ययन अढाई वर्ष की आयु से प्रारंभ हुआ। उसी समय से अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं स्मरण शक्ति से उन्होंने अपने गुरुजनों को अचम्भे में डाल दिया था। जैनेन्द्र- महाव्याकरण जैसे कठिन व्याकरण- ग्रंथ का अध्ययन उन्होंने 10-11 वर्ष की आयु में ही कर लिया और इसी समय मुलतान (वर्तमान पाकिस्तान) में जैन समाज के नाम उन्होंने एक "रहस्यपूर्णचिट्ठी लिखी थी, जो एक गहन चिन्तन पूर्ण आध्यात्मिक पत्र है, जो लघ्वाकार है किन्तु है वह उच्च कोटि का। उसमें सविकल्पक द्वारा निर्विकल्पक परिणाम होने का विधान करते हुए बतलाया गया है कि
11
"वही सम्यकत्वी कदाचित् स्वरूप ध्यान को उद्यमी होता है वहाँ प्रथम भेदविज्ञान स्व-पर का करे, नोकम, द्रव्यकर्म, भावकर्म रहित केवल चैतन्य - चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात् “पर" का भी विचार छूट जाय केवल स्वात्मविचार ही रहता है। वहां अनेक प्रकार निजस्वरूप में अहंबुद्धि धरता है। चिदानंद हूँ शुद्ध है, सिद्ध हैं, इत्यादिक विचार होने पर सहज ही आनन्द तरंग उठती है, रोमांच हो आता है तत्पश्चात् ऐसा विचार भी छूट जाय, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वहाँ सर्वपरिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं, दर्शन-ज्ञानादिक का व नय प्रमाणादिक का भी विचार विलय हो जाता है। चैतन्य स्वरूप का जो सविकल्प से निश्चय किया था, उस ही में व्याप्त व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है जहाँ ध्याता - ध्येयपना दूर हो गया । सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। बडे (बृहत् ) नयचक-ग्रंथ में ऐसा ही कहा है।
तच्चाणेसणकाले समयं बुज्झेहि जुत्तिमग्गेण ।
णो आराहण समए पच्चक्खो अणुहवो जम्हा ॥ ( गाथा 266)
तात्पर्य यह कि शुद्ध आत्मा को नय-प्रमाण द्वारा अवगत कर जो प्रत्यक्ष अनुभव करता है वह सविकल्प से निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार रत्न को खरीदने में