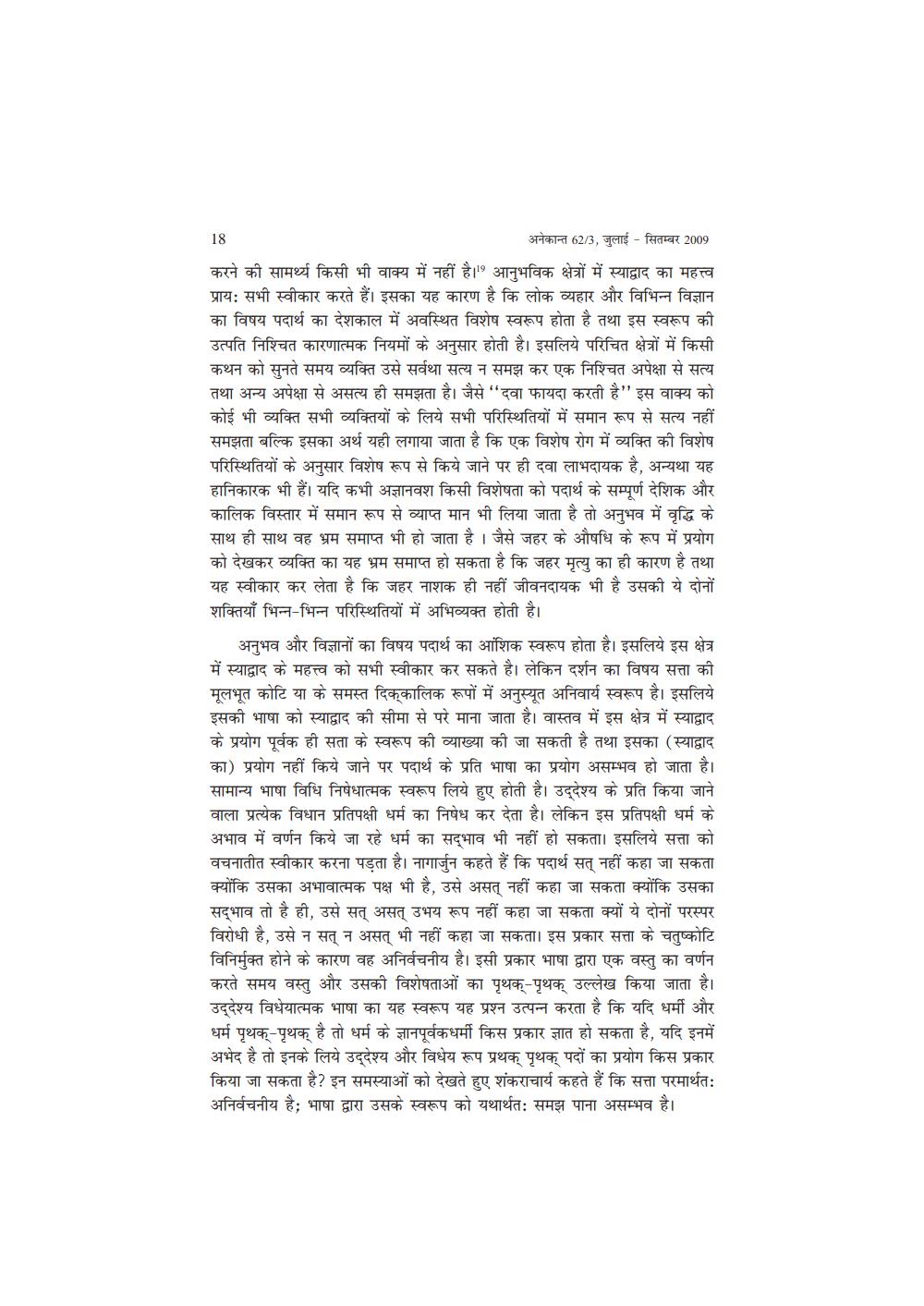________________
अनेकान्त 62/3, जुलाई - सितम्बर 2009
करने की सामर्थ्य किसी भी वाक्य में नहीं है। आनुभविक क्षेत्रों में स्याद्वाद का महत्त्व प्रायः सभी स्वीकार करते हैं। इसका यह कारण है कि लोक व्यहार और विभिन्न विज्ञान का विषय पदार्थ का देशकाल में अवस्थित विशेष स्वरूप होता है तथा इस स्वरूप की उत्पति निश्चित कारणात्मक नियमों के अनुसार होती है। इसलिये परिचित क्षेत्रों में किसी कथन को सुनते समय व्यक्ति उसे सर्वथा सत्य न समझ कर एक निश्चित अपेक्षा से सत्य तथा अन्य अपेक्षा से असत्य ही समझता है। जैसे "दवा फायदा करती है" इस वाक्य को कोई भी व्यक्ति सभी व्यक्तियों के लिये सभी परिस्थितियों में समान रूप से सत्य नहीं समझता बल्कि इसका अर्थ यही लगाया जाता है कि एक विशेष रोग में व्यक्ति की विशेष परिस्थितियों के अनुसार विशेष रूप से किये जाने पर ही दवा लाभदायक है, अन्यथा यह हानिकारक भी हैं। यदि कभी अज्ञानवश किसी विशेषता को पदार्थ के सम्पूर्ण देशिक और कालिक विस्तार में समान रूप से व्याप्त मान भी लिया जाता है तो अनुभव में वृद्धि के साथ ही साथ वह भ्रम समाप्त भी हो जाता है । जैसे जहर के औषधि के रूप में प्रयोग को देखकर व्यक्ति का यह भ्रम समाप्त हो सकता है कि जहर मृत्यु का ही कारण है तथा यह स्वीकार कर लेता है कि जहर नाशक ही नहीं जीवनदायक भी है उसकी ये दोनों शक्तियाँ भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में अभिव्यक्त होती है।
अनुभव और विज्ञानों का विषय पदार्थ का आंशिक स्वरूप होता है। इसलिये इस क्षेत्र में स्याद्वाद के महत्त्व को सभी स्वीकार कर सकते है। लेकिन दर्शन का विषय सत्ता की मूलभूत कोटि या के समस्त दिक्कालिक रूपों में अनुस्यूत अनिवार्य स्वरूप है। इसलिये इसकी भाषा को स्याद्वाद की सीमा से परे माना जाता है। वास्तव में इस क्षेत्र में स्याद्वाद के प्रयोग पूर्वक ही सता के स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है तथा इसका (स्याद्वाद का) प्रयोग नहीं किये जाने पर पदार्थ के प्रति भाषा का प्रयोग असम्भव हो जाता है। सामान्य भाषा विधि निषेधात्मक स्वरूप लिये हुए होती है। उद्देश्य के प्रति किया जाने वाला प्रत्येक विधान प्रतिपक्षी धर्म का निषेध कर देता है। लेकिन इस प्रतिपक्षी धर्म के अभाव में वर्णन किये जा रहे धर्म का सद्भाव भी नहीं हो सकता। इसलिये सत्ता को वचनातीत स्वीकार करना पड़ता है। नागार्जुन कहते हैं कि पदार्थ सत् नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका अभावात्मक पक्ष भी है, उसे असत् नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका सद्भाव तो है ही, उसे सत् असत् उभय रूप नहीं कहा जा सकता क्यों ये दोनों परस्पर विरोधी है, उसे न सत् न असत् भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार सत्ता के चतुष्कोटि विनिर्मुक्त होने के कारण वह अनिर्वचनीय है। इसी प्रकार भाषा द्वारा एक वस्तु का वर्णन करते समय वस्तु और उसकी विशेषताओं का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया जाता है। उद्देश्य विधेयात्मक भाषा का यह स्वरूप यह प्रश्न उत्पन्न करता है कि यदि धर्मी और धर्म पृथक्-पृथक् है तो धर्म के ज्ञानपूर्वकधर्मी किस प्रकार ज्ञात हो सकता है, यदि इनमें अभेद है तो इनके लिये उद्देश्य और विधेय रूप प्रथक् पृथक् पदों का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? इन समस्याओं को देखते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि सत्ता परमार्थतः अनिर्वचनीय है; भाषा द्वारा उसके स्वरूप को यथार्थतः समझ पाना असम्भव है।