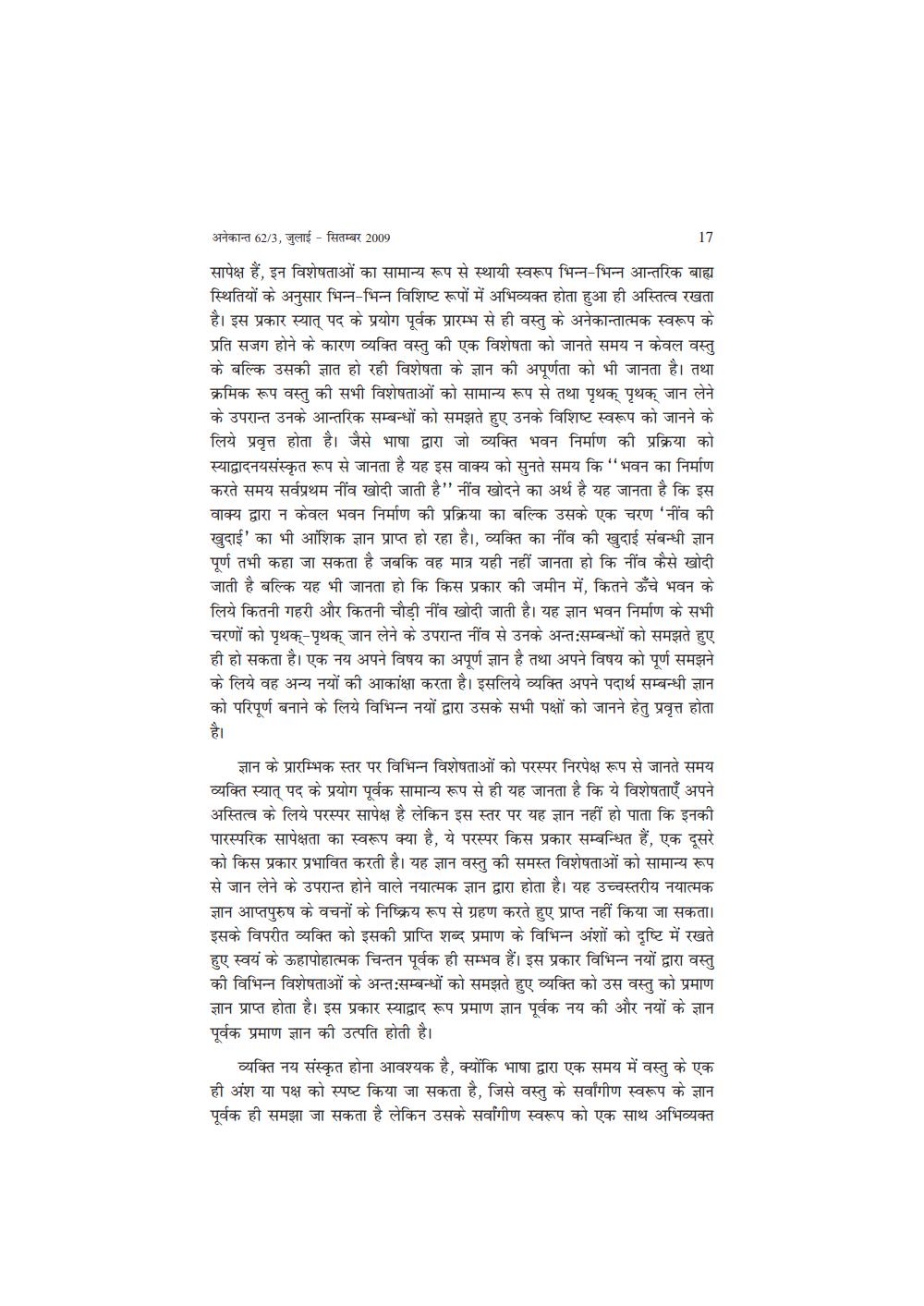________________
अनेकान्त 62/3, जुलाई - सितम्बर 2009
सापेक्ष हैं, इन विशेषताओं का सामान्य रूप से स्थायी स्वरूप भिन्न-भिन्न आन्तरिक बाह्य स्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न विशिष्ट रूपों में अभिव्यक्त होता हुआ ही अस्तित्व रखता है। इस प्रकार स्यात् पद के प्रयोग पूर्वक प्रारम्भ से ही वस्तु के अनेकान्तात्मक स्वरूप के प्रति सजग होने के कारण व्यक्ति वस्तु की एक विशेषता को जानते समय न केवल वस्तु के बल्कि उसकी ज्ञात हो रही विशेषता के ज्ञान की अपूर्णता को भी जानता है। तथा क्रमिक रूप वस्तु की सभी विशेषताओं को सामान्य रूप से तथा पृथक् पृथक् जान लेने के उपरान्त उनके आन्तरिक सम्बन्धों को समझते हुए उनके विशिष्ट स्वरूप को जानने के लिये प्रवृत्त होता है जैसे भाषा द्वारा जो व्यक्ति भवन निर्माण की प्रक्रिया को स्याद्वादनयसंस्कृत रूप से जानता है यह इस वाक्य को सुनते समय कि " भवन का निर्माण करते समय सर्वप्रथम नींव खोदी जाती है" नींव खोदने का अर्थ है यह जानता है कि इस वाक्य द्वारा न केवल भवन निर्माण की प्रक्रिया का बल्कि उसके एक चरण 'नींव की खुदाई' का भी आशिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है। व्यक्ति का नींव की खुदाई संबन्धी ज्ञान पूर्ण तभी कहा जा सकता है जबकि वह मात्र यही नहीं जानता हो कि नींव कैसे खोदी जाती है बल्कि यह भी जानता हो कि किस प्रकार की जमीन में कितने ऊँचे भवन के लिये कितनी गहरी और कितनी चौड़ी नींव खोदी जाती है। यह ज्ञान भवन निर्माण के सभी चरणों को पृथक्-पृथक् जान लेने के उपरान्त नींव से उनके अन्तः सम्बन्धों को समझते हुए ही हो सकता है। एक नय अपने विषय का अपूर्ण ज्ञान है तथा अपने विषय को पूर्ण समझने के लिये वह अन्य नयों की आकांक्षा करता है। इसलिये व्यक्ति अपने पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान को परिपूर्ण बनाने के लिये विभिन्न नयाँ द्वारा उसके सभी पक्षों को जानने हेतु प्रवृत्त होता
है
17
ज्ञान के प्रारम्भिक स्तर पर विभिन्न विशेषताओं को परस्पर निरपेक्ष रूप से जानते समय व्यक्ति स्यात् पद के प्रयोग पूर्वक सामान्य रूप से ही यह जानता है कि ये विशेषताएँ अपने अस्तित्व के लिये परस्पर सापेक्ष है लेकिन इस स्तर पर यह ज्ञान नहीं हो पाता कि इनकी पारस्परिक सापेक्षता का स्वरूप क्या है, ये परस्पर किस प्रकार सम्बन्धित हैं, एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करती है। यह ज्ञान वस्तु की समस्त विशेषताओं को सामान्य रूप से जान लेने के उपरान्त होने वाले नयात्मक ज्ञान द्वारा होता है। यह उच्चस्तरीय नयात्मक ज्ञान आप्तपुरुष के वचनों के निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते हुए प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत व्यक्ति को इसकी प्राप्ति शब्द प्रमाण के विभिन्न अंशों को दृष्टि में रखते हुए स्वयं के ऊहापोहात्मक चिन्तन पूर्वक ही सम्भव हैं। इस प्रकार विभिन्न नयों द्वारा वस्तु की विभिन्न विशेषताओं के अन्तःसम्बन्धों को समझते हुए व्यक्ति को उस वस्तु को प्रमाण ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार स्याद्वाद रूप प्रमाण ज्ञान पूर्वक नय की और नयों के ज्ञान पूर्वक प्रमाण ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
व्यक्ति नय संस्कृत होना आवश्यक है, क्योंकि भाषा द्वारा एक समय में वस्तु के एक ही अंश या पक्ष को स्पष्ट किया जा सकता है, जिसे वस्तु के सर्वांगीण स्वरूप के ज्ञान पूर्वक ही समझा जा सकता है लेकिन उसके सर्वांगीण स्वरूप को एक साथ अभिव्यक्त