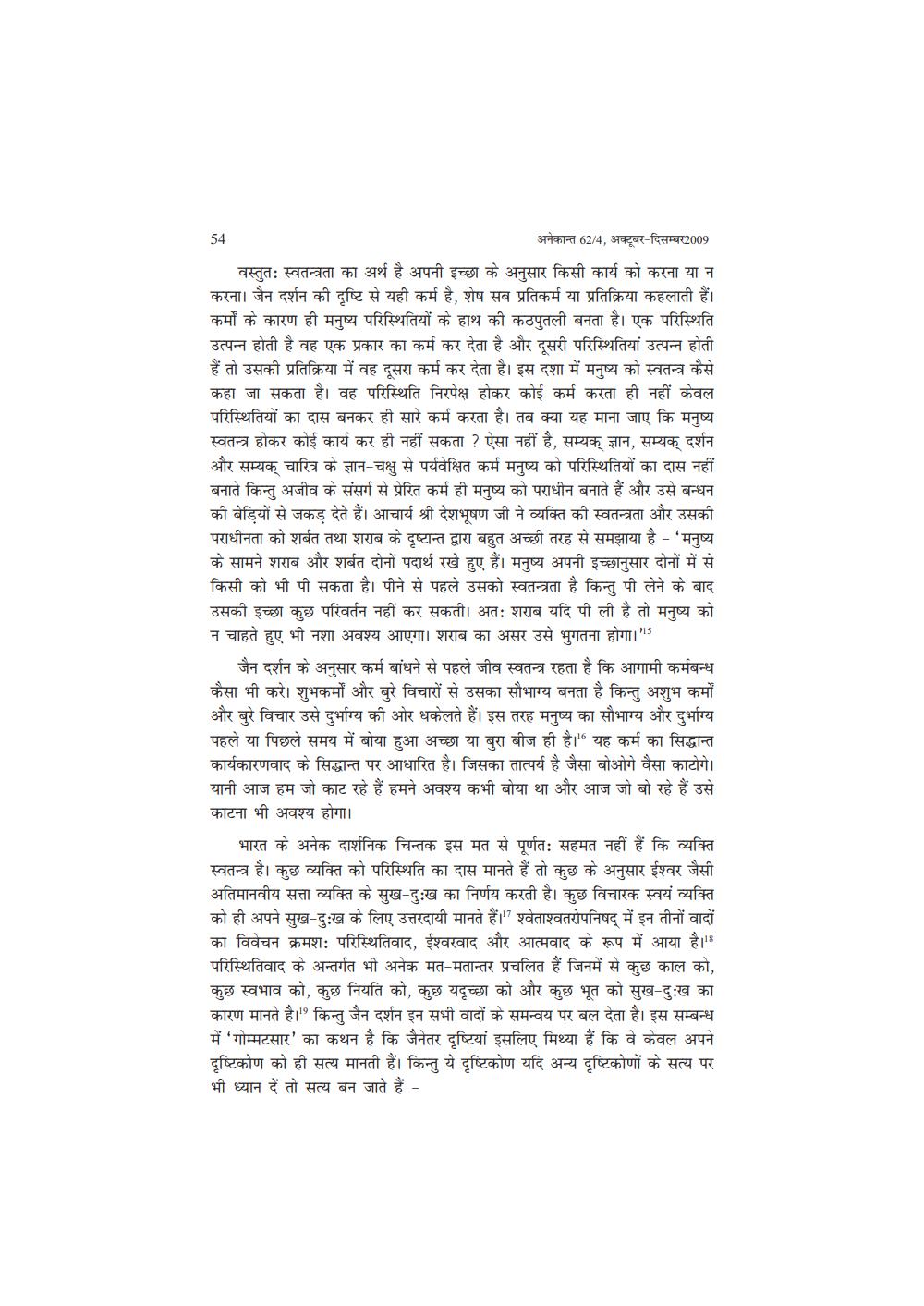________________
अनेकान्त 62/4, अक्टूबर-दिसम्बर2009
वस्तुतः स्वतन्त्रता का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार किसी कार्य को करना या न करना। जैन दर्शन की दृष्टि से यही कर्म है, शेष सब प्रतिकर्म या प्रतिक्रिया कहलाती हैं। कर्मों के कारण ही मनुष्य परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली बनता है। एक परिस्थिति उत्पन्न होती है वह एक प्रकार का कर्म कर देता है और दूसरी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में वह दूसरा कर्म कर देता है। इस दशा में मनुष्य को स्वतन्त्र कैसे कहा जा सकता है। वह परिस्थिति निरपेक्ष होकर कोई कर्म करता ही नहीं केवल परिस्थितियों का दास बनकर ही सारे कर्म करता है। तब क्या यह माना जाए कि मनुष्य स्वतन्त्र होकर कोई कार्य कर ही नहीं सकता ? ऐसा नहीं है, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन
और सम्यक् चारित्र के ज्ञान-चक्षु से पर्यवेक्षित कर्म मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बनाते किन्तु अजीव के संसर्ग से प्रेरित कर्म ही मनुष्य को पराधीन बनाते हैं और उसे बन्धन की बेड़ियों से जकड़ देते हैं। आचार्य श्री देशभूषण जी ने व्यक्ति की स्वतन्त्रता और उसकी पराधीनता को शर्बत तथा शराब के दृष्टान्त द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझाया है - 'मनुष्य के सामने शराब और शर्बत दोनों पदार्थ रखे हुए हैं। मनुष्य अपनी इच्छानुसार दोनों में से किसी को भी पी सकता है। पीने से पहले उसको स्वतन्त्रता है किन्तु पी लेने के बाद उसकी इच्छा कुछ परिवर्तन नहीं कर सकती। अतः शराब यदि पी ली है तो मनुष्य को न चाहते हुए भी नशा अवश्य आएगा। शराब का असर उसे भुगतना होगा।15
जैन दर्शन के अनुसार कर्म बांधने से पहले जीव स्वतन्त्र रहता है कि आगामी कर्मबन्ध कैसा भी करे। शुभकर्मों और बुरे विचारों से उसका सौभाग्य बनता है किन्तु अशुभ कर्मों
और बुरे विचार उसे दुर्भाग्य की ओर धकेलते हैं। इस तरह मनुष्य का सौभाग्य और दुर्भाग्य पहले या पिछले समय में बोया हुआ अच्छा या बुरा बीज ही है। यह कर्म का सिद्धान्त कार्यकारणवाद के सिद्धान्त पर आधारित है। जिसका तात्पर्य है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यानी आज हम जो काट रहे हैं हमने अवश्य कभी बोया था और आज जो बो रहे हैं उसे काटना भी अवश्य होगा।
भारत के अनेक दार्शनिक चिन्तक इस मत से पूर्णतः सहमत नहीं हैं कि व्यक्ति स्वतन्त्र है। कुछ व्यक्ति को परिस्थिति का दास मानते हैं तो कुछ के अनुसार ईश्वर जैसी अतिमानवीय सत्ता व्यक्ति के सुख-दु:ख का निर्णय करती है। कुछ विचारक स्वयं व्यक्ति को ही अपने सुख-दु:ख के लिए उत्तरदायी मानते हैं।" श्वेताश्वतरोपनिषद् में इन तीनों वादों का विवेचन क्रमशः परिस्थितिवाद, ईश्वरवाद और आत्मवाद के रूप में आया है। परिस्थितिवाद के अन्तर्गत भी अनेक मत-मतान्तर प्रचलित हैं जिनमें से कुछ काल को, कुछ स्वभाव को, कुछ नियति को, कुछ यदृच्छा को और कुछ भूत को सुख-दुःख का कारण मानते है। किन्तु जैन दर्शन इन सभी वादों के समन्वय पर बल देता है। इस सम्बन्ध में 'गोम्मटसार' का कथन है कि जैनेतर दृष्टियां इसलिए मिथ्या हैं कि वे केवल अपने दृष्टिकोण को ही सत्य मानती हैं। किन्तु ये दृष्टिकोण यदि अन्य दृष्टिकोणों के सत्य पर भी ध्यान दें तो सत्य बन जाते हैं -