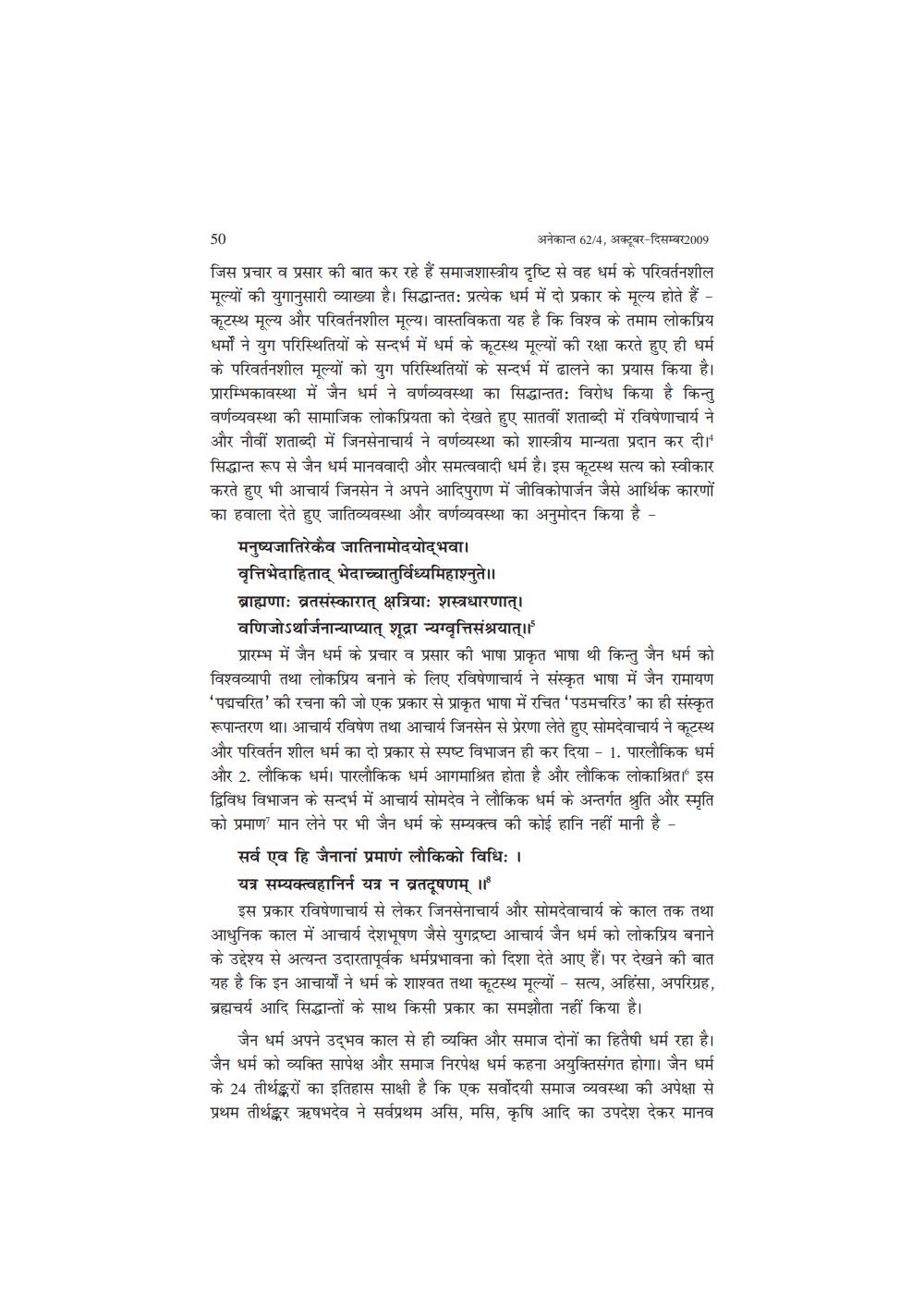________________
अनेकान्त 62/4, अक्टूबर-दिसम्बर2009 जिस प्रचार व प्रसार की बात कर रहे हैं समाजशास्त्रीय दृष्टि से वह धर्म के परिवर्तनशील मूल्यों की युगानुसारी व्याख्या है। सिद्धान्ततः प्रत्येक धर्म में दो प्रकार के मूल्य होते हैं - कूटस्थ मूल्य और परिवर्तनशील मूल्य। वास्तविकता यह है कि विश्व के तमाम लोकप्रिय धर्मों ने युग परिस्थितियों के सन्दर्भ में धर्म के कूटस्थ मूल्यों की रक्षा करते हुए ही धर्म के परिवर्तनशील मूल्यों को युग परिस्थितियों के सन्दर्भ में ढालने का प्रयास किया है। प्रारम्भिकावस्था में जैन धर्म ने वर्णव्यवस्था का सिद्धान्ततः विरोध किया है किन्तु वर्णव्यवस्था की सामाजिक लोकप्रियता को देखते हुए सातवीं शताब्दी में रविषेणाचार्य ने
और नौवीं शताब्दी में जिनसेनाचार्य ने वर्णव्यस्था को शास्त्रीय मान्यता प्रदान कर दी।' सिद्धान्त रूप से जैन धर्म मानववादी और समत्ववादी धर्म है। इस कूटस्थ सत्य को स्वीकार करते हुए भी आचार्य जिनसेन ने अपने आदिपुराण में जीविकोपार्जन जैसे आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए जातिव्यवस्था और वर्णव्यवस्था का अनुमोदन किया है -
मनुष्यजातिरेकैव जातिनामोदयोद्भवा। वृत्तिभेदाहिताद् भेदाच्चातुर्विध्यमिहाश्नुते॥ ब्राह्मणाः व्रतसंस्कारात् क्षत्रियाः शस्त्रधारणात्। वणिजोऽर्थार्जनान्याप्यात् शूद्रा न्यग्वृत्तिसंश्रयात्॥
प्रारम्भ में जैन धर्म के प्रचार व प्रसार की भाषा प्राकृत भाषा थी किन्तु जैन धर्म को विश्वव्यापी तथा लोकप्रिय बनाने के लिए रविषेणाचार्य ने संस्कृत भाषा में जैन रामायण 'पद्मचरित' की रचना की जो एक प्रकार से प्राकृत भाषा में रचित 'पउमचरिउ' का ही संस्कृत रूपान्तरण था। आचार्य रविषेण तथा आचार्य जिनसेन से प्रेरणा लेते हुए सोमदेवाचार्य ने कूटस्थ और परिवर्तन शील धर्म का दो प्रकार से स्पष्ट विभाजन ही कर दिया - 1. पारलौकिक धर्म और 2. लौकिक धर्म। पारलौकिक धर्म आगमाश्रित होता है और लौकिक लोकाश्रित। इस द्विविध विभाजन के सन्दर्भ में आचार्य सोमदेव ने लौकिक धर्म के अन्तर्गत श्रुति और स्मृति को प्रमाण मान लेने पर भी जैन धर्म के सम्यक्त्व की कोई हानि नहीं मानी है -
सर्व एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः । यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न व्रतदूषणम् ॥
इस प्रकार रविषेणाचार्य से लेकर जिनसेनाचार्य और सोमदेवाचार्य के काल तक तथा आधुनिक काल में आचार्य देशभूषण जैसे युगद्रष्टा आचार्य जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से अत्यन्त उदारतापूर्वक धर्मप्रभावना को दिशा देते आए हैं। पर देखने की बात यह है कि इन आचार्यों ने धर्म के शाश्वत तथा कूटस्थ मूल्यों - सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि सिद्धान्तों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया है।
जैन धर्म अपने उद्भव काल से ही व्यक्ति और समाज दोनों का हितैषी धर्म रहा है। जैन धर्म को व्यक्ति सापेक्ष और समाज निरपेक्ष धर्म कहना अयुक्तिसंगत होगा। जैन धर्म के 24 तीर्थङ्करों का इतिहास साक्षी है कि एक सर्वोदयी समाज व्यवस्था की अपेक्षा से प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव ने सर्वप्रथम असि, मसि, कृषि आदि का उपदेश देकर मानव