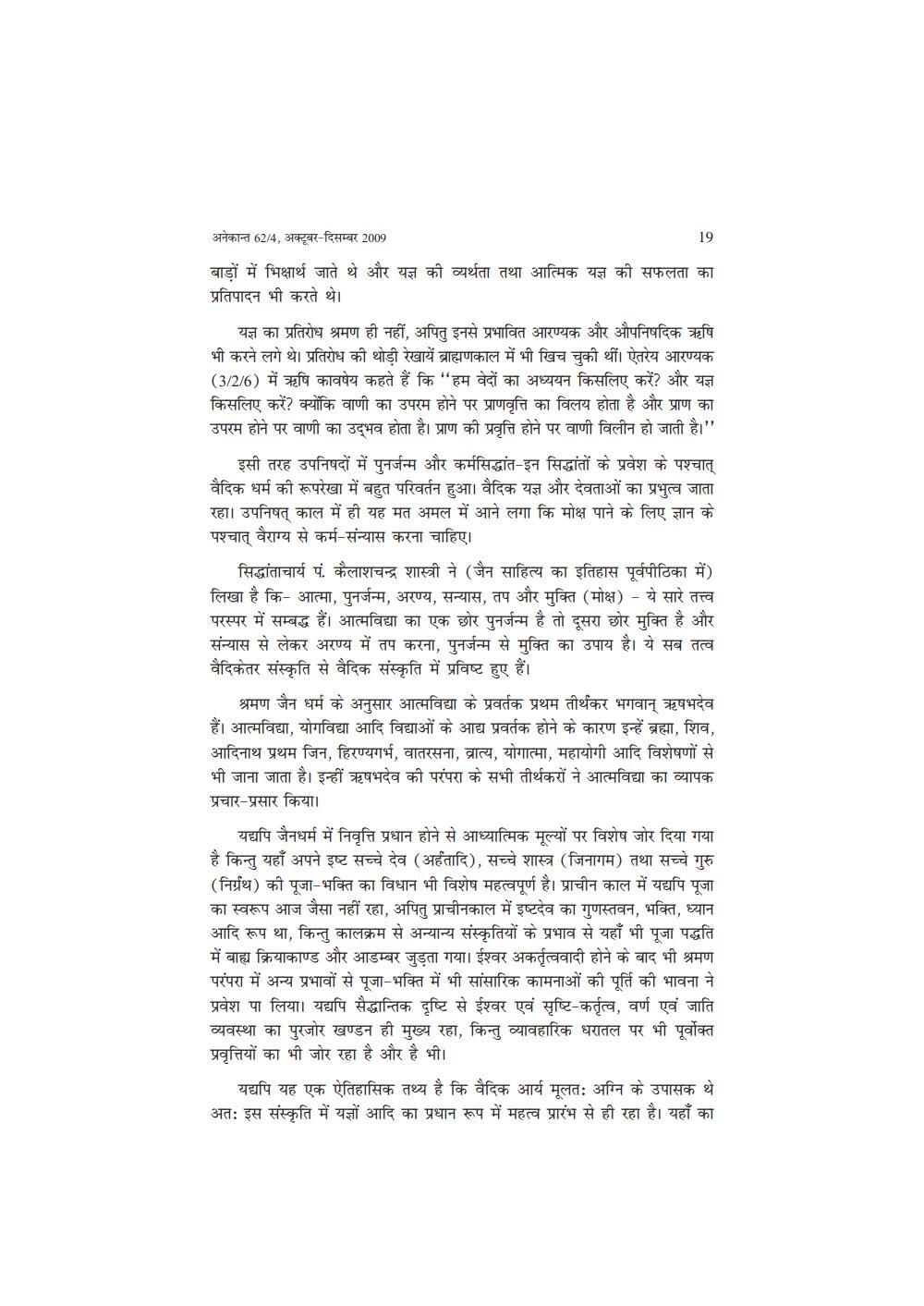________________
अनेकान्त 62/4 अक्टूबर-दिसम्बर 2009
19
बाड़ों में भिक्षार्थ जाते थे और यज्ञ की व्यर्थता तथा आत्मिक यज्ञ की सफलता का प्रतिपादन भी करते थे।
यज्ञ का प्रतिरोध श्रमण ही नहीं, अपितु इनसे प्रभावित आरण्यक और औपनिषदिक ऋषि भी करने लगे थे। प्रतिरोध की थोड़ी रेखायें ब्राह्मणकाल में भी खिच चुकी थीं। ऐतरेय आरण्यक (3/2/6) में ऋषि कावषेय कहते हैं कि "हम वेदों का अध्ययन किसलिए करें? और यज्ञ किसलिए करे? क्योंकि वाणी का उपरम होने पर प्राणवृत्ति का विलय होता है और प्राण का उपर होने पर वाणी का उद्भव होता है। प्राण की प्रवृत्ति होने पर वाणी विलीन हो जाती है । "
इसी तरह उपनिषदों में पुनर्जन्म और कर्मसिद्धांत इन सिद्धांतों के प्रवेश के पश्चात् वैदिक धर्म की रूपरेखा में बहुत परिवर्तन हुआ । वैदिक यज्ञ और देवताओं का प्रभुत्व जाता रहा। उपनिषत् काल में ही यह मत अमल में आने लगा कि मोक्ष पाने के लिए ज्ञान के पश्चात् वैराग्य से कर्म संन्यास करना चाहिए।
सिद्धांताचार्य पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री ने (जैन साहित्य का इतिहास पूर्वपीठिका में) लिखा है कि- आत्मा, पुनर्जन्म, अरण्य, सन्यास, तप और मुक्ति (मोक्ष) – ये सारे तत्त्व परस्पर में सम्बद्ध हैं। आत्मविद्या का एक छोर पुनर्जन्म है तो दूसरा छोर मुक्ति है और संन्यास से लेकर अरण्य में तप करना, पुनर्जन्म से मुक्ति का उपाय है ये सब तत्व वैदिकेतर संस्कृति से वैदिक संस्कृति में प्रविष्ट हुए हैं।
श्रमण जैन धर्म के अनुसार आत्मविद्या के प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव हैं। आत्मविद्या योगविद्या आदि विद्याओं के आद्य प्रवर्तक होने के कारण इन्हें ब्रह्मा, शिव, आदिनाथ प्रथम जिन, हिरण्यगर्भ, वातरसना, व्रात्य, योगात्मा, महायोगी आदि विशेषणों से भी जाना जाता है। इन्हीं ऋषभदेव की परंपरा के सभी तीर्थकरों ने आत्मविद्या का व्यापक प्रचार-प्रसार किया।
यद्यपि जैनधर्म में निवृत्ति प्रधान होने से आध्यात्मिक मूल्यों पर विशेष जोर दिया गया है किन्तु यहाँ अपने इष्ट सच्चे देव (अर्हतादि), सच्चे शास्त्र (जिनागम) तथा सच्चे गुरु (निग्रंथ) की पूजा भक्ति का विधान भी विशेष महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन काल में यद्यपि पूजा का स्वरूप आज जैसा नहीं रहा, अपितु प्राचीनकाल में इष्टदेव का गुणस्तवन, भक्ति, ध्यान आदि रूप था, किन्तु कालक्रम से अन्यान्य संस्कृतियों के प्रभाव से यहाँ भी पूजा पद्धति में बाह्य क्रियाकाण्ड और आडम्बर जुड़ता गया। ईश्वर अकर्तृत्ववादी होने के बाद भी श्रमण परंपरा में अन्य प्रभावों से पूजा भक्ति में भी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति की भावना ने प्रवेश पा लिया। यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से ईश्वर एवं सृष्टि-कर्तृत्व, वर्ण एवं जाति व्यवस्था का पुरजोर खण्डन ही मुख्य रहा, किन्तु व्यावहारिक धरातल पर भी पूर्वोक्त प्रवृत्तियों का भी जोर रहा है और है भी
यद्यपि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि वैदिक आर्य मूलतः अग्नि के उपासक थे अतः इस संस्कृति में यज्ञों आदि का प्रधान रूप में महत्व प्रारंभ से ही रहा है। यहाँ का