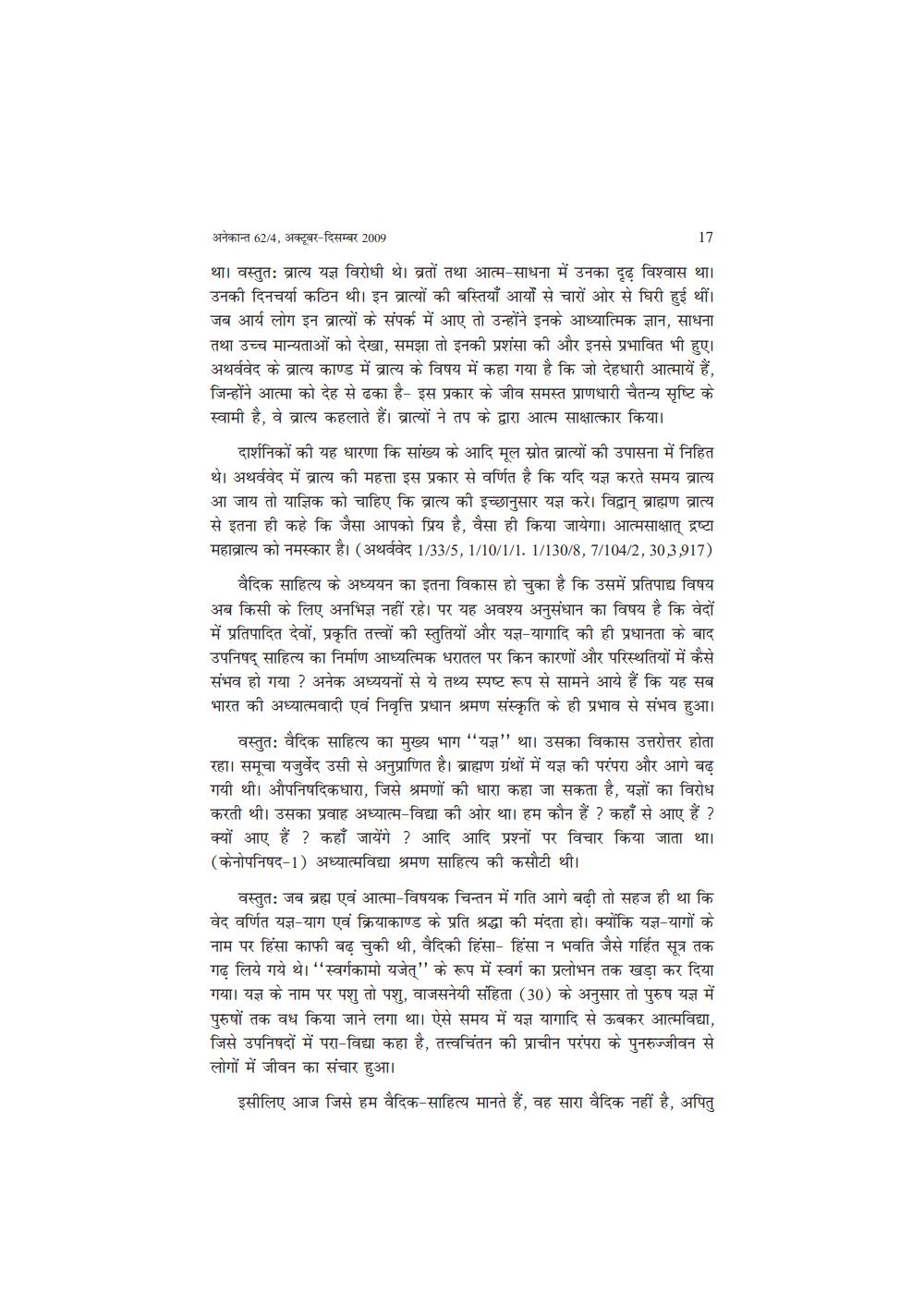________________
अनेकान्त 62/4, अक्टूबर-दिसम्बर 2009
17
था। वस्तुतः व्रात्य यज्ञ विरोधी थे। व्रतों तथा आत्म-साधना में उनका दृढ़ विश्वास था। उनकी दिनचर्या कठिन थी। इन व्रात्यों की बस्तियाँ आर्यों से चारों ओर से घिरी हुई थीं। जब आर्य लोग इन व्रात्यों के संपर्क में आए तो उन्होंने इनके आध्यात्मिक ज्ञान, साधना तथा उच्च मान्यताओं को देखा, समझा तो इनकी प्रशंसा की और इनसे प्रभावित भी हुए। अथर्ववेद के व्रात्य काण्ड में व्रात्य के विषय में कहा गया है कि जो देहधारी आत्मायें हैं, जिन्होंने आत्मा को देह से ढका है- इस प्रकार के जीव समस्त प्राणधारी चैतन्य सृष्टि के स्वामी है, वे व्रात्य कहलाते हैं। व्रात्यों ने तप के द्वारा आत्म साक्षात्कार किया।
दार्शनिकों की यह धारणा कि सांख्य के आदि मूल स्रोत व्रात्यों की उपासना में निहित थे। अथर्ववेद में व्रात्य की महत्ता इस प्रकार से वर्णित है कि यदि यज्ञ करते समय व्रात्य आ जाय तो याज्ञिक को चाहिए कि व्रात्य की इच्छानुसार यज्ञ करे। विद्वान् ब्राह्मण व्रात्य से इतना ही कहे कि जैसा आपको प्रिय है, वैसा ही किया जायेगा। आत्मसाक्षात् द्रष्टा महाव्रात्य को नमस्कार है। (अथर्ववेद 1/33/5, 1/10/1/1. 1/130/8, 7/104/2, 303,917)
वैदिक साहित्य के अध्ययन का इतना विकास हो चुका है कि उसमें प्रतिपाद्य विषय अब किसी के लिए अनभिज्ञ नहीं रहे। पर यह अवश्य अनुसंधान का विषय है कि वेदों में प्रतिपादित देवों, प्रकृति तत्त्वों की स्तुतियों और यज्ञ-यागादि की ही प्रधानता के बाद उपनिषद् साहित्य का निर्माण आध्यत्मिक धरातल पर किन कारणों और परिस्थतियों में कैसे संभव हो गया ? अनेक अध्ययनों से ये तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आये हैं कि यह सब भारत की अध्यात्मवादी एवं निवृत्ति प्रधान श्रमण संस्कृति के ही प्रभाव से संभव हुआ।
वस्तुतः वैदिक साहित्य का मुख्य भाग "यज्ञ" था। उसका विकास उत्तरोत्तर होता रहा। समूचा यजुर्वेद उसी से अनुप्राणित है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की परंपरा और आगे बढ़ गयी थी। औपनिषदिकधारा, जिसे श्रमणों की धारा कहा जा सकता है, यज्ञों का विरोध करती थी। उसका प्रवाह अध्यात्म-विद्या की ओर था। हम कौन हैं ? कहाँ से आए हैं ? क्यों आए हैं ? कहाँ जायेंगे ? आदि आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता था। (केनोपनिषद-1) अध्यात्मविद्या श्रमण साहित्य की कसौटी थी।
वस्तुतः जब ब्रह्म एवं आत्मा-विषयक चिन्तन में गति आगे बढ़ी तो सहज ही था कि वेद वर्णित यज्ञ-याग एवं क्रियाकाण्ड के प्रति श्रद्धा की मंदता हो। क्योंकि यज्ञ-यागों के नाम पर हिंसा काफी बढ़ चुकी थी, वैदिकी हिंसा- हिंसा न भवति जैसे गर्हित सूत्र तक गढ़ लिये गये थे। "स्वर्गकामो यजेत्" के रूप में स्वर्ग का प्रलोभन तक खड़ा कर दिया गया। यज्ञ के नाम पर पशु तो पशु, वाजसनेयी संहिता (30) के अनुसार तो पुरुष यज्ञ में पुरुषों तक वध किया जाने लगा था। ऐसे समय में यज्ञ यागादि से ऊबकर आत्मविद्या, जिसे उपनिषदों में परा-विद्या कहा है, तत्त्वचिंतन की प्राचीन परंपरा के पुनरुज्जीवन से लोगों में जीवन का संचार हुआ।
इसीलिए आज जिसे हम वैदिक-साहित्य मानते हैं, वह सारा वैदिक नहीं है, अपितु