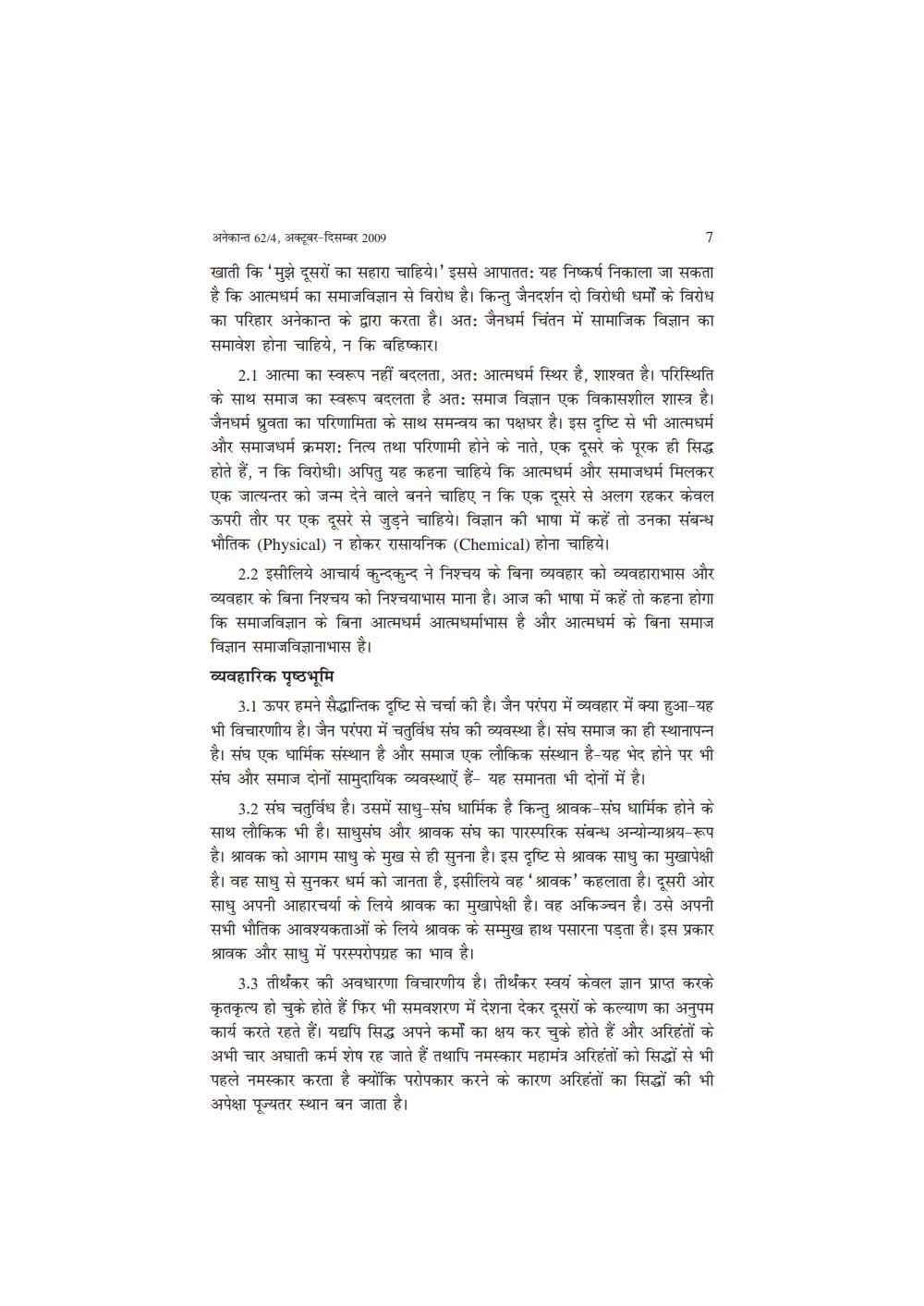________________
अनेकान्त 62/4 अक्टूबर-दिसम्बर 2009
खाती कि 'मुझे दूसरों का सहारा चाहिये।' इससे आपाततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आत्मधर्म का समाजविज्ञान से विरोध है। किन्तु जैनदर्शन दो विरोधी धर्मों के विरोध का परिहार अनेकान्त के द्वारा करता है। अत: जैनधर्म चिंतन में सामाजिक विज्ञान का समावेश होना चाहिये, न कि बहिष्कार।
7
2.1 आत्मा का स्वरूप नहीं बदलता, अतः आत्मधर्म स्थिर है, शाश्वत है। परिस्थिति के साथ समाज का स्वरूप बदलता है अतः समाज विज्ञान एक विकासशील शास्त्र है। जैनधर्म ध्रुवता का परिणामिता के साथ समन्वय का पक्षधर है। इस दृष्टि से भी आत्मधर्म और समाजधर्म क्रमशः नित्य तथा परिणामी होने के नाते, एक दूसरे के पूरक ही सिद्ध होते हैं, न कि विरोधी अपितु यह कहना चाहिये कि आत्मधर्म और समाजधर्म मिलकर एक जात्यन्तर को जन्म देने वाले बनने चाहिए न कि एक दूसरे से अलग रहकर केवल ऊपरी तौर पर एक दूसरे से जुड़ने चाहिये। विज्ञान की भाषा में कहें तो उनका संबन्ध भौतिक (Physical) न होकर रासायनिक (Chemical) होना चाहिये।
2.2 इसीलिये आचार्य कुन्दकुन्द ने निश्चय के बिना व्यवहार को व्यवहाराभास और व्यवहार के बिना निश्चय को निश्चयाभास माना है। आज की भाषा में कहें तो कहना होगा कि समाजविज्ञान के बिना आत्मधर्म आत्मधर्माभास है और आत्मधर्म के बिना समाज विज्ञान समाजविज्ञानाभास है।
व्यवहारिक पृष्ठभूमि
3.1 ऊपर हमने सैद्धान्तिक दृष्टि से चर्चा की है। जैन परंपरा में व्यवहार में क्या हुआ यह भी विचारणीय है। जैन परंपरा में चतुबिंध संघ की व्यवस्था है। संघ समाज का ही स्थानापन्न है। संघ एक धार्मिक संस्थान है और समाज एक लौकिक संस्थान है- यह भेद होने पर भी संघ और समाज दोनों सामुदायिक व्यवस्थाऐं हैं- यह समानता भी दोनों में है।
3.2 संघ चतुर्विध है। उसमें साधु- संघ धार्मिक है किन्तु श्रावक संघ धार्मिक होने के साथ लौकिक भी है। साधुसंघ और श्रावक संघ का पारस्परिक संबन्ध अन्योन्याश्रय रूप है। श्रावक को आगम साधु के मुख से ही सुनना है । इस दृष्टि से श्रावक साधु का मुखापेक्षी है। वह साधु से सुनकर धर्म को जानता है, इसीलिये वह 'श्रावक' कहलाता है। दूसरी ओर साधु अपनी आहारचर्या के लिये श्रावक का मुखापेक्षी है वह अकिञ्चन है। उसे अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं के लिये श्रावक के सम्मुख हाथ पसारना पड़ता है। इस प्रकार श्रावक और साधु में परस्परोपग्रह का भाव है।
3. 3 तीर्थंकर की अवधारणा विचारणीय है। तीर्थंकर स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त करके कृतकृत्य हो चुके होते हैं फिर भी समवशरण में देशना देकर दूसरों के कल्याण का अनु कार्य करते रहते हैं। यद्यपि सिद्ध अपने कर्मों का क्षय कर चुके होते हैं और अरिहंतों के अभी चार अघाती कर्म शेष रह जाते हैं तथापि नमस्कार महामंत्र अरिहंतों को सिद्धों से भी पहले नमस्कार करता है क्योंकि परोपकार करने के कारण अरिहंतों का सिद्धों की भी अपेक्षा पूज्यतर स्थान बन जाता है।